Page 0.
@M.S.Media.
Culture Visheshank.
In Association with.
A & M Media.
Pratham Media.
Times Media.
Shakti : Cover Page.
©️®️ M.S.Media.
⭐
सम्पादकीय : शक्ति आलेख : गद्य पद्य संग्रह.
⭐
लेखक कवि विचारक.

अरूण कुमार सिन्हा.
शक्ति : आरती.
*
आवरण पृष्ठ : कोलाज : विदिशा.
*
सम्पादकीय : शक्ति : गद्य पद्य विचार : संग्रह. आलेख
*
⭐
फोर स्क्वायर होटल : रांची : समर्थित :
समर्थित : आवरण पृष्ठ : विषय सूची : सम्पादकीय. शक्ति. समूह : मार्स मिडिया ऐड : नई दिल्ली.
⭐
*
शक्ति. संयोजक
डॉ. मधुप
एम. एस. मीडिया : शक्ति : प्रस्तुति
सम्पादकीय : शक्ति : आलेख
⭐
---------
विषय सूची : प्रारब्ध : ० सम्पादित. शक्ति.डॉ. सुनीता सीमा शक्ति * प्रिया.
|
----------
विषय सूची : प्रारब्ध : ०
-------
आवरण पृष्ठ : ०
विषय सूची : पृष्ठ : ०
सम्पादकीय. शक्ति. पृष्ठ : ०
राधिका कृष्ण शक्ति दर्शन.पृष्ठ : ०.
सम्पादकीय. शक्ति. गद्य संग्रह : आलेख : पृष्ठ : १
सम्पादकीय. शक्ति. पद्य संग्रह : आलेख : पृष्ठ : २
सम्पादकीय. शक्ति. विचार संग्रह : आलेख : पृष्ठ : ३
सम्पादकीय. शक्ति.दृश्यम संग्रह : आलेख : पृष्ठ : ४
संदेशें आते हैं : चिठ्ठी आई हैं : आपने कहा : पृष्ठ : ५
----------
सम्पादकीय. शक्ति. समूह : पृष्ठ : १
-----------
*
शक्ति. रेनू. अनुभूति. नीलम.
शक्ति.डॉ. सुनीता शक्ति* प्रिया.
शक्ति.डॉ. नूतन. शालिनी. उषा.
शक्ति. डॉ.मीरा श्रीवास्तवा.रीता रानी. कंचन
शक्ति.डॉ.अनुपम अंजलि.रंजना. मानसी.
शक्ति.डॉ.भावना. माधवी. संगीता.
शक्ति. डॉ. रूप कला. सीमा. तनुश्री सर्वाधिकारी.
----------
सम्पादकीय. शक्ति. सज्जा
----------
शक्ति. मंजिता. सुष्मिता.अनीता.
--------
एम एस मीडिया.शक्ति. प्रस्तुति.
संभवामि युगे युगे. प्रारब्ध : पृष्ठ : ०. राधिका कृष्ण शक्ति दर्शन.पृष्ठ : ०.
|
स्वर्णिका ज्वेलर्स सोह सराय बिहार शरीफ़ समर्थित
*
----------
सम्पादकीय. शक्ति : गद्य संग्रह : आलेख : पृष्ठ : १
-----------
*
लेखक कवि विचारक

अरूण कुमार सिन्हा.
शक्ति : आरती.
----------
संपादन.आलेख
शक्ति : रेनू शब्द मुखर / जयपुर.
-----------
पृष्ठ सज्जा.
शक्ति अनुभूति / शिमला.
*
--------
जीवन जैसा है वैसा ही है शक्ति. आलेख :
-------
जीवन न तो उगता है और ना ही डूबता है,यह तो संसार चक्र के साथ अबाध अनवरत,चलता रहता है।
समय कभी ठहरता नहीं तो जीवन कैसे ठहरेगा जैसे किसी लम्बी यात्रा में अनेक पड़ाव या ठहराव आते हैं वैसे ही जीवन की यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पर हमें कुछ पल मिलते हैं जिसमें एक अवसर मिलता है कि पीछे की यात्रा पर विचार करें,मंथन करें, विश्लेषण करें कि क्या खोया क्या पाया और अन्तिम बिन्दु अर्थात् अपने लक्ष्य पर पहुंच कर जो शेष रह जाता है वह समस्त यात्रा का सारांश या निष्कर्ष होता है।
यात्रा की प्रकृति दुखद या सुखद या मिश्रित दोनों हो सकती है। आमतौर पर यात्रा की अपनी अपनी अनुभूतियां होती हैं पर सच तो यह है कि यह मिश्रित अनुभूति ही देती है,एक संभावना बन सकती है कि दुःख या सुख दोनों में से किसी एक की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है पर एकपक्षीय नहीं हो सकती है।
कुछ महापुरुषों ने जीवन को दुखमय तो कुछ ने आनन्द और उत्सव बताया है। तथागत सिद्धार्थ जीवन को दुखमय तो महर्षि रमण जीवन को आनन्द और उत्सव बताते हैं। अब यह दुखमय हो या आनन्दमय हो जैसा भी हो, अनुभूतियों पर ही टिका हुआ है। जो जिस रंग में रंगा, जीवन वैसा ही लगा,सूर कहते हैं कि,
सूरदास की काली कमरिया चढ़ै न दूजो रंग, उनका जीवन श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंगा हुआ है, सबकुछ श्याममय है, कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता है, गोस्वामी जी को लगता है कि,जाके प्रिय न राम वैदेही-----,जिनको श्री राम जानकी प्रिय न हो उनका परित्याग ही श्रेयस्कर है, कोई काहु में मगन कोई काहु में मगन,यही जीवन का यथार्थ है।
गोबरैला गोबर के गंध में ही मगन है तो भौंरा सुगंधित फूलों की खोज में बौरा रहा है,सबकी अपनी-अपनी खोज है और हम मनुष्यों की भी प्रकृति और प्रवृत्ति भी ऐसी है,सबके अपने-अपने सुख हैं और अपने अपने दुःख भी हैं। कोई धन की,कोई जन की तो कोई मान सम्मान की तो कोई यश की तो कोई इन सबकी खोज में स्वयं को भूलकर खोज में लगा हुआ है। प्राप्ति की फ़िक्र नहीं जो अप्राप्त है उसकी खोज में प्राप्त भी उन्हें सुख नहीं दे रहा है। अप्राप्त की खोज ने प्राप्त को भी मूल्यहीन बना दिया, बेचैनी है,विचलन है,उद्वेलन है, कहीं चैन नहीं है।
यात्रा चल रही है,पर हमारी दृष्टि यात्रा पर नहीं,उस अप्राप्त पर टिकी हुई है, फिर सुख चैन कहां से मिलेगा, शान्ति कहां से मिलेगी,इतनी भाग-दौड़ में विश्राम के पल भी खोज की यात्रा बन जाती है। ठहरना होगा, विश्राम में मन को अवस्थित करना होगा तभी तो हम अतीत और वर्तमान का अवलोकन कर सकते हैं, ध्यान देना है पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं,अतीत तो लौटेगा नहीं, भविष्य भी अनिश्चित है तो जीना किस पल में है,इसकी फिक्र हम नहीं कर पाते हैं, जीवन तो ऐसे हर पल अतीत ही होता चला जाता है तो जो सम्मुख है, जीवन्त है,उस पल को जी लेना ही जीवन है।
Why r u crying for the Past and Planning for the Future, why not U try ur level best to live and enjoy the Living Moments of Life as this is the Truth and Fact of Life.
अब हमारा ये कहना है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम आने वाले कल के बारे में सोचना या योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही बंद कर दें। योजनाबद्ध तरीके से काम करना भी वर्तमान का ही एक हिस्सा है, यद्यपि यह अनिश्चितता के गर्भ में ही होता है पर ऐसा इसलिए करना चाहिए कि आने वाले समय में यह अफसोस न हो कि काश,ऐसा किए होते तो ऐसा न होता। माना कि जीवन यात्रा असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं का ही योग है पर भविष्य की फिक्र में वर्तमान को निर्जीव नहीं बनाया जाना चाहिए।
रैम्जे म्यूर कहता है कि,
What r made for U,will come to U and each and every thing and activity is destined and time bound.
इसे हम नियतीवाद या प्रारब्ध का दर्शन या चिन्तन कह सकते हैं पर इसे स्वीकार करते हुए भी हम जीवन को भाग्य या नियती के आगे समर्पण नहीं कर सकते हैं।
वायुयान, सड़क और रेलमार्ग की यात्राओं में अप्रत्याशित दुर्घटनाएं घटती रहती है तो क्या लोग यात्राएं करना बंद कर देते हैं, नहीं न, यात्राएं चलती रहती है,कभी नहीं रुका करती।
जीवन संघर्ष है तो शान्ति और विश्राम भी है, दुःख,शोक, विषाद है तो आनन्द और उत्सव भी है। यात्रा में जैसे हर पड़ाव पर हम कुछ कुछ की खोज करते रहते हैं वैसे ही हर उपलब्ध पल में आनन्द और उत्सव की खोज करते रहिए, दुःख और संघर्ष तो आते रहेंगे पर यात्रा को आनन्द का उत्सव
--------
आत्मशुद्धि और आत्मसिद्धि शक्ति. आलेख :
--------
हिन्दी में ये दो बड़े प्यारे शब्द हैं जिनकी सर्वाधिक महत्ता अध्यात्म में है और सांसारिक व्यवहार और आचरण में भी है। आत्म का सीधा सा अर्थ*स्वयं या खुद होता है जिसे आंग्ल भाषा में Self कहा जाता है और इसमें दो शब्द यथा शुद्धि और सिद्धि जोड़ने पर इसमें अद्भुत परिवर्तन हो जाते हैं।
आत्मशुद्धि अर्थात् Self Purification और आत्मसिद्धि अर्थात् Self Realisation जो वैश्विक स्तर पर सभी मत,पंथ, विचार, विश्वास, सम्प्रदाय आदि में समान रुप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
आत्मशुद्धि ही आत्मसिद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। हम अपमार्जक का प्रयोग कपड़े आदि की सफाई में करते हैं,घर आदि की सफाई में झाड़ू,,ब्रश आदि का प्रयोग करते हैं,बाहरी सफाई के ये उपादान होते हैं। हम अपने शरीर की सफाई के लिए सुगंधित साबुन आदि का प्रयोग करते हैं और अगर इनकी सफाई न की जाए तो ये इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाते हैं। हमारा शरीर, हमारे वस्त्रादि यदि साफ और स्वच्छ न हों तो हम सभा सोसायटी में बैठने लायक नहीं रह जाते हैं। इस सफाई को हम बाह्याचार कह सकते हैं,ठीक इसी तरह मन,भाव,विचार, अन्तर,व्यवहार, आचरण आदि के शुद्धिकरण की भी नितान्त आवश्यकता होती है। हम मन, भाव, विचार आदि से संचालित होते हैं इसलिए इनका भी स्वच्छ, परिष्कृत और परिमार्जित होना जरूरी है कि इनकी शुद्धता से ही हम आत्मसुद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित है कि बाहरी सफाई के लिए अपमार्जक, झाड़ू,ब्रश आदि के प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही अन्तःकरण के अवयवों की शुद्धिकरण के लिए सूक्ष्म उपादानों की जरूरत होती हैं और वे उपादान हैं, स्वस्थ चिन्तन,अच्छे साहित्य काअध्ययन चिन्तन,मनन और विश्लेषण, रचनात्मक व्यक्तियों का सान्निध्य, स्वस्थ परिचर्चा,सही आहार विहार,साधना,ध्यान आदि भीतरी सफाई का काम करते हैं। इन मार्गों से गुजरते हुए जब कोई अन्दर बाहर से परिष्कृत और परिमार्जित हो जाता है तो इसकी परिणति स्वत: स्फूर्त आत्मसिद्धि की ओर होने लगती हैं। जब हमारे मन, भाव, विचार, व्यवहार और आचरण परिष्कृत और परिमार्जित हो जाते हैं तो हमारी बौद्धिक चेतना जागृत होने लगती है और हम धीरे-धीरे आत्मबोध अर्थात् स्वयं को जानने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे भीतर* हंस प्रवृत्ति जागने लगती है जिसे नीर क्षीर विवेक कहा जाता है और नीर-क्षीर विवेक ही हमारी आत्मशुद्धि की उपलब्धि है जो हमें आत्मा और परमात्मा की शक्ति को पहचानने के मार्ग को सुनिश्चित कर देता है।
हमारी दृष्टि और हमारा दृष्टिकोण समभाव हो जाते हैं। समभाव होना, समदर्शी होना ही भगवत्ता को प्राप्त करना है, श्रेष्ठ मानव बनना है जिसकी अभिव्यक्ति ऋषि गोतम ने अपनी उक्ति में की है,
यतो अभ्युदय,नि:श्रेयस स: सिद्धि धर्म,यही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है कि इस सांसारिक जीवन को हम उन्नति के शीर्ष पर ले जाएं और तदुपरांत श्रेयस् की प्राप्ति करें।
---------
लौकिक और अलौकिक शक्ति. आलेख :
--------
शाब्दिक रुप से लौकिक या इहलौकिक का सामान्य अर्थ इस संसार या इस लोक का विषय-वस्तु है जो स्थावर जंगम दोनों हैं और जिनकी अनुभूतियां हमारी ज्ञानेंद्रियां या बाह्यकरण ( Organs of Sense) से होती हैं या होती रहती हैं और इसके विपरीत जो कुछ भी है जिनकी अनुभूतियां बाह्यकरण से नहीं हो सकती अलौकिक या पारलौकिक होती हैं। लौकिकता में हम सब इस प्रकृति के समस्त स्थावर जंगम विषय वस्तुओं का अवलोकन अध्ययन मनन चिन्तन और विश्लेषण करते हैं,जिनकी सत्ता स्थूल होती है और मूलतः जो पदार्थ या पुद्गल
( Matter or Material) हैं, जिनके निश्चित आकार और स्वरुप होते हैं पर इसके विपरीत जो मनोभाव,आवेग, विश्वास,आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ईश्वरीय अस्तित्व, वेदना, संवेदना, अवस्था आदि के बोध होते हैं,जिनकी सत्ता सूक्ष्म होती हैं, उन्हें अलौकिक, पारलौकिक, नैसर्गिक आदि से सम्बोधित किया जाता है और इनकी अनुभूतियां अन्तःकरण या आन्तरिक चेतना ( Inner Conscience or consciousness) से होती है कि ये सब अमूर्त और सूक्ष्म हैं।
हमारे मन में किसी के प्रति कौन से भाव की कितनी मात्रा या गहराई है, कितना समर्पण है,कितनी निष्ठा या विश्वास है,इसकी अनुभूति की जा सकती है या हमारे व्यवहार से परिलक्षित होता है पर इसके मापन के कोई यंत्र नहीं होते हैं,कोई तराजू या बटखरा नहीं होता है परन्तु हमारे शब्द, अभिव्यक्ति, व्यवहार और आचरण उसकी गहराईयों,मोल और मूल्य को बताते हैं।
संसार इसी लौकिकता और अलौकिकता के मध्य चलने वाले जीवन चक्र का नाम है और यह सब हमारी चेतना का विस्तार मात्र हैं। जब हम ब्रह्माण्डीय सृजन और विकास के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्रों पर नजर डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सबकुछ चेतना अर्थात् ऊर्जा का ही विस्तार है,इसी से सभी पंचभूतों और समस्त जीव-जगत का निर्माण और विकास हुआ है। हम आज जो भी हैं, चेतना के ही विकास का परिणाम हैं। चेतना ही हमारा सृजन,लय और विनाश का काम करती है पर हम समझ नहीं पाते हैं कि यह काम कैसे करती है परन्तु यदि हम किसी कार्य को करने के पूर्व थोड़ा सा गंभीर होकर अवलोकन करना शुरु कर दें तो सबकुछ आईने की तरह साफ है जाता है,जैसे एक स्वस्थ बीज का मिट्टी के भीतर दबना या दबाया जाना और अनुकूल वातावरण का मिलना उसके अंकूरण का कारण बनता है,वैसे ही किसी विचार भाव का सृजन होते ही हमारी चेतना जागृत हो जाती है और हम क्रियाशील होने लगते हैं,ये क्रियाशीलता ही चेतना का विस्फोट या विस्तार है। हर अच्छे बुरे कर्म जो हम करते हैं ( तय मापदण्ड के अनुरूप या विरुद्ध) वह चेतना का ही कार्य रुप है।एक बन्दूक के मैग्जीन में गोली भरी रहती है पर वह तब तक चार्ज नहीं होती जबतक उसे बैरेल में लाकर ट्रिगर नहीं दबाया जाता है, ट्रिगर दबते ही उसकी स्थितिज ऊर्जा,गतिज ऊर्जा में रुपान्तरित हो जाती है और निशाने या लक्ष्य को नष्ट कर देती है,यही ऊर्जा या चेतना का रुपान्तरित होना है।
हम सबके भीतर ऐसी ही अपार ऊर्जा स्थिरावस्था में संचित रहती है जिसे परखने की जरूरत होती है और जैसे ही हम उस अलौकिक शक्ति या ऊर्जा की पहचान कर लेते हैं,उसके प्रयोग की चेतना जाग जाती है और उसका प्रयोग करके हम साधारण से असाधारण बन सकते हैं।
इसलिए हमारे जीवन में उस चेतना या शक्ति को जानना पहचानना और प्रयोग करना ही हमें आम से खास बनाने का काम करती है। भौतिक विज्ञानियों ने परमाणु में छिपी शक्ति को पहचाना और उसके सृजनात्मक और विनाशक दोनों गुणों का इस्तेमाल किया। इसी चैतन्य ऊर्जा को पहचान कर श्री कृष्ण योगेश्वर और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गये। वर्द्धमान, महावीर जीण और गोतम सिद्धार्थ, तथागत सिद्धार्थ बन गये। साधारण से रामबोला, गोस्वामी तुलसीदास बन गये, रत्नाकर, ऋषि वाल्मीकि और अंगुलीमाल, बौधिसत्व को प्राप्त हो गये।
ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, क्षय नहीं होती बस रुपान्तरित हो जाती है जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों में सत्य माना जाता है। इसलिए परम चैतन्य ऊर्जा या शक्ति को हम ईश्वरीय सत्ता के रुप में भी स्वीकार करते हैं कि वह भी अलौकिक या पारलौकिक सत्ता ही है, सूक्ष्म और अन्तःकरण से अनुभव करने योग्य है।
चेतना सबके पास है पर चैतन्य बोध सबके पास नहीं है और इस चेतना को ही चैतन्य बोध में विकसित करना आत्मबोध को जागृत करना है और यह किया जा सकता है और जिन्होंने ने भी इसमें सफलता पायी है या उस दिशा में प्रयासरत भी हुए हैं तो उनको स्वयं के बोध की अनुभूति होनी शुरू है गयी है और वे साधारण से असाधारण बनने की ओर अग्रसर हो गये हैं। वैसे व्यक्ति जीवन के जिस भी क्षेत्र में रहते हों, असामान्य प्रदर्शन करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं।
---------
लघु और विराट शक्ति. आलेख :
----------
विराट में लघु और लघु में विराट को देखने की दृष्टि चाहिए। एक अंजुली जल में सागर को नहीं पर सागर के सारे गुणधर्म का ज्ञान जरुर हो जाता है। एक बूंद में वो सारा गुणधर्म समाहित होता है जो एक घड़े के भरे जल में होता है, ठीक ऐसे ही किसी एक तत्व के अणु में वो सबकुछ समावेशित होता है जो उस तत्व के एक बड़े पिण्ड में होता है,यही विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत सच है।
हम सबने बरगद या पीपल के बीज को देखा है,इतना छोटा कि सरसों का एक दाना भी उससे बड़ा होता है परन्तु उसी लघु बीज में विराट बरगद या पीपल का वृक्ष शांतचित्त सोया रहता है और अनुकूल वातावरण पाकर वह अंकूरित होकर पल्लवित और पुष्पित होकर अपनी मौलिकता को प्राप्त कर लेता है पर सरसों के बीज में जितना भी खाद पोषण आदि दिए जाएं,वो झाड़ ही होगा, जिसके भीतर जो मौलिकता होती है, कालान्तर में वह फूटकर बाहर आता ही आता है,उसके विस्फोट को नहीं रोका जा सकता है,इस सम्बन्ध में कठोपनिषद् में एक बड़े रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग की चर्चा भी देखने को मिलती है।
When an unknown seed is sown, no one knows what it is but when it sprouts out and turn to its originality,it is identified what it is. This is the truth of inherent quality.
चेतना और संस्कार के बीज वैसे ही सबके अंदर सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं जिसे अनुकूल वातावरण मिल जाने पर वह फूटकर बाहर आ जाते हैं अन्यथा वे वैसे ही उसी अवस्था में पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं परन्तु ध्यान रहे कि जो जिसका गुणधर्म होता है,वही प्रस्फुटित होता है।
हमारे पौराणिक ग्रन्थों में ऐसे अनेकानेक गाथाएं हैं जो हमारे इस आलेख के सत्य को प्रमाणित करते हैं कि हमें लघु को लघु और विराट को विराट देखकर फर्क नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने वामन रुपी विष्णु को न पहचान करने की भूल की और अपने अस्तित्व को खो दिया,श्री हरि की लघुता को बलि नहीं समझ पाए जिसकी परिणति यह हुयी कि उन्हें अपना देहदान करना पड़ गया।
ऐसी ही कथा कुरु सभा में श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच की है जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने और युद्ध टालने के लिए मध्यस्थता करने आए हैं जिसका बड़ा सुन्दर और जीवन्त चित्रण दिनकर जी ने रश्मिरथी में किया है,
सबको सु मार्ग पर लाने को भीषण विध्वंस बचाने को
दूर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए
पाण्डव का संदेशा लाये हो न्याय अगर तो आधा दो
पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम
रखो अपनी धरती तमाम दुर्योधन वह भी दे न सका
उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है
हरि ने भीषण हूंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया
डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले
जंजीर बढ़ा कर साध मुझे आ आ दूर्योधन बांध मुझे
जब श्री हरि ने अपने विस्तारित स्वरूप में सम्पूर्ण सांसारिक क्रियाशीलताओं और ब्रह्माण्डीय चक्र का प्रदर्शन किया तो सबकी आंखें चुंधिया कर बंद हो गयी,बस विदूर, कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र और कुछ ऋषिगणों को दिखाई पड़ा,कहते हैं एक झलक दुर्योधन ने भी देखा लेकिन तेज प्रकाश और ऊष्मा से उसकी आंखें भयभीत होकर बंद हो गयी फिर भी किसी को भान न हुआ कि यही * विश्वरूप श्री कृष्ण ही हैं।
जब हम आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत और ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ और नाद बिन्दु के सिद्धान्तों का अवलोकन करते हैं तो एक सूक्ष्म अणु में विस्फोट से सृष्टि की रचना का रहस्य खुलता है अर्थात् एक छोटे से अणु में समस्त ब्रह्माण्ड समाया हुआ था जो विस्फोट के बाद फैलता चला गया और हमारे सांसारिक जीवन का भी यही सत्य है कि लघु विराट एक दूसरे में समाविष्ट हैं और लघुता से ही प्रभुता की प्राप्ति होती है, सामर्थ्यवान को इसीलिए विनम्र और क्षमावान होना चाहिए कि इसमें ही उनकी विराटता है।
-----------
अतीत वर्तमान और भविष्य: जीवन : शक्ति. आलेख :
----------
अतीत ,सांसारिक जीवन में दर्पण का काम करता है जिसका अवलोकन करते हूए वर्तमान को जीया जाता है और अतीत तथा वर्तमान के आधार पर भविष्य की रूपरेखा/योजनाएँ बनायी जाती है।
पर अतीत की स्मृतियों का आकलन बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है कि अतीत हमारा * गुरू मार्गदर्शक और परामर्शदाता होता है जिसकी महत्ता निज की जिन्दगी के साथ-साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन मे सहज ही देखा जा सकती है।
परन्तु सांसारिकता से उपर उठ कर जब कोई * आध्यात्मिक तात्विक और दार्शनिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे सबकुछ विस्मृत करना होता है कि संसार जीवन का स्थूल रूप है और आध्यात्मिक तथा तात्विक और दार्शनिक जीवन सूक्ष्म तल पर जीया जाता है और जीवन का ये पक्ष भी सबको अंतिम रूप में देखना और भोगना ही पड़ता है। अतीत दुखद और सुखद दोनों होता है जो हमें आह्लादित भी करता है और दुखी भी करता है तो जो हमें आह्लादित करे, ऊर्जावान बनाए, जिजीविषा को मजबूत करे,उन स्मृतियों से हमें प्रेरित होना चाहिए और मन हृदय और मस्तिष्क को जो ह्रासात्मक बनाए,उनका परित्याग करना चाहिए।अब आपके समक्ष अतीत वर्तमान और भविष्य, तीनों मौजूद हैं,पर भविष्य सदैव अनिश्चित और अंधकार के गर्भ में होता है और इन्हीं के आधार पर समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताओं का
संचालन होता है या किया जाता है। हमारी सारी योजनाएं अतीत का अवलोकन करते हुए वर्तमान की बुनियाद पर ही तय की जाती हैं जो अतीत को दर्पण बनाकर सामने नहीं रखते, वर्तमान तो सुखद अनुभूति नहीं ही देता है, भविष्य भी संकटापन्न हो जाता है। हमारे निज के और पारिवारिक जीवन में इस विचार का सिर्फ सैद्धान्तिक मोल नहीं है बल्कि व्यवहारिक मोल और मूल्य भी है। व्यक्तिगत जीवन में * बौद्धिक विवेक या चेतना के बावजूद भी हम गलतियाँ करते हैं जो वर्तमान में परछाईयों की तरह हमारे समक्ष रहती है और हमें सचेत करती रहती है और इसका सीधा सम्बन्ध * मन मस्तिष्क और हृदय से होता है। मन जिसे स्वीकारता है, हृदय कोमलता से अवलोकन करता है परन्तु मस्तिष्क * विश्लेषण करता है, विवेचना करता है, मन हृदय के भावों को समेकित करता है और चीजों को उपसंहारित करता है।
इससे जो स्वीकार्यता प्राप्त होती है, वह तर्कसंगत और तथ्यात्मक होती है जो अगर अपेक्षित परिणाम न दे सके पर अलाभकारी तो हो ही नहीं सकता है। हम अपनी शक्ति सामर्थ्य गुण दोष क्षमता अक्षमता आदि की पहचान और प्रयोग इनके तुलनात्मक आधार पर ही करते हैं जो सदैव* हितकारी और सहयोगी की तरह हमारा संरक्षण और संवर्धन करता रहता है। वर्तमान के भीतर अतीत को और दोनो का समायोजन करके भविष्य का आकलन सावधानी से करते रहने की जरूरत है जो जीवन को सरल सहज और सुगम बनाने में सहायक होगा।
यह निजी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नीति निर्धारण में भी सहायक साबित होती है। अतीत में हमारे सम्बन्ध किनके साथ कैसा रहा है,कौन सी नीति कुटनीति कारगर और फलदाई रही है,उनका आकलन और विश्लेषण भी अतीत के आधार पर ही किया जाता है। वैदेशिक सम्बन्ध सदैव बदलते रहते हैं,उनका भी आकलन नेतृत्व के आधार पर बदलते परिवेश में अतीत के आधार पर ही किया जाता है और करिश्मा ये है कि पारिवारिक जीवन के कुछ अपवादों को छोड़कर यह पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी विचार और विश्लेषण का आधार बनता है,किसने कब, क्यों और कैसा व्यवहार किया,इनके लिए अतीत मार्गदर्शन करता है और हम उन्हीं आधारों पर सही निर्णय ले पाने में सफल होते हैं। इसलिए सांसारिक जीवन में अतीत हमारे लिए** मार्गदर्शक और मित्र का काम करता है,जिसकी महत्ता से कोई इंकार नहीं कर सकता है।
---------
श्रेष्ठ जन का सम्मान और समृद्ध भारतीय परम्परा : शक्ति. आलेख :
---------
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समावेशित कुछ विषय या परम्पराएं ऐसी ही जो वैश्विक स्तर पर दुर्लभ है।ऐसे वैश्विक स्तर पर हर मत,पंथ, विचार, विश्वास, सम्प्रदाय आदि में बड़े बुजुर्गो के सम्मान और आदर को स्थापित देखा जाता है परन्तु भारतीय हिन्दू जीवन दर्शन और चिन्तन में इन्हें तो जीवन्त देवता ही माना गया है और इसलिए कहा भी गया है,मातृ देवो भव पितृ देवो भव अर्थात् माता पिता दोनों ही देवतुल्य नहीं देव ही हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी इसे बड़ी खुबसूरती के साथ कहा गया है कि ** God can't be found in visibility on the earth so he created mother and father on the earth, इस्लाम भी कहता है कि मां के कदमों तले जन्नत होता है।
बुजुर्गों की इज्ज़त तो कीजिए ही कीजिए पर माता पिता की इज्ज़त में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि उनकी सत्ता स्थूल रूप में तो आपके साथ रहती ही है, उनके महाप्रयाण के बाद भी सूक्ष्म रूप में आपके अंतिम पल तक आपके साथ रहती है और यह * आध्यात्मिक मोल एवं मूल्य ही नहीं शुद्ध व्यवहारिक सत्य भी है कि सब एक दिन माता पिता बनते हैं और यह क्रम चलता ही रहता है और यही संसार है। Transactional analysis of human behaviour भी इस सत्य से इंकार नहीं करता है कि हम मनुष्यों के भीतर तीन शरीर, तीन चेतना और तीन संस्कारबद्ध गुण दोष होते हैं जिनमें दो माता पिता होते हैं और एक हम स्वयं होते हैं। हमें इसलिए भी अपने माता-पिता का श्रद्धापूर्वक सम्मान और प्रेम करना चाहिए कि हमसे जो आने वाली पीढ़ियों का सृजन होता है वे आध्यात्मिक और जैव रासायन विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हमारे गुणधर्म को ग्रहण करते रहते हैं जिसे जैविक विज्ञान में डी एन ए कहा जाता है जो वंशानुगत होता है।
इसलिए जो गुण और संस्कार हम माता पिता और स्वार्जित संस्कारों से संप्रेषित करते हैं,वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। हम हमारे बच्चों के सामने जो व्यवहार अपने अभिभावकों के साथ करते हैं,वे स्थूल और सूक्ष्म रुप से उन्हें प्रभावित करते हैं और ऐसा देखा गया है आमतौर पर बड़े बुजुर्गो को अपनी संतानों से तकलीफ और शिकायत रहती है कि मेरे बच्चों का मेरे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। यह वेदना और पीड़ा जीवन के अंतिम चरण में बड़ी दुखदाई होती है।
हम हमारे जीवन में कितने कारण रुपों से प्रभावित होते रहते हैं,इसका अवलोकन करते रहना निहायत जरूरी है जो आध्यात्मिक दर्शन के साथ साथ प्रकृति का विज्ञान भी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया समानुपातिक होती है,हम जो भी अच्छा बुरा करेंगे,वह हमारे पास लौटकर आएगा और यही संसार चक्र है जिसे औपनिषदिक दर्शन में* कारण और कारण या कर्म फलाफल या प्रतीत्यसमुत्पाद का दर्शन कहा गया है जो शाश्वत सनातन सत्य है।
अपेक्षाओं के बगैर इस संसार में न तो कोई रिश्ते नाते होते हैं और न कोई लौकिक अलौकिक सम्बन्ध ही बनते हैं। पर यह भी सत्य है कि अपेक्षाएँ किसी के संसाधनों और इच्छाओं पर निर्भर करता है, सांसारिक सम्बन्धों की गहराइयों पर निर्भर करता है। आकलन कर लीजिये फिर अपेक्षा कीजिए, तकलीफ कम होगी,पर माता-पिता की सारी अपेक्षाएं जो अपनी संतानों से होती है कि उनकी प्रगति और सुख सुविधा में ही वे अपना सुख दुःख देखते हैं। इसलिए माता पिता अपने सुख और सपनों को त्यागकर सबकुछ उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगा देते हैं और तब उन्हें पीड़ा होती है जब वे अपेक्षित परिणाम नहीं देते और
अपने जीवन में स्थापित हो जाने के बाद उनसे कटकर रहने लगते हैं।
======।।
संसार को इसीलिए सम्यक् गति और प्रकृति के साथ चलने वाला चक्र कहा जाता है। संसार बिना भेदभाव के चलता रहता है, किसी के होने या न होने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सांसारिक आदमी को कुछ हद तक फर्क पड़ता है पर सब विकल्पों पर चलते रहते हैं। संसार विकल्पों का चयन करता रहता है। किसी स्थान पर यदि हवा की शून्यता बनने लगती है तो * अचानक से तेज हवा आंधी चलने लगती है और शून्य अवस्था तिरोहित हो जाती है। ऐसे ही जीवन चलता रहता है परन्तु इस मृण्मय संसार में सिर्फ माता पिता ही वो अस्तित्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं हो सकता है,ये निर्विकल्प होते हैं परन्तु सारे विकल्पों के ये विकल्प होते हैं।
माता पिता का भी संस्कारित होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इनपर ही सृजन और विनाश का उत्तरदायित्व होता है।
नेपोलियन कहा करता था,तुम हमें अच्छी मांए दो, मैं तुम्हें एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र दुंगा,इस उक्ति का सच यही है कि आज जो वैश्विक समुदाय में इतनी हिंसा, रक्तपात, अत्याचार,लूट, बलात्कार आदि जो अपराध हो रहे हैं,उनकी जड़ों में अच्छे अभिभावकों का अभाव ही महत्वपूर्ण कारक और कारण हैं। इसलिए इस स्वस्थ और समृद्ध परम्परा को मजबूत बनाए रखना ही एक स्वस्थ और समृद्ध पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बुनियाद है।
---------
अभिव्यक्ति : हम और हमारे रिश्ते शक्ति. आलेख :
---------
आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं, कैसे रहते हैं आदि मायने तो रखते हैं, आप जान पहचान वाले लोगों में सम्मिलित तो हो सकते हैं परन्तु मित्र या दोस्त नहीं हो सकते। दोस्ती या मित्रता की बुनियाद * वैचारिक साम्य और पारस्परिक सम्बन्धों की समझदारी एहसास ओ जज्बात और जरुरतों पर बनती है। पद पैसा प्रतिष्ठा प्रभाव आदि से प्रभावित संसार की समस्त सोंच सिद्धान्त और व्यवहार प्राकृतिक क्रियाशीलताएँ हैं और कोई क्रियाशीलता या अवस्था स्थायी भाव नहीं रखते,सब बदलते रहते हैं पर नहीं बदलती हैं * आदमी की मौलिक प्रवृत्ति और प्रकृति, जज्बात ओ एहसास और यही भाव उस मैत्री भाव को बनाए रखता है। देश काल परिस्थितियाँ भी शाश्वत नहीं होती है। वैश्विक स्तर पर सब मे समान भाव से कुछ न कुछ बदलते रहते हैं नहीं बदलते हैं तो * मन हृदय और मस्तिष्क के मौलिक समन्वित और समेकित भाव और पर युगधर्म तात्कालिक समय की मांग से बदलते रहते हैं। यद्यपि युगधर्म बदलते रहते है पर * धर्म के मर्म कभी नहीं बदलते। यहां भगवान श्री कृष्ण को उद्धृत करना उचित प्रतीत होता है कि जब कंस के वध के बाद जरासंध अपने दामाद की हत्या का बदला लेने के लिए मगध की विशाल सेना और मय दानव और काल यवन के साथ मथुरा पर हमला करता है तब बलदाऊ कहते हैं कि, हे केशव,अबतक के युद्धों में हमने इसे पराजित किया है पर इस बार के युद्ध का स्वरूप कुछ और है पर हम युद्ध करेंगे।यह सुनते ही आम आदमी की तरह श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं,दाउ,यह युद्ध असाधारण होने वाला है और मैं नहीं चाहुंगा कि समस्त यदुवंशी सेना का सर्वनाश हो जाए। क्षात्र धर्म तो कहता है कि युद्ध से पलायन करना कायरता, अधर्म और नपुंसकता है परन्तु उसी धर्म का मर्म ये कहता है कि अपने आश्रितों की रक्षा करना धर्म ही नहीं धर्म का मर्म भी है इसलिए आज हम इस युद्ध से पलायन करेंगे और श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर द्वारका चले जाते हैं और इसलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा गया है। अब गौर से देखिए ये वही कृष्ण हैं जो कुरुक्षेत्र में विहित कर्तव्य और कर्म को सबसे बड़ा योग बताते हैं और युद्ध वहां धर्म है तो पारस्परिक रिश्ते और उसकी महत्ता को विस्मृत कर जाते हैं और फिर वही कृष्ण अर्जुन और द्रौपदी तथा पाण्डवों के रिश्ते का सम्मान करते हुए उनकी हर आकांक्षा और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर नीति और कुटनीति का अनुसरण करते हैं। इसलिए कि मौलिक मर्यादा,मोल और मूल्य जो रिश्तों का सार है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है माँ की ममता,बच्चे की निश्छल हँसी, पिता का वात्सल्य,भाई बहन का स्नेह, दोस्त की हमदर्दी, संवेदना और समवेदना के भाव, सृजनशीलता और रचनाधर्मिता और ये सारे भाव हमारे आपके भीतर समावेशित रहते हैं। बस इनको समझते रहने और आत्मसात करने की जरूरत है और जिस दिन, जिस पल क्षण आप इनके *मर्म को समझने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, यकीनन बहुत कुछ बदल जाएगा,संसार जिसमें जीवित रहते हैं, जीते हैं, सुख के ताने-बाने बुनते हैं, स्वतःस्फूर्त सुखमय हो जाएगा। जीवन को जिस रूप में देखेंगे, जीवन वैसा ही रूपान्तरित होता चला जाएगा।
परिवर्तन और परिणाम साथ साथ चलते हैं। समस्त आधारभूत संरचनाएँ परिवर्तन के फलस्वरूप ही परिणाम की अपेक्षा करती है और जो हम आप जीवन को देते हैं, जैसा समझते हैं, जीवन वैसे ही देता चला जाता है।
भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान में वास्तव में कोई फर्क नहीं होता है। विज्ञान की अपनी प्रयोगशाला है और अध्यात्म की अपनी प्रयोगशाला है। पर दोनों में एक मौलिक अन्तर है कि विज्ञान * प्रयोग निरीक्षण और निष्कर्षों पर चलता है और अध्यात्म * आत्मावलोकन आत्मनिरीक्षण और आत्मानुभूति
पर चलता है।
बस आत्मावलोकन और आत्मनिरीक्षण ही संसार की गति को सम्यक् बना सकता है तो संसार को सम्यक् और संवेदनशील बनाने में हम सब अपना-अपना योगदान करें ताकि * महाप्रयाण काल में जब * खुद से खुद को प्रश्न पुछा जाए तो हमारी आत्मा पर , हमसे विदा लेती चैतन्य सत्ता पर कोई बोझ न हो
और हमारी आँखो से आँसू न बहे, हमारे चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय पीड़ित और आहत महसूस न करे।
बस।
--------
प्रवाही और अप्रवाही शक्ति. आलेख :
---------
नदी और तालाब, दोनों में पानी होता है पर दोनों में बड़ा फर्क होता है। पोखरा, तालाब,जलाशय, झील आदि का पानी स्थिर और गतिमान नहीं होता है अर्थात् उनका जल अप्रवाही होता है,ठीक इसके विपरीत नदियों का जल सदैव गतिमान अर्थात् प्रवाही होता है।
हम मनुष्यों में भी ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति पायी जाती है। कुछ लोग स्थिर विचार और भावों के होते हैं जिनकी सोंच प्रवाहमान या गतिशील नहीं होती और ठीक इसके विपरीत कुछ लोग बदलते परिवेश और समय में आपने भाव विचारों में अनुकूल परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और लाते रहते हैं जो उन्हें जीवन्त बनाए रखने का काम करता है।
हम सबने देखा होगा कि जो जल जमा रह जाता है, उसमें सड़ांध उत्पन्न हो जाता है, गंदगी धीरे धीरे जमा होने लगती है और उसके जल का मोल और मूल्य बदल जाते हैं।
वैसे ही जो विचार,चिन्तन, व्यवहार, आचरण आदि समय की मांग के अनुरूप नहीं चलते हैं, नष्ट हो जाते हैं कि उसमें समय के अनुरूप उसकी मांगों को पूर्ति करने की क्षमता में ह्रास हो जाता है।
इसलिए जीवन के मौलिक मोल और मूल्यों को छोड़कर चीजें बदलती रहनी चाहिए।
हम समयानुसार आहार और विहार दोनों को बदलते रहते हैं जो जीवन को प्रवाहमान बनाए रखते हैं और जो हम नहीं बदल पाते उन्हें समय बदल देता है।
संसार भी इसी सिद्धांत और व्यवहार पर सम्यक् गति से अबाध रुप में चलते रहता है। चाणक्य इसी दर्शन के व्यवहारिक पक्ष को समझाते हुए एक गह पर चन्द्रगुप्त को कहता है, हे चन्द्रगुप्त, काल क्षीप्र गति से चलायमान है,इसके राहों जो बाधा बनकर इसे रोकना चाहता है,इसके दो पाटों के बीच में पीसकर रह जाता है। इसलिए काल की गति का अवलोकन करते रहो और उसके साथ चलते रहो।
अब हम थोड़ा प्राचीन सभ्यताओं के जन्म और विकास की ओर भी नजर डालें तो पाते हैं कि जितनी भी प्राचीन वैश्विक सभ्यताओं का विकास हुआ,सभी का नदी तट या उनके आसपास ही हुआ है जो जीवन के इस यथार्थ का परिचायक है।
इसलिए मौलिकता को छोड़कर जिन विषयों को हम नहीं बदलकर चलते हैं या चलने की कोशिश नहीं करते हैं तो परिवार, समाज, प्रदेश,देश और विश्व व्यवसाय और व्यवस्था में विद्रूपताएं उत्पन्न हो जाती हैं और समस्त व्यवस्था में अराजकता फैल जाती है।
------------
योद्धा: एक वृत्ति,एक प्रवृत्ति : शक्ति. आलेख :
--------
हिन्दी के ये दो बड़े प्यारे शब्द हैं जिनके अर्थों से हम सब प्रायः अवगत होते ही हैं और नहीं हैं तो एक बार जानने और समझने की कोशिश तो जरूर कीजिए या करना चाहिए कि यह हमारे जीवन के क्रियाकलापों से सीधे जुड़े हुए हैं।
वृत्ति के मुख्यतः दो अर्थ होते हैं, स्वभाव और पेशा अर्थात् यह किसी के स्वभावगत
गुण-दोष का परिचायक है,सहज स्वभाव है और चेतना का प्रथम तल है जिसे अंग्रेजी में आमतौर पर Nature कहा जाता है जो हमारे नित्य के कर्मों का भी परिचायक है।
Natural Activity इसी से संचालित होती है।यह हमारे जीविकोपार्जन के साधनों को भी बताता है जैसे कोई सैनिक या शिक्षक होता है।
अब प्रवृत्ति को समझना है जो वृत्ति से ही बना है पर उससे मौलिक रुप में भिन्न है कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के अर्थ और स्वरुप दोनों बदल देते हैं। प्रवृत्ति हमारी स्वभावगत गुण दोषों की निरन्तरता अर्थात् हमारी आदतों का समूच्चय है जिसे
Attitude या Mentality या Inherent Quality भी कह सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। अंग्रेजी में एक बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति है,
Not ur efforts and diligence makes u successful and great but the attitude.
प्रवृत्ति हमें जुनूनी बनाने का काम करती है जो मनुष्य के भीतर का वह गुण है जो कभी उसे हारने नहीं देता है और वह अगर हारता भी तो फिर शक्ति और साहस संचय करके उठ खड़ा होता है। इसी से हमारे मन में अनेक धारणाओं का जन्म होता है, एक इन्सटिंक्ट पैदा होता है जिससे किसी भी हाल में आदमी की जिज्ञासा और जिजीविषा को मरने नहीं देती है और आदमी अपराजेय हो जाता है, इतिहास गवाह है कि रोबर्ट ब्रूस सात बार हारकर भी हार नहीं माना और आठवीं बार इंग्लैंड से जीत गया। शिवाजी दो चार मोर्चों पर हारते हुए भी अंतिम रुप में विजयी होकर क्षत्रपति महाराज शिवाजी बन ही गए।
महाराणा प्रताप ने अंतिम रुप में मेवाड़ जीत ही लिया कि इन लोगों में एक एटिट्यूड था कि हार नहीं मानेंगे।
अब ये जरूरी नहीं कि एक सिपाही या योद्धा में ही ये जूझारुपन होता है। हम हमारी जिन्दगी में ऐसे लोगों को देखते हैं जो टूट गए पर झूके नहीं, जीवन भर संघर्षों को झेलते रहे पर परिस्थितियों से और समस्याओं से लड़ना नहीं छोड़ा और अंत में विजयी हो गए और जिनके भीतर*एक योद्धा की प्रवृत्ति होती है,वे हार नहीं मानते कि उनके भीतर एक Hunter's Instinct का जन्म हो जाता है और जैसा हम सबने किसी शिकारी जानवरों को टी वी के पर्दों पर देखा है कि एक दो शिकार छूट जाने पर भी वह प्रयास नहीं छोड़ता है कि वह जानता है कि अगर मैं शिकार नहीं करुंगा तो भूख से मर जाउंगा। उसके जीवित रहने के लिए यही Attitude and Instinct उसके अस्तित्व और पीढ़ियों को जीवित रखती है।
योद्धा होना एक वृत्ति है और एक प्रवृत्ति भी है। एक योद्धा में दोनों समाहित और समाविष्ट हैं पर हम सामान्य जन में भी योद्धा प्रवृत्ति का होना इसलिए अनिवार्य है कि यह हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं अपरिहार्य है जो हर हार में और हर हाल में उठने और उठकर दौड़ने की ऊर्जा देता है और हम जीत जाते हैं।
विशेषकर यह विद्यार्थियों के लिए तो एक अमोघ अस्त्र है कि विद्यार्थी परीक्षाओं में विफल होने या वांछित परिणाम न पाने पर हताश और निराश होने लगते हैं तो उन्हें इस प्रवृत्ति की सख्त जरूरत होती है कि एक या दो बार चूक गए तो चूक गए, अगली बार छीन कर ले लेंगे और इस Attitude and Instinct वाले विद्यार्थी या प्रतियोगी कभी नहीं हारते हैं। योद्धा प्रवृत्ति अपनाइए और संसार जीत लीजिए।
----------
सत्य की जटिलता:अनेकान्तवाद : शक्ति. आलेख :
----------
सत्य एक ऐसा शब्द है जो लिखने,बोलने और सुनने में बड़ा सरल और सहज लगता है परन्तु यह बड़ा जटिल और बहुआयामी है जिसकी व्याख्या आदिकाल से होती रही है और होती रहेगी। इसी जटिलता को ई पू छठी शताब्दी में सुलझाने की एक कोशिश जीण महावीर ने भी अपने दर्शन और चिन्तन में की थी जिसे अनेकान्तवाद के नाम से जाना जाता है जो बड़ा तार्किक और तथ्यात्मक भी है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन से लेकर यूनानी चिन्तन में भी इस पर गहन मंथन किया गया है। इसके शब्द विन्यास से पता चलता है कि अनेक आयामों के अवलोकन और विश्लेषण के बाद ही किसी एक बिन्दु पर पहुंचा जा सकता है जो सत्य हो सकता है और यहां भी संदेह इसलिए व्यक्त किया जाता है कि सत्य को समस्त या समग्रता के साथ नहीं जाना जा सकता है।
आधुनिक दार्शनिकों में लिविंगस्टोन का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसने इस पर अपना विचार * Knowing the World में देते हुए कहा है कि,When we observe the moon with a powerful telescope,we r able to see the face part of the moon but we can't see the moon in the whole.
सत्य है कि हम सांसारिक जीवन में भी व्यवहारिक रुप में ऐसा ही करते हैं कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति का मोल और मूल्यांकन एकांगी ही कर पाते हैं,उसका मूल्यांकन कभी समग्रता में नहीं हो पाता है। जिस जिस नजरिए से जो देखता है,उसे वह वैसा ही प्रतीत होता है। इस पर ईसप की कहानियों में एक बड़ी रोचक कहानी है जिसका नाम सात अंधे और एक हाथी है। इस कहानी में सात अंधों को एक हाथी के बारे में बताने को कहा जाता है। सातों ने हाथी के अलग-अलग अंगों को छूकर वैसा ही विवरण दिया जैसे उसके अंग थे। किसी ने सूप तो किसी ने खंभा,किसी ने रस्सी तो किसी ने दीवार आदि बताया।
धीरे-धीरे वे आपस में लड़ने लगे कि हाथी ऐसा ही है। उसी रास्ते एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था,उसने सातों को बुलाया और कहा,तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो कि तुमने जो छूकर देखा, तुम्हारे लिए वही सत्य है जबकि हाथी ऐसा नहीं है बल्कि तुम सबने जो महसूस किया उसका समूच्चय है।
अनेक पक्षों और आयामों के मिलने से ही सत्य को समझा जा सकता है। क से ग लाभान्वित होता है और ख उससे हानि में रहता है तो इसमें ग का क्या कसूर है,वह तो अपनी जगह पर स्थित है,क और ख की अनुभूतियां अलग अलग है। अब ग के सही मूल्यांकन के लिए क और ख का विश्लेषण किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में कौन कैसे लाभान्वित हुआ और कौन घाटे में रहा और तभी सत्य के निकट पहुंचा जा सकता है।
हम भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में किसी के मोल और मूल्यों का मूल्यांकन उन सात अंधों की तरह ही करते हैं पर सत्य तो इनसे बिल्कुल इतर होता है।
इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति या विचारधारा का निष्कर्ष निकालने के पूर्व उसके अनेक पक्षों और आयामों का गहन अवलोकन और विश्लेषण अनिवार्य होता है अन्यथा हम या आप कभी भी सत्य के करीब नहीं पहुंच सकते हैं।
समग्रता में देखने और आंकने के लिए एकाग्रता और समग्रता में मूल्यांकन करने की जरूरत होती है और यहां भी आकलनकर्ता के ज्ञान, चिन्तन, सोंच, अध्ययन ,मानसिक क्षमता और विवेक बड़ा महत्व रखता है कि पोखर या झील में तैरने वाला प्रवाहमान नदी की धार में नहीं तैर सकता है। एक जौहरी ही हीरे को उलट-पुलट कर उसका मूल्यांकन कर सकता है, कबाड़ी के लिए तो वह कांच का एक चमकता टुकड़ा भर ही हो सकता है।
सत्य बहुआयामी और जटिल तभी नहीं रह पाता है जब अनेक से गुजर कर एक बिंदु पर सिमट जाता है।
धन्यवाद।
--------
संघर्ष या समर्पण या पलायन शक्ति. आलेख :
---------
शत्रु से पीठ दिखाने पर आंखें आगे की ओर हो जाती हैं और हम पर वार करना सरल हो जाता है, सम्मुख होकर या तो जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे,चयन आपके हाथों में हैं।यहां शत्रु एक प्रतीकात्मक प्रयोग भर है क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में एक नहीं अनेक शत्रु होते हैं,सम्मुख हो जाने पर हम उसकी हर चाल और गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं,उसकी चालों का काट ढुंढ सकते हैं, इसलिए उससे रुबरु होना ही सफलता की पहली शर्त है।
दूसरी शर्त है उसके समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष बलों का आकलन करना कि जो सामने दिखाई पड़ता है, वही सच नहीं होता बल्कि परोक्ष भी सत्य होता है जो आजकल के युद्धों में सच उभर कर सामने आते हैं, इसीलिए उसका भी आकलन होना जरूरी है। संभवतः चाणक्य ने इसी को मद्देनजर रखते हुए** अरि मित्र सिद्धान्त का सृजन किया था। उसके शत्रु और मित्र पक्षों का आकलन और मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है।
अगली बात स्वयं की कुल क्षमताओं का भी मूल्यांकन होता है कि हमसे बेहतर हमारी क्षमताओं को दूसरा कोई नहीं जानता है। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर ही नहीं लड़े जाते हैं बल्कि आन्तरिक समर्थन और निष्ठा की परख भी जरूरी होती है, युद्ध सिर्फ अस्त्र-शस्त्र के बदौलत ही नहीं अपने मनोबल और जन समर्थन के बल पर भी जीते जाते हैं।यदि उस देश का जनमत या आपके लोग आपके साथ खड़े न हों तो युद्ध जीतना असंभव नहीं तो चुनौती जरुर हो जाती है।
अगली बात रणनीति और कुटनीति की होती है जिनके अनुगमन करने से सैन्यबल या संसाधनों की कमी होते हुए भी विजयी होते इतिहास में देखा गया है। चाहे वह रणक्षेत्र हो या हमारा निजी जीवन हो,सफल रणनीति की जरूरत सब जगह होती है।
दूसरी बात होती है अपनी दुर्बलताओं और कमियों का आकलन और मूल्यांकन कि ये दोनों कारक भी जीवन के जंग और मैदानी जंग में बड़ा मायने रखते हैं। शरीर जब रुग्ण हो जाता है तब हमें सबसे पहले आहार और विहार अर्थात् खान-पान और जीवनशैली बदलने की जरूरत होती है कि यही दोनों हमें ज्यादा प्रभावित और परेशान कर सकते हैं,ऐसा ही समाज और देश के साथ होता है कि यह अवलोकन करना जरूरी हो जाता है कि संकट या युद्ध काल में कौन सी कड़ी कमजोर हो सकती है,उस पर गहरी नज़र रखने और निदान ढुंढने की जरूरत होती है,कौन सी कमजोरी और कमी हमें भीतर से आहत कर सकती है,इसे गंभीरता से देखने की जरूरत होती है।
अब हम इससे थोड़ा सा हटकर विचार करते हैं कि जीवन स्वयं एक संघर्ष या युद्ध है तो इसके साथ हमें कैसे चलना है या कैसे चलना होगा। इससे लड़ना होगा या काट ढुंढना होगा या समन्वय बनाकर चलना होगा या पलायन कि समर्पण कर देना होगा तो पलायन या समर्पण, दोनों में पराजय निश्चित है तो क्यों न पुरी ताकत और उपलब्ध संसाधनों के बल पर पुरी ताकत से लड़ा जाए कि जीत गए तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे और अगर पराजय मिली तो शौर्य पराक्रम से परिपूर्ण पराजय या मौत मिलेगी पर मैदान नहीं छोड़ना होगा,
सब जाए अभी पर
मान रहे
मरने पर गुंजित गान रहे
यह जन्म हुआ किस अर्थ गहो
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो
समझो जग को न निरा सपना
पथ आप प्रशस्त करो अपना
ईश्वर हैं बस अवलम्बन को
नर हो,
न निराश करो मन को।
इसके लिए भीतर से जागना और जागकर उठना और उठकर चलना और चलकर दौड़ना पड़ता है। तभी तो निराला बोल उठते हैं,
जागो फिर एक बार
श्रेष्ठतम जन जीते हैं
गीता की उक्ति है
स्मरण करो बार बार
जागो फिर एकबार
जीवन संग्राम में हमें बार बार गिरना उठना और चलना पड़ता है।
शायद डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धान्त में सर्वाइवल औफ द फिटेस्ट का दर्शन गीता से ही लिया हो और यह सच भी है कि प्रकृति एक ही साथ निर्मम और दयालु दोनों है,वह शक्तिशाली की रक्षा करती है और कमजोर को मार देती है, हवा जलते हुए दीपक को बुझा देती है पर आग को और भड़का देती है।
यह हमारे सामाजिक राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन का भी सच है कि बाज नहीं**कबूतर और मुर्गे ही शिकार किए जाते हैं।
--------
जीवन समग्र रुप में दो आयामों शक्ति. आलेख :
-------
जीवन समग्र रुप में दो आयामों से मिलकर एकत्व का, समग्रता के साथ एक होने का बोध कराता है।
हर सिक्के के उसी तरह दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पृष्ठभाग और हम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं।
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय व्यवस्था भी इसी आधार पर चलती रहती है। आग और पानी जहां सृजन और विकास में सहायक होते हैं, वहीं विनाशकारी भी होते हैं और इसे गंभीरता से समझने की जरूरत होती है कि हम सब किन किन रुपों में उनका कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं। इसी आग ने मानव सभ्यता के विकास के मार्ग प्रशस्त कर दिए तो आज भी उसके गलत इस्तेमाल से विनाश भी होते रहे हैं। पानी हमारे जीव-जगत के जीवन का आधार है तो हर वर्ष अरबों खरबों के विनाश का कारण भी पानी ही है।
जैसा हमने पूर्व में कहा है कि सबकुछ द्विआयामी हैं और ये द्विआयामी होना ही सबकी सार्थकता को सिद्ध करता है,बस इसकी उपयोगिता और उपादेयता को समझकर इसके प्रयोग के परिणामों को पहले समझ लेना जरूरी होता है कि जिस घी के सेवन से शरीर मजबूत और पुष्ट होता है वही घी अतिसार रोगी के लिए विष हो जाता है। जो पानी जीवन सृजित करके हमें जीवन देता है,उसी की अतिशयता भयानक बर्बादी भी लाती है।
इसलिए हमें जब भी किसी के मोल और मूल्यों का आकलन करना हो तो द्विपक्षीय करना होगा अन्यथा वह कभी सही आकलन नहीं हो सकेगा।
--------
अंधकार और एकान्त शक्ति. आलेख :
--------
अंधेरा सदैव से उपेक्षित और लांछित रहा है वैसे ही जैसे असफलता ग्राह्य और सराहनीय नहीं होती है। परन्तु अंधकार और असफलता को कोसिए मत, कोई जब अंधकार में होता है, असफल होता है,तभी किसी और को रौशनी और कामयाबी मिलती है।
जीवन सर्वत्र प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा ही है जहां सब कोई अपने अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं, निरन्तर भाग-दौड़ मची रहती है। बाजार पहले पहुंचना है कि अच्छी और ताजी सब्जियां मिल जाए,बस स्टैंड या रेलवे प्लेटफॉर्म पहले पहुंचना है कि टिकट और अच्छी जगह मिल जाए या अग्रिम टिकट लेनी है तो पहले से तैयार रहें अन्यथा सीटें बूक हो जाएगी, चारों तरफ मारा-मारी है और यही जिन्दगी का एक कड़वा सच भी है और इसी भाग-दौड़ में, आपा-धापी में हम सब जीते रहते हैं। ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा इसी भाग-दौड़ में खर्च हो जाती है और जब थोड़ी स्थिरता आने वाली होती है या आ जाती है तो वह ऊर्जा इतनी शेष नहीं रह जाती कि संसार रुपी सागर में जीवन रुपी नौका का संचालन अपने तरीके से किया जा सके। अगर हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो वही अंधकार,वही एकान्त,वही असफलताएं,वही अतीत हमें बहुत कुछ सोंचने, विचारने,मंथन और विश्लेषण करने का सही समय प्रदान करता है।
अंधकार और असफलताएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने का काम करते हैं।हम लोगों की भीड़ में, चकाचौंध रौशनी में, सफलताओं के उन्माद में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। रौशनी में सबकुछ नजर आते हैं पर हम खुद नजर नहीं आते हैं, भीड़ और जलसे में सब नज़र आते हैं पर हम खुद को नहीं देख पाते हैं जो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सबको देखते सुनते उम्र निकल जाती है और हम खुद को न देख पाते हैं,न सुन पाते हैं और न समझ ही पाते हैं। संसार को समझ लिया और खुद को ही नहीं समझे तो हासिल क्या होगा, इसलिए एकान्त, अंधकार और अतीत हमें खुद को समझने के लिए निहायत ही जरूरी कारक है। अंधेरे और एकान्त में एकाग्रता के भाव पैदा होते हैं और उन्हीं क्षणों में ही हम खुद को देख समझ पाने में सक्षम हो पाते हैं। वर्द्धमान और सिद्धार्थ को ऐसे ही अंधकार और एकान्त क्षणों में इस सच का बोध हुआ और वे खुद की खोज में निकल पड़े और खुद को पाकर सबकुछ पा लिया। क्या क्या जतन नहीं करना पड़ता है पर अन्त में सबकुछ निस्सार और व्यर्थ साबित हो जाता है।एक आम आदमी क्या करता है, बड़ी मेहनत मशक्कत से नौकरी पाता है या रोजगार धंधा करता है, धनोपार्जन करता है,शादी ब्याह करके घर परिवार बसाता है,खुब नाम -धाम कमाता है और एक रोज अकेले चला जाता है।इस अकेले आने जाने का सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है और
चलता भी रहेगा और आने जाने के मध्य काल में ही सब पाये खोये के किस्से समाप्त हो जाते हैं।
खुद के लिए और खुद को जानने के लिए आदमी को मोहलत ही नहीं मिलता,
अजीबो गरीब सिलसिला है ज़िन्दगी का,
सब हासिल करते हैं सब लूटा देने के लिए।
हम सब अपनी खुशियों को अपनों की खुशियों में तलाश करते हैं और उन्हीं पलों में अगर खुद की खुशियों के लिए अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त भी एक अनजाना सा डर मन में समाया रहता है कि इनसे अपनों की खुशियों पर कहीं बर्फ न पड़ जाए और हम सिमट कर रह जाते हैं। हालांकि जिन्दगी का यह सुखद और कड़वा सच, दोनों ही है।
अब यहां अतीत के अंधकारमय और प्रकाशमय दोनों पक्षों का अवलोकन करें, दोनों दुखदाई होते हैं।
अतीत के सुख दुःख, इसलिए दुखदाई होते हैं कि मौजूदा हालात अगर सुखमय है तो छीन जाने का डर सताता है और दुखमय है तो अतीत का सुख रुलाया करता है, इसलिए दोनों से बचने की जरूरत है और दोनों हमारे सच भी हैं।
इसलिए अंधकार और भीड़ से दिग्भ्रमित होने या भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है, अंधकार और एकान्त के क्षणों में ही हम अपने आप का अवलोकन करते हुए पाने खोने का आकलन कर सकते हैं
और खुद को समझ भी सकते हैं।
अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हैं,अपनी रचना*ओल्ड मैन ऐन्ड द सी में कहते हैं कि,
अकेले समंदर में चुपचाप मछलियां पकड़ने का जो सुख है उससे बड़ा सुख तो एकान्त का है कि मैं जिन्दगी के बारे में कुछ सोंच सकता हूॅं।
इसलिए अकेलापन से बचते हुए, रौशनी और भीड़ से बचते हुए* एकान्तिक जीवन के सुख का आनन्द लीजिए,यही सच है।
-------
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस शक्ति. आलेख :
---------
आज वैश्विक समाज ११ वां अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है जो मूलतः भारत भूमि की वैश्विक समाज को एक अनमोल देन है। यद्यपि यह भारतीय आध्यात्मिक जीवन दर्शन, चिन्तन एवं व्यवहार आचरण से निकल कर आया है फिर भी इसका स्वरूप किसी मत,पंथ, विश्वास, विचार आदि से उपर उठकर वैश्विक आदर्श एवं व्यवहार बन गया है। इसकी जड़ें आदियोगी शिव से निकल कर, वेदों, उपनिषदों, योग शास्त्रों,जैन, बौद्ध मतों और समस्त विश्व में फैल गयी और आज वैश्विक धरोहर बन गया है।
ऐसे तो यह मूलतः दो शब्दों यथा,योग और आसन से बना है परन्तु आमतौर पर लोग योग के नाम से ही जानते हैं परन्तु इसकी समग्र व्याख्या तो अद्भुत है जैसे ईश्वर की समग्र व्याख्या नहीं की जा सकती है वैसे ही योग भी है। जब हम इसके व्यूत्पत्ति पर विचार करते हैं तो यह * यूज्
धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है और यहीं से इसकी गहराईयों से पड़ताल शुरू हो जाती है कि किससे और कैसे जोड़ना और क्यों जोड़ना तो हम ज्यादा गहराईयों में न जाकर
इस रुप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करुंगा कि आप सहजता और सरलता से समझ लें और इसे आत्मसात करने की कोशिश करें।
ऐसे तो शिव संवाद, वेदों, उपनिषदों,योग शास्त्रों,जैन और बौद्ध मतों में इसकी विशद् व्याख्या की गयी है जिससे अनुप्रेरित अनुप्राणित होकर यह चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और अन्य द पू एशियाई देशों में भी व्यापक रुप में फैल गया। द पू एशियाई देशों में इसे स्थापित करने का काम बोधिधर्मन ने किया जो भारतीय ध्यान पद्धति से झेन या जेन बन गया। हम दो सूत्र वाक्यों पर ही इसकी महत्ता, उपयोगिता और उपादेयता पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूॅं,वे दो सूत्र वाक्य,
योग: कर्म सु कौशलम्
और योगश्चित्तवृत्ति निरोध: है
और इसे हम सहज तरीके से आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे।
लेकिन इसके पहले यह बताना भी उचित प्रतीत होता है कि जैसे मानव शरीर स्थूल, सूक्ष्म एवं कारणिक होता है वैसे ही योग विद्या के तीन आयाम होते हैं,आसन, स्थूल अवस्था, प्राणायाम,सूक्ष्मावस्था
और योग,कारणिक अवस्था से जुड़ा है जो हमारे समस्त क्रियाशीलताओं से युक्त है।
आसन से शरीर शुद्ध और स्वस्थ होता है तो प्राणायाम, हमारे प्राणशक्ति को सशक्त करता है और योग साधना आत्मा और अन्तश्चेतना को परम शक्ति से जोड़ने का काम करता है और ये समस्त क्रियाशीलताऍं
अष्टांगयोग या मार्ग से जुड़े हैं जिनमें ध्यान की बड़ी महत्ता और महिमा है जिसे मेडिटेशन भी कहा जाता है जो वैश्विक स्तर पर सभी मत,पंथ और सम्प्रदायों में द्रष्टव्य है।
अब हम उपरोक्त दो सूत्र वाक्यों पर आते हैं
जिसे समझना बहुत जरूरी है।
पहला सूत्र क्या कहता है जो भगवद्गीता से उद्धृत है,योग: कर्म सु कौशलम् अर्थात् योग और कुछ नहीं आपके विहित और निर्धारित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है,इसे समझना ही संसार चक्र को समझना है। हम सभी मनुष्यों को कुछ न कुछ कामों के लिए निर्दिष्ट किया गया है जिसका पालन करना
हमारा परम धर्म ( कर्तव्य) है और इससे पलायन ही अपकर्म या पाप है। अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से इन्कार कर रहा है तब श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का ज्ञान देते हुए बताते हैं कि इस कर्मक्षेत्र में जो कर्म तुम्हारे लिए निर्धारित है अर्थात् युद्ध करना, उसमें श्रेष्ठता ही योग है। जो जिस कर्म करने के लिए चयनित हैं,उसका श्रेष्ठतापूर्वक
पालन करना ही योगी का धर्म और धर्म का मर्म है और वही कर्मयोगी भी है। कितना सुन्दर और व्यवहारिक संदेश है कि बगैर किसी पुर्वाग्रह या दूराग्रह के हमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए,क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है, नहीं और यही परम सत्य है जो हमें हमारे संसार चक्र से मुक्त करता है।
दूसरा सूत्र जो योग शास्त्रों, औपनिषदिक दर्शन और जैन तथा बौद्ध मतों का सार है,
योगश्चित्तवृत्ति निरोध:
अर्थात् अपनी अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है।
मनुष्य के दुःख के मूल में इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना,मोह, आकर्षण,अतीत आदि की सत्ता है। इच्छा और कामना हमारी चित्तवृत्तियों को संचालित, नियमित और नियंत्रित करती हैं और इच्छाओं के संसार का कोई अंत नहीं है,एक की प्राप्ति हुयी नहीं कि दूसरी पैदा है गयी, रक्तबीज की तरह अनन्त हैं ये इच्छाएं और कामनाएं जो कभी तृप्त ही नहीं हो सकती हैं और इनका तृप्त न होना ही
दुःख और क्लेश को जन्म देता है। हमारे संसाधन सीमित और न्यून हैं जिनसे वांछित की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है।यदि आप समस्त संसाधनों से युक्त भी हैं तो आरोग्य,भूख, नींद, शान्ति आदि नहीं खरीद सकते हैं तब क्या करना है, अपने मन चित्त को योग-साधना के द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश करनी है ताकि जीवन संयमित, मर्यादित और परिमार्जित हो सके।
चित्त की चंचलता हम मनुष्यों को दिग्भ्रमित करती रहती है,माया,भ्रम और कल्पनाओं के संसार का सृजन करती रहती है, हमें सत्य से सदैव दूर ले जाने का काम करती है, इसलिए योग-साधना के द्वारा ही हम सुखी रह सकते हैं।
यह औषधियों का औषधि है,मानव जाति के लिए वरदान है और निरपेक्ष भाव से युक्त है।
इसे गहराई से समझने की जरूरत है कि किसे सुख और शान्ति नहीं चाहिए पर उनकी खोज हम बाहर करते हैं जबकि वह हमारे भीतर ही उपलब्ध है, इसलिए योग सिर्फ अपने अपने इष्ट से जुड़ने की कला और विज्ञान नहीं है बल्कि स्वयं को स्वयं से जोड़ने की कला और विज्ञान भी योग है।
--------
जीवन और हम : शक्ति. आलेख : ८५ .
-----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
किसी ने किसी से पुछा कि जिन्दगी क्या है तो दूसरे ने कहा कि जिन्दगी और कुछ नहीं बस एक प्याली चाय की तरह है,पी लिए तो सही और पुरा अनुभव है,छलक गयी तो अधुरा अनुभव है और सबकी कुछ न कुछ छलकती ही है। जिन्दगी एक ऐसी सच्चाई है जो सबकी अपनी-अपनी सच्चाई है,जैसा भोगा वैसी ही जीवन की परिभाषा बन गयी। एक धनाढ्य व्यक्ति से पुछिए और उसके हम उम्र पड़ोसी से पुछिए तो दोनों की अनुभूतियों में आसमान जमीन का फर्क दिखाई पड़ेगा। इसी तरह एक संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, नेता,अभिनेता, विभिन्न पेशेवर,
मजदूर, भिखारी आदि आदि की जिन्दगी की अनुभूतियां भी अलग अलग और अद्भुत होती हैं जिनकी अलग-अलग अनुभूतियों पर शोध किए जा सकते हैं। तथागत सिद्धार्थ ने जीवन को दुःख ही दुःख ही बताया वहीं कृष्ण ने जीवन को रसमय और प्रेममय के साथ साथ संघर्षमय भी बताया और इनके भेद के भी कारण हैं। कृष्ण ने अपने जीवन के आरम्भिक काल से ही जीवन को रसमय,गीतमय और प्रेममय देखने के साथ साथ संघर्षमय भी देखा। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध बाल्यकाल से ही लड़ते रहे। परन्तु सिद्धार्थ को समस्त सुखों को भोगने के बाद ऐसी अनुभूति हुयी कि जीवन में दुःख ही दुःख है और इन दुःखों से मुक्ति मार्ग खोजना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीसस ने प्रेम, करुणा और क्षमा को मानव जीवन का सार बताया कि उनके जीवन में कृष्ण जैसा न तो गीत था न नृत्य और संगीत था और ना ही बड़े बड़े युद्ध ही थे। सिद्धार्थ ने भी कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े थे,तो जो उन्होंने देखा, किया और भोगा,वही उनका जीवन बन गया। फिर एक गंभीर सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर जीवन है क्या,तो जो आपकी अनुभूति होगी,वही आपका जीवन होगा। एक निर्धन और संसाधनहीन व्यक्ति की भी चाहतें होती है कि वह भी अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे मकान में रहे,वाहन और अन्य सुविधाएं हों पर वह ऐसा नहीं कर पाता और वह बुद्ध की तरह कह उठता है कि जीवन में और कुछ नहीं दुःख ही दुःख है लेकिन इसके ठीक विपरीत एक धनी और साधन सम्पन्न व्यक्ति कहेगा कि जीवन सुखमय है और सुख भोगना ही जीवन है। कुछ के लिए जीवन दोनों के मध्य का है,कभी दुःख काल तो कभी सुख काल का वह भोग करता है।इस तरह दो अति पर जी रहे हैं और एक मध्य में जी रहा है,इसे ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा कि दोनों अतियों से बचने की जरूरत है,अति किसी भी परिस्थिति में किसी अवस्था में पूर्णता का बोध नहीं करा सकता है,इस तरह आप जीवन के विभिन्न आयामों में जीवित रहते हुए जीवन जीते रहते हैं,जो चाहा मिल गया तो अंगूर मीठे हैं और नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। इसलिए जीवन को जिस रुप में आप जीना चाहते हैं, अगर नहीं हो पाता तो जिस रुप में उपलब्ध है, सहर्ष स्वीकार करने का प्रयास कीजिए और जो है उसका सुख लीजिए अन्यथा जो है उनसे भी आप वंचित रह जाएंगे। कहीं धन है तो भोग नहीं और भोग की कामना है तो संसाधन नहीं और धन और कामना दोनों हैं तो भाग्य नहीं,यही जीवन का सच है।
---------
जिम्मेदार कौन शक्ति. आलेख :
----------
आदमी ने आदमी के साथ मिलकर परिवार और समाज बनाया, आदमी ने आदमी को जीने रहने का सलीका सीखाया, फिर आदमी ने आदमी को हत्या लूट, बलात्कार,फरेब, हकमारी आदि करना भी सीखाया और आज दोषारोपण तंत्र और व्यवस्था पर करता है। समस्त जीवन व्यवहार व्यवस्था,कायदा कानून,नीति नियम, नैतिकता के मापदण्ड आदि आदमियों ने निर्धारित किए फिर आज सबकी विफलताओं के लिए सब एक दूसरे को दोषी ठहराना भी शुरु कर दिया।
जो जिनका निर्माण करता है, बदलाव और नष्ट करने की जवाबदेही भी उन्हें ही लेनी चाहिए पर आज हम सब इस जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। एक बड़ी रोचक कहानी है जो सिर्फ कथा कहानी नहीं बल्कि जीवन का व्यवहार भी है जिसका अवलोकन रोज़मर्रा की जिन्दगी में भी देखा जा सकता है। एक शिक्षक कहीं से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अपने विद्यालय के एक छात्र पर पड़ी जो सड़क के किनारे बिना किसी आड़ के खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि यह आचरण सभ्य और शिष्ट नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए उसे कहा कि,ठहरो ठहरो, परन्तु वह लड़का भाग गया।शिक्षक ने सोंचा कि आगे चलकर वह उसके पिता से इसकी शिकायत करेगा। जब शिक्षक उसके घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका पिता छत पर से ही पेशाब कर रहा था,शिक्षक यह देखकर हतप्रभ रह गये और वहीं से लौट गये कि अब शिकायत किससे करें कि वह विद्यालय में भी सबको समझाते रहते थे।
यही दुर्गति आज हमारे समस्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन की है जिसकी जिम्मेदारी हर नागरिक को लेने की जरूरत है।चारो तरफ हिंसा, रक्तपात, युद्ध और आतंकवाद आदि फैले हुए हैं जिनसे मानवता कराह रही है पर इसके लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और ये स्थिति वैसी ही है गांव में लगी आग को बुझाने में पक्के मकान वाले इसलिए तमाशबीन बने हुए थे कि हमारा घर तो सुरक्षित है पर उनकी समझ में ये बातें नहीं आ रही थी कि उनके घर भी जलेंगे और बच भी गए तो भूखे नंगे उनको लूट लेंगे और मार देंगे। जब आग जंगल में लगती है तो सारे पेड़ जल जाते हैं,सूखे तो जलते ही हैं,उनके साथ हरे और मजबूत पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही स्थिति हमारे समाज और देश की है कि उनके बेटे बेटी खराब हो रहे हैं, वहां गलत हो रहा है,उसके साथ अत्याचार और शोषण दोहन हो रहा है, हमें क्या,पर ये दावानल है,जब भड़केगी तो पुरा जंगल जलेगा इसलिए सबको सचेष्ट और सावधान रहने की जरूरत है। हमारे बच्चे भी इसी समाज का हिस्सा हैं और इसी परिवेश में पल बढ़ रहे हैं और उसके प्रभाव से वे भी वंचित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जहां तक गलत के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है, जरुर उठाएं अन्यथा कल आपका ज़मीर इसके लिए आपसे सवाल पूछेगा तब आप मौन रह जाएंगे। बोलकर, सड़क पर खड़ा होकर, लिखकर या जिस भी स्वरूप में हो,जिस दिन सब गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू कर देंगे, बदलाव तो सुनिश्चित है पर ऐसा करने के लिए बड़े साहस, आत्मबल,
निःस्वार्थता और त्याग की जरूरत होती है जो सहज नहीं है जिसके कारण ये प्रवृत्तियां अनियंत्रित हो जाती है।हम निज के हित और स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं जो मनुष्यों की सहज वृत्ति है और इसके कारण भी विडम्बनाएं जन्म लेती हैं। आज विश्व बड़े युद्ध के कगार पर खड़ा नजर आ रहा है,हर देश अपना अपना लाभ हानि देख रहा है, समस्त मानव समुदाय आसन्न युद्ध से सशंकित है पर जिन्हें लगता है कि हम प्रभावित नहीं हो सकते हैं ,खामोशी से तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि यह दावानल है, भड़केगा तो सारा जंगल अर्थात् संसार जलेगा पर सब अपनी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक चालें चल रहे हैं और खेल देख रहे हैं। सनद रहे कि दो बड़े विश्व युद्धों की आग में सब कमोबेश झूलसे थे।
ऐसे ही समाज और व्यवस्था का विद्रूपीकरण है जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं पर यह सोंचकर खामोश रह जाते हैं कि हम सुरक्षित हैं और यही सोंच हमें पतनोन्मुख बनाने का काम करती रही है। इसलिए वैयक्तिक चेतना के साथ साथ नागरिक चेतना, सामाजिक चेतना, राष्ट्र चेतना और वैश्विक चेतना की सख्त जरूरत है। आज के बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं,गलत राह पकड़ रहे हैं जिनकी परिणति अपराध,हिंसा, बलात्कार आदि में हो रही है, विवाहित जोड़े एक दूसरे की हत्या कर करवा रहे हैं जो धीरे-धीरे एक विकराल रुप ले रहा है। रोज रोज अपहरण और बलात्कार की घटनाओं से दिल बैठा जाता है।लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, आखिर हो क्या रहा है, सिर्फ सरकारी तंत्र और व्यवस्था ही नहीं हम भी जिम्मेदार है कि कहा गया है कि अपराध और अन्याय वहीं पनपते हैं जहां उन्हें प्रश्रय दिया जाता है, इसलिए हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी सरकार और व्यवस्था है।
स्मरण रहे कि जो गलत है सो हर हाल में गलत है और सही सदैव सही है और सबकी अपनी-अपनी कीमत होती है।
--------
रुपान्तरण और सृजन शक्ति. आलेख :
---------
रुपान्तरण और सृजन इस सृष्टि का एक अद्भुत सत्य है जो विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय और संयोजन भी है।स्थावर जंगम सभी सदैव रुपान्तरित होते रहते हैं और इसके पीछे का दर्शन, सिद्धान्त और व्यवहार भी एक असामान्य सी अनुभूति देता है जिसे सामान्य तरीके से न तो देखा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है।इसे जानने और इसके मर्म को समझने के लिए गहन और अन्तर्भेदी दृष्टि की जरूरत होती है अन्यथा इसे हम साधारण सा सृजन और विनाश का नियम भर समझ कर जानकर ही रह जाएंगे।
हर गहन पीड़ाएं और घना अंधकार अर्थात् जब पीड़ाएं और अंधकार गहन होते होते अपने चरम पर पहुंचते हैं तभी उसी क्षण रुपान्तरित होने की प्रक्रिया शुरु हो जाती है।यह सिर्फ दुःख, वेदना, पीड़ा, अंधकार और संघर्ष आदि के बारे में ही सत्य नहीं है बल्कि सुख,भोग, ऐश्वर्य आदि भी अपने अपने चरम पर रुपान्तरित होते रहते हैं जिसके अवलोकन की जरूरत होती है। शारीरिक मानसिक अवस्थाएं भी रुपान्तरित होती रहती हैं और इतिहास तथा भूगोल इसके प्रमाण हैं। कहते हैं आदिकाल में जहां पर्वत थे,वे जंगल हो गए, नदी सागर में पर्वत उग आए, रेगिस्तान, खेत मैदान में और खेत मैदान, रेगिस्तानों में बदल गए और यह परिवर्तन अनवरत और अबाधित रुप से चल रहे हैं।
हर सृजन और रुपान्तरण को एक चरम बिन्दु से होकर ही गुजरना होता है। एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो प्रसव काल तक उसे जो अनुभूतियां होती रहती हैं,वे रोमांचक और गहरी होती हैं पर पीड़ादायक नहीं होती
हैं परन्तु सृजन अर्थात् प्रसव काल जब एक शिशु गर्भ से बाहर आने लगता है जिसे प्रसव वेदना कहते हैं, बड़ी भयानक शारीरिक वेदना एक स्त्री को सहना पड़ता है जिसे चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है जिसे पुरुषों को सहना अगर असंभव नहीं तो असह्य जरुर होता है। पर सृजनात्मक शक्ति स्त्री के पास होती है,वह जब प्रसव वेदना सहती है,उसके अंग जख्मी होते हैं तो वह एक नया जीवन सृजित करती है। उसकी काया रुपान्तरित हो जाती है,वह नारी से सम्पूर्ण स्त्री के रुप में रुपान्तरित हो जाती है जो इस बात का प्रमाण है कि सृजन और रुपान्तरण के पूर्व एक अस्तित्व को,एक अवस्था को चरम पर पहुंचना और सहना पड़ता है और तब कहीं रुपान्तरण हो पाता है। सुबह होने के ठीक पहले का जो अंधकार होता है,गहन और गहरा होता है और इसका अवलोकन किया जा सकता है,बस वही ब्रह्म मुहूर्त का काल है, पूर्व दिशा में सफेदी आने लगती है फिर अरुणोदय हो जाता है,एक निश्चित तापमान पर जल,वाष्प में और बर्फ में बदल जाता है जो रुपान्तरित होने का चरम बिन्दु है।वनस्पतियों में भी लगभग ऐसी ही क्रियाशीलताएं होती हैं, उसके रुपान्तरण को आधुनिक यंत्रों से देखा तो जा सकता है पर बीजों के फूलने और सड़कर अंकूरित होने की पीड़ा जो बीज सहता है,उसकी अनुभूति मनुष्य की तरह नहीं की जा सकती है। बीज को अपने मौलिक अस्तित्व को मिटाना पड़ता है,तब एक नए पौधे का जन्म होता है।कहा भी गया है,
मिटा दो खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है,
खाक अर्थात् मिट्टी में मिलाना होता है, सबकुछ खत्म हो जाता है तब नया सृजन होता है। चाहे वह गौतम सिद्धार्थ का बुद्ध बनना हो या वर्द्धमान का महावीर बनना हो, अस्तित्व को खोना पड़ता है, अनन्त पीड़ाएं झेलनी पड़ती है तब रुपान्तरण होता है, वनवास झेलना पड़ता है, लाक्षागृह की भयावहता झेलनी पड़ती है,रण छोड़कर भागना पड़ता है,घास की रोटियां खानी पड़ती है तब कहीं जाकर कुछ मिलता है। कहते हैं गौतम सिद्धार्थ को अर्हत्व या बोधी प्राप्ति के पूर्व असह्य पीड़ा झेलनी पड़ी थी और महापरिनिर्वाण काल में भी मर्मान्तक पीड़ा झेलनी पड़ी थी। राम चौदह वर्षों तक वन वन भटके तभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सके।
अब हम साधारण मनुष्यों को अपनी पीड़ाओं के, संघर्षों के, वेदनाओं आदि के
चरम को जानना और समझना बड़ा कठिन है पर यह समझना बड़ा सहज है कि कोई
अवस्था या क्रियाशीलता जब अपने चरम पर पहुंचती है तो स्वत: स्फूर्त रुपान्तरित हो जाती है,बस बड़े धैर्य,साहस, सहनशीलता और समय के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर यहां पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि प्रतीक्षा का भी तो चरम होता होगा,सीमा होती होगी जो अनबूझ सवाल रहा है कि सीमा या हद वही है जहां से रुपान्तरण और सृजन शुरु हो जाता है।
इन्सान और इन्सानियत. शक्ति. आलेख :आलेख : ८४ .
--------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
अगर इन्सान अपनी मेहनत मशक्कत और ईमानदारी से अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके भीतर इन्सानियत का जज्बा उतना ही मजबूत होता है, हां, अगर वो ऊंचाई बेईमानी से मिलती है तो उसके भीतर इन्सानियत मर जाती है और वह इन्सान और इन्सानियत की कीमत कद,पद,पैसे और रुतबों से आंकता है। यह प्रवृत्ति आज के सामान्य जीवन में भी दिखाई पड़ती है जिसे आप हर जगह विभिन्न रुपों में देख सकते हैं और वैश्विक स्तर पर भी अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कई बड़े नाम हैं जिनमें से मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचन्द और फणीश्वर नाथ रेणु, राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम, समाज सुधारकों में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और डॉ अम्बेडकर और ऐसे कितने नाम कितने क्षेत्रों में हैं जिन्होंने अपनी अथक मेहनत,अदम्य साहस,लगन और कुछ कर गुजरने की जुनून के बल पर अपनी-अपनी ऊंचाईयों को छुते हुए एक इतिहास को रचा और एक प्रतिमान बना दिया जिसे आज तक कोई स्पर्श नहीं कर सका और वो ऐसा इसलिए कर सके कि उन्हें विरासत में दुःख, अभाव, पीड़ाएं और सतत् संघर्ष मिले थे।
शास्त्री जी जीवन भर एक आम आदमी की तरह जिए, अपने बच्चों को कतार में लगवाकर नामांकन करवाने को कहा और अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया। जब वे शपथ ग्रहण करने जा रहे थे तो उनके कुर्ते का कोर फटा हुआ था जिसे देखकर उनकी पत्नी ने टोका तो उन्होंने बड़े सपाट शब्दों में कहा कि,करोड़ों भारतवासी अभी भी अधनंगे और फटे कपड़े पहनते हैं तो उनके प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह नये कपड़े पहनकर शपथ लेने जाए। राजेन्द्र बाबू,उद्भट विद्वान जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहकर सरकारी रसोईया के बदले अपनी पत्नी से खाना बनवाकर खाया,जीरादेई से चने का भूंजा और सत्तू खाए पर सरकारी धन का दुरुपयोग कभी नहीं किया और जीवन के अंतिम काल तक उनके पास पटना में एक मकान तक नहीं था और सदाकत आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली, सरदार पटेल का जीवन भी ऐसे ही संघर्षों और परिश्रम तथा अदम्य साहस का परिचायक है। अकेले दम भारत के हितों के लिए लड़ते रहे और भारत के एकीकरण में अकेले दम अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इनके हृदय में भी देश के वंचितों और पीड़ितों के लिए अनन्य प्रेम था। ठीक इन्हीं के तरह अब्दुल कलाम अखबार बेचकर देश के शीर्ष वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने परन्तु इनके मन में कभी अहंकार नहीं जगा और देश समाज के लिए बस जीते रहे। इन महान विभूतियों के हृदय में जीवन पर्यन्त गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के प्रति समर्पण और प्रेम रहा।
ऐसे ही संघर्ष और अभावों में पले बढ़े मुंशी जी और रेणु जी रहे हैं जिनके सम्पूर्ण साहित्य में मानवीय पीड़ा, वेदना, शोषण दोहन,असमानता के प्रति विद्रोह आदि के जीवन्त चित्रण मिलते हैं। संघर्ष और पीड़ाएं जब सघन होती है तो वह उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में झलकती है। उनके हर
नजरिए में इन्सान और इन्सानियत नजर आती है जो एक प्रेरणा और आदर्श बनकर सबके सम्मुख उत्पन्न होता है। अमरीकी राष्ट्रपतियों में जौर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन भी मानव और मानवता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वाशिंगटन ने भी गरीबी और संघर्षों को देखा और अमेरिका को एक नया स्वरूप देते हुए उसे स्वतंत्र रुप दिलवाया और आम अमरीकी होने का मापदंड स्थापित किया। लिंकन ने जिस गरीबी, संघर्ष और नस्ली भेदभाव को झेला था, उसके विरुद्ध संघर्ष किया और वहां गुलामी प्रथा को खत्म कर एक वैश्विक उदाहरण स्थापित किया। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं जो आम आदमी को संघर्ष और पीड़ाओं से निकलकर खास आदमी बनाते हैं और वे इन्सान और इन्सानियत की बेमिसाल मिसाल बनकर एक युग का निर्माण करते हुए युग नायक और युग निर्माता बन जाते हैं। जिन्हें विरासत में पद,पैसा, प्रतिष्ठा और सत्ता मिल जाती है वे कभी भी जीवन के मोल और मूल्यों की स्थापना नहीं कर सकते हैं,उनके भीतर मानवीय वेदना और संवेदना का कोई स्थान नहीं होता है। पद और सत्ता या धन और प्रतिष्ठा जिन्हें संघर्षों और अदम्य साहस से मिलता है,वे ही इन्सान और इन्सानियत का कद्र कर सकते हैं और एक
मिसाल बन सकते हैं।
आज भी वैश्विक स्तर पर ऐसी विभूतियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानक स्थापित करते हुए देखे जा सकते हैं और तभी तो कहा जाता है कि जो जितने संघर्षों और पीड़ाओं से गुजरता है,उसके भीतर मानवीय वेदना,संवेदना और करुणा उतनी ही सघन होती है।
--------
अहं बोध की प्रकृति और प्रवृत्ति शक्ति. आलेख :आलेख :८३.
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
अहं बोध की अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। अंत:करण पांचष्य के पांच तत्वों यथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और विवेक में से एक तत्व अहंकार भी है और अहंकार की प्रकृति साकारात्मक और नाकारात्मक दोनों होती है जिसमें साकारात्मक बोध की अपनी कीमत है। अहं का सीधा अर्थ होता है, मैं हूॅं और इसका अस्तित्व ही किसी को अपने अस्तित्व में बनाए रखने में उत्प्रेरक का काम करता है परन्तु और कोई नहीं बस मैं ही हूॅं यही नाकारात्मक भाव है जो व्यक्ति को पतन और विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार को दर्प या घमंड के रुप में भी देखा सुना जाता है पर यह अभिमान या स्वाभिमान नहीं है।आंग्ल भाषा में यह ईगो है जो एक नाकारात्मक भाव को पैदा करता है परन्तु प्राउड या सेल्फ प्राईड फीलिंग इससे इतर भाव रखता है, उल्लेखनीय है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत में भी अहंकार को त्याज्य माना गया है जो समस्त मत,पंथ, विश्वास, विचार, मार्ग आदि में अग्राह्य माना गया है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में भी इसे त्याज्य माना गया है और प्रेम मार्ग में तो इसे सबसे बड़ी बाधा माना गया है।इसे सीस से विम्बित करते हुए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा भी है,
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय
राजा परजा जे रुचे सीस देइ ले जाए।
यहां सीस का अभिप्राय सर या माथा नहीं बल्कि वहीं अहंकार है जिसे तजे बगैर प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अहंकार को तजना पड़ता है, कर्ता बोध से मुक्त होना पड़ता है। व्यवहारिक जगत में भी पारस्परिक रिश्तों को बनाए रखने के मार्ग में इसे बड़ी बाधा माना गया है। अब ये व्यक्ति की निज की चेतना पर निर्भर करता है कि अहं बोध को वह किस रुप में लेता और व्यवहार करता है।
देकार्त कहता है कि, मैं सोंचता हूॅं इसलिए मेरा अस्तित्व है और यह सोंच किसी को स्वाभिमानी बनाता है, अहंकारी नहीं बनाता है। विनम्र और विनीत होना एक बड़ा गुण है पर उसका मूल्यांकन अगर कायरता हो तो त्याज्य है, वहां स्वयं का बोध होना जरूरी है। महाभारत और भारतीय पौराणिक गाथाओं में इस अहंकार पर बड़ी रोचक और प्रेरक गाथाएं भरी पड़ी है।
भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अहंकार को देखा कि अर्जुन कहने लगा कि,हे केशव,इस महायुद्ध में मेरे बाणों की शक्ति का जवाब कोई नहीं दे सकता है, देखिए मेरे बाणों की प्रहार से कर्ण का रथ
पांच कदम पीछे चला जाता है और उसके प्रहार से मेरा दो कदम ही पीछे जाता है,यह सुनकर भी श्री कृष्ण ने कर्ण की वीरता और शौर्य की ही प्रशंसा की जो अर्जुन को बुरा लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ने के लिए ध्वज पर आरुढ़ हनुमान जी को और रथ के पहिए में सूक्ष्म रुप में लिपटे शेषनाग को संकेत किया और वे हट गए। इस बार कर्ण के बाणों की प्रहार से अर्जुन का रथ सात कदम पीछे चला गया जबकि श्री कृष्ण स्वयं आरुढ़ थे।
अब श्री कृष्ण ने इस रहस्य को बताया तो अर्जुन मौन रह गया और उसका अहंकार टूट गया। यह कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन का सत्य और यथार्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं में इतना सामर्थ्यवान नहीं होता कि वह सबकुछ स्वयं कर ले बल्कि उसे भी एक समीकरण के तहत ही काम करना पड़ता है। हर परिवार,हर समाज और हर राष्ट्र के मुखिया की सफलता उसके टीम वर्क पर ही निर्भर करती है कि उसके टीम के सदस्य किस रुप में उसका सहयोग करते हैं और वह अपने कुशल नेतृत्व से कैसे सबको
समन्वित नियंत्रित और संचालित करता है,अगर वह यह समझ ले कि सफलता का सारा श्रेय मेरा ही है तो वह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र पतनोन्मुख होकर एक दिन नष्ट हो जाता है।
--------
आदमी का मोल और मूल्य शक्ति. आलेख : ८२.
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
स्थान,काल और जरूरत के अनुसार तो तिनके की भी उपयोगिता और उपादेयता सिद्ध हो जाती है, आदमी तो आदमी होता है,भला उसकी उपयोगिता और उपादेयता की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। इसके अनगनित उदाहरण वैश्विक स्तर पर भरे पड़े हैं बस शर्त यही है कि अपने आप को कभी दीन हीन न समझें। जो स्वयं को सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं देता,उसे कहीं प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिलता,जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, स्वयं को प्यार नहीं दे सकता भला वह दूसरे को कैसे प्रेम कर सकता है। हीरा स्वयं अपना मोल और मूल्य नहीं जानता, सिर्फ जौहरी ही उसका मूल्यांकन कर सकता है। पर हीरा अपनी कीमत कभी नहीं बता सकता पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह मूल्यहीन चमकदार टुकड़ा भर है। जिस दिन किसी जौहरी की नजर उस पर पड़ जाती है,वह एकाएक सर पर सुसज्जित हो जाता है,बस आपको भी अपने गुणवत्ता पर विश्वास करना है और उस दिशा में सचेष्ट होकर कर्मरत रहना है,काल क्षीप्र गति से चलायमान है,वह अपनी गति से चलता रहता है और सबकी परख करता रहता है और अनुकूल वातावरण और अवसर पर उसकी उपयोगिता सिद्ध कर देता है। एक बड़ी रोचक कहानी है जो सत्य प्रतीत होता है। एक विशाल व्यापारिक जहाज कहीं जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े लोग यात्रा कर रहे थे।
सब बड़े व्यापारी, धनाढ्य यात्री और पर्यटक भरे हुए थे। सब अपनी अपनी मस्ती में मग्न थे कि अचानक से जहाज रुक गया। जहाज का कप्तान और मालिक दोनों परेशान हो गए कि उनका कोई विशेषज्ञ तकनीशियन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर गड़बड़ी कहां है। सब परेशान थे। उसी भीड़ में एक गरीब मेकैनिक एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ सब देख रहा था। उसने कप्तान और मालिक से कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे देख सकता हूॅं। दोनों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा कि, बड़े बड़े मेकैनिक हार गए तो तुम क्या कर लोगे,उसने आग्रहपूर्वक धीरे से कहा कि जब सब थक हार गए तो मेरे देखने में क्या दिक्कत है। कप्तान ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरी झलक देखा और कहा कि ठीक है,देख लो। उस मेकैनिक ने अपना गंदा सा झोला उठाया और बोला कि पहले मुझे जांचने दें फिर अपनी मजदूरी भी बताउंगा। वह जहाज के यांत्रिक कक्ष में गया और हर मशीन का गहराई से अवलोकन किया, फिर कुछ ठोक पिटकर देखा और उपर आया और बोला कि मैं इसे ठीक कर दुंगा पर एक लाख रुपए लुंगा। सब लोग राजी हो गए। उसने भाप निकलने नली के नली को गौर से देखा और पाया कि उसका नट ढीला था जिससे जहाज को गति नहीं मिल रही थी। सारा भाप नीचे से लीक होकर निकल जा रहा था,बस उसने उस नट को कस दिया और चालक को कहा कि चालू करो। जहाज चलने लगा। मालिक और कप्तान देख रहे थे, उन्होंने उसकी गुणवत्ता को पहचाना,पहले तो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी,एक लाख रुपए भी दिए और अपनी कम्पनी का मुख्य मेकैनिक के पद पर बहाल कर दिया।
बात बहुत छोटी सी है पर संदेश बहुत बड़ा है कि किसी के पोशाक और परिस्थितियों को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। धूलों में लिपटा हुआ हीरा और सोना भी उतना ही मूल्यवान होता है जितना कि आभूषणालय में सजाकर रखे हीरे जवाहरात होते हैं। समय और जरूरत पर ही आदमी का मोल और मूल्य होता है। स्थान काल और जरूरत पर ही सबके मोल और मूल्य होते हैं और इस चराचर जगत में कुछ भी मूल्यहीन नहीं है।
-------
पिघलना तो सबको पड़ता है : शक्ति. आलेख : ८१
---------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
लोहा चाहे कितना भी सख्त क्यों न हो,भट्ठी में जाने के बाद पिघल ही जाता है और उसे जिस आकार में ढाला जाए,ढल जाता है। इस प्रसंग को एक नहीं कितने ही नजरिए से देखा और मूल्यांकन किया जा सकता है।
यह मनुष्य और उसके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ा सवाल है।आदमी को अगर लोहा मान लिया जाए और संसार को भट्ठी तो इसके कितने ही निष्कर्ष निकल सकते हैं।
मनुष्य प्रकृति प्रदत्त स्वभाव से कोमल, दयालु, क्षमावान, प्रेमपूर्ण, अहिंसक, दयावान आदि होने के साथ साथ इनके विपरीत स्वभावों से भी युक्त होता है। वह परोपकार और दया में सबकुछ लुटा सकता है वहीं क्रोध में आकर, हिंसक बनकर एक निमिष में सबकुछ नष्ट भी कर सकता है। सत्य, धर्म और न्याय के रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है तो इसके विपरीत जाकर महाभारत की रचना भी कर सकता है।काल की भट्ठी सदैव जलती रहती है,जिसकी अनुभूति सबको होकर भी नहीं होती है कि कब वह किसको कैसे पिघलाकर रुपान्तरित कर देती है।वह रत्नाकर को वाल्मीकि और अंगुलीमाल को संन्यासी बना सकती है, वर्द्धमान को जीण महावीर और सिद्धार्थ गौतम को तथागत सिद्धार्थ बना सकती है,राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कन्हैया को योगेश्वर कृष्ण बना सकती है, जीसस को जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद को हज़रत मोहम्मद बना सकती है, नरेन्द्र को विवेकानन्द तो चंगेज, स्टालिन, तैमूर लंग, नादिरशाह आदि को साधारण सिपाही और नेता से भयानक हत्यारा बना सकती है, कालचक्र वह भट्ठी है जो सबको उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप रुपान्तरित करती रहती है। एक अनपढ़ गंवार को कालीदास बना सकती है तो एक हिंसक डकैत से रामायण लिखवा सकती है। स्मरण रहे सबकुछ आपकी आन्तरिक प्रकृति और प्रवृत्ति का खेल है,काल तो हेतु बनने का काम करता है। आज आप बहुत सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं,लोहे की तरह मजबूत हैं पर आप सदैव ऐसे नहीं थे,अतीत को दर्पण बनाकर उसमें झांकने की कोशिश कीजिए तो वह आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा और आप खामोश हो जाएंगे कि कल हम कहां थे और आज हम कहां हैं और कल हम कहां होंगे,ये सब काल की भट्ठी के गर्भ में है कि वह आपको पिघलाकर किस रुप में रुपान्तरित कर देगी पर हम सब इस रहस्य के यथार्थ को कभी समझ नहीं पाते हैं और अपने अपने लौह अहंकार में आत्ममुग्धता के शिकार होकर अपने अस्तित्व के सच को भूल जाते हैं कि फूल बनकर देवताओं के सर पर चढ़ेंगे कि धूल बनकर अर्थहीन हो जाएंगे। काल की गति अद्भुत है,
तिनका कबहुं न निन्दिए जो पायन तर होए
जो उड़ कभी आंखिन पड़े पीर घनेरी होए,
वक्त हमें सदैव यही सीखाता रहता है कि तुम सदैव सावधान और सचेष्ट रहो, हमारी भट्ठी तुम्हें कभी भी पिघलाकर आसमान में बिठा सकती है या धूलकण बनाकर जमीन पर गिरा सकती है। रुप ही तो बदलना है कि या तो कांटे बनोगे या
फूल बनोगे, इसलिए काल की भट्ठी के रुपान्तरण को समझने की सदैव कोशिश करते रहें,कभी वह सिंहासनारुढ़ करवा सकती है तो भीक्षाटन करवा सकती है।
---------
जीवन में कृपया और धन्यवाद : शक्ति. आलेख : ८०
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
लोग अपने संबोधन और संदेशों में बड़ी ऊंची ऊंची बातें कह जाते हैं जो जीवन में व्यवहार और आचरण
की कसौटी पर खरे उतरते नहीं दिखते हैं इसलिए हमने बराबर कोशिश की है कि बात संवाद और संदेश
ऐसे हों जिसे जीवन में आत्मसात करके व्यवहार और आचरण में लाना बिल्कुल सहज हो और आप सबों के समक्ष इसी सन्दर्भ में संवाद करने की कोशिश करता हूॅं।
अरस्तू ने अपने सामाजिक दर्शन में कहा है कि, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,वह समाज में ही रह सकता है और ऐसा नहीं है तो वह देवता या दानव है। अब अपने मनन और चिन्तन में हमनें इसे एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश की कि चाहे देवता हो या दानव,पशु हों या पक्षी,सबका अपना समूह और समाज होता है, बगैर समाज या समूह के या साथ और सहयोग के प्राणियों का अस्तित्व नहीं हो सकता है।आपने कबूतर, गौरैया,तोता,मैनों, आदि पक्षियों के समूह को रोज देखते हैं, तालाबों, पोखरों आदि में जलीय जीवों के समूह भी देखे होंगे। जंगलों में एक सजातीय प्राणियों के झूंड भी आपने देखे होंगे कि सब अपने अपने समूह और समाज में ही रहना पसन्द करते हैं, फिर हम सब तो मनुष्य हैं।
अब यह सहज ही समझने योग्य है कि समूह या समाज मनुष्य को सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करता हैं।अब हम मानवीय व्यवहार और आचरण की बात करते हैं कि सिर्फ मनुष्य के पास ही अभिव्यक्ति के लिए भाषा और उसकी एक मर्यादा भी है जिसे हर मनुष्य को समाज में रहने के लिए समझना ही जरूरी नहीं बल्कि पालन करना भी जरूरी है। सभ्य मानव समाज में उठने बैठने, खाने पीने, चलने और बातचीत करने के कुछ निश्चित मापदंड भी निश्चित किए गए हैं जो हमें एक सभ्य नागरिक बनाते हैं। वैश्विक स्तर पर सभी वर्ग समूह और समाज में इनकी महत्ता है।इस सन्दर्भ में अंग्रेजी के महत्वपूर्ण लेखक ए जी गार्डीनर ने अपने एक रोचक आलेख * On Saying Please में
प्लीज़ और थैंक यू की अद्भुत व्याख्या की है।इसे कृपया, मेहरबानी करके और धन्यवाद और बहुत शुक्रिया कहकर भी सम्बोधित किया जाता है जो आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सहज ही हल करने की ताकत रखता है। इसकी व्यवहारिकता की चर्चा करते हुए गार्डिनर कहता है कि, कृपया और धन्यवाद दो ऐसे शब्द हैं जो आपके दिनभर के कार्यकलापों को या तो बहुत सुन्दर बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए अपने दिन की शुरुआत सु प्रभात, कृपया और धन्यवाद से शुरू करने की आदत डाल लीजिए।
एक रोज उसकी पत्नी ने उसे सुबह सुबह सु प्रभात कहना गलती से भूल गयी,वह भी प्रत्युत्तर में धन्यवाद,सु प्रभात कहा करता था। उसे अजीब लगा। उसका मन एकाएक खिन्न हो गया।उसने गुस्से में बच्चों को डांट दिया। बस में कंडक्टर से और दफ्तर में अपने सहकर्मियों से बहस कर लिया। सब आश्चर्यचकित थे कि इस दफ्तर के सबसे शालीन आदमी आज ऐसा क्यों कर रहा है। रास्ते में उसने अपने व्यवहार पर मन्थन किया कि इसके मूल में क्या है और बात उसकी समझ में आ गयी।उसने पत्नी के लिए एक बूके, बच्चों के लिए चाकलेट और पेट डौग के लिए बिस्कुट लिया। घर लौटते ही अपनी पत्नी को शुभ संध्या कहते हुए सुबह के लिए माफी मांगी, बच्चों को लिपटा कर माफ करना,बोला और अपने पालतू कुत्ते को प्यार से बिस्कुट खिलाया और सबकुछ सामान्य हो गया। यही जीवन के श्रेष्ठ मूल्य और मोल हैं जिसकी हम सब उपेक्षा करते हैं और स्वयं को दुखी करने के साथ साथ दूसरे को भी दुखी करने का काम करते हैं।
जीवन को हम हीं सुखद और दुखद बनाने का काम करते हैं। अपने अच्छे बुरे व्यवहार आचरण के लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। यह हम सबको इसलिए पालन करना चाहिए कि आपसे हमसे आने वाली पीढ़ियां सीखने का काम करती है और जैसा वर्तमान होगा वही आपका भविष्य तय करेगा। घर,बाहर, दफ्तर या अन्य जगहों पर , कृपया,क्षमा करें, धन्यवाद, मेहरबानी करके, शुक्रिया आदि औषधीय गुण रखते हैं जो बिगड़ती परिस्थितियों को भी बदल देती हैं। अगर आपको महसूस हो कि हमसे भूल हो गयी है तो वह छोटा हो बड़ा हो,खुले दिल से माफी मांग लें और उसका असर देखें,आपका मन भी हल्का हो जाएगा और अगला भी शान्त हो जाएगा और अगला को यह लगे कि आपने कोई ग़लती नहीं की है फिर भी क्षमा याचना कर रहे हैं तो उसकी नज़रों में आपकी कीमत बढ़ जाएगी।
जीवन की अनेक शर्तों में यह व्यवहार सबसे बड़ी शर्त है कि किसी से कोई काम हो तो कृपया या मेहरबानी करके या प्लीज़ का इस्तेमाल करें, कार्य सिद्ध होने पर धन्यवाद, शुक्रिया का सम्बोधन करें और भूल महसूस होने पर माफ़ करें, क्षमा करें या सौरी या एक्सक्यूज करते हुए विनीत हो जाएं।
-------
आदमी नियति काल और जतन शक्ति. आलेख : ७९
---------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
कल सब ठीक हो जाएगा ही सोंच कर आज की सारी पीड़ाएँ आदमी झेल जाता है और यही क्रम चलते रहता है। समस्त कालबद्ध क्रियाशीलताएँ सबकुछ विधि विधान के अनुरूप बदलती रहती है और उनमें से कुछ सुखद परिवर्तन या अनुकूलताएँ जीजिविषा और संघर्ष को मजबूत करने का काम करती है और आदमी जीने के लिए फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
जीजिविषा और संघर्ष को इसलिए बनाए रखना चाहिए कि आदमी के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। यही जिजीविषा और संघर्षों की भावनाएं आपात्काल में, प्रतिकूलताओं में और कठिन परिस्थितियों में जूझते रहने का माद्दा पैदा करती हैं और मनुष्य अपने जीवन की लड़ाईयां लड़ते रहता है। अनुकूलताएं हमारे संस्कारों और अहंकार की परख करती हैं और प्रतिकूलताएं धैर्य साहस, सहनशीलता, जिजीविषा, संघर्षशील प्रवृत्तियों की परीक्षा लेती हैं। इनघड़ियों में कुछ चीजें छूट जाती हैं तो कुछ मिल जाती हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं तो कुछ खड़े मिल जाते हैं जो इस सांसारिक जीवन के यथार्थ को जानने पहचानने में मनुष्य की मदद करते हैं। इस सन्दर्भ में गोस्वामी जी ने सच ही कहा है,
धीरज धरम (विहित कर्तव्य)मित्र अरु नारी
आपतकाल परखिए चारी
अर्थात् बुरे और संकटकाल में धैर्य, हमारे कर्तव्य, मित्र और पत्नी के अर्थ और मर्म की परख हो जाती है।
रह गयी बात * ईश्वरीय सत्ता के विधि विधान और नियति या प्रारब्ध का तो कोई इतनी सहजता से नहीं कह सकता है कि वास्तव में सत्य क्या है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा सही होगा, इतनी सहजता से कोई नहीं कह सकता है कि वैश्विक स्तर पर ऐसी कितनी घटनाएँ घटती रहती है जिसे देख सुनकर कोई नहीं कह सकता है कि यह सही हुआ या हो रहा है या ग़लत हो रहा है। रोज दुर्घटनाएं घट रही हैं,लोग मर रहे हैं पर इन मरने वालों या गंभीर रुप से घायल होने वाले लोगों के बारे में सुनकर या देखकर ऐसी अनुभूति होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था,यह तो सरासर अन्याय है।
किसी किसी की मौत तो ऐसी होती है कि उस पर शैलेश मटियानी ने कहा हे कि,कुछ मृत्यु ऐसी होती हैं मानो ईश्वर ने ही उसकी हत्या की है अर्थात् किसी की मृत्यु किसी भी विधान के तहत स्वीकार्य नहीं होती है पर लोग यह कहकर चुप हो जाते हैं कि विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। अवांछित संसार में नजर आते हैं और वांछित अचानक काल कवलित हो जाते हैं। यह रहस्य काल के गर्भ में छुपा रहता है और जब इसके औचित्य या अनौचित्य की बात समझ में आती है तो स्वयं समझने वाला समझने और समझाने की स्थिति में खुद को नहीं पाता है कि वह इसे कैसे स्पष्ट करें।
बस यही संसार का चक्र है जो इस * द्वन्द्वात्मक भाव में चलता रहता है और सब इस चक्र को देखते हुए जीवन को जीने समझने की कोशिश करते रहते हैं। अनुकूलताएँ आदमी को ऊर्जावान और उत्साही बनाती है और प्रतिकूलताएँ भीतर से तोड़ती और कमजोर करती है और साथ ही उसे लड़कर फिर से खड़ा होने की प्रेरणा भी देती है परन्तु लागातार के संघर्ष और पीड़ाएं अगर तोड़ती नहीं तो थका जरूर देती हैं और ऐसे में वह किसी अज्ञेय सत्ता से संरक्षण और सहयोग की कामना करता है।फिर आदमी बस इनमें सहज संतुलन और समन्वय बनाकर जीने की तरकीब करता है और जीने के लिए फिर से जीवन का स्वागत करता है। जो हल हो जाए पहेली है और जो न हल हो * रहस्य है। ईश्वरीय सत्ता ** अज्ञेय और रहस्य है, बस अवलोकन करते रहिए कि आदमी के पास कोई इसका कोई विकल्प नहीं होता है।
जीवन में ऐसे कितने मक़ाम आते हैं जहां आदमी अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य का महत्तम प्रयास करके जब थक जाता है तब वह विकल्पहीन होकर किसी दैवी विकल्प या चमत्कार की आशा करता है कि अंधकार अपने चरम पर है,कल एक चमकदार सुबह होगी और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ वह फिर नये सिरे से एक नये संघर्ष के लिए उठ खड़ा होता है जो जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके जिजीविषा को बनाए रखने का काम करती है। वह निराशा और नाउम्मीदियों के क्षणों में भी उस अज्ञेय की ओर एक आशा भरी नजरों से देखता और प्रयास करते रहता है कि कल उसे अपने आप पर और अपने किए पर पश्चात्ताप न हो कि हमने सबल और सफल होने के लिए ऐसा कुछ न था जो हमने नहीं किया और विश्वास कीजिए वह क्षण रुपान्तरण का क्षण होता है,
When there is deep darkness in the sky,there is bright and golden dawn behind it.
Believe in urself and have trust in thy agnostic power, there will be a miracle and that will be ur victory.
--------
संवाद और हम : शक्ति. आलेख : ७८
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
संवादहीनता एक शून्यता : आप सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अपने प्रियजनों और जरूरत के लोगों से वांछित संवाद करते ही रहते हैं। संवाद हमें एक दूसरे से जोड़े रहता है,आप अपने मन की कहते और दूसरे के मन की सुनते रहते हैं। इस पारस्परिक संवाद में सिर्फ जरुरयात बातें ही नहीं होती, जज्बातों की बातें भी होती है और जिस दिन आप एक संवाद न करें कितनी बेचैनी सी होती है।
संवाद, सिर्फ निजी और पारिवारिक जीवन में ही नहीं सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में भी बड़ा महत्व रखता है। संवादहीनता एक शून्य पैदा करती है जहां भय,संशय और घबराहट की भावनाएं स्वत: स्फूर्त पैदा होने लगती है।
समझे सुने कहें : और इसलिए हम सबको संवाद करते रहना चाहिए परन्तु जब कोई आपकी बातों को अनमने ढंग से या औपचारिक होकर सुने तो उसकी अनुभूति हो जाती है और उससे उपजे विषाद दुःख देते हैं इसलिए जब भी किसी से संवाद कीजिए तो उस विषय पर खुल कर बातें कीजिए,अपनी कहिए और उनकी सुनिए,इससे मानसिक अवसाद उत्पन्न नहीं होते और मन को शान्ति भी मिलती है।
त्रासदी तो इस बात की है कि आज कोई न तो खुलकर कहना चाहता है और न सुनना चाहता है। मानव धीरे धीरे अपने आप में सिमटता जा रहा है और जिसकी परिणति हिंसा, अपराध, सम्बन्धों में बिखराव और यहां तक कि आत्महत्याएं भी इसी संवादहीनता की उपज है।
U make a quarrelsome talk with ur owns, but don't be quiet and silent,it creates a vacuum among the relationships and latter on a breach among relationships takes place,which is very painful.
कोई भूल भी हो तो स्वीकारे : यह तो आपके अपनों से रिश्तों को बनाए रखने का प्रथम और अंतिम सूत्र है। यही नहीं, कोई भूल भी हो जाए तो खुले मन और हृदय से माफी भी मांगने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, इससे सम्बन्धों में दरार नहीं पड़ते और मधुरता बढ़ जाती है।
अब दूसरा पक्ष भी बड़ा रोचक है जो स्वयं से संवाद करने का है और जिसने स्वयं से संवाद करने का हुनर सीख लिया,उसके निज की पीड़ाएं तिरोहित हो जाती है। स्वयं से संवाद आपके व्यक्तित्व को एक बड़े
वर्णपट पर लाने का काम करता है।
इस सन्दर्भ में वैश्विक स्तर के भारतीय चिन्तक और दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि, निराशा के क्षणों में आत्मसंवाद बल देता है,जब आप किसी को कुछ कह नहीं पाते तो आत्मसंवाद ही एकमात्र साधन है जो आपको अवसाद और आत्मिक पीड़ाओं से उबारने का काम करता है, इसलिए स्वयं से भी बातें करते
रहिए।
यह दार्शनिक चिन्तन है पर उससे बड़ा जीवन व्यवहार है जिसे सबको समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। अगर कोई साथ न हो तो स्वयं के साथ से बेहतर कोई सान्निध्य नहीं होता है। आत्म संवाद व्यक्ति के भीतर आत्मविकास, आत्मचिन्तन, आत्मगौरव, आत्मोन्नति, आत्मोद्धार आदि के मार्ग प्रशस्त करता है। स्वयं की पहचान स्वयं से करवाता है। कहा भी गया है कि, When someone talks to oneself,he talks to his innermost Conscience and reach to the Godliness.
इसलिए संवाद तो सबसे करते ही रहिए पर कोई न मिले तो स्वयं से संवाद कीजिए जो आपको स्वयं से और संसार से आपका साक्षात्कार करवाएगा।
--------
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां शक्ति. आलेख : ७७
--------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
आपकी जिजीविषा और आत्मविश्वास : आज छोटी सी बात पर ही हम अपनी बात कहकर संदेशित करना चाहते हैं। जीवन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का एक सुन्दर खेल है,बस खेलते है,खेलते रहिए और खेल देखते रहिए। राहें हर जगह समतल थोड़े ही होती हैं, कहीं चढ़ाव कहीं उतार, कहीं कच्ची कहीं पक्की,कहीं उजाड़ कहीं हरी-भरी, बस आपको सबको धीरे धीरे चलते रहना है।
प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने का साहस रखना,जूझते रहने का माद्दा रखना ही जिन्दगी की बेहतरीन परिभाषाओं में से एक है। एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहता है, लहरों के मजे ले रहे हो, थोड़ा झंझावाती लहरों को भी जीने का साहस रखो, न तो समुद्र में न उतरो।
वाजिब बात है,पर मानव मन या तो बड़ा साहसी होता है या बड़ा चंचल और डरपोक। जरा सा साहस खोया कि सारा खेल खत्म और यहीं से जीवन मरण का रोमांचक खेल शुरु होता है,आप खेल खेलेंगे कि खेल छोड़कर भाग जाएंगे,यह आपकी जिजीविषा और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है।
विक्रम बत्रा, एक इतिहास करगिल द्रास : नियती या तकदीर या प्रारब्ध को किसने देखा जाना है, हो सकता है लक्ष्य की ओर आपके साहसिक कदम बढ़ रहे हों और अगले कदम पर जीत हो,तो बस सांस की आखरी सांस के पहले तक चलते रहें,जीत गए तो इतिहास रच जाएंगे, जीवन आपका होगा और हार गए तो मृत्यु तो सबको एक न एक दिन आनी ही है। करगिल द्रास के युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा को छ: सात गोलियां लग चुकी थी और टाईगर हिल प्वाइंट बस कुछ डग रह गया था,बस गोलियां चलती रही, ग्रेनेड से पाकिस्तानी बंकर को उड़ाया और तिरंगा लहराते हुए शहीद हो गए विक्रम बत्रा, एक इतिहास रचा गया, मरणोपरांत परम वीर चक्र से नवाजे गए और माता-पिता ने कहा, इसी दिन के लिए हमने पैदा किया और पोस पाल कर बड़ा किया था।
एक सच्चे फ़ौजी का यही परम कर्तव्य होता है जिसका निर्वहन कैप्टन बत्रा ने किया था। उनकी टुकड़ी के एक जवान ने बताया कि वह चाहते तो बच सकते थे पर टाईगर हिल हाथों से निकल जाता पर हमारे कैप्टन ने जान तो दी पर देश की आन बान शान जाने नही दी और इसी जूझारुपन का एक नाम जिन्दगी है, सांसों की आखरी सांस तक अपनी समस्याओं से लड़ते रहो और लक्ष्यों की प्राप्ति तक न रुको,विजय सुनिश्चित है।
----------
प्रेम : जहां श्रेष्ठता या अहंकार का भाव नहीं हो : शक्ति. आलेख : ७६
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय.
प्रेम बहता हुआ जल प्रवाह अर्थात् नदी या जलप्रपात है जो किसी कारण बाधित हो गया तो स्थिर जलाशय में रुपान्तरित हो जाता है। इसलिए प्रेम में सातत्य का होना एक जरुरत है। हम सब जीवन में एक दूसरे से जरूरत, जज्बात और पारस्परिक समझ के आधार पर प्रेम करते रहते हैं। और उन तीनों का सातत्य उस प्रेम को जीवित रखने का काम करता है जिसके बीच हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि सम्मान भी प्रेम से ही जुड़ा रहता है।
प्रेम के लिए सबकुछ स्वीकार्य है पर श्रेष्ठता और अहंकार का बोध प्रेम रुपी वृक्ष का दीमक है जो बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ता पर भीतर ही भीतर वह खोखला करता जाता है और एक दिन वृक्ष की तरह नष्ट हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने तो कह ही दिया है.
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय
राजा परजा जे रुचे सीस दिए ले जाए,
अर्थात् प्रेम सबके लिए सुलभ है, वह हाट बाजार में बिकने वाला सामान नहीं जिसकी कीमत देकर क्रय विक्रय किया जाए। यह जो धनी निर्धन सबके लिए सुलभ है परन्तु एक शर्त है कि सहज भाव से एक दूसरे के प्रति समर्पण करना होगा, जहां श्रेष्ठता या अहंकार का भाव नहीं होगा, वही कबीर जी ने कहा है कि प्रेम के लिए सीस अर्थात् अहंकार देना होगा, स्वयं को समर्पित कर देना होगा, द्वैत को अद्वैत में रुपान्तरित करना होगा और तभी प्रेम अपने आकार को ग्रहण कर सकेगा अन्यथा वह प्रेम नहीं होगा बल्कि मोह, चाहत, जरुरत और आकर्षण होकर रह जाएगा।
प्रेम के प्रवाह में सम्पूर्ण प्रकृति बहती नजर आती है,आप सुबह-शाम इसका अवलोकन कर सकते हैं,सब प्रेम के आश्रय में जाने के लिए व्याकुल रहते हैं और व्याकुलता ही प्रेम का शाश्वत गुण है। पीड़ा,विरहानुभूति,
वेदना, प्रतीक्षा आदि प्रेम के गुण हैं और जो इनकी अनुभूति करते हैं,वही प्रेम के रहस्य को समझ सकते हैं।
सती के लिए शिव का विलाप, जानकी के विरह में राम का विलाप, कृष्ण के लिए राधा,मीरा और गोपियों का विलाप, हीर के लिए रांझा का और लैला के लिए मजनूं का विलाप,कुछ ऐसे ही अलौकिक और लौकिक उदाहरण हैं जिसे समझने के लिए गहराईयों में डूबना पड़ता है जैसे सागर की अतल वितल गहराईयों में डूबे बगैर रत्न नहीं मिलते, वैसे ही प्रेम रुपी रत्न की प्राप्ति के लिए भावों की गहराईयों में डूबना पड़ता है,बाकी सब माया मोह है।
--------
आस्था, श्रद्धा, विश्वास,भक्ति और प्रेम : शक्ति. आलेख : ७५
--------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
प्रेम स्वत: स्फूर्त होता है : ये ऐसे विषय और ऐसी अनुभूतियां हैं जिसके प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती,ये स्वत: स्फूर्त प्रदर्शित होते रहते हैं जैसे सूर्य को स्वयं प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं सिद्ध है।
यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर किसी को प्रेम करते हैं तो दिखना चाहिए,क्या हनुमान ने कभी घोषणा की कि वह श्री राम से प्रेम करते हैं, क्या मीरा,राधा, गोपियों और उद्धव चैतन्य महाप्रभु ने कभी कहा कि वे श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ? क्या कभी कोई कभी अपने बच्चों से कभी कहती हैं कि मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करती हूॅं ?
अपनों के लिए भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति ही प्रेम है : है ना ? नहीं न ! पर सांसारिक जीवन प्रश्न चिह्न खड़ा करता रहता है कि प्रेम दिखना चाहिए तो हमने कहा ही कि इसका प्रदर्शन स्वत: स्फूर्त होता रहता है और यह भावों की गहराईयों को भी बताते रहता है। अब यहां एक द्वन्द्व पैदा होता है कि कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम का स्वरूप क्या है कि प्रेम मूलतः प्रेम ही है पर सौर रश्मियों की तरह उसके रंग अलग-अलग होते हैं पर वो रहता प्रेम ही है।
पर संसार में प्रेम की अभिव्यक्ति लोग देखना चाहते हैं जो भौतिक रुपों में की जाती है जो संसाधनों और समर्पण के एक सम्मिलित रुप में समय समय पर प्रदर्शित होते रहते हैं।
भावनाओं की अभिव्यक्ति कभी छुपती नहीं,वैसे ही प्रेम कभी छुपता नहीं तो फिर प्रदर्शन की क्या जरूरत है, कविवर रहीम जी कह ही गए हैं,
खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मधुपान
छिपाए से भी ना छिपे कह गए रहीम सुजान
तो चीजें छिप नहीं सकती उनके प्रदर्शन की फिर क्या जरूरत है पर तथ्य आस्था श्रद्धा विश्वास और भक्ति में बड़ा द्वन्द्वात्मक सा प्रतीत होता है,जो जितने भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए कर्मकाण्ड के प्रदर्शन में लगे रहते हैं उनके इष्ट उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते हैं पर ऐसा भी पूर्ण सत्य नहीं है। परन्तु भक्ति आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ हो तो स्वीकार्य है अन्यथा याचना सुरक्षा और प्रदर्शन ही है।इसे एक बड़े रोचक प्रसंग से बताने की कोशिश करता हूॅं।
एक पूजारी और एक मौलवी :किसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनमें एक पूजारी और एक मौलवी थे जो दिन रात अपने अपने पांथिक कर्मकांड का निष्पादन किया करते थे। मौलवी साहब हाजी भी थे, पांचों वक्त के नमाज़ी और नियमित रोजा भी रखते थे। मस्जिद में अपनी तकरीर भी किया करते थे।
इधर पूजारी जी भी त्रिसंध्या करते,हर व्रत त्योहार में उपवास करते, निश्चित समयों पर मंदिर में घंटा और शंख भी बजाया करते। यही नहीं अपने मित्र की तरह चारों धामों और सारे तीर्थों की परिक्रमा भी कर चुके थे। संयोगवश उन दोनों की मौत एक ही दिन और एक ही समय हो गया। दोनों की ये समझ थी कि हम तो बड़े पूण्यात्मा रहे हैं, हमें तो स्वर्ग या जन्नत ही मिलेगा।
दोनों एक साथ वहां पहुंचे तो स्वर्ग और नर्क के दरवाजे अगल-बगल ही थे। दोनों दरवाजों पर देवदूत या फ़रिश्ते खड़े थे। वे बगैर कुछ कहे सुने सीधे स्वर्ग में घुसने लगे तो उनको रोक लिया गया। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि हमदोनों तो जीवन भर अपने अपने इष्ट की पूजा उपासना इबादत की है, हमनें हज किया है,सारे धामों और तीर्थ स्थलों की यात्राए भी की है, तो हम तो सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे, जन्नत ही अब हमारा आश्रय है।
तब दोनों को बताया गया कि आप दोनों ने सिर्फ आडंबर और पाखंड किया है। मौलवी साहब रोज़े में भी दिनभर बढ़िया बढ़िया खाने पर नजर रखते थे, इफ्तार पर सारा जेहन रहता था और आप भी उपवास में ऐसा ही किया करते थे कि कब शाम हो और मेवा मिष्ठान खाया जाए जबकि उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं अपने इष्ट के सान्निध्य में रहकर ध्यान करना है।
आप शंख और घंटे पब्लिक को आकर्षित करने और दक्षिणा लेने पर ध्यान रखते थे। तीर्थाटन के नाम पर सीधे सरल लोगों से पैसा ठगकर आपने अपना घर बनवा लिया और बाकी कर्म आपने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया।
आस्था,श्रद्धा, विश्वास और भक्ति : आपके पूजा पाठ आपकी आस्था,श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से कोसों दूर थे और यही काम आपके दोस्त मौलवी साहब ने किया कि चंदा उठाकर हज कर आए और हाजी होने के नाम पर झगड़ों का ग़लत फैसला करके कमाई का जरिया बना लिया।
नमाज़ और रोज़ा इनका फरेब था,उनके आड़ में ये सारे गलत काम करते थे, इसलिए आप दोनों को माफी नहीं मिलेगी। आप दोनों नर्क या दोजख में जाकर प्रायश्चित और पश्चाताप करें और अपने अपने इष्ट की सच्ची आराधना करें फिर आप दोनों पर विचार किया जाएगा और यह कहकर उन दोनों को नर्क में धकेल दिया गया।
इस कथा का यह अंत नहीं है और यह संदेश देना भी नहीं है कि आप अपने मत,पंथ, विश्वास आदि में मान्य
परम्परागत पूजा पाठ न करें,जरुर करें पर स्वयं को, लोगों को और अपने अपने भगवान को परमात्मा को धोखा न दें।
साक्षी आप स्वयं : सबसे बड़ी गवाही या साक्षी आप स्वयं होते हैं जिसे आत्मसाक्षी कहा जाता है। आत्मसाक्षी ही परमात्मा की साक्षी है। परमात्मा स्थूल रुप में नहीं देखते पर आप अपने हर कर्म को स्वयं साक्षी बनकर देखते और करते हैं, परमात्मा सूक्ष्म साक्षी भाव में रहते हैं इसलिए आस्था, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति आपके निज की चेतना और बोध है।मन, चित्त,हृदय और आत्मा की शुद्धता और अपने प्रति और सबके प्रति विहीत कर्मों अर्थात् कर्तव्यों का निर्वहन ही श्रेष्ठ पूजा है,यही सच्ची आराधना, उपासना और इबादत है। व्रत त्योहार आदि मन को उनके प्रति निष्ठा और समर्पण का एक माध्यम है तो उनमें दिखावा, प्रदर्शन और आडम्बर नहीं होना चाहिए। दूसरों का धन आदि हड़पकर दान और तीर्थाटन करने से क्या लाभ होगा, दूसरों का दिल दुखाकर उपवास करने के क्या लाभ होंगे कि जो आपके व्यवहार आचरण आदि से पीड़ित होंगे उनके भीतर से आह और हाय निकलेगी जो आपके सुख चैन को छीन लेगी। यह सच्चा हज और तीर्थाटन और चारों धाम की यात्रा नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा भी है,
तुलसी आह गरीब के कबहुं न निष्फल जाए
मुआ खाल के चाम से लौह भस्म हो जाए।
इसलिए अगर सबकी दुआएं न ले सकें तो बद्दुआओं से भी बचिए। साफ रहिए और वही दिखने की कोशिश कीजिए जो आप हैं कि एक दिन तो सबकी किताब पढ़ी ही जानी है और जब आपकी किताब पढ़ी जाएगी तो उस मूल्यांकन का कोई काट नहीं होगा।
--------
समय पूर्ण और अस्तित्व खत्म : शक्ति. आलेख : ७४
------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
सम्बन्धों का यथार्थ चित्रण : आज फिर एक जेन या झेन यात्रा पर आप सबको ले चल रहा हूॅं जो जीवन में समस्त सम्बन्धों का यथार्थ चित्रण करता है।वह चाहे वस्तु हो,भवन हो, उपयोग की सामग्रियां, सौन्दर्य हो या स्वास्थ्य या फिर मनुष्य ही क्यों न हो,सबका साथ एक निश्चित समय सीमा से बंधा हुआ है,समय सीमा समाप्त और सारे अस्तित्व समाप्त पर इसे समझ पाना उतना ही सरल या उतना ही दुष्कर है। हम अपने जीवन में जुड़ी हुयी चीजों या सम्बन्धों को स्थाई समझ लेते हैं और सारा झमेला यहीं से शुरू हो जाता है। स्थाई समझना ही मोह या आसक्ति के भाव का सृजन करता है और यहीं से दुःख और अवसाद हमारे अस्तित्व पर हावी होने लगता है और जीवन दुश्चिंताओं से आवृत्त हो जाता है।
सुख चैन छीन जाते हैं और हम परिवर्तन के शाश्वत सिद्धान्त को विस्मृत कर जाते हैं। आप आज बलवान और सामर्थ्यवान हैं, प्रभुत्वशाली और प्रभावशाली हैं, धनवान और समृद्ध हैं और आपने यह समझ लिया कि ये सब हमारे जीवन में शाश्वत हैं और यह आत्ममुग्धता आपको समय बदलने के साथ अवसादग्रस्त कर देता है।
जीवन में उपलब्ध सुख चैन भी निरर्थक से हो जाते हैं और उसकी एक ही वजह है, स्थायित्व के मतिभ्रम का शिकार होना और कुछ नहीं। बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था,कुछ भी स्थाई नहीं है,सब कालखंडों में बदलते रहते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में समय से पहले भी रुपान्तरित हो जाते हैं। न धन रहता है,न प्रभूता न प्रभाव,न बल न सामर्थ्य,सबके सब एक निश्चित काल के बाद ऊर्जा की तरह रुपान्तरित होते रहते हैं।
क्या कोई यात्रा या ठहराव स्थाई हो सकता है, हम सब यात्राएं करते रहते हैं और तदनुरूप गंतव्य भी बदलते रहते हैं और एक दिन सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। इसी समापन से सम्बन्धित एक बड़ी रोचक कथा जापान के एक जेन साधक के आश्रम की है। एक जेन गुरु के आश्रम में एक किशोर साधक भी रहता था जो आश्रम की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्था की देखभाल करता था और उपदेश और प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित भी हो जाता था। एक दिन साफ सफाई के क्रम में उसके हाथों की ठोकर से तथागत सिद्धार्थ की छोटी सी प्रतिमा गिरकर टूट गयी। वह तो बुरी तरह डर गया और किंकर्तव्यविमूढ़ वहीं खड़ा रह गया। गुरु उस प्रतिमा की बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा करते और उसके सम्मुख दीपक जलाकर ध्यान करते थे। वह किशोर साधक इस सत्य को जानता था।तभी उसे गुरु की पदचाप सुनाई पड़ी और वह स्थिर होकर उनका इन्तजार करने लगा।
गुरु के सामने आते ही उसने पुछा कि, किसी की मृत्यु कैसे हो जाती है या कोई वस्तु कैसे नष्ट हो जाती है? गुरु ने छुटते मुंह कहा, उसका समय पुरा हो गया। यह सुनते ही उसने दोनों हाथ आगे कर दिए जिनमें खंडित मूर्ति थी।
गुरु ने कोई क्रोध न किया और ना दंड दिया,बस कहा कि, हे किशोर,इस सूत्र वाक्य को याद रखना कि समय पुरा हो गया और तुम्हारी शिक्षा पुरी हो गयी। तुम जीवन के एक नये यात्रा पर जा सकते हो। उस किशोर ने इस सूत्र वाक्य को समझकर आत्मसात कर लिया और साधना के सफर पर निकल गया कि जीवन के सत्य को उसने समझ लिया था,सार को समझ लिया था। जीवन में किसी का साथ, सम्बन्ध, अन्तरंगता,घृणा और प्रेम,मिलन और विरह, दुःख और सुख, स्वस्थ्य और सौन्दर्य आदि कुछ भी शाश्वत नहीं हैं,सब नाशवान और परिवर्तनशील हैं।
प्रिय का मिलन और अप्रिय का मिलन सब समय के पुरा होने पर खत्म हो जाने हैं। यही जीवन यात्रा का सच है कि यहां सब कुछ अस्थाई है,उसे स्थाई समझना ही आत्मप्रवंचित होना है। किसी वस्तु, सामग्री,भवन, व्यक्ति आदि का खत्म होना एक बड़े भ्रम या मृगतृष्णा से मुक्त होना है। यही आत्मप्रवंचना मानव जीवन में अहंकार को जन्म देती है,उसे भ्रमित रखती है और मनुष्य एकाएक इस सच का सामना करते ही किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है।
अस्तित्व का सिद्धान्त : अस्तित्व का सिद्धान्त स्वयं की सत्ता को इस रुप में समझना है कि अतीत में बड़ी बड़ी विभूतियां और बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए,उनके अवशेष के रुप में उनके कृतित्व ही रह गए और इसलिए रह गए कि वे भौतिक नहीं सूक्ष्म और कारणिक रहे हैं,उनका भौतिक अस्तित्व नहीं रहा है, भौतिक सदैव नाशवान है,पर कर्म और कर्मजनित उपलब्धियां शाश्वत हैं पर एक सृष्टि के विनाश के बाद वे भी नष्ट हो जाती हैं अर्थात समय पुरा होने पर सबकुछ नष्ट हो जाना है।
-------
जुड़ाव और हम : शक्ति. आलेख : ७३
-------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
अलग - अलग प्रकृति, प्रवृत्ति,जरूरत और परिस्थितियां : सांसारिक जीवन में यह बड़ा गंभीर सवाल है कि हम कैसे लोगों से अपना जुड़ाव बनाएं और उस सम्बन्ध को बनाए रखें।यह चयन भी सबकी अलग - अलग प्रकृति, प्रवृत्ति,जरूरत और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति इन्हीं आधारों पर जुड़ाव बनाना चाहता है।
निर्बल ताकतवर से, निर्धन धनी से, धनवान सामर्थ्यवान से, जिज्ञासु ज्ञानी से, सद्वृत्ति वाले आध्यात्मिक से, लोकप्रिय होने वाले प्रभावशाली से, कलाकार साहित्यकार समवृत्ति वालों से आदि आदि और शायद यही संसार का सच भी है। परन्तु कुछ लोग वैसे लोगों से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं जो उनको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और वैसी संभावनाएं भी रखते हैं।
राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की बुनियाद भी यही है। एक कमजोर और जरूरतमंद देश अपने सम्बन्ध वैसे ही देशों से बनाना पसन्द करता है जो उसे आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने की संभावनाएं रखता है और उस दिशा में कार्य भी करता है।
कभी - कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक व्यक्ति को एक अच्छे और सच्चे सलाह के लिए एक सलाहकार की भी जरूरत होती है या ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो एक दूसरे की जरूरत और भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को राहत दे और सांसत से दूर करे और यह भी एक बड़ी जरूरत है जिस पर पारस्परिक सम्बन्ध बनते हैं। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और कुटनीतिक सम्बन्ध आज नहीं आदिकाल से इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर बनते बिगड़ते रहे हैं।
भगवान राम और भगवान कृष्ण : प्राचीन काल में भगवान राम और भगवान कृष्ण के कुटनीतिक सम्बन्धों का विश्लेषण इन आधारों पर किया जा सकता है। उन्होंने अपने मैत्री सम्बन्ध हनुमान, सुग्रीव, वानर और भालूओं के साथ बनाया रावण के पतन को सुनिश्चित करने के लिए विभिषण से मैत्री स्थापित की।
भगवान कृष्ण ने भी सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का चयन किया। जरासंध ने मय नामक दानव और काल यवन से मित्रता की ताकि श्री कृष्ण को पराजित किया जा सके। वैदिक काल से पूर्व दसराज्ञ युद्ध में भी ऐसी मैत्री के उदाहरण मिलते हैं।
छठी सदी ईसापूर्व में भी सोलह महाजनपदों के बीच ऐसे मैत्री सम्बन्धों की चर्चा इतिहास में मिलती है। सिकन्दर पोरस से लेकर तराईन के युद्धों, पानीपत के युद्धों, प्लासी युद्ध आदि में भी ऐसे कुटनीतिक और जरूरत आधारित सम्बन्धों की गाथाएं इतिहास में प्रामाणिक रुप में उपलब्ध है।
विश्व की दो बड़े महायुद्धों में भी विश्व के दो भागों में विभाजन इसका जीवन्त उदाहरण है। आज भी वैश्विक स्तर पर ऐसे बनते बिगड़ते सम्बन्धों को देखा जा सकता है। परन्तु जहां तक निजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सम्बन्धों के बनाने और निर्वाह करने का सवाल है,यह भी उपर वर्णित बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी हुई है।
हम आज भी भौतिक और सूक्ष्म जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप ही सम्बन्ध बनाने और जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। इसमें एक विषय महत्वपूर्ण है कि कालखंडों में मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति जरूरत और परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती हैं परन्तु अतीत के अच्छे सम्बन्ध वर्तमान में भी कारगर साबित होते हैं। आज आप किसी के जरूरत और जज्बात के अनुरूप नहीं हैं,कल हो सकते हैं,आज किन्हीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं,कल हो सकते हैं, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
यथासंभव सम्मान : सबकी जरूरतों और जज्बातों का यथासंभव सम्मान करना चाहिए और यही परम धर्म ( कर्तव्य ) है। सम्बन्ध या रिश्ते अगर जरूरत हैं तो जज्बात भी हैं, रिश्तों की मर्यादा और सम्मान भी है। भगवान राम सामर्थ्यवान तो थे पर उन्होंने सबका सम्मान किया। आप धनवान हैं तो धन से, बलवान हैं तो बल से, ज्ञानवान हैं तो ज्ञान से, सामर्थ्यवान हैं तो सामर्थ्य से या परमात्मा ने जो सामर्थ्य आपको दिया है, उनसे रिश्तों का सम्मान करें कि जीवन में रिश्तों को बनाने और बनाए रखने का यही मूल मंत्र है।
----------
किसी के बारे कौन कह सकता है शक्ति. आलेख : ७२
--------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
जो जिसको जानता पहचानता समझता है, वही कुछ कह सकता है। मन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, हृदय, मस्तिष्क,आत्मा,अन्तरात्मा, अन्तःकरण, अन्तश्चेतना, प्रज्ञान, प्राण ,ईश्वर , ब्रह्म और परब्रह्म चैतन्य ऊर्जा के ही विभिन्न रूप होते हैं जो क्रियार्थक रूप में भिन्न होने के कारण अलग-अलग दिखाई पड़ते है पर मूल तो चेतना ही है।
इसलिए मन को मन से, हृदय को हृदय से और मस्तिष्क को मस्तिष्क से,आत्मा से आत्मा को और प्रज्ञान से ईश्वरीय चेतना को समझा जा सकता है। ईश्वरीय सत्ता कर्मकाण्ड से इतर की सत्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले सभी मत,पंथ, विश्वास, विचार, साम्प्रदायिक पंथों आदि के पुरोहितों पूजारियों को उनका साक्षात्कार होता रहता पर ऐसा नहीं होता है, सत्य यही है।
कहा जाता है,सत्य ही ईश्वर है,प्रेम ही ईश्वर है, करुणा और क्षमा ही ईश्वर है, सेवा और दया ही ईश्वर है तो जिन्होंने इन्हें जाना नहीं भला वे ईश्वरीय सत्ता को कैसे जान पाएंगे। पहले तो इन गुणधर्मों को अपनाकर आत्मसात करना होगा और तभी कोई प्रतिक्रिया और परिवर्तन संभव हो सकेगा।
शिव,राम और कृष्ण ने प्रेम, सेवा,क्षमा, करुणा और त्याग में उन्हें देखने को कहा,यहोबा और जीसस ने प्रेम, करुणा,सेवा और क्षमा में उनको खोजने को कहा, महावीर और बुद्ध ने अहिंसा,प्रेम,सत्य,करुणा,क्षमा, सेवा और त्याग को ही परम सत्य और सत्ता माना, कुरान मजीद ने अपने अपने दीनों ईमान से मोहब्बत करने को कहते हुए कहा,लकूम दीन कूम वलिय दीन कहा कि सबके अपने-अपने विश्वास हैं और सबको अपने अपने विश्वास पर कायम रहना ही ईश्वरीय सत्ता से प्रेम करना है तो इस सत्य और यथार्थ को जो जानेगा,समझेगा और आत्मसात करेगा, वही सत्य के सत् ( Abstract or Essence of The Truth) को जान पाएगा,शेष वही भ्रम, मृगतृष्णा और माया है जिसमें इस मृण्मय संसार के लोग आत्मप्रवंचित और आत्ममुग्ध होकर जी रहे हैं और मनुष्य जबतक आत्ममुग्धता का शिकार रहता है तब तक उसे सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है।
Knowing the self is the knowing if the World and God, गलत नहीं कहा गया है। खुदी का इल्म होना ही खुदा का इल्हाम होना है लेकिन जब किसी ने इसकी घोषणा की उसे झूठ और ग़लत मानकर पाखंडियों और आडम्बरवादियों के बहुमत ने उस सत्य को कुचल दिया पर सत्य सदैव आग के भीतर की राख है जो अनुकूलता पाकर भड़ककर धधकती आग बन जाती है। जीसस को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया पर सत्य फिर जी उठा। इसलिए किसी वस्तु, सिद्धान्त, दर्शन, चिन्तन और व्यक्ति पर कुछ कहने के पूर्व उसे जानना, समझना, पहचानना और उसके मोल और मूल्यों का आकलन करना होगा तभी कुछ टिप्पणी करना सम्यक् कथन होगा वरना इस संसार में अनर्गल प्रलाप करने वाले बहुतायत और बहुमत में हैं। इसलिए अपने ज्ञान और अपनी समझ का आकलन कर चलते रहिए,कहा भी गया है,
Bent upon ur own,never mind what the world says.
----------
सच,भ्रम और जीवन शक्ति. आलेख : ७१
-----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
सच को जानना या तो बड़ा सरल और सहज है पर इसके लिए हृदय का सरल होना जरूरी है अन्यथा मन तो विचलित करता है र मस्तिष्क विश्लेषण करने लगता है। ऐसे तो सच चारो तरफ फैला हुआ है,जो नजर में है और जो नजर में नहीं भी है,सच है। संसार में सच के अलावा और कुछ नहीं है,भ्रम और माया (illusion) जिसे कहा जाता है,उनसे निरासक्त होने के लिए कहा जाता है कि जो चीजें आपके जीवन में है,सब भौतिक पदार्थों का ही संग्रह है जिन्हें विभिन्न रुपों में आप उसका उपभोग करते हैं। एक पाश्चात्य दार्शनिक का कहना है कि, That all which is visible, r real in their existence but those which seem to be not existing as they r not visible, when they come close to the sense,they r in their existence.
संसार का यही सच है। जिसे हम नहीं देखते, नहीं जानते,उसकी अनुभूति भी नहीं करते,उसे झूठ या अस्तित्वहीन मान लेते हैं।वैसे तो इस ब्रह्माण्ड में अनेकानेक ऐसे पिण्ड या पदार्थ हैं जिन्हें सामान्य आदमी क्या जानेगा, आधुनिक भौतिक विज्ञान तक नहीं जान पाया है और खगोलीय भौतिकी तथा क्वांटम भौतिकी में निरन्तर शोध जारी है लेकिन ब्रह्माण्ड अज्ञेय है,इसे कभी नहीं जाना जा सकता है, अभी-अभी पता चला है कि इतालवी भौतिक विज्ञानियों ने प्रकाश को ठोस रुप में जमा कर दिखा दिया है जबकि प्रकाश एक ऊर्जा है पर पानी की तरह नहीं है,इस तरह चीजें रोज बदल रही है। जो कल सत्य था,आज असत्य साबित हो रहा है और जो असत्य था वो सत्य साबित हो रहा है। परन्तु एक विषय पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि मनुष्य भौतिक और सूक्ष्म पिण्ड दोनों है। अगर यह सिर्फ भौतिक पदार्थों का संलयन होता तो मन, बुद्धि,हृदय,विवेक, भाव, विचार, चेतना आदि को उधेड़ कर रख दिया गया होता परन्तु शरीर क्रिया विज्ञान से इतर मनुष्य का सूक्ष्म अस्तित्व भी होता है जो कल भी अनबूझ था और कल भी अनबूझ रहेगा और जीवन के इसी सच को जानने के प्रयास युगों युगों से होते रहे हैं और होते रहेंगे,जैसे समुद्र के तह में गए बगैर उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता है वैसे ही जीवन के रहस्य हैं जिसके तह तक गए बगैर जीवन कभी समझ में नहीं आ सकता है और जीवन को जिन मनीषियों ने जैसे देखा और समझा, उनकी नजरों में जीवन वैसा ही नजर आया। तथागत सिद्धार्थ ने तो कह दिया,
जरा दुक्खं मरन दुक्खं अपिय मिलन दुक्खं
पिय बिछोह दुक्खं,सब्बं दुक्खं।
जीवन में सब दुःख ही दुःख है,जन्म दुःख है,मरण दुःख है, अप्रिय का मिलन और प्रिय का बिलगाव दुःख है, जीवन दुःखों का पर्याय है। आदिगुरु शंकराचार्य ने सबको माया और भ्रम ही कह दिया कि संसार और कुछ नहीं सब माया,भ्रम और मृगतृष्णा है, फिर जीवन क्या है, क्यों इतनी भाग-दौड़ और आपा-धापी है। संसार में लोग परेशान हैं कि सब उनके आसक्ति के शिकार हैं और यही आसक्ति उन्हें सच को जानने नहीं देती है और जीवन के सच को जानने के लिए सारे भेदों को समझना होगा।जैसा हमने पूर्व में अंकित किया है कि कण कण सत्य से आच्छादित है,असत्य कुछ भी नहीं है।हमारी दृष्टि और हमारे दृष्टिकोण पर सबकुछ निर्भर करता है,जिसे जिस रूप में देखेंगे उसे वैसा ही पाएंगे। जीवन को दुखमय समझेंगे तो जीवन वैसा ही नजर आएगा और इसके विपरीत देखने पर सुखमय नजर आएगा। परन्तु तथागत सिद्धार्थ के संसार चक्र के अनुरूप सबकुछ बदलता रहता है परन्तु जो शाश्वत सनातन सत्य है कभी नहीं बदलता है, इसलिए हर भौतिक और सूक्ष्म में इस फर्क को सदैव समझते हुए सच को जानने का प्रयास करते रहना है।
एथेंस के सत्यार्थी देवकुलीश की आंखों ने सत्य को देखना चाहा तो सत्य के चमकते प्रकाश से उसकी आंखें अंधी हो गयी,इस प्रसंग का अभिप्राय यह है कि सच को नंगा करके नहीं देखा,सुना,बोला और लिखा जा सकता है,उसे आवृत करना पड़ता है,जिसे कबीर दृष्टि से देखने की जरूरत होती है। संभवतः शंकर ने इसीलिए सबको माया कहा होगा और तथागत सिद्धार्थ ने दुःख कहा होगा। परन्तु जीवन ऐसा नहीं है कि शायद महावीर, बुद्ध, शंकर, आदि मनीषियों के विचार आज भी द्वन्द्वात्मक भाव पैदा करते हैं और एक दूसरे को खंडित करते रहते हैं।
ऐसे ही द्वन्द्वात्मक भाव स्पिनोजा,हीगेल, बर्क, नित्शे,लिबनित्ज,स्पेन्शर, लिविंगस्टोन आदि के विचारों में दिखाई पड़ते हैं।यह बताता है कि सबने अपने कालखंडों में व्याप्त सच को देखा, जीवन को जैसा भोगा,कह दिया कि जीवन और कुछ नहीं बस भोगा हुआ यथार्थ ही तो है। कबीर जी और तुलसीदास ने नारी को जिस रुप में देखा और जिया कह दिया पर आप बताइए कि क्या यह सच सबका सच है,कतई नहीं कि जो जैसी अनुभूति करते हैं,लिख बोल देते हैं।मछली बोलेगी कि पानी जीवन है और पक्षी बोलेगा कि आकाश जीवन है,वृक्ष जीवन है और यही उनके लिए सच है। मनुष्य जबतक स्वस्थ समृद्ध और सामर्थ्यवान होता है, जीवन को अपने तरीके से जीता और मस्त रहता है, जीवन उसके लिए स्वर्ग सादृश्य होता है और इसकी विपरीत अवस्थाएं नरक होती है।
इसलिए जीवन का सच भोगा हुआ यथार्थ होने के साथ साथ एक अज्ञेय सत्ता भी है,नित नवीन, नित
परिवर्तनशील और नित अद्भुत अनुभूति, बस जो समक्ष है उसके यथार्थ को समझने की कोशिश कीजिए और जीवन के खत्म होने तक दुःख सुख की अनुभूति करते हुए रहस्यों को समझने की कोशिश कीजिए और जीवन के भौतिक और सूक्ष्म पक्षों को आत्मसात कीजिए कि इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।जो परिवर्तन होते आप देख रहे हैं,न आप उसके हेतु हैं न कारक आप महज दर्शक भर हैं,आप अगर यह समझ रहे हैं कि पांचाली महाभारत का कारण थी तो आप भ्रम में हैं,वह तात्कालिक कारण थी,कारण समूह तो पहले से मौजूद थे। लोगों ने,सबने कह दिया कि पांचाली अगर तंज न कसी होती तो महाभारत न होता, महाभारत होना था, इसलिए उसने तंज कसा, जीवन का एक सच यह भी है जिसे जानने के लिए गहरे डूबना होगा।
--------
भाषा और हम :शक्ति. आलेख : ७०
---------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
भाषा लेखनी और वाणी : भाषा वैचारिक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है जो लेखनी और वाणी से प्रत्यक्ष होती है। आदिकाल में मनुष्य की कोई भाषा नहीं थी, वह संकेतों से और मौखिक विशिष्ट ध्वनियां उत्पन्न करके संवाद देते लेते थे। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न प्रदेशों और प्रक्षेत्रों में मनुष्यों ने भाषाओं का विकास किया जो आदिकाल में चित्र लिपि, सांकेतिक चिह्नों आदि रुपों में विकसित होती है और आज वर्ण या अक्षर रुप में स्थापित हो गयी हर देश प्रदेश की अपनी वर्णमाला और शब्दों के संग्रह, शब्दकोष,व्याकरण, भाषा शैली आदि हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा चीन की भाषा जिसे मन्डारीन कहते हैं, चित्र लिपि की तरह है जिसमें शब्दों को याद किया जाता हैं,अन्य भाषाओं की तरह उनमें रुपान्तरित होने की व्यवस्था नहीं है।सैंधव सभ्यता की लिपि आज भी अपठनीय है और शोध का विषय है।
अब भाषा जो भी हो सबकी अपनी-अपनी महिमा हैं। हमारी भाषा हमारी योग्यता, भाषायी मर्यादा,अनुभव,बौद्धिकता और ज्ञान को ही नहीं बताती,हमारे पारिवारिक,शैक्षणिक सामाजिक और निज संस्कारों को भी आईना दिखाती है।
अपशब्दों के प्रयोग और तंज कसने की भी अपनी सीमाऔर मर्यादा होती है। यह हमारे * अहंकार, आचरण और व्यवहार को भी परिलक्षित करती है। हम और हमारे विरोध के स्वर * भाषायी मर्यादा के भीतर ज्यादा प्रभावी हो सकते है।
एक छोटा सा शब्द समूह * आपका ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता*, किसी के भीतर बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है परन्तु जिनके भीतर ऐसी कोई प्रतिक्रिया ही न हो, ऐसे भी बहुतायत है जो आत्ममुग्धता के शिकार होते हैं।भाषा सिर्फ भावों और विचारों संप्रेषणीयता का ही माध्यम नहीं है बल्कि हमारे व्यक्तित्व के * अन्तर्निहित गुण-संस्कार और अन्तः चरित्र का भी परिचायक है।
यह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लैटफार्म पर हमारी पहचान भी बनाता है। अगर स्वरचित रचनाएँ या संदेश न डालकर, यदि किन्हीं और के पोस्ट को भी हम repost करते है तो वह पोस्ट भी हमारे व्यक्तिगत भावों विचारों और संस्कारों को सबके सामने ला खड़ा करता है।अतएव जिनको भी जो कहना हो कहिए, पुरी आजादी है, व्यंग्य और तंज कसिए परन्तु खुद को नंगा न कीजिए। काल देखता ही नहीं वरन अवलोकन भी करता है और हमारा मोल और मूल्य भी आकलन करता है और जब काल तंज कसता है तो उस तंज का कोई जवाब नहीं होता है।
शब्द, अक्षर से बनते हैं और अक्षर,अक्षय अक्षुण्ण ऊर्जा हैं,अक्षर ब्रह्म है जिसका रूपान्तरण वैसै ही होता रहता है जैसे सौर रश्मियां रुपान्तरित होती रहती हैं,ऊर्जा का स्वरूप बहुआयामी होता है जो हर पल क्षण रुपान्तरित होती रहती है।आज आप सबल, ऊर्जावान हैं, काल आपके साथ है, कल उसका रूपान्तरण हो जाएगा और काल उसके पक्ष में हो जाएगा और आप मूकदर्शक बनकर रह जाएंगे। इसलिए * शब्दों को रचनात्मक साकारात्मक और सृजनात्मक बनाने की कोशिश सदैव करनी चाहिए ताकि काल , शब्द बनकर न हँसे और ना तंज कसे। शब्दों के भाव और असर तो देखें कितनी करिश्माई और प्रभावी
होती हैं।
सद्गुरु कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास : सद्गुरु कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास समकालीन कवि, भक्त और चिन्तक थे। संत कबीर की भाषा घुमक्कड़ी और उधेड़ कर रख देने वाली थी वहीं गोस्वामी जी की भाषा कोमल और मर्यादित थी। एक बार दोनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में दोनों को प्यास लगी। सामने एक कुएं पर एक वृद्धा पानी भर रही थी। पहले संत कबीर गए और उन्होंने कहा कि,
हे मेरे पिता की पत्नी, हमें पानी पिला दो,वृद्धा ने उनके सर पर बाल्टी दे मारी।
बेचारे कबीर जी आहत होकर गोस्वामी जी को सारा वृत्तांत सुनाए। फिर गोस्वामी जी वहां गए और कहा, हे माते,मुझे जोरों की प्यास लगी है, पानी पिला देती तो बड़ी कृपा होती। उस वृद्धा ने गांठ खोलकर गुड़ की डली दी,पानी पिलाया और उनके लोटे में पानी के साथ आशीर्वाद भी दिया। अब समझने की कोशिश कीजिए कि फर्क कहां पड़ा, कबीर जी ने वही कहा जो सच था परन्तु भाषा अमर्यादित और अशिष्ट थी और गोस्वामी जी की भाषा शिष्ट और मर्यादित थी। कहते हैं,
शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव
एक शब्द कर औषधि एक शब्द कर घाव।
ऐसे ही घाव करने वाले पांचाली के तंज ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था। कोयल और कौए दिखने में समान होते हैं पर उनकी बोली ही उनकी पहचान है। पशु पक्षियों की भी अपनी अभिव्यक्ति होती है,भाषा नहीं होती है पर वे मनुष्यों के प्रेम और घृणा को समझकर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। अगर आपके घर में पालतू जानवर या पक्षी हैं तो इसकी सहज अनुभूति आपको होती होगी। भाषा,शान्ति अशान्ति, प्रेम घृणा और युद्ध, अपनत्व और गैरपन आदि का सृजन करती है। पारस्परिक रिश्तों को बनाती बिगाड़ती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संतुलित और मर्यादित रखने का काम करती है। ए जी गार्डीनर कहता है, आपके तीन शब्द यथा,कृपया, धन्यवाद और क्षमा करें, वक्त को बदल सकते हैं, बना या बिगाड़ सकते हैं।
-------
सिद्धार्थ : सुजाता : सम्बोधि : तथागत सिद्धार्थ की प्रासंगिकता : शक्ति : आलेख : ६९
---------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
*
टाइम्स मीडिया. शक्ति * प्रस्तुति.
*
हरि के कल्कि अवतार : गौतम बुद्ध
अहिंसा परमो धर्मः
दुःख है, दुःख का कारण भी है, इसका निवारण भी है : मध्यम मार्ग : अष्टांगिक मार्ग.
सम्यक साथ : सम्यक दृष्टि : सम्यक कर्म
छठी शताब्दी ई पू का दौर भारत के लिए संक्रमण काल : आज सम्पूर्ण विश्व एक महामानव अर्हंत भगवान बुद्ध की जयन्ती बना रहा है जिन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। छठी शताब्दी ई पू का दौर भारत के लिए संक्रमण काल था जो एक महति परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा था।
यज्ञ और कर्मकाण्ड प्रधान समाज : तत्कालीन भारतीय समाज यज्ञ और कर्मकाण्ड प्रधान समाज था जहां ज्ञान और चेतना, मौलिक चिन्तन और विश्लेषण की जगह नहीं रह गयी थी। इस चेतना और ज्ञान को जगाने की दिशा में इनके पूर्व आजीवक सम्प्रदाय के अनेक मत और जैन मत के उदय हो चुके थे जिन्हें अपेक्षाकृत जन समर्थन और राजकीय संरक्षण कम मिलने के कारण बड़े वर्णपट पर नहीं जा सके पर और ये तत्कालीन भारत के कुछ क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गए। परन्तु बौद्ध दर्शन और चिन्तन ज्यादा व्यवहारिक होने के कारण भारत भूमि की सीमाओं के पार चला गया। है तो बड़ा लम्बा और गंभीर विषय कि बुद्ध आज भी प्रासंगिक हैं पर मैं महत्तम प्रयास करुंगा कि कम से कम समय और कम से कम शब्दों में अपनी बातों को ग्राह्य बना सकुँ।
धर्म-कर्म सुधार आन्दोलन : भगवान बुद्ध की महिमा कुछ ऐसी थी कि इन्हें एशिया का प्रकाश तक कहा गया आजीवक ( चार्वाक ) सम्प्रदाय, जैन मत और बौद्ध मत को तत्कालीन भारत में भारतीय सामाजिक आर्थिक, धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधारभूत संरचनाओं में एक मौलिक बदलाव के रुप में इनको देखा गया और इसलिए इतिहासकारों का एक वर्ग इसे धर्म-कर्म सुधार आन्दोलन भी बताया है।
It was not the emergence of any faith belief or dogma based on the concept of Dharma but a new way and methodologies of life which was the need and demand of the time.
इस सन्दर्भ में भगवान बुद्ध ने अपनी धम्मदेसना में स्वयं कहा है कि, मैं किसी नवीन धर्म या मत सम्प्रदाय की बात नहीं कर रहा हूॅं पर स्थापित जीवन मोल और मूल्यों में परिवर्तन की बात कर रहा हूॅं जिससे जीवन परिष्कृत मर्यादित और चैतन्य हो और मनुष्य जीवन के अर्थों को समझ सके।
तथागत सिद्धार्थ : सुजाता : सम्बोधि : तथागत सिद्धार्थ ने इसीलिए वैदिक और वेदान्त दर्शन का भी अध्ययन चिन्तन और मनन किया और इसके लिए वे अनेक सिद्ध विद्वानों के पास जाकर ज्ञान भी हासिल की। उनके पहले गुरु आलार कलाम थे। परन्तु इन्हें कहीं भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, प्यास नहीं बुझी और ये भटकते भटकते निरंजना नदी के किनारे आज का बोधगया पहुंच कर साधनारत हो गए पर वहां भी इन्हें वह न मिला जिसकी खोज थी।
जब ये खोज की अति पर पहुंच गए तो सुजाता के गीत सुनकर और उसके हाथों खीर खाकर इनकी चेतना का विस्फोट हुआ जिससे सम्बोधि की प्राप्ति हुयी और सिद्धार्थ एक निमिष में मानव से महामानव बन गए। 'बुद्ध ' को आमतौर पर लोग एक नाम समझते हैं पर ' बुद्ध ' तो एक संज्ञा नहीं ' विशेषण है। ' बुद्ध ' होना एक ' चैतन्य अवस्था ' है और इस अवस्था की प्राप्ति स्वयं के श्रेष्ठ कर्म और गुण जनित संस्कारों से की जा सकती है। गौतम सिद्धार्थ के पूर्व भी कई ' बुद्ध ' हुए हैं जो विभिन्न कालखंडो में विभिन्न प्रदेशों में अवतरित जन्म के अर्थ में हुए हैं।
जीवन के चार आर्य सत्य : मध्यम मार्ग : ढाई हजार साल से भी ज्यादा समय ५४० ई पू पूर्व जिन बातों को स्थापित , सत्यापित और प्रमाणित किया गया था उनमें से बहुत सी बातें आज भी प्रासंगिक और सन्दर्भित हैं। उनके प्रथम धम्मदेसना को धम्मचक्कपवत्तन अर्थात् धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जिसमें जीवन के चार आर्य सत्य अर्थात् चत्तारि अरिय सच्चानि की व्याख्या की गयी कि
जीवन में दुःख है,
दुःख के कारण हैं,
उनके निदान हैं
और निदान के मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग
और उनके निदान का मार्ग मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग है जिसे पाली भाषा में अट्ठंगिकोमग्गो कहा गया है। बुद्ध के दर्शन ऐसे मूल रुप से वेदांत या औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन से प्रेरित और प्रभावित हैं पर भगवान बुद्ध ने उसे अपने तरीके से आमजन के सामने लोकभाषा में प्रस्तुत किया जिसे आमजन के साथ साथ तत्कालीन बड़े बड़े सम्राटों ने भी स्वीकार किया, मान्यता प्रदान किया और संरक्षण भी दिया जिससे बौद्ध मत काफी लोकप्रिय होकर भारतीय सीमाओं के पार चला गया।
अहिंसा, करुणा क्षमा, प्रेम और त्याग : तथागत सिद्धार्थ के अहिंसा, करुणा क्षमा, प्रेम और त्याग की प्रेरणा के साथ साथ प्रचलित याज्ञिक कर्मकाण्ड के विरोध और जीवन को नवीन रुप में परिभाषित करने के कारण उनका मत और विचार चतुर्दिक विस्तारित हो गया और तत्कालीन भारतीय आमजन समाज में स्थापित हो गया।
लोग बलि, हत्या,यज्ञ हिंसा और अन्य कर्मकाण्डों से उबे हुए थे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध मत ग्राह्य हो गया। ऐसे उनके जितने दर्शन और चिन्तन हैं, महत्वपूर्ण और व्यवहार के योग्य हैं परन्तु एक दर्शन ने सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान को पाया वह ' पटिच्चसमुप्पाद् ' है जिसे संस्कृत में ' प्रतीत्यसमुत्पाद ' कहा गया है। इसका सीधा सादा मतलब ' कार्य और कारण का सिद्धान्त ' हैं।
अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन और चिंतन से इस सिद्धान्त का क्या लेना देना है। लेना देना तो यह है कि यह सम्पूर्ण बौद्ध धर्म और दर्शन के मूल में रीढ़ की हड्डी की तरह है, कहा जाता है कि इस दर्शन और चिंतन के बगैर सिद्धार्थ कभी तथागत बुद्ध नहीं हो सकते थे। शब्दार्थ के बाद इसके कार्यभेद को भी जानना जरूरी हो जाता है।
इसकी व्याख्या करते हुए एक पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि ' this law establishes the fact of the existence of any thing whether it is living or non living whether it is an object Or incident then there must be a set of causes or reasonable reasons behind it '
अनात्मवाद और अनिश्वरवाद : अर्थात् किसी का होना अगर उद्देश्यपूर्ण है तो निश्चय ही उसका कोई कारण होगा, 'प्रतीत्य' ( कारण ) है तो ' समुत्पाद ' उसका उत्पाद या परिणाम अवश्य होगा। सिद्धार्थ ने इसी नियम के आधार पर अपने ' धर्म दर्शन और चिंतन को विकसित किया और ' अनात्मवाद और अनिश्वरवाद ' की व्याख्या की और बताया कि समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताओं का आधार कारण और कार्य का सिद्धान्त है जो स्वत: स्फूर्त क्रियाशील है जिसके पीछे कोई अलौकिक सत्ता का अस्तित्व नहीं हैं।
यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अगर बुद्ध किसी बाह्य सत्ता की बात करते तो उन्हें आत्मा परमात्मा और अन्य सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता और जिस बदलाव को वह लाना चाह रहे थे, नहीं आता और कोई परिवर्तन नहीं हो पाता और यही कारण है कि उन्होंने ईश्वरीय सत्ता और इससे सम्बन्धित बारह सवालों के कोई जवाब नहीं दिए और ऐसे प्रश्न किए जाने पर या तो मौन हो जाते या उन प्रश्नों को अव्याकृत कहकर अस्वीकार कर देते।
कर्म की श्रेष्ठता : कर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कर्म जनित श्रेष्ठता से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा मोक्ष की जगह ' निर्वाण और महापरिनिर्वाण ' की बात की। मूलतः यह सिद्धान्त ' औपनिषदिक दर्शन और चिंतन में स्थापित ' कर्मवाद के सिद्धान्त ' से अभिप्रेरित और अनुप्राणित है जिसकी व्याख्या तथागत सिद्धार्थ ने अपने तरीके से की। यही सिद्धान्त विज्ञानवाद भी कहलाता है जिससे प्रकृति के सारे क्रियाकलापों की व्याख्या की जाती है।
इस कालखंड के बड़े भौतिकविद् आईजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त और न जाने कितने आधुनिक सिद्धान्त इसी पर आधारित है। सम्प्रति संसार की जो अवस्था है और हम मनुष्य जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, क्या यह बताने की जरूरत है कि हमें ' किसी भी क्रियाशीलता की अति से बचना ' चाहिए। या तो हमने इस प्रकृति के साथ अति किया है या विज्ञान के साथ अति अर्थात् विज्ञान को विकृत करने का काम करने का काम किया है।
इस तरह अगर ' प्रतीत्य ' हम हैं तो त्रिविध ताप संकट इसका ' समुत्पाद ' है और यही परिदृश्य उस सिद्धान्त की प्रासंगिकता को सही सिद्ध करता है। हमने इसी आलेखों के माध्यम से कितनी बार कहा है कि सत्य का जो हिस्सा निरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है वही टिकेगा शेष कालप्रवाह में बह जाएगा।
अब आज की वैश्विक व्यवस्था में अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, त्याग आदि की कितनी जरूरत और प्रासंगिकता है, विश्लेषण का विषय है। उनके सारे दर्शन और चिन्तन आज भी व्यवहारिक और ग्राह्य हैं बस बहस हिंसा और अहिंसा के उपर है। प्रेम, क्षमा ,दया , त्याग और करुणा सार्वकालिक और सार्वभौमिक है पर अहिंसा और हिंसा को नये सन्दर्भों में देखने की जरूरत है।
अहिंसा परमो धर्म : जिस कालखण्ड में तथागत सिद्धार्थ ने अहिंसा परमो धर्म की बात की थी,वह कुछ और था और आज की वैश्विक व्यवस्था कुछ और है। कोई भी दर्शन और चिन्तन में सामयिक जीवन मोल और मूल्यों के रक्षा के आधार होने चाहिए अन्यथा वह मूल्यहीन हो जाता है। रक्षा करने का सामर्थ्य सिर्फ शक्तिशाली में ही हो सकता है, निर्बल न तो स्वयं की रक्षा कर सकता है न औरों की रक्षा कर सकता है। कहा भी गया है कि ,समरथ को नहीं दोष गुसाईं अर्थात् जो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हैं वे कभी दोषी नहीं ठहराए जाते हैं। भय नाग से किया जाता है,जलसर्प से कोई नहीं भयाक्रांत होता है। दिनकर जी ने भी कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसलिए अहिंसा जैसे सद्गुण की रक्षा तभी हो सकती है जब बुद्ध के पीछे कृष्ण हों अन्यथा अहिंसा की महत्ता समाप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता कल भी थी और कल भी रहेगी पर शान्ति और क्षमा के पीछे उनके रक्षार्थ वांछित शक्ति भी हो, शक्ति के बगैर अहिंसा कायरता और और दुर्गुण है। वीर और सामर्थ्यवान के लिए अहिंसा और क्षमा आभूषण हैं पर कायरों के लिए अर्थहीन है।
सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा,क्षमा,प्रेम और त्याग के लिए, बुद्ध और बुद्धत्व की रक्षा के लिए कृष्ण का होना अनिवार्य है।तथागत बुद्ध की जयन्ती पर उनको कोटिशः नमन । नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय।
-----------
मातृ दिवस : मातृदेवो भव पितृदेवो भव. शक्ति : आलेख : ६८
-------------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माता पिता तो नित्य पूजित हैं,जो नित्य हैं वे एक दिन के लिए कैसे आयोजित हो सकते हैं, मैं तो रोज प्रातः काल, कहीं बाहर निकलते वक्त और रात में सोने के पूर्व** मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उच्चारण करते हुए नमन करता हूॅं। दिवस तो एक औपचारिक रुप से तय उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें सालभर में एकबार याद किया जाता है। हमारी स्मृतियां जहां तक काम करती है ऐसे दिवस आजकल के सृजन हैं जिन्हें एक नवीन फैशन के रूप में सृजित और विकसित किया गया है।
माॅं के प्रति सच्चा सम्मान और श्रेष्ठ पूजा तो वही है जो हमारे किसी कृत्य से उनकी आंखें नम न हो जाए,सर न झुक जाए, उनकी आत्मा आहत न हो और माॅं चाहती भी क्या है हम सबसे,बस प्रेमपूर्वक आग्रह,सेवा भाव, सम्मान, उपकृत और अनुग्रहित होने का भाव और उसे कुछ न चाहिए।
माॅं की ममता, स्नेह, वात्सल्य,क्षमा, त्याग, सहनशीलता, बलिदान आदि के भावों का न तो कोई मोल है न मूल्य है, अप्रतिम है माॅं। इस सन्दर्भ में बाईबल की एक सुक्ति का भाव है,
God can't be physically available in the world and can't be seen so he made mother on the earth. So Mother is the real reflection of thy Merciful God.
If U serve ur best ur mother U serve best God.
The service to Mother is the best prayer and worship to God
यही सच भी है कि हमारे माता-पिता ही धरती पर जीवित भगवान हैं और सच्चे मन से उनकी सेवा ही ईश्वर की साधना और आराधना है। इस्लाम में भी माॅं के पैरों तले जन्नत बताया गया है।
माॅं और मातृभूमि को इसीलिए स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में हम उनका मोल और मूल्य नहीं समझ पाते और फिर दिवसों का आयोजन करते हैं। अगर उनके मोल सच में दिए जाते तो संसार भर में एक भी * वृद्धाश्रम नहीं होते और मानवता धन्य होती। माॅं तो ईश्वर सादृश्य है जिसपर लिखते-लिखते स्याही खत्म हो जाए पर लेख खत्म न हो। सद्गुरु कबीर साहब ने एक पद लिखा है जो माता पिता पर भी लागु होता है,
सात समंद की मसि करौ लेखनी सब बनराइ
धरती सब कागद करौ हरि गुण लिखा न जाइ।
अन्त में संसार के समस्त माताओं को सादर नमन। कोटि-कोटि प्रणाम।
---------
निर्णय: पूर्वाग्रह और दुराग्रह शक्ति : आलेख :६७
------------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती
जब हम किसी व्यक्ति,नीति या सिद्धांत,वस्तु ,पांथिक कर्मकांड, सांस्कृतिक मान्यताओं तथा मतों के बारे में निर्णय लेने जा रहे हों तो हमें सभी पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से खुद को मुक्त करते हुए सहज और सरल होना पड़ेगा अन्यथा वह निर्णय या मूल्यांकन कभी भी सम्यक् नहीं हो सकता है।
हमारा जीवन ' व्यष्टि से समष्टि की यात्रा ' है जिसमें हमारे जीवन की शुरूआत अपनी माँ के गर्भ से होता है जो व्यष्टिमूलक है और अंत इस समाज के बीच होता है जो समष्टिमूलक है और यही पूर्णता ( सांसारिक) का द्योतक है।
परन्तु यह सम्पूर्ण जीवन यात्रा या चक्र की समाप्ति नहीं है।
तथागत बुद्ध ने इसी जीवन चक्र को " पटिच्चसमुत्पाद " पर आधारित ' the wheels of life ' कहा था जो सदैव चलता रहता है। आज भी हमारा जीवन ऐसे ही चक्रों के बीच चलता रहता है। इस जीवन यात्रा मे हम किसी व्यक्ति के एक परिदृश्य को ही देख पाते है जैसे कि पृथ्वी या चन्द्रमा के सम्पूर्णता को एक साथ नहीं देख सकते। फिर हम किसी का मूल्य निर्धारण एक पक्षीय होकर कैसे कर सकते है और ऐसा करना ही हमारे सामाजिक आधारभूत संरचना को पूर्वाग्रहित या दुराग्रहित करता है।
जब भी हम किसी का मूल्यांकन करें तो एक बार सहज,सरल और विश्लेषणपरक हो जाएँ जहां कोई आग्रह पुर्वाग्रह या दूराग्रह नहीं होना चाहिए कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय के लिए मन मस्तिष्क और हृदय में एक औचित्यपूर्ण संतुलन और समन्वय होना अनिवार्य है। मामला घर का हो, समाज का हो,देश प्रदेश का हो,यह नियम सार्वकालिक और सार्वलौकिक है।
घर के मुखिया को किसी भी मुद्दे पर बड़ा सोच-समझकर निर्णय लेना पड़ता है जिसमें परिवार के सारे सदस्यों की सहमति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है और यही यथार्थ जीवन के हर क्षेत्र में लागु होता है। परिस्थितियां सदैव परिस्थिति जन्य कारणों से बदलती रहती है और बदलते परिवेश में निर्णय भी बदलते रहते हैं जिसे वैश्विक स्तर पर आदिकाल से देखा जा सकता है कि एक देश स्थायी तौर पर मित्र या अमित्र ( अपवादों को छोड़कर) नहीं हो सकता है, संसार के दो बड़े महायुद्ध और बाद के छोटे बड़े युद्ध इसके जीवन्त उदाहरण हैं।
एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा भी है, In modern world setup there nothing can be permanent right or wrong in the broad field of Politics and Diplomacy. Today Politics is on the screen but Diplomatic Policies r in the Playback.
ऐसी परिस्थितियों को अब घर और समाज में भी देखा जा सकता है कि एक ही परिवार में, रक्त सम्बन्धों में, सामाजिक सम्बन्धों में घात प्रतिघात चलते रहते हैं और आए दिन हो रही आपराधिक घटनाएं इसका जीवन्त प्रमाण हैं। इस यथार्थ को आज समझने की नितांत जरूरत है।
अपनी श्रेष्ठता और प्रभुता को सब कोई स्थापित करना चाहता है जिससे एक द्वन्द्वात्मक परिदृश्य का निर्माण होता है जो विवाद और संघर्षों को जन्म देता है और मैं समझता हूॅं आप सब इससे सहमत होंगे। आज राजनीति विकृत रूप में घर से लेकर समस्त संसार में व्याप्त हो गयी है और यह अब छद्मवेशी कुटनीति बन गयी है जिससे सबको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। पर यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सत्य और असत्य दोनों सूर्य की भांति होते हैं जो आज न कल प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते में सियासत नहीं और सियासत में रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए और हो तो सबकुछ सदरी हो कि कल तो सबकुछ साफ होना ही होना है।
---------
प्रेम और झेन कथा शक्ति : आलेख :६६
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती
संसार अगर अशांत,व्यग्र, बेचैन और हिंसाग्रस्त : आज समस्त संसार अगर अशांत,व्यग्र, बेचैन और हिंसाग्रस्त है तो उसके मूल में एक ही कारण है और वह प्रेम का अभाव,सबके सब मत,पंथ, विश्वास, विचार, वर्ग सम्प्रदाय आदि प्रेम की बात करते हैं पर वे सब बातें सतही होती हैं,किसी में गहराई नहीं होती और किसी में होती भी है तो दूसरा उसकी भाषा समझ ही नहीं पाता फिर द्वन्द्व पैदा होता है और यही द्वन्द्व विषाद और विवाद को जन्म देता है।
झेन या झान कथा : इस सन्दर्भ में एक जेन या झेन या झान कथा बड़ी अद्भुत है लेकिन आपको पहले इस जेन या झेन को समझना होगा कि बगैर इसको समझे आप इसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। यह जेन या झेन शब्द मूलतः ध्यान शब्द का चीनी और जापानी रुपान्तरित रुप है। उन्होंने ध्यान को जेन या झेन कहा है जिसमें प्रेम का बड़ा गहरा प्रभाव है कि ध्यान में उतरने के लिए, करने के लिए नहीं,हृदय को प्रेमासक्त होना पड़ता है,प्रेम की गहराईयों में उतरना पड़ता है और जब तक हृदय उन गहराईयों में नहीं उतरेगा वह ध्यान में नहीं उतर सकता है।
ध्यान का अर्थ आंखों को बंद कर शांत हो जाना नहीं होता बल्कि प्रेम रस में उतरकर डूब जाना होता है और यह डूबना ऐसे ही होता है जैसे नदियों का सागर से महामिलन हो जाता है, नदियां विलीन होकर सागर बन जाती है,यही ध्यान है।आपका अस्तित्व भी अस्तित्वहीन हो जाए जहां आपको स्वयं का बोध ही न हो,वही प्रेम में डूबना या ध्यान में उतरना है।
जापान में एक धनी वृद्धा थी जिसके पास एक युवा संन्यासी आया और एक झोपड़ी देने का आग्रह किया। उसने सहर्ष उस संन्यासी के रहने खाने-पीने की व्यवस्था कर दी। युवा संन्यासी ध्यान करने लगा और दिन रात उसी क्रिया में संलग्न रहने लगा। एक दिन एक बहुत ही सुन्दर युवती उस वृद्धा के पास आयी और कहा, मां, मैं उस युवा संन्यासी से बहुत प्रेम करती हूॅं पर कहने का साहस नहीं कर पा रही हूॅं।
वृद्धा ने कहा, भला प्रेम का आग्रह करने के लिए साहस की क्या जरूरत है,सीधे जाओ और अपने मन की बातें कह दो। वह युवती गयी और खड़ी हो गयी।
युवा संन्यासी भी बैठा हुआ था। उसने उसकी तरफ न देखा और न औपचारिकता से बैठने को ही कहा। उस युवती ने सीधे कहा, हे संन्यासी, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूॅं और आपसे ब्याह करना चाहती हूॅं। उस संन्यासी से यह सुनते ही बड़े क्रोध में आकर उसे झिड़कते हुए कहा, तुम देखती नहीं मैं साधक हूॅं, साधना में लगा हुआ हूॅं,जेन साधक हूॅं,भागो यहां से।
वह युवती रोती हुई वहां से चुपचाप चली गयी। इस दृश्य को देखकर वह वृद्धा उठी और उस युवा संन्यासी के झोपड़ी को तोड़-फोड़ कर कहा,अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कहते हो कि मैं जेन साधक हूॅं और प्रेम को न तो समझते हो और न जानते हों तो ध्यान कैसे करोगे।
जो रस तुम्हारे भीतर है ही नहीं उस रस की खोज बाहर करोगे तो कहां से मिलेगा। तुम उस युवती को प्रेम और भावपूर्ण तरीके से समझा सकते थे कि मैं ब्याह नहीं कर सकता क्योंकि मुक्त जीवन के लिए अभी मैं किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूॅं। न तो तुमने उसे प्रेम से बैठाया और न बात ही की तो तुम्हारे ऐसा प्रेम रसविहीन व्यक्ति साधक कैसे हो सकता है,जो प्रेम में डूबा नहीं,वह ध्यान में उतर कैसे सकता है। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उसके कोमल हृदय को आहत किया है जो अक्षम्य अपराध है,तुम इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
यही सत्य है प्रेम का कि सब प्रेम की बातें तो करते हैं पर वह प्रेम सतही होता है,वह महज आकर्षण है, सांसारिक चाह या जरूरत है,मोह है, विषयासक्त भाव है।प्रेम तो मुक्त होना सीखाता है,स्वच्छंद और उन्मुक्त होना सीखाता है पर उच्छृंखल होना नहीं सीखाता है। वह युवा
संन्यासी चाहता तो सहज भाषा में अपनी विवशताओं और साधना को प्रेम पूर्वक समझा कर बगैर उसका हृदय आहत किए भी उसके आग्रह को अस्वीकार कर सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। जो आपके भीतर नहीं है वह कभी भी बाहर नहीं मिल सकता है।
---------
अनुभूति, आलोचना और आपत्ति शक्ति : आलेख :६५
----------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती
आलोचनाएं मानव या भगवान की इस चराचर जगत में साधारण मानव से लेकर महामानव अर्थात् देवता या भगवान भी आलोचना और आपत्ति से नहीं बचे हैं। चाहे श्री राम हों या श्री कृष्ण हों, जीण महावीर हों या तथागत सिद्धार्थ हों,कतिपय विषयों को लेकर सभी की कुछ न कुछ आलोचनाएं होती रही हैं जिनके जवाब वे स्वयं या उनके अनुयाई, प्रशंसक या भक्त भी देते रहे हैं।
अब सवाल यह उठता है कि किनके विरुद्ध आपत्तियां उठायी जाती हैं या आलोचनाएं की जाती हैं।इसके पीछे एक सीधा सा दर्शन है कि सबके एक साथ खुश या संतुष्ट नहीं किया जा सकता है कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अन्तर्मात्मा से सबके मोल और मूल्यों का आकलन करता है और तदनुरूप स्वीकार भी करता है।
इस संसार में ऐसा कोई भी दार्शनिक, चिन्तक,विचारक, समाज सुधारक, संदेशवाहक या अवतरित विभूति नहीं हुए जिनका विरोध नहीं हुआ और विरोध के कारणों के निराकरण होने के बाद ही वे अपने आदर्श और सिद्धांतों के लिए स्थापित हो सके और लोगों ने उनका सम्मान किया।
बावजूद उसके आज भी सबकी आलोचनाएं होती रहती है जो संसार का व्यवहारिक सत्य है। एक व्यक्ति को स्वाद के लिए पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करैला अच्छा लगता है वहीं दूसरा उसे पसन्द भी नहीं करता कि करैला भी कोई खाने की चीज है। जो मांसाहारी हैं, मांसाहार के लिए उनके अपने तर्क हैं और इसके विपरीत शाकाहारी के अपने पक्ष और तर्क हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही प्रतीत भी होते हैं।
तुलसीदास भक्त श्री राम और श्री कृष्ण : कवि तुलसीदास एकबार अपने एक भक्त के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक श्री कृष्ण का मंदिर मिला। उनके भक्त ने कहा,प्रभु,वन्दन कर लें,सामने श्री कृष्ण का मंदिर है। तुलसीदास जी ने कहा,
हमें कोई आपत्ति नहीं, श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं पर इनके हाथों में बंसी की जगह धनुष - बाण दे दो तो मैं नमन कर लूं। है न अद्भुत बात, गोस्वामी जी सब जानते हैं पर वे श्री राम के अलावा किसी और के सम्मुख नतमस्तक नहीं हो सकते हैं। जब उनके जैसे ज्ञानी पुरुष भी अपनी पसंद का सम्मान कर सकते हैं तो साधारण मनुष्य क्या कर सकते हैं।
निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए : कर्ता के भाव,कृत्य और कृतित्व ही सम्मान और आलोचना के विषय बनाते हैं और उनके कृत्यों और व्यवहार से जो सहमत होंगे,वे उनकी प्रशंसा करेंगे और उसके विपरीत वे निन्दा और आलोचना के पात्र होंगे।पर ध्यान रहे कि उद्देश्यपूर्ण और कर्मनिष्ठ ही आलोचना और निन्दा के पात्र होते हैं, कर्महीन और
उद्देश्यहीन कर्ता नहीं।
आपत्तियों से कतई विचलित न हो : आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, निश्चय ही श्रेष्ठता के साथ करने की कोशिश करते होंगे और जब कार्यरत होंगे तो सबकी नजरों में कतई पूर्ण नहीं होंगे,कुछ लोग खोंच निकालने की कोशिश करेंगे पर एक उद्देश्यपूर्ण कर्मनिष्ठ व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होते।
वे आलोचनाओं और आपत्तियों से कतई विचलित नहीं होते और कर्मरत रहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का मूल्यांकन समय करता है और वही मिटाता और शाश्वत भी बनाता है। बहुत सी राजनीतिक विचारधाराएं आज विलोपित हो गयीं या अप्रासंगिक और गौण हो गयीं और कुछ आज भी अस्तित्व में हैं पर आलोचनाएं तो होती रहती हैं।आलोचना और निन्दा असल में परिष्कृत और मर्यादित करने का काम करती हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा भी है,
निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए
बिन साबुन पानी बिना निरमल करे सुभाव
अर्थात् निन्दक और आलोचक ही हमें हमारे चरित्र व्यवहार और आचरण को शुद्ध और साफ रखने का काम करते हैं जैसे साबुन और पानी से गंदे कपड़े साफ किए जाते हैं।
आलोचना और आपत्ति होने पर किसी को न तो निराश होना चाहिए और घबराना चाहिए बल्कि
आत्ममंथन और आत्ममूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में वह कहां सही और कहां गलत है और अन्ततः अन्त:प्रज्ञा जिसे स्वीकार करे उसे मान लेना चाहिए। यही आत्मोद्धार का एकमात्र मार्ग है जिससे आलोचक भी शान्त हो जाएंगे और आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और अन्त में इसका अन्तिम निर्णय तो काल करेगा ही कौन सही और कौन गलत है।
--------
जीवन और आत्मशक्ति : शक्ति : आलेख : ६४
----------
हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि बराहिल के भरोसे खेती तो खेती बैठकर रोती अर्थात् खेती मजदूरों के भरोसे नहीं होती और ऐसा होता है तो खेती कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती है, किसान को स्वयं उसमें संलग्न होना पड़ता है। यह कथन हमारे सामान्य जीवन में भी लागू है जिसकी अनुभूति सबको होती रहती है। जो शक्ति और संसाधन आपके पास है,उसी पर भरोसा करें,उधार की शक्ति और संसाधन आपके लिए घातक हो सकती है।
आप जब दूसरे की नजरों में समर्थ और शक्तिशाली होंगे तभी दूसरे आपका सम्मान करेंगे और अपना समर्थन भी देंगे।किसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर झूकने,संधि, समर्पण या समझौता करने का नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह झुकना परन्तु मान, सम्मान और स्वाभिमान को कभी झुकने न देना। स्मरण रहे,सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और ग़लत के साथ समझौता करना है, इसलिए एक कवि का कहना है कि,
सब जाए अभी पर मान रहे मरने पर गुंजित गान रहे
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो
हिम्मते मर्दां मददे खुदा : सच में जीवन की सार्थकता इसी में है कि जीवन अपने मोल और मूल्यों से न कटे न हटे। सबके जीवन में संघर्ष आपदाएं, विपदाएं और प्रतिकूलताएं आती रहती हैं जिनसे उनको स्वयं ही जूझना पड़ता है यद्यपि उन घड़ियों में अपने और शुभचिंतक साथ रहते हैं पर लड़ना तो उस मनुष्य को ही होता है और वह अपने तन,मन और धन के सामर्थ्य के हिसाब से ही लड़ सकता है। इसलिए संघर्ष छोटा हो या बड़ा हो,पहले स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए ताकि
अंतिम क्षण में, जीवन के समरांगन में निराश न होना पड़े,कहा भी गया है, हिम्मते मर्दां मददे खुदा अर्थात् ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, God helps those who help themselves, अर्थात स्वयं की आत्मशक्ति,आत्मबल और आत्मविश्वास ही मनुष्य को विजयी बनाता है, ईश्वरीय सत्ता और शक्ति एक अवलम्ब की तरह परोक्ष रुप में,किसी न किसी रुप में आपके साथ साथ रहती है।
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की शक्ति अर्जुन के साथ तभी जुड़ी जब वह स्वयं युद्ध के लिए उद्धत होकर अपना गांडीव उठा लिया। युग बदलता है, युगधर्म भी बदलता है परन्तु सत्य और शाश्वत धर्म (कर्म और कर्तव्य) कभी नहीं बदलता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपने सामर्थ्य और शक्ति के सम्बन्ध में कभी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य की जानकारी
रहती है पर कभी भी आत्ममुग्धता का शिकार नहीं होइएगा। अगर आपके पास कार होगी तभी दूसरा कार वाला आपको कार देगा या इसके अनुपात में वह आपसे उम्मीद रखेगा कि साईकिल वाले को कोई उधार में कार नहीं देगा,यही संसार की व्यवहारिकता है। इसलिए सार्थक जीवन के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का आकलन करते रहें और तदनुरूप ही कार्य करें, सफलता निश्चित ही मिलेगी और सफलता में यदि विलम्ब हुआ तो कम से कम निराशा तो नहीं मिलेगी।
प्राणों के एक एक तार के शेष रहने तक हार नहीं मानना चाहिए कि हो सकता है कि आपका अगला एक कदम या प्रयास ही आपके विजय का मार्ग प्रशस्त कर दे।
---------
सम्पादकीय यात्रा आलेख : जीवन चलने का नाम : शक्ति : आलेख : ६३
----------
*
नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती
चैरेवती चैरेवती : गति ही जीवन है पर लक्षयविहीन गति दुर्गति है.
 |
गति ही जीवन हैआ कही दूर चले जाए हम : फोटो : हिमाचल : शक्ति डॉ. भावना |
किस दिशा में किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए : जीवन गति, अबाध गति अनवरत प्रवाह का नाम है। जो थम गया, ठहर गया, मर गया। मृत्यु शरीर की होती है, जीवन की मृत्यु नहीं होती है। जीवन सृजित होता रहता है,लयवस्था में रहता है फिर रूपान्तरित हो जाता है।जिस शरीर को धारण करता है वह शरीर नष्ट हो जाता है। चार्वाकों से लेकर जैनों से लेकर बौद्धों तक में जीवन को ऐसे ही परिभाषित किया गया है।
औपनिषदिक/ वेदान्त दर्शन और चिन्तन में भी कहा गया है चैरेवती चैरेवती अर्थात् चलते रहो चलते रहो। पर किस दिशा में किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यह जानना भी जरूरी है। आप जब किसी यात्रा या सफर पर निकलते हैं तो स्टेशन/ लक्ष्य पहले से निर्धारित रहता है। उसी हिसाब से आप सारी तैयारियाँ करते हैं, धन एवं अन्य जरूरी संसाधनों का जुगाड़ करते हैं कि सफर में कोई परेशानी न हो। पर सफर और मंजिल तय है।
जीवन की अंतिम परिणति : ठीक ऐसे ही मानव जीवन है। जीवन की अंतिम परिणति तय है। कभी-कभी किसी कारणवश आप सफर की दिशा दशा बदल भी लेते हैं, मंजिल भी बदल जाती है। जा रहे थे मसूरी तो रास्ते में मन हो गया कि शिमला चलते हैं फिर मसूरी यात्रा की दिशा बदल जाएगी परन्तु जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।
इसे गंभीरता से समझते हुए ही भारतीय आर्ष पुरूषों ने शायद चैरेवती चैरेवती कहा होगा पर लक्षयविहीन होकर नहीं कहा होगा। आधुनिक युग में भी जो व्यवस्था और तंत्र गतिमान और लक्षयसिद्ध न हो,नष्ट हो जाता है। गति ही जीवन है पर लक्षयविहीन गति दुर्गति है।
जीवन चलने का नाम : इस रुपान्तरण में गति और स्थिरता दोनों प्रक्रियाओं का महामिलन होता है। हमारे भीतर सबकुछ ठहर जाता है और चेतनाएं गतिमान हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ शरीर ठहर भर जाते हैं और चेतनाएं जाग्रत नहीं होती, गतिमान नहीं होती तो चैरेवती चैरेवती की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती है,चलते रहने होगा। यह कितना व्यवहारिक और अनुभूत सच है कि जिसे आसानी से समझकर आत्मसात किया जा सकता है उसे हम न तो कभी समझने की कोशिश करते हैं और न समझ पाते हैं और नदी से सागर नहीं बन पाते हैं। यह निजी जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर सच है। एक विद्यार्थी,एक खिलाड़ी,एक वैज्ञानिक,एक शोधक एक कलाकार,एक चिकित्सक,एक साहित्यकार,एक योद्धा आदि को नियमित अभ्यास करते रहना पड़ता है तभी वह अपने कार्यक्षेत्र में सफल और स्थापित हो सकता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकता है।
नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में : गतिहीनता तो मृत्यु है सृष्टि, सृजन, लय और विनाश के साथ अनवरत, अबाध मंथर गति से चलती रहती है,कभी न रुकती न कभी थकती है और ऐसी ही प्रकृति और प्रवृत्ति नदियों की भी होती है, कभी स्थिर नहीं, सदैव गतिमान और जिस क्षण उसका प्रवाह रुक गया,वह अस्तित्वहीन होकर इतिहास का विषय बन जाती है और विश्व की कितनी नदियां आज विलुप्त हो गयी हैं।
पर ध्यान रहे, उसका महामिलन जब सागर के साथ होता है तो उनका नाम और अस्तित्व दोनों सागर बन जाते हैं पर यह अन्त उस अन्त से भिन्न स्तर पर होता है जो गतिहीन होकर,सूख कर अस्तित्वहीन हो जाती हैं। यहां वही नदी लघु से विराट बन जाती है।
ऐसे ही हम मनुष्यों की अवस्था और परिणीति होती है या तो हम मनुष्य के रुप में जन्म लेकर मनुष्य रुप में ही नष्ट हो जाते हैं या महामानव के रुप में रुपान्तरित होकर लघु से विराट बन जाते हैं। शरीर वही रहता है पर समस्त चेतनाएं बदल जाती है, दृष्टि वही रहती हैं पर दृष्टिकोण बदल जाता है और यह रुपान्तरण सिर्फ स्थूल ही नहीं सूक्ष्म भी हो जाता है। अन्दर बाहर मौलिक रुप से बदल जाता है।
बगैर अभ्यास के कलम की धार और तलवार की धार कुंद हो सकती है इसलिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों में चैरेवती चैरेवती कहा गया है। ब्रह्माण्ड के सारे छोटे-बड़े पिण्ड सदैव गतिमान हैं,एक क्षण भी रुके,स्थिर हुए कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। सांसें थमीं नहीं कि प्राण निकल गए,शरीर निष्क्रिय और निष्प्राण हो गए। आधुनिक राज व्यवस्था में भी इसीलिए विधि विधान अर्थात् संविधान को समयानुकूल परिवर्तनशील बनाया गया है कि वह समय की मांग के अनुरूप बदलता रहे, चलता रहे अन्यथा वह और उससे संचालित राष्ट्र दोनों नष्ट हो जाएंगे।
इसी तरह वैचारिक रूप से गतिमान, प्रवाहमान और चलायमान रहना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। जिस दिन मनुष्य के भीतर बदलाव होना बन्द हो जाएगा,वह जीवित होते हुए भी निष्प्राण मांस का पिण्ड भर रह जाएगा। अब निर्णय आपके हाथों में है कि नदी बनकर, प्रवाहमान होते हुए सागर के साथ महामिलन करके लघु से विराट होना चाहते हैं या एक निष्क्रिय मांस पिण्ड होकर पोखर या नाले की तरह रहना चाहते हैं। परमात्मा ने, प्रकृति ने इसीलिए हम मनुष्यों को इच्छा स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य के
अधिकारी बनाए हैं कि क्या-क्या चयन करें और क्या क्या करें।
शिव इसीलिए सदैव गतिमान और प्रवाहमान हैं, जब वे आनन्द ताण्डव करते हैं तो सृजन होता है, स्थिर भाव से स्वस्थित हो जाते हैं, सदाशिव की अवस्था में आ जाते हैं तो संसार लयवस्था में आ जाता है। और जब रूद्र ताण्डव करते हैं तो शंकर का स्वरूप धारण करके नये सृजन के लिए पुरानी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं।यही जीवन का रहस्य और सत्य है जो मानव जीवन के लिए भी सत्य है।
शिव ही स्थूल और सूक्ष्म तथा कारणिक हैं, शेष सौर रश्मियों की तरह शैव ऊर्जा का प्रक्षेपण मात्र है।
यात्रा संगीत :
मेरी पसंद
शक्ति मीना स्मिता रेनू भारती प्रिया
*
फिल्म : अनोखी रात.१९६८.
गाना :ओह रे ताल मिले नदी के जल में
सूरज को धरती तरसे धरती को चन्द्रमा
सितारे : संजीव कुमार. जाहिदा.
गीत : इंदीवर. संगीत : रोशन गायक : मुकेश
गाना सुनने व देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को दवाएं
स्तंभ संपादन : शक्ति डॉ. सुनीता शक्ति प्रिया
सज्जा : शक्ति मंजिता स्वाति अनुभूति
-------
अध्ययन, चिन्तन मनन, संवाद,अनुभव और विश्लेषण शक्ति : आलेख : ६२
------------
मैंने जब कभी कुछ लिखा है उसका आधार अध्ययन, चिन्तन मनन, संवाद,अनुभव और विश्लेषण रहा है।आज मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई जो पहले भी हुयी थी पर वो आज पुनर्जीवित हो उठी कि हम अपने अपने पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं, क्या हम अपने अपने इष्ट से सिर्फ याचना करने जाते हैं, दुःख दर्द सुनाने जाते हैं, कोई कष्ट आदि न हो की कामना करने जाते हैं या इसके पीछे कोई और भी उद्देश्य होता है।इस सन्दर्भ में सत्य को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि हम सब एक विशाल सागर से एक अंजुली जल उठाकर उसे ही सम्पूर्ण सागर समझने की भूल करते हैं और आत्ममुग्धता का शिकार होते रहते हैं और आज इस तथ्य से मेरा साक्षात्कार भी हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्ञान अनुभव हासिल कर लिया है पर अनभिज्ञों के बीच में थोड़ा भिज्ञ होना भी ऐसी ही अनुभूति करवा देता है।
आज मुझे ऐसा लगा कि किसी ने सत्य ही कहा है कि ज्ञान और अनुभूतियां अनन्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस सन्दर्भ में महान भौतिकविद् आइजक न्यूटन और जेम्स जीन्स को उद्धृत करना सम्यक् प्रतीत होता है कि उन्होंने कहा था, ब्रह्माण्ड अनन्त, असीम, रहस्यमय और अज्ञेय है, इसके बारे में हमारा ज्ञान वैसा ही है जैसे समुद्र तट पर फैले हुए रेत कण और हमनें उनमें से दो चार कण ही चुन पाए हैं। जब ऐसे सारस्वत कृपा प्राप्त की ऐसी अनुभूति है तो उस विशाल वर्णपट पर हम अकिंचन कहां होंगे,सहज ही अनुभूत है। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूजा स्थलों पर मनुष्यों के जाने के औचित्य और अनौचित्य पर इससे प्रकाश पड़ेगा और एक निष्कर्ष पर लोग पहुंच सकेंगे कि इस सन्दर्भ में हमने कितने
ज्ञान हासिल कर रखे हैं।
ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति तो ऐसे कहीं भी हो सकती है,हम कहीं भी नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं और उस सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं परन्तु पूजा स्थल हमारी अमूर्त भावनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति होती है जहां एकान्तिक बोध होने लगता है। तस्वीरें हों, प्रतिमा हों या प्रतीक हों,सबके साथ हमारी आन्तरिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और लगता है कि सामने वाला हमें सुन और समझ रहा है और हम संवाद कर रहे हैं।अब सवाल उठता है कि आखिर हम सबका वहां जाने का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्या याचना, कामना, क्षमा याचना या कुछ और होता है।
एक छोटी सी रसियन कथा है कि छोटी बच्ची गिरजाघर से बाहर निकल रही थी और एक वृद्धा धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो उस वृद्धा ने छुटते मुंह पुछा कि,
मेरी प्यारी बच्ची, तुमने अपनी प्रार्थना में परमात्मा से क्या मांगा, उस बच्ची का जवाब बड़ा अद्भुत और विस्मयकारी था। उसने कहा, दादी मां, प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, इसमें कहीं उस महान परमात्मा से कुछ मांगा जाता है क्या?
यकीनन वह बच्ची शत प्रतिशत सही थी कि प्रार्थना तो मनुष्य के अन्त:करण की मौन अभिव्यक्ति है और वह ईश्वर मौन की भाषा सहजता से सुनता और समझता है जैसे आत्मा की वाणी भौतिक नहीं होती,मौन की होती है और ईश्वर उसी आत्मा का परम चैतन्य रुप है, इसलिए वह मुखर वाणी से ज्यादा मौन की भाषा समझता है।
इसी मौन की अभिव्यक्ति प्रार्थना है जिसमें याचना नहीं अनुग्रह के भाव होते हैं। हम अपने इष्ट के पूजा स्थल पर इसी अनुग्रह की अभिव्यक्ति करने भी जाते हैं कि हे परमात्मा, तूने जो कुछ भी मुझे दिया है, लाखों करोड़ों इनसे वंचित हैं,इसके लिए भी अनुग्रहित होने की अभिव्यक्ति करने के लिए भी लोग अपने अपने पूजा स्थलों को जाते हैं। हमने जो कुछ भी मांगा और नहीं भी मांगा,तूने दिया और जो मेरे योग्य होता है, वांछित होता है,मिल जाता है।
परमात्मा के उन्हीं अनुग्रहों के प्रति जो अभिव्यक्ति होती है वो सर्वोच्च प्रार्थना है। श्रेष्ठ जन स्वयं के लिए नहीं अन्य जरूरतमंदों के लिए भी प्रार्थना करते और याचना करते हैं जो श्रेष्ठ भाव है। इसलिए ईश्वर के साथ साथ सबके प्रति अनुग्रह और उपकार के भावों को रखिए,यह भी प्रभु की प्रार्थना और अनुग्रहित होने के भाव हैं। आज की इस अनुभूति के पुनर्जीवित करने की हेतु बनी एक सम्मानित स्त्री श्रीमती सुभद्रा साहा के प्रति मैं भी अनुग्रहित होने का भाव रखता हूॅं। ज्ञान बड़ी बड़ी शैक्षणिक डिग्रियों की मोहताज नहीं होती बल्कि सहज चेतना और बोध से प्राप्त ज्ञान भी अद्भुत होता है।
--------
अनदेखा अनबुझ प्रेम : शक्ति : आलेख : ६१
--------
प्रेम अजस्र प्रवाह है जिसमें सब चीजें समाहित होती चली जाती हैं। समस्त ब्रह्माण्ड के जितने पिण्ड हैं जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के बंधे हुए हैं, जिससे जड़ चेतन सबका अस्तित्व है,वह और कुछ नहीं प्रेम ही है।
तथागत ने प्रेम को भरपूर जीया ही नहीं, प्रेम को नख शिख जाना ही नहीं, वह तो संसार की निस्सारता
को दुःखों को समझा और उसी से सबको मुक्त करने के लिए, स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होने की दिशा में लगे रहे, अहिंसा क्षमा करुणा अपारिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य पर ध्यान केन्द्रित करते रहे बुद्धत्व की प्राप्ति की। जीण महावीर ने भी सिद्धार्थ के पूर्व यही किया। किसी ने प्रेम की गहराईयों में जाकर प्रेम को न जाना न जानने की कोशिश की,वे दुःख और दुःखों से मुक्ति मार्ग की खोज, कैवल्य, निर्वाण, महापरिनिर्वाण आदि की खोज में लगे रहे। संभवतः इनकी नजरों में प्रेम बंधन का कारण नजर आया हो और जीवन के रस से ये चूक गए।इनके पूर्व भी भारतीय दार्शनिकों में** आजीवक या चार्वाक सम्प्रदाय के लोगों ने भी जीवन की नश्वरता और यथार्थ पर ही केन्द्रित होकर रह गए और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष से ही अछूते रह गए,
एक पाश्चात्य समीक्षक ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि,
They were the divine light on the earth sent for the revelation of the truth of life but they did never looked into the essence of life which makes life meaningful.
प्रेम बहुरुपिए की तरह : जीवन से उसके सार तत्त्व को ही निकाल दिया जाए तो जो शेष बचेगा वह रसहीन गन्ने का अवशेष ही होगा। प्रेम जैसे ही मानव मन हृदय और आत्मा में जगता है, जीवन रसमय हो जाता है,वह संसार के समस्त जड़ चेतन को समझने और आत्मसात करने लगता है। इस पर एक बड़ी रोचक और मार्मिक कहानी है। एक स्त्री बड़ी खुबसूरत थी जिसका पति बदसुरत, निकम्मा और शराबी था। वह रोज शराब पीकर आता और और पत्नी के साथ मार-पीट करता और गालियां देता, फिर शराब के नशे में सो जाता। एक दिन एक फकीर उधर से गुजर रहा था और उसने यह सबकुछ देखा।
उसने कहा कि तुम इसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो,उसने कहा,कितनी बार छोड़कर गयी पर मुआ वहां भी चला आता है,मर जाता तो अच्छा होता। वह फकीर चला गया और कुछ समय बाद फिर उधर से ही गुजर रहा था तो उसने देखा कि वह औरत बिल्कुल थकी हारी और सौन्दर्य विहीन होकर चुपचाप बैठी हुयी थी। फकीर ने पुछा कि क्या हुआ,तुम विरान बाग सी क्यूं लग रही हो,उस स्त्री ने कहा कि मेरा पति मर गया।
फकीर ने कहा, अच्छा हुआ,तुम तो यही चाहती भी थी। उस स्त्री ने बड़ी सहजता से कहा,ये सब श्रृंगार तो मैं उसी के लिए करती थी,मेरा गुमान तो उससे ही था, झगड़ा करके मजा आता था,उससे में गुस्सा तो करती पर प्रेम भी करती थी,अब श्रृंगार किसके लिए करुंगी और झगड़ा किस्से करुंगी। फकीर ने कहा,सच कहा तुमने,यही तो सच है।
प्रेम बहुरुपिए की तरह होता है, कितना भी रुप बदल ले पर आत्मा तो वही रहती है। जिसने जीवन में प्रेम न जाना,सब जानकर भी जीवन को नहीं जान पाया,जो प्रेम में डूबा नहीं वह भला ईश्वरीय सत्ता के रहस्यों को क्या जानेगा,वह किसी से प्रेम क्या करेगा और अगर ऐसा करता दिखाई देगा तो उससे बड़ा पाखंड और आडम्बर और क्या होगा।
प्रेम रस को चखा नहीं
छुअन चला आकाश
अधंकार में डूबा रहा
वो क्या जाने प्रकाश.
प्रेम के कई तल : प्रेम के कई तल हैं, नाभी तल,उदर तल, बुद्धि तल,मन तल, हृदय तल और आत्म तल, जिनमें प्रेम अपने अपने हिसाब से चलता है और लोग उसी हिसाब से उसे संज्ञायित भी करते हैं, आमतौर पर लोग प्रेम को हृदय का वस्तु समझते हैं पर प्रेम तो आत्मा का विषय है,आत्मरस है, प्राणतत्व है। इसी रस को ** सत्यम् शिवम् सुन्दरम् भी कहा गया है,जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुन्दर है।
प्रेम गया कि जीवन से चूके, रस खत्म हुआ तो आपकी अवस्था रस निकाल दिए गन्ने के समान हो जाएगी, निरस निष्ठुर और प्राणहीन,गन्ने के प्राण क्या है रस,नदियों के प्राण क्या हैं जल, सूर्य चन्द्रमा के प्राण क्या हैं प्रकाश, शरीर के प्राण क्या हैं आत्मयुक्त प्राण, इनके प्राण निकले नहीं कि सबके सब अस्तित्वहीन हो गए।
प्रेम जरूरत है, आवश्यकता है किसी के अस्तित्व की, प्रेम नहीं तो सब निरर्थक, सब अर्थहीन पर आप सबकी खोज जिस तल पर है वहां प्रेम कभी नहीं मिलेगा,मिलेगा तो एषणा,वासना,कामना मोह, आकर्षण आदि और वह कभी प्रेम नहीं हो सकता है।
प्रेम को जानना : प्रेम को जानना समझना होगा तो शिव राम और कृष्ण को समझना होगा, सति यज्ञकुंड में जल रही है,शिव, शंकर हो गए,प्रेमी हो गए, सति के शव को कांधों पर लादे विलाप कर रहे हैं, विनाश तांडव शुरू हो गया, कहीं शिव विलाप करते हैं, नहीं, पर शिव की चेतना भी उसी अनन्त चैतन्य प्रेम से जुड़ी हुयी है, जानकी का हरण हो गया, वन वन भटक रहे हैं राम, विलाप करते हुए सबसे पुछ रहे हैं क्या तुमने जानकी को जाते देखा है, प्रेम को अनंत गहराईयों में जानना होगा तो कृष्ण को गहराईयों में जाकर समझना होगा, ब्रज छोड़ने के बाद उद्धव से कहते हैं,हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाहीं।
लोग आज भी सिर्फ राधा को प्रेम से जोड़कर देखते हैं पर राधा तो उनकी आह्लादिनी शक्ति भर है,उनका प्रेम तो राधा के अस्तित्व के सीमाओं के पार है।
कबीर तुलसी , रैदास और मीरा : प्रेम को जानना समझना हो तो कबीर तुलसी , रैदास और मीरा को समझना होगा, प्रेम तो साक्षात् ब्रह्म है, ईश्वरीय सत्ता है, अल्लाह और वाहेगुरु है जिसकी कोई भाषा नहीं, सबकी भाषा ही प्रेम है। आप प्रेम को अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं पर प्रेम की एक ही भाषा है, द्वैत से अद्वैत हो जाना जैसे नदियां सागर में समाकर एक हो जाती है और आप प्रेमगीत शेर और कविताओं में प्रेम ढुंढ रहे हैं।
सद्गुरु कबीर के शब्दों में,
प्रेम गली अति सांकरी
जामे दोउ न समाय
जब मैं था तब हरि नहीं
जब मैं हूॅं हरि नाय।
प्रेम इति ब्रह्म ब्रह्म इति प्रेम।
प्रेम शिव, राम और कृष्ण है जो इसे सत्यापित करते हैं कि यही प्रेम है और इसके मर्म को समझने वाला ही परमात्मा को और उसके सृजित संसार और प्रकृति को समझ पाएगा।
-------
नागरिक चेतना और हम शक्ति : आलेख : ६०
-----------
परिवार सामाजिक आधारभूत संरचना की प्राथमिक इकाई है और इसी से वैश्विक स्तर पर समाज का निर्माण होता है। परिवार की सफलता विफलता परिवार के मुखिया/ प्रधान के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। परिवार का मुखिया यदि स्वयं ***अनुशासित मर्यादित और संयमित हो तो परिवार के सारे सदस्य ( अपवादों को छोड़कर) मुखिया का अनुसरण करते है और परिवार तथा समाज के परिष्कृत और परिमार्जित होने से देश भी स्वस्थ, समृद्ध, अनुशासित और सशक्त होता है।
इस चेतना का मूलाधार * नागरिक चेतना है। इसलिए मौजूदा पीढ़ी को कुछ दीजिए कि न दीजिए पर नागरिक चेतना जरूर देने का प्रयास कीजिए ताकि उसका * कल सुरक्षित और निश्चित हो। नागरिक
चेतना ही वह बोध है जो किसी व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत सचेष्ट और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और निजी जीवन के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को समेटे हुए सामंजस्य और समन्वय बैठाने की ओर उन्मुख करता है। यह बौद्धिक चेतना वाहन में एक ब्रेक के समान काम करती है और मनुष्य अनुशासित और मर्यादित होना और रहना सीखने लगता है। सम्यक् शिक्षा और
अनुशासन इसके रक्त प्राण हैं,एक इसे जीवित रखता है और दूसरा इसे गतिमान बनाए रखता है।इस सन्दर्भ में शिक्षा की महत्ता और गरिमा को पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी स्वीकार किया है। अरस्तू,प्लेटो,चाणक्य,लौक, रूसो,फेबर आदि ने शिक्षा को ही ज्ञान, विज्ञान,कला, साहित्य, जीवन मोल और मूल्यों को जानने और आत्मसात करने का साधन माना है। हीगेल ने मानवीय सभ्यता, संस्कार और संस्कृति तथा इतिहास को जानने और विश्लेषण करने का एकमात्र साधन माना है और इन्हीं गुणों से लैस होकर एक मनुष्य सभ्य सुसंस्कृत और नागरिक चेतना से युक्त होता है। यह शिक्षा से सृजित बौद्धिक चेतना ही है जो किसी समाज और राष्ट्र को संवेदनशील,जागरुक, सशक्त और समृद्ध बनाने का काम करती है। नागरिक चेतना युक्त एक नेता ही किसी समाज या राष्ट्र को वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने का काम करता है,एक प्रशासक तभी कुशल प्रशासक होता है जब वह नागरिक चेतना से युक्त होता है,एक संवेदनशील सरकार और प्रशासक यदि नागरिक चेतना से युक्त नहीं होगा तो वह समदर्शी कभी नहीं हो सकता है,वह चुनो और लाभ पहुंचाओ की नीति पर काम करने की प्रवृत्ति और
प्रकृति के वशिभूत होकर रहेगा और विकास तथा प्रशासन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कभी नहीं हो सकेगा।
नागरिक चेतना से युक्त समाज में आपराधिक भावनाओं का जन्म गौण रुप में होगा, समाज का अपराधीकरण नहीं होगा,लोग कानून का सम्मान करेंगे और समाज भयमुक्त होगा।
पर इसके लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा कि यह परिवार, समाज और सरकार सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है अन्यथा हम सब एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे परन्तु एक चीज महत्वपूर्ण है कि इसकी प्राथमिक जवाबदेही और जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए तभी हम परिवार,समाज और राष्ट्र को सशक्त,सबल और समृद्ध बनाने में सफल हो सकेंगे।
---------
संगीत और मनुष्य : शक्ति : आलेख : ५९
----------
साहित्यकार सिर्फ कथा,कहानियां, उपन्यास,नाटक, काव्य आदि का ही सृजन नहीं करते बल्कि अपने पात्रों के माध्यम से मानवीय चरित्रगत गुण दोषों की विवेचना करने के साथ साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य का आकलन भी करते हैं।
पाश्चात्य साहित्यकारों में विलियम शेक्सपियर भी ऐसे ही साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपने नाटक * The Merchant Of Venice में लौरेंजो और जेसिका के माध्यम से मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले संगीत के प्रभाव और उसके चरित्रगत आचरण और व्यवहार को सद्गुरु कबीर की भांति उधेड़ कर रख दिया है,
शेक्सपियर कहता है कि, The Heart Which Is Not Moved By The Waves Of Music Is Not Subject To Be Believed. इस छोटे से वाक्य ने मनुष्य के हृदय के बारे में क्या नहीं कह दिया कि जो जिस मनुष्य का मन हृदय और आत्मा संगीत की लहरों से विचलित न हो,वह कभी विश्वास के योग्य नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, मानों शेक्सपियर ने हृदय के मापने का पैमाना संगीत को ही बना दिया और ये सच भी है। हम मनुष्यों का संगीत से सम्बन्ध गर्भ नाल के रिश्ते जैसा है।
एक शिशु जब गर्भस्थ रहता है और जैसे ही वह चैतन्य होता है,उसे सबसे पहली अनुभूति जलीय संगीत की होती है। गर्भाशय जल से भरा एक थैला होता है जिसमें छोटी छोटी जल तरंगें उठती रहती है और शिशु उसी में हाथ पैर थपथपाते रहता है और एक नैसर्गिक संगीत का जन्म होता है। गर्भवती स्त्री पेट के उपर से सहलाने का काम करती है जिससे एक कम्पन होता है जिसकी अनुभूति बच्चों को होती रहती है।यही कारण है कि सभी स्तनपाई प्राणियों के बच्चों को जलक्रीड़ा करने में अतिरेक सुख की अनुभूति होती है।
संगीत प्रकृति का महान गुण है जिसे हम पत्तों के सरगम, चिड़ियों की चहचहाहट, नदी और झरनों के प्रवाह, सागर की लहरों, बच्चों की मुस्कान और तोतली बोली, वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि, गायन और वादन आदि के माध्यम से सुनते रहते हैं।
संगीत मन,तन और प्राणों की भाषा है जो किसी भाषा की मोहताज नहीं होती है और इसका प्रमाण लोक संगीत का मधुर संगीत है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी जीवन्त है और उनका अपना सुर ताल है। संगीत की तीन धाराएं यथा,गायन,वादन और नृत्य है जो स्वर, ताल और लय की साधना है जिनका सम्बन्ध तन मन और प्राणों से है जो इन्हें पुनर्जीवित, शुद्ध और चैतन्य बनाने का काम करते रहता है। संगीत मनुष्य को मनोवैज्ञानिक रुप से प्रभावित करते हुए सम्पूर्ण चेतना को प्रभावित करने का काम करता है। यह भौतिक होते हुए भी मानव मन,हृदय और आत्मा को झंकृत करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सकीय प्रभाव डालने के साथ साथ आध्यात्मिक रुप से भी मनुष्य को प्रभावित करता है जिसे आज का आधुनिक भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसका प्रयोग आजकल चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़े व्यापक तौर पर किया जा रहा है। संगीत का सीधा सम्बन्ध हमारे हार्मोनिक परिवर्तन से भी है। आप जिस प्रकार का संगीत सुनते हैं,मन की गतियां भी वैसे ही रुपान्तरित होने लगती है। उदास और दर्द भरे गीत संगीत मनुष्य को एक ऐसी दुनिया में लेकर चला जाता है जहां उसे एकान्तिकता का बोध होने लगता है।
प्रेम में व्यथित हृदय एक अजीब सी अनुभूति करने लगता है जहां रोमांच,दुःख, पीड़ा,विरह और सुख की सम्मिलित अनुभूति होने लगती है और मन हृदय एक कल्पना की दुनिया में खो जाता है और संगीत ही उसका हमदर्द और हमनफस बन जाता है।
प्राचीन भारतीय संगीत में ऐसे ऐसे रागों की चर्चा मिलती है कि उनसे अग्नि,जल,तेज हवा आदि की उत्पत्ति होने लगती थी। अकबर के दरबार में तानसेन और बैजु बावरा की बड़ी रोचक कहानियां मिलती हैं कि बैजू की तान पर हिरण तक दौड़े चले आते थे।
श्री कृष्ण के वंशी वादन : श्री कृष्ण के वंशी वादन की मधुर स्वर लहरियां सुनकर राधा और गोपियां भाव-विभोर होकर दौड़ी चली आती थी। वे अपना सुध-बुध खोकर सबकुछ विस्मृत कर जाती थीं। एक मनोवैज्ञानिक का शोध है कि गीत,संगीत और नृत्य के पसन्द से किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है जो सच ही लगता है। आपकी पसन्द ही आपका पर्सनेलिटी है जो जैसा पसन्द करता है,वही उसका आन्तरिक मोल और मूल्य है,इस सन्दर्भ में मार्क्स के हृदय की कठोरता इस कथन से झलकती है कि, वीणा के तारों से निकलने वाले संगीत से पत्थरों पर चलने वाले हथोड़े की आवाज अच्छी लगती है जिससे मजदूर को रोटी मिलती है।
यहां मार्क्स भूल जाता है कि मनुष्य हाड़ मांस का बना हुआ एक जीवित पुतला भर नहीं बल्कि एक संवेदनशील प्राणी है जिसके सीने में एक कोमल हृदय धड़कता रहता है। संगीत मनुष्य की वेदना, संवेदना,कोमल और प्रेमपूर्ण अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है जो इसे नहीं समझता वह मानव हृदय हो ही नहीं सकता है।
--------
उम्र के उस पार : शक्ति : आलेख : ५८
----
उम्र के किस पड़ाव पर खड़े हो,
चुप क्यों हो,
कुछ गा कर देखो,
कुछ गुनगुना कर देखो,
जहाँ छोड़ कर आए हो खुद को
वहीं फिर खड़े हो सकते हो
बस नजर घुमाकर देखो
एक छोटी-सी अभिव्यक्ति के साथ एक अमरिकी लेखक महाशय फ्रैंक मैक्फोर्ट : पुलित्जर पुरस्कार विजेता ने अपने उम्र के लगभग सातवें दशक में लिखते है कि" हर काम को करने की एक उम्र होती है ' एक ऐसा झूठ है जिसे हम ताउम्र एक हकीकत के रूप मे जीते रहते है, इसे झूठलाते हुए फिर लिखते है कि, ' मेरी उम्र के आखिरी दिनों मे भी जो सूरज उगेगा, वह मुझसे उतनी ही उम्मीद रखेगा जैसे उसने मेरी जिन्दगी के पहले दिन रखा था, फिर मैं उसकी उम्मीद क्यों तोड़ दूँ।'
इसी क्रम में विश्वविख्यात अंग्रेजी साहित्य जगत के दीप्तिमान नक्षत्र जी बी शाॅ लिखते हैं कि " हम इसलिए खेलना नहीं छोड़ देते हैं कि हम बुढ़े हो जाते हैं बल्कि हम इसलिए बुढ़े हो जाते हैं कि हम खेलना छोड़ देते है। अगर हम मानते हैं कि कोई भी नया काम युवावस्था में ही शुरू किया जाना चाहिए तो यह भी मानना चाहिए कि युवा किसी अवस्था या आयु का नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा का नाम है। जिसने अपने मन और अपनी आत्मा की ऊर्जा को जगा लिया है या जगा रक्खा है, वह युवा है , भले ही वह कुछ भी हो।"
जापान के एक १०५ वर्षीय बुजुर्ग युवा हिडकिची मियाजाकी ने जब १०० मीटर के फर्राटा दौड़ को ४२ सेकण्ड में जीत कर पुरस्कार लिया तो वे बच्चों की तरह किलकारियां मार रहे थे और उसेन बैल्ट उन्हें नमन कर रहा था। जिन्दगी के अपने मायने और नजरिया होते है , जैसे स्वीकार करेंगे,आपको वैसी ही मिलेगी।
बस उम्र के किसी भी पड़ाव पर और किसी भी हाल में जीना न छोड़े तो जिन्दगी आपको भी नहीं छोड़ेगी और हमनफस, हमनवाज और हमसफर बन जाएगी। आप अगर वक्त की इज्जत करेंगे तो वक्त आपकी भी इज्ज़त अफ़जाई करेगा। मौत तो जिन्दगी के साथ तयशुदा समझौता है, वक्त पर ही आएगी तो हम
वक्त के साथ मुकम्मल जी लें और जीने की कोशिश करें पर सब मनुष्यों का दुर्भाग्य है या समझ की एक ऐसी दिव्यांगता है जो आदमी को उन्मुक्त और स्वच्छंदता के साथ जीने नहीं देती है और हर आदमी अपनी अपनी उम्मीदों विवशताओं, जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों से जुझता हुआ पिंजरे में बंद परिन्दे की तरह फड़फड़ाता तो जरूर है पर अनन्त आकाश को देखकर खामोश रह जाता है और जिन्दगी तन्हां और खामोश सफ़र बनकर रह जाती है जिसे एक दूसरे नजरिए से देखने और जीने की जरूरत है। अब यहां नियती, प्रारब्ध, तकदीर,नसीब या भाग्य की बात आती है जिसे समस्त मानव समुदाय किसी न किसी रूप में स्वीकार करता है तो सबकुछ उसी भाग्य या नसीब को मानकर बैठ जाया जाए और जैसे जिन्दगी गुजर रही है उसे गुजरने दिया जाए या अपनी उद्यमिता और पुरुषार्थ के साथ बदलने की कोशिश करते हुए जिया जाए, कोई नहीं जानता है कि जिस प्रयास से आप थक हार कर प्रयास करना छोड़ रहे हैं,वही अगला प्रयास आपको सफलता के शीर्ष पर खड़ा कर दे और आपकी नियती या आपका भाग्य बदल जाए। एक बड़ी रोचक कहानी है कि एक खोजी सोने के खदान की तलाश में लगातार खुदाई करता और शाम ढले अपने
शिविर में चला आता।
कई बरस गुजर गए और एक दिन वह बीमार होकर अपने शिविर में सो गया और निराश होकर खोदना छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद वहीं मर गया। लोगों ने जब उसे देखा तो सोंचा कि उसे इसी शिविर के बगल में दफन कर दिया जाए जो जमीन अभी तक खोदी नहीं गयी थी,वही टुकड़ा सिर्फ बचा था। जब उसे दफन करने के खुदाई की जाने लगी तो उसी जमीन के अन्दर सोने का विशाल भंडार मिल गया,जिस सोने की खोज में उसने पुरा इलाका खोद डाला,वह सोना उसके पास ही था पर वह वहीं खोद नहीं सका था। अब इसे कुछ नियती का खेल तो कुछ अंतिम प्रयास को छोड़ देना मान सकते हैं,अब सोचिए कि उस व्यक्ति ने सारे इलाके की खुदाई कर डाली पर वही जगह छूट गयी जो उसके कदम भर आगे थी, हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है कि जहां से एक नये जीवन का सूत्रपात होने वाला होता है,हम वहीं पर थक हारकर छोड़ देते हैं और जीवन से चूक जाते हैं। जीवन न तो बाल्यावस्था है,न युवा न प्रौढ़ावस्था और न वृद्धावस्था,जीवन को जहां से जीने की समझ शुरू हो जाए, वहीं से जीवन है, अगर वह खनिक उस दिन एक प्रयास और कर लेता तो उसका जीवन पुनर्जीवित हो जाता और एक नए इतिहास का सृजन हो जाता।
--------
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बल शक्ति : आलेख : ५७
---------
एक प्राचीन कथा है पर उसका सच और प्रासंगिकता आज भी यथावत है।
एक ऋषि थे जो नगर से दूर एक आश्रम बनाकर रहते थे। उनके अनेक शिष्यों में से एक संसार से विरक्त होकर वहीं आस-पास में एक आश्रम बनाकर रहने लगा था। उस शिष्य पर ऋषि का बड़ा स्नेह था पर पठन पाठन की काफी व्यस्तता के कारण वे उसके पास जा नहीं पाते थे। शिष्य अपने आश्रम में चुहों से काफी परेशान था पर गुरु की शिक्षा के कारण उसे मार नहीं पाता था। इसकी खबर गुरु को थी। एक दिन वह समय निकालकर अपने प्रिय शिष्य के आश्रम पर आए। शिष्य ने बड़ी आत्मीयता से उनकी सेवा सुश्रुषा की। दिन के भोजन के उपरान्त गुरु जी आराम करने के लिए लेटे और शिष्य उनके पांव दबाने लगा। दीवार की खुंटी पर उनका थैला टंगा था। तभी वे देखते हैं कि दो छोटे छोटे चुहे आकर नीचे से छलांग लगाकर थैले में घुस जाते और भीतर से खाने के सामान लेकर नीचे आते और अपने बिल में घुसकर गायब हो जाते। यह खेल गुरु जी देखते रहे और सो गए। सुबह शौचादिक से निवृत होकर जलपान किया और अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि शायद तुम इन्हीं चुहों से तंग हो और मार भी नहीं सकते हो,तो बगैर मारे यह मर जाएगा।तुम एक काम करो,एक फावड़े से इसके बिल की खुदाई करो। कुछ दूर खुदाई करने के उपरान्त दोनों ने देखा कि दोनों चुहे आराम से बैठकर कुछ खा रहे थे और वहां खाने के सामान और कुतरे हुए कपड़ों का ढेर लगा था। कुछ छोटे मोटे अन्य सामान भी थे। गुरु जी ने कहा, इन्हें मारने की जरूरत नहीं,बस इसके बिल के सारे सामान को बाहर कर दो। चुहे वहां से तत्काल कुदकर भाग गए। उसी दिन जब दोनों भोजनोपरान्त आराम कर रहे थे तो देखा कि चुहे आज भी जमीन से थैले के उपर छलांग लगा रहे थे पर उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहे थे और फिर थक हार कर वे बिल में चले गए। अब शिष्य के चौंकने की बारी थी कि आज क्या हो गया जो चुहे वहां तक उछल नहीं पा रहे थे। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि,
बेटा,पहले तो हम भी नहीं समझ पाए थे कि इनकी शक्ति का रहस्य क्या है,ये तो छोटे छोटे चुहे हैं। तब लगा कि इनकी इस शक्ति का रहस्य कुछ और है और हमने बिल की खुदाई करवाई और देखा कि इनके पास अनाज और अन्य सामग्रियों के भंडार हैं जो इन्हें सुरक्षा और अतिरिक्त बल देते हैं, इसलिए इन्हें मारने के बजाय इन्हें शक्तिहीन कर देना है,ये स्वत: स्फूर्त बिना मारे मर जाएंगे और वही हुआ। इनकी शक्ति के स्रोत को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और ये शक्तिहीन होकर बिना मारे मृतवत हो गए। इसलिए जीवन में जब कभी किसी शत्रु से सामना हो तो उसके प्रत्यक्ष बल से ही नहीं वरन् उसके पीछे की शक्तियों का भी आकलन करो। तुम चाहते तो उन चुहों को बड़ी आसानी से मार सकते थे पर बगैर हिंसा किए ही हम लोगों ने उस शत्रु को खत्म कर दिया। इसलिए स्मरण रहे कि
बल की दो प्रकृति होती है, प्रत्यक्ष और
परोक्ष,प्रत्यक्ष तो दिखाई पड़ता है जिसका आकलन आम आदमी भी कर सकता है पर परोक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए वैचारिक और बौद्धिक मंथन करना पड़ता है और तभी युद्ध की रणनीति बनाई जाती है।अगर यह समस्या किसी अन्य जानवर की होती तो रणनीति बदलनी पड़ती।
ध्यान रहे कि शत्रु की प्रकृति और प्रवृत्ति का आकलन करना जरूरी होता है और विजय का मार्ग इसी से प्रशस्त होता है।
---------
आघात प्रतिघात : शक्ति : आलेख : ५६
---------
आघात शब्द बोलते लिखते सुनते या पढ़ते ही एक बात तो साफ हो जाती है कि आघात के दो स्वरुप होते हैं, भौतिक और अभौतिक या सूक्ष्म,जिस आघात में अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग हों,हिंसक आघात है और जिस आघात में इनके प्रयोग न हों सूक्ष्म, अभौतिक या वैचारिक आघात है।अस्त्र शस्त्र के आघात से ज्यादा घातक सूक्ष्म या वैचारिक आघात होते हैं जो शरीर को तो आहत नहीं करते पर ज्यादा सांघातिक होते हैं जो मनुष्य के मन मस्तिष्क हृदय और आत्मा को गहराईयों में जाकर आहत कर देते हैं।बाहरी आघात के घाव कालान्तर में भर जाते हैं और धीरे-धीरे मिट भी जाते हैं परन्तु जो सूक्ष्म या वैचारिक आघात होते हैं, सबसे घातक होते हैं। वैचारिक आघात एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करता है जो मनुष्य को भीतर से छिलता रहता है।इस सन्दर्भ में सद्गुरु कबीर साहब ने सच ही कहा है कि,
शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव
एक शब्द कर औषधि एक शब्द कर घाव
प्रायश्चित और पश्चाताप : और यह घाव ऐसा होता है जो जीवनपर्यन्त सालता रहता है जिसका कोई निदान नहीं होता। और होता भी है तो सच्चे हृदय से किया गया प्रायश्चित और पश्चाताप पर फिर भी मनोमस्तिष्क के किसी कोने में वह सुशुप्तावस्था में पड़ा रहता है जो सुशुप्त ज्वालामुखी की तरह किसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फूटकर निकल भी सकता है।
आघात करना उतना गंभीर नहीं होता है जितना कि आघात करने या पहुँचाने के बीज और गुण-धर्म का होना, पल्लवित और पुष्पित होना कि एकाएक आप लाठी उठाकर किसी पर प्रहार नहीं कर सकते है। वह भाव * प्रच्छन्न रूप से आपके * मन हृदय और मस्तिष्क में कहीं न कहीं बीज रूप में दबा रहता है जो समय की अनुकूलता को पाकर जीवित हो उठता है और आघात का सृजन होता है।
अब आप कुछ प्रसंगों का अवलोकन करें जो एक जीवित दस्तावेज हैं।
पांचाली का तंज : अंधे का बेटा अंधा महाभारत के नवनिर्मित पाण्डवों के रंगमहल का शुभारंभ होना था, जिसमें अद्भुत वास्तुकला का प्रयोग किया गया था कि सतह जो सुखी हुयी थी, पानी से लबालब भरी नजर आती थी और सतह जिस पर पानी था,सुखी नजर आती थी। दूर्योधन गुजर रहा था, जहां पानी न हो वह अपनी धोती उठा लेता था और जहां पानी हो धोती छोड़ देता था। पांचाली छज्जे पर से सब देख रही थी,उसने अट्टहास करते हुए तंज कसा कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है।
चीरहरण : भीम की प्रतिज्ञा : और महाभारत यह तंज दूर्योधन को भीतर तक शूल की तरह चूभ गया और उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस अपमान का बदला द्रौपदी से जरूर लेगा जिसकी परिणति उसके चीरहरण से हुयी जो महाभारत का कारण बना।यह वैचारिक या सूक्ष्म आघात का जीवन्त उदाहरण है।
हिटलर प्रथम विश्वयुद्ध में बातौर एक जर्मन सिपाही की तरह लड़ा था। वह नख शिख घायल होकर पड़ा था जिसे डॉक्टरों ने लगभग मृत घोषित कर दिया था, उसके कानों में यह घोषणा सुनाई पड़ी कि जर्मनी युद्ध में हार गया है और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मन प्रतिनिधियों को बुरी तरह अपमानित किया है तो यह आघात वह सह नहीं सका और वह चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ कि जर्मन कौम एक स्वाभिमानी कौम है,वह कभी पराजित नहीं हो सकता और वह स्वस्थ हो गया और उसने नात्सी दल की स्थापना की और जर्मनी पर कब्जा कर लिया,यह वैचारिक आघात था जिसने संसार को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। वैचारिक आघात बड़े विध्वंसक होते हैं जो बड़े वर्णपटों पर परिणाम को ला खड़ा करते हैं।
इसलिए निजी जिन्दगी से लेकर सामाजिक जीवन में इस आघात प्रतिघात से सदैव बचने की जरूरत है कि इसके परिणाम अधिकांशतः नाकारात्मक ही होते दिखाई दिए हैं।
---------
कृतज्ञता और कृतघ्नता : शक्ति : आलेख : ५५
-----------
कृतज्ञता और कृतघ्नता साहित्य मानवीय संवेदनाओं और चेतनाओं को बड़ी जीवन्तता से चित्रित करने का काम करता है जिसका चित्रण वैश्विक स्तर पर अनेकानेक भाषाओं में देखने को मिलता है। इनमें पाश्चात्य साहित्यकारों मेंचेखव,लियो टाल्सटाय,गोर्की, काफ्का,इट्स, वर्ड्सवर्थ, हेमिंग्वे, शेक्सपियर आदि की रचनाओं में बड़ी सहजता से वर्णित मिलता है। हमारे हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द, रेणु,अज्ञेय, यशपाल, जैनेन्द्र, महादेवी,निराला उषा प्रियम्बदा आदि की रचनाओं में भी ऐसे ही भाव सहजता से दिखाई पड़ते हैं।उन मानवीय वेदनाओं में कृतज्ञता और कृतघ्नता के भाव बड़ी गहराईयों तक मानव मन को छुते हुए कोमलता से आहत कर जाते हैं। भारतीय धर्म-कर्म और दर्शन चिन्तन में उपकृत और अनुग्रहित होने के भाव अर्थात् कृतज्ञता और कृतघ्नता के भाव बड़ी गहराईयों में अंकित किए गए हैं। हमारे वैदिक, वेदांत अर्थात् औपनिषदिक,जैन और बौद्ध दर्शन में भी इन भावों को बड़ी महत्ता दी गयी है।अभी उनमें से एक दो को मैं सन्दर्भित करना चाहुंगा।
विलियम शेक्सपियर मनुष्य के कृतज्ञता और कृतघ्नता के भावों को बड़ी जीवन्तता के साथ उकेरते हुए एक नाटक में कहते हैं,
Blow Blow
Thou Winter Wind
Thou art Not So
Unkindest Like
The Ingratitude Of Human Kind.
इस नाट्य कथा एक महत्वपूर्ण पात्र अपने लोगों की दगाबाजी से हारकर और निराश होकर एक जंगल में बैठा है। तेज बर्फीली
पछुवा हवा चल रही है,वह कहता है,
ऐ बर्फीली ठंडी हवाएं,
तुम खुब बहो खुब बहो कि तुम उतनी कष्टदायक नहीं हो जितनी कि मनुष्य की कृतघ्नता।
कितनी वेदना और कितनी पीड़ा उस राजा के मन में है जिसे बर्फीली हवाओं
( जाड़े में ब्रिटेन की सर्द हवाएं हड्डियों को कंपकंपा देती हैं) से ज्यादा मनुष्य की दगाबाजी कष्ट दे रही है इसलिए वह बार बार कहता है कि ऐ हवाओं,तुम खुब बहो।
अब आप मुंशी प्रेमचन्द जी को देखें,
पंच परमेश्वर में पंचायत एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठी है।शाम हो चली है, पेड़ पर पक्षी आश्रय हेतु
इकट्ठा हो रहे हैं। उनमें कुछ सुग्गे भी हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं कि,
भला इन बेमुरव्वत मनुष्यों को हमें तोता चश्म( बेईमान,पलट जाने वाले,नमक की शरियत नहीं देने वाला)कहने का अधिकार किसने दिया,ये तो खुद मतलब के हिसाब से बदल जाते हैं।
दो परिदृश्य दो पात्र दो स्थान पर दोनों में भाव एक ही है कि मनुष्य का चरित्र आमतौर पर
निहितार्थ बदल जाने वाला होता है। निहितार्थ लाभ हानि के आधार पर सांसारिक रिश्ते नाते चल रहे हैं पर मैं यह नहीं कहना चाहता हूॅं कि सभी मनुष्यों का चरित्र एक समान होता है। कुछ लोग इस संसार में आज भी ऐसे हैं जो रिश्तों के मान के रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना से घिर गयी तो उनकी सखी झलकारी बाई ने रानी का पोषाक धारण कर उन्हें भगा दिया कि रानी सा,आप जीवित रहेंगी तो झांसी सलामत रहेगी और स्वयं शहीद हो गयी।
पन्ना धाय ने राणा जी को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को उनकी जगह सुला दिया और सेनापति ने उस अबोध बच्चे को उसकी माॅं के सामने ही मार डाला। बलिदान का ये नैसर्गिक गुण आज भी है जिससे संसार अपने अस्तित्व में है।
कृतज्ञता या उपकृत होने का भाव मनुष्य के महानतम गुणों में सबसे उपर है।हमें अपने गुरु, माता-पिता, हमदर्द, शुभचिंतक, समाज, प्रकृति,राष्ट्र, अभिभावक और अंत में परम चैतन्य आत्मा अर्थात् अज्ञेय सत्ता के प्रति सदैव उपकृत होने का भाव रखना चाहिए। हम हमारे जीवन में चाहे जितना भी समर्थ और सक्षम क्यों न हो जाएं,एक दूसरे के सहयोग की जरूरत वक्त बेवक्त हो
ही जाती है और जो भी हमारे रक्षार्थ खड़ा हो, उसके प्रति उपकृत होने का भाव रखना चाहिए।
यही कारण है कि जैन और बौद्ध दर्शन चिन्तन में क्षमा और उपकार के भावों को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे वैदिक दर्शन में भी मनुष्यों को ** पृथ्वी,
आकाश, वनस्पतियों,जीव जंतुओं और सभी जड़ चेतन के प्रति उपकृत होने के भाव रखने का संकल्प लेने को कहा गया है। यहां तक कि पशु पक्षियों में भी इस भाव को देखा गया है।
एक जगह कहा गया है कि,
आप अगर स्वयं को मनुष्य कहते हैं और आपके भीतर उपकृत और अनुग्रहित होने के भाव नहीं हैं तो आप जीवित होकर भी मृतवत् हैं।
---------
अभी-अभी, दिनकर पूण्य तिथि शक्ति : आलेख : ५४
----------
स्मृति शेष राष्ट्रकवि दिनकर जी जिनकी आज पूण्य तिथि है।
जय हो जग में जले जहाँ भी
नमन पुनीत अनल को,
जिस तन मे भी बसे,
हमारा नमन, उस तेज को, बल को.
इस यशोगान से जाति - गोत्र से इतर तेजोमय संस्कार और प्रज्जवलित अग्नि सम प्रकाश पूँज को नमन करने वाले युगद्रष्टा और राष्ट्रवादी कवि जिनके अन्तस में प्रेम, सौन्दर्य, श्रृंगार, काम- अध्यात्म, पुरूष और प्रकृति की अवधारणा एक साथ समावेशित हों, उस युगान्तकारी पुरूष " दिनकर" जी की पूण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ । एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि जिनके स्वर में जनसत्ता की हुँकार, जनवाद की उभार, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनशक्ति की ऐसी धमक सुनायी पड़ती है जिसके सामने एकबारगी फ्रांसीसी राज्य क्रांति की हनक भी फीकी पड़ती दिखाई देती है। जरा देखिए तो,
सदियों की ठंडी आग सुगबुगा उठी
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाता है
दो राह , समय के रथ का घर्घर नाथ सुनो,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
और सनद रहे कि इसी नाद को हुँकार बनाकर लोकनायक ने एक समय देश की सत्ता को चुनौती देते हुए " सम्पूर्ण क्रांति " का सिंहनाद किया और देश में एक नयी व्यवस्था का जन्म हुआ। सत्ता चाहे किसी की हो पर जब निर॔कुश हो जाती है और उसके लोकतांत्रिक मूल्य और मोल दोनो खत्म हो जाते है तो कलम भिन्न भिन्न रूपों में विरोध के स्वरों का सृजन करती है।जब देश उन शहीदों की शहादत का मोल नहीअदा करता है तब एक रचनाकार अपनी रचनाओं से उनके यशोगान करता है,
जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी
जो चढ़ गए पूण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल,
कलम, आज उनकी जय बोल.
मानवतावाद और मानवीय संवेदनाओं के स्वर उनकी लेखनी में उतनी ही प्रबलता और उद्दात्त रूप मे दिखाई पड़ता है।जो आजादी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी , नंगे को वस्त्र और आश्रय देने मे नाकाम हो , वह आजादी बेमानी है।
दिनकर जी कहते हैं ,
आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में वैर नहीं
पर कहीं भूख बेताब हुयी तो आजादी की खैर नहीं।
चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में ईर्ष्या और निन्दा की क्या भूमिका होती है ,कहते है, " ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निन्दा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है , बुरे किस्म का निन्दक भी होता है। मनुष्य दूसरों की निन्दा करके कभी बड़ा नहीं हो सकता है,बड़ा तो वह तभी हो सकता है जब वह अपने व्यक्तित्व और चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे।" कितनी बड़ी बात है जो दर्शन नहीं व्यवहार है।व्यक्तित्व निर्माण और संवर्धन का मूल मंत्र है परनिन्दा से बचते हुए स्वयं को अनवरत क्षरण और कुंठा से बचाना है। परनिन्दा हमारी ही क्षमताओं का राहू - केतू होता है।
मानवोचित सहजता और सरलता जितनी सुग्राह्य होती है कि उसे समझने के लिए बड़े ज्ञान और विद्वत्ता की जरूरत नहीं होती है बल्कि एक सरल हृदय और भाव की जरूरत होती है ।एक विद्वान चिन्तन मनन करता रहता है तब तक एक सरल हृदय उसे पढ़ लेता है ।
कविवर दिनकर एक युगान्तकारी कवि हैं जिन्होंने काव्यशिल्प और काव्य विधा में हिन्दी साहित्य को एक नयी दिशा और दशा देने का काम किया है। छायावाद का उतार काल था और देश को एक नयी चेतना की ज़रूरत थी। ऐसे कालखंड में दिनकर जी ने वीर रस, उद्दात्त राष्ट्रवाद,लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवीय मूल्यों के साथ साथ सत्ता की निरंकुशता को भी ललकारा है। प्रेम, सौन्दर्य और श्रृंगार की रहस्यमयी आभा से अपनी रचनाओं को आभासित कर हिन्दी काव्य के संसार मे एक नए युग का सूत्रपात किया। जरा उनके ओज को सुनिए,
सुनूँ क्या ; सिन्धु गर्जन तुम्हारा,स्वयं युग का हुँकार हूँ मैं
ये पंडित नेहरू के बड़े प्रशंसकों मे से थे पर नेहरू जी की पंचशील की विफलता ने इन्हें भीतर से उद्वेलित कर दिया। भारत की शर्मनाक हार ये पचा नहीं पा रहे थे। "परशुराम की प्रतीक्षा " में कहते है कि
वीरता जहाँ नहीं वहाँ पूण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है,
तलवार पूण्य की सार, धार पालता है , लालच पर अंकुश का लोभ सालता है,
अग्नि छोड़ भीरू बना धर्म जहाँ सोता है,पातप प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है।
आज किसी का साहस नहीं होता है कि हिन्दु और हिन्दुत्व की सही व्याख्या कर लोगों कोअवगत करावे, पर वह इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहते है कि, "उत्तर - दक्षिण, पूर्व - पश्चिम देश मे जितने भी हिन्दु बसते है उनकी संस्कृति एक है और भारत की प़त्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी सांस्कृतिक विरासत की ही विशेषता है।
हमारा धर्म पंडितों का नहीं, संतों और द्रष्टाओं की रचना है।हिन्दूत्व का मूलाधार विद्या और अज्ञान नहीं है , सीधी अनुभूति है," अर्थात् अन्तस का प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष होता है और अनुभूति भी प्रत्यक्ष होती हैं और यहाँ हिन्दू का अर्थ भारत और भारतीयता है,
भारतीय संस्कार है। हम भारतीयों के पंथ , विचार , सामाजिक और अन्य मान्यताएँ अलग अलग हो सकती है परन्तु भारतीयता तो एक ही है ।परिपक्व मनुष्य जाति भेद से उपर उठ जाता है।
हिंसा उन्हें कभी भी ग्राह्य नहीं है पर वैसी अहिंसा जिस पर हिंसा भी मुस्कुराए, वह अहिंसा उन्हें कभी ग्राह्य नही है। अहिंसा की पूण्य भावना वही सुरक्षित रह सकती है जहाँ उसके पीछे
शक्ति और सामर्थ्य का का अग्नि पूँज और खड्ग शक्ति हो। चीन से एक शर्मनाक हार के बाद वे कह उठते है कि,
तांडव तेज फिर से पुकार उठा है
लोहित में जो था कुठार उठा है
परशुराम जी ने मातृहंता के पाप मुक्ति के लिए अपने कुठार को लोहित कुण्ड मे फेंक दिया था और इसी कुठार से उन्होने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय विहीन किया था, अब उसी कुठार का आह्वान करते है कि आततायियों का नाश फिर से किया जा सके।
वे युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने से नहीं रोकते पर अर्जुन- भीम को वापस लौटाने की बात करते हैं । वे अहिंसा और क्षमा को परिभाषित करते हुए कहते है,
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन , विनीत, सरल हो।"
इतिहास के प्राध्यापक रहे हैं, भारतीय इतिहास बोध से समावेशित हैं, इसलिए एक समर्थ भारत और अखंड भारत की बात करते है, भारतीयता की बात करते हैं ।
उनकी बहुमुखी रचनात्मक प्रतिभा " भारतीय संस्कृति के चार अध्याय" में निखर कर सामने आती है जो प्रौढ़ गद्द की अद्भुत कृति है, जिसका मूल भाव यह है कि भारत एक जीवन्त राष्ट्र है जिसके प्राण वायु में अनेक सभ्यताएँ, संस्कृतियाँ, धर्म, जाति, दर्शन और चिंतन समावेशित हैं और कोई इस पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसका निर्माण एक सामासिक भाव और बोध है।
इनकी सारी रचनाएँ अपने आप मे एक विचार और दर्शन है पर " परशुराम की प्रतीक्षा ", रश्मिरथी" और " उर्वशी " कुछ अपने में विशेष है। उर्वशी को महाकाव्य की संज्ञा दी गयी है जिसमें
एक साथ प्रेम, सौन्दर्य और श्रृंगार,पुरूष और प्रकृति और उनकी रचनाधर्मिता,स्त्री और पुरूष के लौकिक भोग और अध्यात्मिक मूल्यों के अद्भुत चित्रण मिलते हैं । अब जहाँ
रश्मिरथी का सवाल हैं, इसके दो पक्ष हैं, एक तो महाभारत के एक महान पात्र के उत्कर्ष, त्याग और मैत्री भाव को दिखाया गया है वही जीवन संघर्षों के तिमिर तोम को मिटा कर विजय मार्ग को प्रशस्त करने की अद्भुत प्रेरणा दी गयी है। वे कहते है,
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है,
शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते
विघ्नों को गले लगाते है काँटो में राह बनाते हैं ।
खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़
मानव जब जोर लगाता हैपत्थर पानी बन जाता है।
संघर्ष अनवरत संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। जय पराजय से परे
होकर एक सही योद्धा की तरह संघर्ष करते रहना ही परम धर्म है।
दिनकर जी न्याय,सत्य और धर्म अर्थात् कर्म सिद्धान्त के पक्षधर हैं। न्याय यदि सही न हो तो वह अन्याय युद्ध को जन्म देता है जिसे स्पष्ट करते हुए वे रश्मिरथी में उद्गघोष करते हैं,
दूर्योधन को समझाने
को
भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए
पांडव का संदेशा लाए हो न्याय अगर तो आधा दो
पर इसमें भी यदि बाधा हो तो रखो अपनी धरती तमाम
हम इसी में खुशी से खायेंगे परिजन पर असि न उठाएंगे
दूर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका
उलटे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है
यही विवेकहीनता व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को और वैश्विक समुदाय को पतनोन्मुख बनाता है जिसे अवलोकन करने की बात श्री कृष्ण ने कुरु सभा में कहा था।
विभिन्न कालखंडो में अलग-अलग युगधर्म होते हैं, सम्प्रति देश को इसी युगधर्म को पालन करने की ज़रूरत है कि फिर भारत की मान मर्यादा पददलित न हो, परिवार,समाज, राष्ट्र और वैश्विक समुदाय आहत न हो और सर्वत्र न्याय और सत्य की स्थापना हो। इसीलिए श्री कृष्ण को
काल पुरुष या युग ऋषि नहीं बल्कि अकाल पुरुष भी कहा जाता है जिस सत्य को दिनकर जी कुरु सभा में दिखाने की सफल कोशिश की है।
एक बार फिर उन विभूति को शत् शत् नमन्।
-------
राष्ट्रकवि दिनकर :उद्यमिता च साहसे जयतु : शक्ति : आलेख : ५३.
---------
राष्ट्रकवि दिनकर जी की रचनाओं का मैं प्रेमी रहा हूॅं, विशेषकर**
रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के चार अध्याय से बड़ा लगाव रहा है, इनमें भी रश्मिरथी मुझे सदैव जीवंत रखती रही है। इस काव्य रचना को मैंने सातवें वर्ग में ही किसी से मांगकर पढ़ा था और उसके प्रेरक प्रसंग आज भी मुझे ऊर्जावान बनाते हैं। वैसे तो पुरा काव्य ही अद्भुत है पर द्वितीय और तृतीय सर्ग तो मानो उसके प्राण हैं। मैं जब जब स्वयं को थका हारा सा महसूस किया हूॅं तो इन अधोलिखित पॅंक्तियों को मन ही मन में स्मरण किया हूॅं और फिर जीवन संग्राम में उतर गया हूॅं,
सच है विपत्ति जब आती है
कायर को ही दहलाती है
सूरमा नहीं विचलित होते
क्षण एक नहीं
धीरज खोते
विघ्नों को गले
लगाते हैं
कांटों में राह बनाते हैं
खम ठोक ठेलता है जब नर
पर्वत के जाते
पांव उखड़
मानव जब जोर
लगाता है
पत्थर पानी
बन जाता है
जो दीपक नहीं
जलाता है
रौशनी नहीं वह
पाता है
••••••••••
पेरा जाता जब
इक्षु दंड
झरती रस की
धारा अखंड
मेहंदी जब सहती है प्रहार
बनती ललनाओं
के श्रृंगार
जब फूल पिरोए
जाते हैं हम
उनको गले लगाते हैं
वसूधा का नेता
कौन हुआ
भुखंड विजेता
कौन हुआ
जिसने न कभी
आराम किया
विघ्नों में रहकर
काम किया
.........
यकीनन इन पॅंक्तियों में मनुष्य को पुनर्जीवित करने की ऊर्जा है, शक्ति है कि संघर्षों से जो स्वयं को थका महसूस करने लगे, उनमें प्राणवायु संचार करने का काम करती है।
सबके जीवन में छोटी बड़ी आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं,इस मृण्मय संसार में कोई मुक्त नहीं है फर्क बस संसाधनों, धैर्य, सहनशीलता आदि की होती है। कोई साधन सम्पन्न होते हैं, धैर्यवान और सहनशील होते हैं और कोई साधनहीन, अल्प धैर्य और सहते सहते उबे होते हैं,उनके लिए जीवन का संघर्ष थोड़ा कठिन होता है। संघर्षों का स्वरूप चाहे जो हो, अवधि चाहे जो हो परन्तु घबराहट कमोबेश तो सबको होती है और ऐसी परिस्थितियों में हर मनुष्य को पीछे घूम कर देखने की जरूरत होती है कि किन विषम परिस्थितियों में उसने संघर्ष किया और उनसे उबर गया। कभी-कभी संकट इतने उग्र होते हैं कि जान पर बन आती है तब ये पॅंक्तियां जिजीविषा को मजबूत करती है। जीने के लिए लड़ने का साहस पैदा करती है कि, मृत्यु अटल है, स्थान,काल और हेतु निश्चित है,पर तुम लड़ना मत छोड़ना,हो सकता है कि सबकुछ टल जाए और तुम विजयी हो जाओ। जबतक शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है, युद्धरत रहो,हो सकता है कि मृत्यु या पराजय टल जाए और तुम जीत जाओ। जय पराजय की परवाह किए बगैर अपनी महत्तम क्षमताओं का प्रयोग करो कि कालान्तर में स्वयं के प्रयास और साहस पर पछतावा न हो और फिर उस नियती और प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना। हार को भी हार मान लेनी पड़ती है,आया हुआ काल भी टल सकता है परन्तु खम ठोकना बन्द मत करना।
आशा और उम्मीद के दीए जलाए रखना, समय के साथ चलते हुए समय की विपरीत अवस्थाओं से लड़ते रहना कि मन के जीते जीत है,मन के हारे हार।
मेहंदी की लालिमा और चकमक पत्थर की अग्नि रगड़ खाकर ही बाहर आती है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है बस मैदान नहीं छोड़ना है।
उद्यमिता च साहसे जयतु।
-------
प्रेम, प्रकृति और मनुष्य: अनुभूति शक्ति : आलेख : : ५२ .
-------
मनुष्य युगों युगों से प्रेम और प्रकृति के बारे में पढ़ता, सुनता, लिखता, बोलता,गुनता, चिन्तन मनन करता रहा है पर आज भी इससे उतना ही दूर है जितना कि मृगतृष्णा और यथार्थ।
प्रेम ही प्रकृति है, प्रकृति का नियम है और समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताओं का आधार है। ब्रह्माण्ड के सारे पिण्ड इसी प्रेम से आबद्ध होकर क्रियाशील रहते हैं और अपने अक्ष पर घुमते हुए एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। भौतिक विज्ञान जिसे गुरुत्वाकर्षण कहता है, वह सूक्ष्म रुप में प्रेम ही है जिससे सब बंधे होते हैं और जीव जगत की भांति संचालित होते हैं। उल्लेखनीय है कि संसार के समस्त स्थावर जंगम
अणुओं के बने होते हैं,अणु ऊर्जा से निर्मित हैं और ऊर्जा का आधार चेतना है और इसी चेतना का नाम प्रेम है। He who loves mankind,he loves God and the heart which is not filled with the essence of love, can't live with God.
जीवन की सुन्दरता इसी में है कि हम मनुष्य होने के नाते
किसी के सुख समृद्धि का कारण बनें और अगर ऐसा न हो सके या न कर सकें तो इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी के दुःख या विपदा का कारण न बनें,यही श्रेष्ठ मार्ग है।
परमात्मा ने अपने नजरिए से सबको श्रेष्ठ और अद्वितीय ही बनाया है जिसकी परख आपकी समय समय पर होती रहती है पर आप अपनी श्रेष्ठता को नहीं समझ पाते हैं और स्वयं को अमहत्तवपूर्ण और अकर्मण्य मान लेते हैं पर ध्यान रहे कि सुई और तलवार की उपयोगिता और उपादेयता अलग अलग है कि दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं।
--------
जीवन समग्रता का नाम है। शक्ति : आलेख : ५१ .
----------
जो जानेगा ही नहीं वो मानेगा कैसे : स्वयं को या किसी विषय या वस्तु या व्यक्ति या दर्शन या सिद्धान्त या सत्ता को जानने फिर मानने का ही मोल और मूल्य होता है। जो जानेगा ही नहीं वो मानेगा कैसे और मानेगा तो महज दृष्टिभ्रम होगा, मतिभ्रम होगा और ऐसी अवस्था ही मुर्छा या विक्षिप्तावस्था की होती है और वह ऐसी अवस्था में सिर्फ प्रलाप भर ही कर सकता है, कोई आर्ष या प्रबुद्ध वाणी नहीं बोल सकता है।
When a rational talks, talks with intuition not in vague. He talks what is * right and just.
सिद्धार्थ : * आत्मा और ईश्वर की सत्ता : सिद्धार्थ ने पहले खुद को जाना, माना और फिर संसार ने इस तथ्य और सत्य को सहजता से स्वीकार कर लिया कि सिद्धार्थ कोई अवतारी पुरूष नहीं थे, शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित चेतना थे। ये बात अलग है कि आमजन की भाषा में उन्होने * आत्मा और ईश्वर की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया पर सीधे सीधे अस्वीकार भी नहीं किया। उनके चिन्तन में * चित्त और उसकी वृत्तियाँ ही आत्मा है और ईश्वर अव्याकृत सत्ता है अर्थात् उसकी स्पष्ट व्यख्या नहीं की जा सकती है।
उन्होने * आत्मबोध की प्राप्ति की, अपने स्वचैतन्य बोध और अन्तःप्रज्ञा को जागृत किया और जगत ने * भगवान मान लिया, ध्यान रहे, भगवान कोई भी हो सकता है, अरहत्त्व की प्राप्ति कोई भी कर सकता है पर उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता है।
तथागत का सम्पूर्ण चिन्तन : तथागत का सम्पूर्ण चिन्तन * आत्मबोध आत्मचैतन्य और अन्तःप्रज्ञा के जागरण की अवस्था पर आधारित है। मानवमात्र जीवमात्र के सर्वार्थ कल्याण पर आधारित है जिसे
* total goodness , right and just कहा जाता है जो हमारे औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन में समावेशित तथ्य* शिवत्व का है। जिसके हृदय में बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण स्थावर जंगम के लिए सम्पूर्ण कल्याण का भाव हो * शिव है कि शिव काअर्थ ही सर्वार्थ कल्याणकारी सत्ता होता है। सभी कल्याणकारी सत्ता को नमन ही वास्तविक पूजा, आराधना,साधना और उपासना है।
ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताएँ : ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताएँ मानने की नहीं जानने का विषय है कि जान कर मानने का ही मोल और मूल्य है। मानकर तो संसार युगों से चलता आ रहा है और चलता भी रहेगा पर जिसने अंश भी जानने की कोशिश की, उसने तथ्य और सत्य को जान लिया। ये बात अलग है कि तथ्य और सत्य को कभी समग्रता में नहीं जाना जा सकता है। सत्य का अस्तित्व बना रहता है, चारो तरफ बिखरा रहता है जैसे सौर रश्मियों का विकिर्णण होता रहता है और जब उसे एकीकृत और समन्वित किया जाता है तो उससे अग्नि ऊर्जा का सृजन होता है,एक त्रिपाश्व से होकर जब उसे गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में बंटकर एक वर्णपट का निर्माण करता है और वैसे ही सत्य भी है।
आग जलाने,ऊष्मा और प्रकाश पैदा करने का काम करती है अर्थात् सृजन और विनाश दोनों का काम करती है वैसे ही सत्य का भी अस्तित्व है,वह बहुआयामी है पर समन्वित रुप में एक बिंदु पर केंद्रित है।वह कभी पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है। वह * प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न दोनों होता है। सत्य है और भौतिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि मनुष्य के भीतर फैले अनन्त कोशिका जाल से निर्मित * मन हृदय और मस्तिष्क में समावेशित ऊर्जा का स्थूल और सूक्ष्म रूप है। मन का स्थूल रूप मनुष्य है। हृदय और मस्तिष्क के स्थूल रूपों को तो सहज ही देखा जा सकता है परन्तु उन तीनों के सूक्ष्म रूप को संसार का कोई भी विज्ञान कभी नहीं दिखा सकता है। प्राण, जीवन का मूलाधार है, चेतना का सर्वोच्च रूप है पर कोई विज्ञान कभी नहीं बता सकता कि प्राण क्या है जैसे आप बोलचाल की भाषा मे बोलते हैं कि हम उसे दिल से चाहते हैं, वह हमें प्राणों से भी प्यारा है अर्थात् हृदय और प्राणों की तरह अनमोल है कि उसके बगैर जीवित नहीं रहा जा सकता है। सत्य को जो किसी का सत्य हो,किसी व्यक्ति या विषय या सिद्धांत का सत्य हो, समग्रता में कभी नहीं देखा जा सकता है बस देखने की कोशिश भर की जा सकती है।
लिविंगस्टोन कहता है,
*even the most powerful telescope when observes the cosmological object in the universe, it can observe only the face part if the object and half of the same is always hidden.
और यही यथार्थ जीवन और जीवन से भरे संसार का है। जब आप किसी व्यक्ति/ विषय/ सिद्धान्त आदि का अवलोकन और मूल्यांकन करते हैं तो उसी टेलिस्कोप की तरह करते हैं और उनका एक ही हिस्सा देख पाते हैं और कहते हैं कि हम उसके बारे में सबकुछ जानते हैं और यही दशा * दृष्टिभ्रम और मतिभ्रम की होती है जिससे आपको बचने की जरूरत है। निष्कर्षतः कोई भी सत्य कभी पूर्ण रूप से दृष्टिगत नहीं हो सकता है, प्रच्छन्न सत्य तो सदैव आवृत ही रहता है।ईश्वर परम सत्य है पर समग्रता से कोई नहीं बता पाया है कि वह क्या है कि वह अज्ञेय सत्ता है और जिस दिन किसी का उससे साक्षात्कार हो गया, जल जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा और मौन हो जाएगा कि समग्र को जान लेने के बाद वह भी समग्र ही हो जाता है, नदियां सागर में मिलने के बाद नदियां नहीं रह जाती,सागर बन जाती है।इस सन्दर्भ में सद्गुरु कबीर साहब ने सच ही कहा है कि
लाली मेरे लाल की जित देखौं तित लाल
लाली देखन मैं गयी मैं भी हो गयी लाल।
संत सुरदास ने भी इसी सच को ऐसे कहा है कि सुरदास की काली कमरिया चढै न दूजो रंग,
जो श्याम के श्याम रंग में रंग गया अब कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। वह समग्र में समा गया और समग्र ही बन गया।हम तो जरा सा रंग भर ही देख पाते हैं और समग्र को जानने की बात करते हैं। समग्र तो मंसूर और सरमद ने देखा,मीरा और रैदास ने देखा,रुमी और कबीर ने देखा,नानक और जीसस ने देखा और खामोश हो गए।समस्त संसार अब तक उसका अंश ही जान पाया है। संसार के समस्त धर्म दर्शन और चिन्तन में समावेशित तथ्य यही है कि कालखण्डों में युगधर्म की मांग के अनुरूप उसकी अलग-अलग व्याख्या होती रही है पर अज्ञेय के सत्य की समग्र व्याख्या कैसे की जा सकती है।
उसे न तो नकारा जा सकता है और न समग्रता में स्वीकारा जा सकता है। सदं एकः विप्रा बहुधा वदन्ति सत्य, हक, ईमान और न्याय तो एक ही पर विद्वत् जन अपनी अपनी अनुभूतियों से इसकी व्याख्या अलग-अलग करते हैं।
आप भी जब कभी किसी का आकलन मूल्यांकन करें तो दृष्टि द्रष्टा और दृश्य को समेकित और समन्वित करके करें, भूल की संभावनाएँ न्यूनतम होंगी और आपको खुशी और शान्ति की अनुभूति होगी। यही जीवन के एक और समग्र का रहस्य और सत्य है कि एक छत के नीचे रहते हुए भी हम जीवन पर्यन्त एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं फिर उस ब्रह्माण्डीय रहस्य को समग्रता में कैसै जान पाएंगे।
विज्ञान भौतिक पदार्थों की खोज कर सकता है, अणुओं और ऊर्जा की खोज कर सकता है पर चेतना की खोज कैसै कर सकता है जो अणुओं और ऊर्जा का आधार है।
---------
सहज रहें,सरल रहें, साकारात्मक रहें और आत्मसंतुष्ट रहें : शक्ति : आलेख : ५०.
-------------
सहज रहें,सरल रहें : जीवन आपका है, जीवन शैली आपकी है इसलिए चयन आपका ही होना चाहिए पर ध्यान रहे कि लोग क्या कहेंगे या क्या कहते हैं,ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने चयन से मानसिक और वैचारिक रूप से कितना संतुष्ट हैं।
आपका चयन और आपके कृत्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसलिए ध्यान रहे कि आपके चयन और कृत्य औचित्यपूर्ण हों ताकि अन्तिम रूप में उसके लिए पश्चाताप न करना पड़े। यह आपके मन हृदय और मस्तिष्क के सही समन्वय और संतुलन पर निर्भर करता है कि तीनों के सम्यक् समन्वय और संतुलन से चयन और कृत्य के गलत होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है।
आपको सुख हो और सुख कारणों से जुड़ा होता है : आपका जीवन भौतिक और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सामुच्चय है। मानव शरीर एक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सम्मिश्रण है जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। आप वही सोंचना, करना,खान पान करना, सान्निध्य पाना चाहते हैं जिससे आपको सुख हो और सुख कारणों से जुड़ा होता है,कारण हटे कि सुख तिरोहित हो गया। इसलिए जीवन को कारणों से बांधकर नहीं रखना चाहिए कि ये कालान्तर में सदैव दुःख ही देते हैं। चयन कर्म और जीवन, तीनों में बड़ा गहरा सम्बन्ध हैं,इन तीनों का सही संतुलन ही जीवन को औचित्यपूर्ण बनाते हैं और आपको अन्त में पश्चाताप के कारण नहीं उत्पन्न होते हैं।
सहज रहें,सरल रहें, साकारात्मक रहें और आत्मसंतुष्ट रहें ताकि आपको इसका भय न हो कि लोग क्या कहेंगे।
----------
जागना और सोना : शक्ति : आलेख : ४९ .
-----------
जागकर सोने का उपक्रम : तथागत सिद्धार्थ ने एकबार धम्मदेसना में कहा था, जो सोया है उसे तो जगाया जा सकता है पर जो जागकर सोने का उपक्रम करता है उसे नहीं जगाया जा सकता है। बात बहुत छोटी सी है परन्तु इसका अर्थ मर्म और महत्त्व बड़ी महत्वपूर्ण है।
यह जीवन के व्यवहार और चैतन्य भाव से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर मनुष्य की चेतना भौतिक सूक्ष्म और कारणिक भावों से जुड़ी होती है, समस्त क्रियाशीलताऍं इन्हीं भावों से नियंत्रित निर्देशित और संचालित होती है पर सब लोग इसे समझ नहीं पाते हैं।
यहां सोए रहने और जागकर सोने का बहाना करने के जो अर्थ हैं, अद्भुत हैं। जो अबोध हैं,अज्ञानी हैं, अल्प चैतन्य हैं, जो जीवन के सत्य असत्य को नहीं जानते हैं और जो जानते हैं आधे अधूरे जानते हैं,न तो सही अधिकार जानते हैं और ना ही कर्तव्य जानते हैं,न तो धर्म : स्वभावगत वृत्ति : कर्म जानते हैं और ना ही अधर्म जानते हैं, बस किसी तरह पशुवत जीना जानते हैं,सोए हुए हैं।
ऐसे लोगों की सुषुप्त चेतना को जागृत किया जा सकता है कि उनके भीतर सोये मानव मोल और मूल्यों का बीजारोपण किया जा सकता है। उन्हें अधिकार और कर्त्तव्य बताए जा सकते हैं, उन्हें धर्म : कर्तव्य : और उसके मर्म को समझाया जा सकता है कि वे मूढ़ मति या जड़ बुद्धि नहीं हैं,अज्ञानी हैं और ऐसे अज्ञानियों के तमस और अंधकार को दूर किया जा सकता है।
सिद्धार्थ ने ऐसे मनुष्य को ही सोया हुआ कहा है पर जो जिस डाल पर बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा हो उसे नहीं समझाया जा सकता है। अज्ञानता एक ऐसी अवस्था है जैसे रखे हुए बीज की होती है, जैसे ही उसे समुचित
जो प्रकृति और प्रवृत्ति से ही मृतवत : वातावरण अर्थात् उर्वर मिट्टी,जल, वायु ऊष्मा,आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे वो अंकुरित होकर पौधों में और कालान्तर में एक सशक्त वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही व्यक्ति सोए हुए लोग हैं जिनकी चेतना मरी हुयी नहीं बल्कि सोयी हुयी जिन्हें जगाया जा सकता है और ऐसे लोग जागकर बौद्धिक हो सकते हैं जैसे रत्नाकर और अंगुली माल का रुपान्तरित होना है। परन्तु जो प्रकृति और प्रवृत्ति से ही मृतवत हैं,जिनकी चेतना भूने हुए बीज कि तरह है,जो जागकर भी सोने का उपक्रम किए हुए हैं उन्हें कभी भी जागृत नहीं किया जा सकता है। न तो उनके भीतर स्थूल चेतना है,न सूक्ष्म चेतना है और ना ही कारणिक चेतना है। वे पशुवत जीवन जी रहे हैं, जीवित तो हैं परन्तु जीवन का कोई कारण या उद्देश्य नहीं है।वे पशुवत खाते,सोते,प्रजनन करते और एक दिन मर जाते हैं। कहा भी गया है,
He who doesn't know the true difference between True and False,Right and Wrong,can be alive but actually he is as good as dead.
मनुष्य होकर मानवोचित गुणधर्म का पालन न करना, समाज, राष्ट्र, परिवार, मित्र,विवश,निर्बल,
निर्धन आदि के प्रतिअपने कर्तव्यों को न समझना आदि वैसे ही सोए हुए लोग हैं जिन्हें कभी नहीं जगाया जा सकता है।वही व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र जीवित रहता है जो जागा रहता है अन्यथा वह धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। जागृतम् इति जीवितम् ,न सो मृतवत् सम इति।
----------
सत्य की व्याख्या शक्ति : आलेख : ४८ .
-----------
सत्य की व्याख्या : सत्य की व्याख्या कभी की ही नहीं जा सकती है।यह हमने कब कहा कि सत्य की व्याख्या जा सकती है,जो कहा जाएगा वही सत्य है। सत्य को कहने या अभिव्यक्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं पर जितने भी मार्ग होंगे वे एक ही बिंदु पर समेकित हो जाएंगे जैसा हमारा ऋग्वेद कहता है, एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति।
सत्य अनुभूति है : सत्य अनुभूति है जिसकी अनुभूति के अनेक मार्ग हो सकते हैं पर वह एक अनुभूति ही है जो स्थूल और सूक्ष्म हो सकती है। जल का, अग्नि का गुणधर्म वैश्विक स्तर पर एक ही होगा, कालखंड जो भी हो और यही सार्वभौम और सार्वकालिक सत्य है जिसकी व्याख्या किसी को जैसे करनी हो करे।सत्य तो सत्य ही है चाहे आप जिस रुप में कहें सुने लिखें या अभिव्यक्त करें।
सत्य इसलिए शाश्वत है कि इसका ज्ञान विकल्पहीन है,असत्य के स्वरूप को चाहे जितना भी घुमा-फिरा कर कहा जाए जो भी कहा जाएगा वही असत्य हो जाएगा, ठीक इसके विपरीत सत्य को कहने या अभिव्यक्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं पर जितने भी मार्ग होंगे वे एक ही बिंदु पर समेकित हो जाएंगे वह सत्य ही रहेगा।
Truth can be twisted in different ways of expressions but in the conclusion truth is always one in single entity. U can name a rose in different names but it never gives up giving good smell.
अन्त:प्रज्ञा का बोध हो जाना : सत्य अनुभूति है जिसकी अनुभूति के अनेक मार्ग हो सकते हैं पर वह एक अनुभूति ही है जो स्थूल और सूक्ष्म हो सकती है। गन्ने का गुणधर्म वैश्विक स्तर पर एक ही होगा, उसका मीठास कभी नहीं बदलेगा, कालखंड जो भी हो और यही सार्वभौम और सार्वकालिक सत्य है जिसकी व्याख्या किसी को जैसे करनी हो करे।
सत्य तो सत्य ही है चाहे आप जिस रुप में कहें सुने लिखें या अभिव्यक्त करें। सत्य इसलिए शाश्वत है कि इसका ज्ञान विकल्पहीन है,असत्य के स्वरूप को चाहे जितना भी घुमा-फिरा कर कहा जाए,असत्य ही रहेगा वैसे ही सत्य भी है। इसलिए सत्य का बोध चैतन्य या जाग्रत अवस्था में ही हो सकता है और यही चैतन्य या जाग्रत अवस्था*ठहर जाना है,जो ठहर गया सो सत्य को समझ गया।
ठहरना,गति को रोकना नहीं बल्कि विचारों को, क्रियाशीलताओं को समझना है, जहां विचारों के प्रवाह रुक जाते हैं वहां क्रियाशीलताएं भी रुक जाती है और अन्तश्चेतना जागने लगती है और इसी का जागना अर्हत्व या बुद्धत्व का जागरण है, इस्लाम में यही इलहाम है, बौद्ध मत में अन्त:प्रज्ञा का बोध हो जाना है, जैनों में भी ऐसा ही विश्वास है।
-----------
गौतम बुद्ध : अंगुलीमाल : हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे ? शक्ति : आलेख : ४७ .
-------------
अरूण कुमार सिन्हा.
 |
गौतम बुद्ध : अंगुलीमाल : हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे : फोटो : नेट से साभार |
बीच जंगल में आवाज गूंजी : ' ठहरो, कौन है, विरान जंगल में एक कठोर और कर्कश आवाज गूंज उठी....,
एक शमित जवाब मिला कि, ' हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे ?
इस जवाब को सुनकर पहले बोलने वाला दंग रह गया कि उसकी आवाज सुनकर लोगों की घिग्घी बंध जाती थी,डर से लोग थर-थर कांपनें लगते थे।
भला यह कौन है जो जवाब दे रहा है। वह बिहडों से निकलकर बाहर आया। बड़ी-बड़ी लाल लाल आंखें, भयानक डरावना चेहरा, गले में मानव अंगुलियों की माला और खून सनी तलवार लिए वह सामने खड़े आदमी को देख रहा था जो अपने हाथों में भिक्षा पात्र लिए, संन्यासी वेशभूषा वाला, दैदीप्यमान चेहरा वाला एक व्यक्ति सामने खड़ा था जिसके तेज से वातावरण में एक अजीब सी आभा फैल रही थी।
हिंसक डकैत जो अंगुलीमाल था,उसने बड़े शान्त स्वर में पुछा, हे महानुभाव,आप कौन हैं और इस विरान जंगल में क्या कर रहे हैं, संन्यासी जो तथागत सिद्धार्थ थे, उन्होंने बड़े शान्त स्वर में जवाब दिया कि,
मैं तो समझ गया हूॅं कि मैं कौन हूॅं और इसलिए मैं ठहर गया पर तुम कब ठहरोगे।
अंगुलीमाल समझ नहीं पाया कि इसका क्या जवाब दें,उसने कहा कि, हे संन्यासी कहीं आप गौतम बुद्ध तो नहीं हैं कि राजा प्रसेनजीत तक हमसे भयाक्रांत रहते हैं,उनके सेनापति और सेना भी हमसे डरती है और ऐसा निर्भय तो गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। हमने आपके बारे में सुना था,आज साक्षात्कार भी हो गया। अब आप ही बताएं कि आपके ठहरने और हमारे ठहरने का क्या अभिप्राय है,इसे स्पष्ट करने की कृपा करें।
तब तथागत सिद्धार्थ ने कहा,
आप शान्त भाव से बैठकर हमारी बातों को सुनें। अंगुलीमाल अपने कटार को जमीन पर रखकर घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गया।
बुद्ध ने कहा, हम भी ऐसे ही गतिशील थे और सुखभोग में लीन थे, कपिलवस्तु के राज्य का अधिपति था,किसी भी सुख वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी पर हम जब ठहर गए अर्थात् जीवन के निस्सारता को समझ गए तो परिव्राजक हो गए और ठहरी हुई अवस्था में चैतन्य हो गए और उसके बाद मैं गतिशील हो गया कि आप जैसे लोगों को ठहरा कर जीवन के यथार्थ को समझा सकुं।
हम सब किसके लिए सुकर्म या अपकर्म करते रहते हैं,इसके जिम्मेदार कौन होते हैं। हमारे कर्म हमारे होते हैं, कर्मजनित संस्कारों के प्रतिफल को कर्ता होने के कारण हमें ही भोगना पड़ता है और यही भोग जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ साथ चलते रहता है और जबतक वे संस्कार जीवित रहते हैं, हमें भोग से मुक्ति नहीं मिलती और यही पुनर्जन्म के कारण बनते हैं जिनसे हमारा प्रारब्ध बनता है। इसलिए हे अंगुलीमाल,अब ठहर जाओ और शेष जीवन को परिष्कृत और मर्यादित करने की कोशिश करो और इस जीवन की त्रासदी से मुक्त हो जाओ कि तुम ही तुम्हारे कर्मों के भोक्ता हो।
अंगुलीमाल रोने लगा, हे महात्मना,अब आप हमें मुक्ति मार्ग बताकर मुक्त करने की कृपा करें। बुद्ध ने उसे दीक्षित करके भिक्षु समूह में शामिल कर लिया और कालान्तर में वह सिद्ध संन्यासी हो गया।
अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस कथा को सुनाने का क्या औचित्य है, हम तो कोई हिंसा या लूटमार नहीं कर रहे हैं तो हमें ठहरने की या अंगुलीमाल की तरह विलाप करने या पश्चाताप आदि करने की क्या जरूरत है।
हिंसा का अर्थ सिर्फ खून-खराबा नहीं होता है,
सवाल वाजिब है पर आपको इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हिंसा का अर्थ सिर्फ खून-खराबा नहीं होता है, लूटपाट का मतलब सिर्फ लोगों को लूटना ही नहीं होता है। हिंसा बहुआयामी कृत्य है। हम सब रोज हिंसा करते रहते हैं कि हिंसात्मक क्रियाशीलता स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के होते हैं,एक तो मार पीट कर किसी को आहत करना या हत्या कर देना जिसके लिए वैधानिक कानून की व्यवस्था है और आपको इसके लिए वाजिब दण्ड भी दिया जाता है परन्तु उससे भी बड़े वर्णपट पर सूक्ष्म हिंसा का स्वरूप है जिसका गंभीरता से अवलोकन करने की जरूरत है। भगवान महावीर ने इसीलिए** खम्मन परब अर्थात् क्षमापर्व की अवधारणा को जन्म दिया कि हमें एकबार जड़ चेतन सबसे क्षमा मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने में हम सब ऐसी भूल करते रहते हैं। अब आप अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समस्त क्रियाशीलताओं का अवलोकन और विश्लेषण करें कि चौबीस घंटों में आपने किसके साथ क्या बोला, क्या व्यवहार और आचरण किया तो आपको हिंसा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आपने अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों के साथ क्या व्यवहार किया,कितने झूठ बोले, कितनों के साथ दुर्व्यवहार किया आदि सभी हिंसा के ही रुप हैं। आप परिवार में समर्थ हैं, समाज में ताकतवर हैं,पदबल, भुजबल से समर्थ हैं,लोग आपके भय से कुछ नहीं बोलते पर भीतर से उनका मन उनका हृदय और आत्मा आहत होती होगी,आह निकलती होगी और इसका प्रतिफल आपको ही भोगना होगा कि आप ही कर्ता है तो आपको ही भोक्ता होना होगा, इसलिए तथागत सिद्धार्थ ने अंगुलीमाल को सम्बोधित करते हुए सबको कहा कि हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे।
सवाल हम सबके सामने है और जवाब हम सबको ही देना है। देर सबेर सबको ठहरना होगा कि ठहरने का कोई विकल्प नहीं है।
अति से, हिंसा से, झूठ फरेब आदि से बचिए कि यही ठहरना है,महत्तम प्रयास करें कि आपके व्यवहार आचरण आदि से किसी का मन हृदय और आत्मा आहत न हो,यही हिंसा है, सिर्फ मार-पीट ही हिंसा नहीं है। सबके पास इतना समय जरूर शेष रहता है कि वह ठहर जाए और ठहर कर अपने को रुपान्तरित कर लें ।
--------
शब्द, पदार्थ, ईश्वर और हम. शक्ति : आलेख : ४६ .
-----------
किसी का नाम एक संज्ञा भर है, शब्द है।आप जब किसी का नाम लेते हैं जो एक शब्द भर है पर जबतक आपका उससे साक्षात्कार परोक्ष या प्रत्यक्ष न हुआ हो तो आप किसी भी कीमत पर नहीं बता सकते कि वह क्या है और उसका अस्तित्व क्या है।
फूल भर कह देने से एक फूल भर का बोध होता है पर कौन सा फूल है, यह भी बताना पड़ता है तब स्पष्ट होता है और उसकी एक छबि आपकी स्मृतियों से गुजर कर मनोमस्तिष्क में बनती है। अब आपने गुलाब को बेली चमेली कमल आदि को प्रत्यक्ष देखा हो या किताबों में देखा हो तभी वह छबि बनेगी। फल मात्र कहने से किसी फल का बोध होता है, किसी विशेष का नहीं, ऐसे ही जितनी वस्तुएँ होती हैं उनका प्रमाण प्रत्यक्षीकरण है। अनुमान से उसे नहीं बताया जा सकता है।
यहीं पर एक विरोधाभास होता है कि एक अचेतन बच्चे से पुछा जाए कि फल या फूल क्या है तो वह सुन लेगा पर कुछ जवाब नहीं दे पाएगा कि उसकी चेतना या समझ में वह नहीं आएगा कि उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष साक्षात्कार न हुआ हो। एक अबोध बच्चे को साँप दिखाकर पुछिए कि यह क्या है तो वह चलने वाला खिलौना समझेगा या एकाएक डर जाएगा पर उसे समझा दिया जाए कि इसके काटने से तुमको दर्द होगा
( वह मृत्यु को नहीं जानता है), आग को नहीं जानता कि क्या है पर थोड़ा सा लैम्प के शीशे से उसकी अंगुली सटा दीजिए तो उसे जलन होगी तो वह जान जाएगा कि इसे छुने से जलन होती है( वह जलन भी नहीं जानता है)तो वह उससे डरेगा और उसे नहीं फिर नहीं छुएगा। फिर यही संवेदी चेतना उसे साँप या अन्य कीड़ों से उसे भयाक्रांत करेगा। फिर यही तथ्य जीवन की हर क्रियाशीलताओं में लागु होता है।
शब्द मात्र को सुनने से भी उसके अर्थ मूल्य और मोल प्रभाव आदि का बोध तबतक नहीं होता जबतक कि वह स्वयं इसे न जाने या उसे कोई न बताए कि वह क्या है।
कोई शब्द तभी आकार लेता है जब किसी को उसका बोध किसी रूप मे हुआ होता है। शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं जो अस्तित्व में तो हैं पर अमूर्त होते हैं और जबतक उसे मूर्त रूप नहीं दिखाया जाता है, समझ से परे होता है। प्रेम घृणा हिंसा युद्ध ईर्ष्या जवानी बुढ़ापा काम क्रोध लोभ अहंकार
लालच दया त्याग क्षमा जन्म मरण भूख प्यास दुख सुख करूणा जैसे शब्द हैं, इनका अस्तित्व भी है पर आप आम गुलाब गेहूँ चना पानी रोटी आदि की तरह नहीं देखा बता सकते हैं। भूख प्यास के प्रत्यक्षीकरण के लिए आप किसी भूख प्यास से पीड़ित आदमी को दिखाकर, खिला पिला कर बता सकते हैं कि इस अवस्था को भूख या प्यास कहते हैं। किसी हिंसक घटना को दिखाकर हिंसा और अहिंसा का फर्क और अर्थ बता सकते हैं। बच्चों के गलती करने पर उन्हें माफी देकर यह बता सकते हैं कि यह गलत है और यह क्षमा है। इसी यथार्थ का सजीव चित्रण बौद्ध दर्शन और चिन्तन की पुष्टि उसके एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ * मिलिन्दपह्यियों ( मिलिन्द प्रश्न ) में होती है जिसमें ग्रीक राजा मिणान्डर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन का वृहद् संवाद है। शब्द तबतक अस्तित्व में आकर प्रमाण नहीं बनते जबतक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी अनुभूति न हो। अशोक अंजनी राजीव सुरेश आदि कह देने भर से किसी भारतीय पुरूष भर के नाम का बोध होता है पर कौन अशोक कौन अंजनी इसका बोध नहीं होता है,बताना पड़ता है कि वह जो अमूक मोहल्ले या शहर या प्रदेश में रहता है और ऐसा है।
जैसे कारण समुदय से कोई घटना घटती है वैसे ही विवरण समुदय से किसी अस्तित्व का बोध होता है। यह तथ्य और सत्य वैश्विक स्तर पर मौजूद है और सनातन है। पुरी दुनियाँ में * शराब कहीं भी पीजिए, नशा होना ही होना है और सर्वत्र शराब का एक ही गुणधर्म है। हिंसा का गुणधर्म भी सार्वलौकिक और सनातन है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य है। पर ईश्वर की चर्चा करते ही, ईश्वर शब्द का नाम लेते ही उपरोक्त के अर्थ भाव अस्तित्व बदल जाते हैं।
वैश्विक स्तर पर ईश्वरीय सत्ता के रूप अनन्त हैं और नाम भी अनेकानेक हैं। पेड़ पहाड़ बोलते ही एक छबि बनने लगती है( पर कौन पर्वत वृक्ष बोलना पड़ता है) पर जिसने पहाड़ न देखा हो न पढ़ा सुना जाना हो नहीं बता सकता है कि पहाड़ कैसा होता है। प्रशान्त महासागर हमने भी नहीं देखा है पर किताबों में पढ़ा टीवी में देखा है कि कैसा होता है जो सबके लिए एक समान होता है। इसके अस्तित्व की व्याख्या समान की जाती है, विशिष्टताएँ अलग-अलग हो सकती है।
ईश्वर शब्द अद्भुत : परन्तु ईश्वर शब्द अद्भुत है। किसी हिन्दु के सामने ईश्वर की छबि अलग होगी, वहाबी,मुसलमान,यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, शिन्तो, जेन आदि के सामने अलग-अलग होगी कि ईश्वरीय सत्ता की अवधारणा सबकी अलग-अलग होती है। किसी * नास्तिक के सामने कोई छबि नहीं बनेगी कि उसकी चेतना में उसका कोई आकार अस्तित्व नहीं है। ईश्वरीय सत्ता की अवधारणा भी * मूर्त अमूर्त साकार निराकार सगुण निर्गुण
आदि कई भेदों में दृष्टिगत है। यह आम या गुलाब की तरह नहीं है जो सबके लिए एक समान है।
जिसके भीतर जो गुण-संस्कार बचपन से डाले जाते हैं, जिस परिवार परिवेश में वह जन्म लेकर फलता फूलता है, उसका ईश्वर वैसा ही दिखाई पड़ता है।
ईश्वर भी * शब्द ही है पर अलग-अलग अनुभूति और ज्ञानबोध से जुड़ा हुआ है। परन्तु औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन में समावेशित तथ्य यह है कि वे कहते हैं कि * सदं एकः विप्रा बहुधा वदन्ति( यहाँ विप्र का अर्थ वो ब्राह्मण या पंडित नहीं है) अर्थात् सत्( सत्य का सार) अर्थात् हक( इस्लामिक दर्शन)
एक ही है परन्तु ज्ञानीजन बहुविध रूपों में इसकी व्याख्या अलग-अलग कालखण्डों में अलग-अलग करते रहे हैं। जैसे जल को पानी आब नीर अम्बूज वाटर आदि कुछ भी कह लीजिए पर उस पदार्थ का एक ही गुणधर्म है, प्यास बुझाना, सिंचाई करना, सृजन करना, आग बुझाना, इसका यह गुणधर्म सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। जैनों बौद्धों आजीवकों और चार्वाकों को छोड़कर ईश्वरीय सत्ता सर्वत्र किसी न किसी रूप में व्याप्त है। वैसे बौद्ध और जैन तथागत और महावीर को ईश्वर ही मानते हैं।
शब्द के अर्थ की मौलिकता काल स्थान पर कभी नहीं बदलती परन्तु पात्रों के हिसाब से बदलती रहती है परन्तु सत्य का सत् कभी नहीं बदलता है।
ईश्वर सर्वत्र( भाषायी और धार्मिक भेदों को छोड़कर) * सच्चिदानन्द ही है। वह सत् ( हक या truth) है चित्त ( चेतना का आधार) और परम आनन्द (
न्यायपूर्ण और निष्पक्ष) है।
That Which is the Supreme state of Essence of Truth Conscience and Pleasure is Thy Lord Which is Omniscient and Omnipresent and Within Us not far from Us. What r Ur * feelings and emotions, is Ur God.
यह दर्शन और अध्यात्म ही नहीं वरन् जीवन व्यवहार भी है।
अनुभूति के दो आयाम होते हैं, स्वानुभूति जो प्रत्यक्ष है और परानुभूति या जो दूसरे ने लिखा बोला या कहा है,यह दूसरे के लिए स्वानुभूति है पर आपके लिए परानुभूति है जो आपके मन में संशय, तर्क वितर्क आदि की संभावनाओं को जन्म देता है परन्तु पूर्व में यदि आपकी भी ऐसी अनुभूति हुयी हो या आपकी बुद्धि और विवेक इसे तथ्य और सत्य मानता हो तो आप इसे सहजता से स्वीकार कर लेंगे। यहीं से मानने और जानने का द्वन्द्वात्मक भेद खड़ा होता है जिसपर चिन्तकों का एक वर्ग कहता है कि,
Seeing is believing,
पर ये तर्क कहां तक सही है,आप पर निर्भर करता है कि आपने न तो मन को देखा है,न बुद्धि और विवेक को देखा है ना ही आपने प्रेम घृणा क्षमा आदि को देखा है पर उसका
प्रत्यक्षण व्यवहार आचरण में दिखाई पड़ता है और आप कहते हैं कि हां,इनका अस्तित्व है पर भौतिक रुप से इनका प्रत्यक्षण नहीं किया जा सकता है वैसे ही सत्य है जिसका प्रत्यक्षण हमारी ज्ञानेंद्रियां और अन्तश्चेतना अपने तरीके से करती है। इसलिए जिसका भौतिक अस्तित्व उस रुप में नहीं है जिस रुप में आप चाहते हैं
उसकी अनुभूति विभिन्न रुपों में अपनी
बौद्धिक चेतना से करने की कोशिश कीजिए और सत्य को स्वीकार कीजिए।
---------
इसी खोने पाने के क्रम का नाम जीवन है। शक्ति : आलेख : ४५ .
-------------
जो कुछ भी कारण के या प्रभाव के रूप में देखा जाता है,भ्रम है। वह हर चीज या विषय जिसका आरम्भऔर अन्त है,असत्य है,भ्रम है। अब इस कथन को गंभीरता से समझने और विश्लेषण करने की जरूरत है। वास्तव में हम सब पुरे जीवन में इसी असत्य या भ्रम में जीते रहते हैं और उसे ही सत्य समझ लेते हैं जो सबके लिए दुःख, पीड़ा और अवसाद के कारण बनते हैं।
आप इसे ऐसे समझने की कीजिए कि आप अपने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था (अगर इन अवस्थाओं से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं ) का स्मरण करें,अतीत के दुःख सुख संघर्ष जय पराजय सफलता विफलता आदि का स्मरण करें तो पाएंगे कि सबका आरम्भ और अन्त हैं,सबकी अनुभूतियों का आदि और अन्त हैं जो एक मृगतृष्णा सा प्रतीत होता है कि यथार्थ के सामने आने पर सब एक भ्रम सा दिखाई पड़ता है।
कोई घटना, कोई विषय, कोई वस्तु स्थायी रुप से आपके पास नहीं है,जो है सब आभासी है और जो ऐसा है,भ्रम है,असत्य है। इनके खोने पाने के मध्य एक ही विषय भ्रम या असत्य नहीं है,वह है अर्जित आत्मबोध और ज्ञान,यह आपकी अर्जित चेतना पर निर्भर करता है जो सदैव उर्ध्वगामी होता है परन्तु इसके लिए भी आपको सदैव चिन्तनशील और विचारवान होना होगा। यह भी ध्यान रहे कि ऐसी चेतना सबके पास नहीं होती। लोग भ्रम और असत्य में ही जीना पसन्द करते हैं जैसे एक गोबरैले को गोबर में ही सुखानुभूति होती है,वह गुलाब के ढेर में जीवित नहीं रह सकता है,वही उसके लिए सत्य है।
हम सब जीवन में पाने के भ्रम में जीवित रहते हैं। पर सच यह है कि हम सब खोते रहते हैं,पाते कुछ नहीं हैं और जिसे पाना कहते हैं वह भ्रम है और भ्रम का टूट जाना ही खोना कहलाता है और
इसीलिए लोग दुःख पीड़ा और अवसाद से ग्रसित रहते हैं। जो पाया है उसे जाना है और नया कुछ आना है फिर उसे भी जाना है और इसी खोने पाने के क्रम का नाम जीवन है।
--------
मानवीय संवेदनाएं : अनुभूति : शक्ति : आलेख : ४४.
---------
मानवीय संवेदनाएं : हिन्दी साहित्य ही नहीं वैश्विक साहित्य में जितने साहित्यकारों ने मानवीय संवेदनाओं, पीड़ाओं, वेदनाओं,शोषण दोहन,प्रेम घृणा आदि पर लिखा है उनमें से मुंशी प्रेमचन्द का स्थान अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा,ऐसा लगता है कि आज भी उतना ही सच और प्रासंगिक है। भूख की पीड़ा और वेदना पर लिखते हुए एक जगह कहते हैं कि, जिस बन्दे को पेट भर रोटी नहीं मिलती,उसके लिए मर्यादा और प्रतिष्ठा ढोंग है, दर्शन और चिन्तन की बातें पाखण्ड हैं।
जब रोटी ही हो जाए उसका ईमान धर्म : अब बहुतों के लिए यह छोटा सा विषय है पर जिन्होंने सच में भूख की अनुभूति की है,उनसे पुछिए कि भूख के सामने कैसे सबकुछ व्यर्थ और निरर्थक प्रतीत होता है। भूखे रहने का मतलब उपवास नहीं होता है कि उपवास एक आयोजन है जिसे किसी उद्देश्य विशेष के लिए रखा जाता है और उसके उपरान्त अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है। पर भूख की वेदना और पीड़ा इससे बहुत अलग होती है। एक भूखे को इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि भोजन मिल ही जाएगा।
भूख,एक आदमी की सारी चेतना छीन लेती है,आदमी भूख से पीड़ित होने के बिना जाति, धर्म,ऊंच नीच,सही गलत आदि के भेद भाव भूल जाता है। रोटी ही उसका ईमान धर्म बन जाती है। भूख की इस वेदना को महाप्राण निराला जी ने भी बड़े जीवन्तता के साथ भिक्षुक कविता में चित्रित किया है,
पेट पीठ मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक,
भूख के कारण पेट और पीठ सिमटकर एक हो गए हैं और वह लाठी के सहारे किसी तरह चल रहा है।
अब उस भिखारी से कभी जिज्ञासा कीजिए कि भूख की पीड़ा क्या होती है,उसे उस समय भजन,कीर्तन,
पूजा पाठ,ईश्वर आदि सब रोटी होती है। उसे गोल चांद में भी रोटी ही नजर आएगी और अघाए पेट को अपनी माशूका का चेहरा नजर आएगा।
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर और बच्ची : भूख मानवीय त्रासदी है जिससे सम्बंधित एक बड़ी मार्मिक सच घटना है। केन्या के एक क्षेत्र में भारी सुखा पड़ा था,लोग भूख प्यास से मर रहे थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर वहां के हालात को देखने गया था। संयोगवश एक राहत शिविर से थोड़ी दूरी पर उसने एक अजीब दृश्य देखा कि एक मरणासन्न बच्ची किसी तरह घिसट कर शिविर की ओर आने की कोशिश कर रही थी और ठीक उसके पीछे एक गिद्ध उसके मरने का इन्तजार कर रहा था। उस फोटोग्राफर को यह दृश्य जबरदस्त लगा और उसने उस बच्ची को शूट करने लगा और इसी बीच वह मर गयी।
वह फोटो जब प्रकाशित हुआ तो उसकी बड़ी वाहवाही हुयी। उसके एक दो दिन बाद पत्रकारों ने उससे सवाल करना शुरू किया कि आपने पहले उस बच्ची को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया,उसने जवाब दिया कि मेरी फ्लाइट छूट जाती।
पत्रकारों में एक महिला ने पुछा कि,आप सक्षम थे,आप पहले उस भूखी प्यासी बच्ची की जान बचाते फिर दूसरी फ्लाइट से वापस आ जाते पर आपने भूख प्यास की पीड़ा और जान की की कीमत नहीं समझी। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि उस त्रासदी पूर्ण समय में वहां एक नहीं दो दो गीद्ध थे और उसी रात उस फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर ली।
क्या मानवीय वेदना और त्रासदी की प्रतिक्रिया के बाद कोई आत्महत्या कर लेता है, अधिकांश लोग के भीतर तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती कि वे भूख प्यास की पीड़ा और संत्रास को जानते ही नहीं है। सच को जानने के लिए सच की अनुभूति करनी पड़ती है,सच के मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है तभी सच की सही अनुभूति होती है।
कभी तपती दोपहरी में प्यासे और भूखे रह कर देखिए, सुनसान सड़कों पर चलकर देखिए, हालांकि यह एक प्रयोग होगा, पूर्ण सत्य नहीं होगा, अर्द्धसत्य ही होगा पर कुछ तो अनुभूति होगी। इसलिए जीवन में भूख और प्यास का सम्मान करना सीखें कि भूख और प्यास का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मत पंथ, विचार, सम्प्रदाय आदि नहीं होते,भूख बस भूख होती है। जब कभी कोई भूख प्यास से पीड़ित नजर आवे तो यथा साध्य उसकी सहायता करें कि ईश्वरीय सेवा का यह सर्वोत्तम रुप है।
---------
प्रकृति और गुणधर्म के अनुरूप : जैसी सोच वैसी ख़ोज आलेख : ४३ .
------------
प्रकृति और गुणधर्म के अनुरूप : बीज और विचार की प्रकृति समान होती है हम जमीन पर जैसे बीज बोते हैं, देखभाल करते हैं, खाद पानी देते हैं,उस बीज की प्रकृति और गुणधर्म के अनुरूप ही वो पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है।
विचारों की जन्मभूमि मन है,मन से निकलकर वो विचार आपकी वाणी और कर्म में रुपान्तरित होते रहते
हैं और कहा जाता है कि विचार वाणी और व्यवहार में बड़ा साम्य होता है और इन विचारों पर आपके आहार, विहार, अध्ययन,चिन्तन, मनन आदि के स्पष्ट प्रभाव पड़ते हैं।
अब यहां आहार को समझना आप सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना किस पौधे को कैसा पोषण मिलना चाहिए और उसे यदि वह पोषण नहीं मिलेगा तो पौधे का विकास अवरूद्ध हो जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा वैसे ही आहार आपके जीवन का निर्माण करता है और जीवन का आधार विचार है और विचार से ही संस्कार और संस्कृति बनते हैं। आहार ही विचार है तो फिर सहज ही आपके मन में यह भाव पैदा होगा कि अनाज फल फूल जल आदि ही तो आहार हैं पर सच इनसे कोसों दूर है।
ये सब आहार का एक हिस्सा भर हैं। मूलतः आपके आहार में वे सब चीजें शामिल हैं जिन्हें आप कई तरीकों से ग्रहण करते हैं और वे सब चीजें श्रव्य, द्रष्टव्य, खाद्य,पेय, चिन्तनीय आदि विषय हैं।आप जीवन भर इन्हें ग्रहण करते रहते हैं और एक आदमी यही समझता रहता है कि खाद्यान्न और पेय पदार्थ ही तो आहार हैं पर आप जो दिनभर सुनते, देखते, लिखते, पढ़ते हैं, वे सब आहार ही हैं जो आपके विचारों का सृजन करते हैं।
विचार ही सृजन और विनाश का काम करते हैं चाहे वह निजी जीवन हो या पारिवारिक या सामाजिक या वैश्विक,सब विचारों की ही परिणति है।
सदैव संश्यात्मक और अनिश्चयात्मक : विचार मन से निकलने के कारण ही मन की तरह सदैव संश्यात्मक और अनिश्चयात्मक होते हैं इसलिए वे बुद्धि, हृदय, विवेक, मस्तिष्क और आत्मतत्व से छनकर बाहर आते हैं और छनकर बाहर आते हैं वे शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित होते हैं और जो छनकर बाहर नहीं आते वे कभी रचनात्मक और साकारात्मक नहीं हो सकते हैं इसलिए आहार पर ध्यान देना अनिवार्य हैं जैसे पौधों का भरण-पोषण और संरक्षण और इसे समझना जीवन के लिए जरूरी है।
---------
जीवन को प्रवाहमान बनाए रखें : आलेख : ४२.
---------
प्रवाहमान जीवन : जीवन को प्रवाहमान बनाए रखने का सतत् प्रयास इसलिए करते रहना चाहिए कि जैसे जमा हुआ पानी किसी योग्य नहीं रह जाता है।वह धीरे-धीरे सड़ने लगता है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है,वह गंदे तालाब या पोखर में रुपान्तरित हो जाता है जहां सिर्फ जलकुंभियां ही पनप सकती हैं।
यही जीवन का यथार्थ है कि आप चाहे जिस पद पर आसीन हों,जो भी अवस्था हो, स्वयं को गतिमान रखने की कोशिश करें और यह गतिशीलता ही आपको जीवन्त रखेगी। अब जीवन्तता का अभिप्राय यह नहीं कि आप मैदान में दौड़ते रहें बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि जिस क्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता और क्रियाशीलता है,उसे जीवित रखें, उसमें सक्रियता बनाए रखें। यह सक्रियता आपको सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक रुप में सशक्त बनाए रखने का काम करेगी। परिवार में आपके सदस्य आपसे प्रेरित और ऊर्जावान बने रहेंगे।
आपसे कर्मठता और जीवन्तता की सीख लेंगे। समाज भी आपसे प्रेरित होगा। आप यह न समझेंगे कि अमूक आदमी यह काम करता है और हम उससे कमतर हैं,आपका कमतर होना ही किसी के लिए बेहतर होना है। हर काम अपने आप में श्रेष्ठ होता है।
श्रेष्ठता का सम्मान करें।
समझ और चेतना : सभी जीवित प्राणियों में आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और सिर्फ आप ही सभी जीवित प्राणियों का भला या बुरा कर सकते हैं। आप ही कल्याण या अकल्याण के हेतु बन सकते हैं, शान्ति या अशान्ति के कारण बन सकते हैं, विनाश या विकास के कारण बन सकते हैं और इसका निर्णय करने के लिए परमात्मा ने आपको विवेक सहित इच्छा स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है। अब निर्णय आपके हाथों में है कि आप क्या चयन करते हैं और चयन ऐसा हो कि अंतिम काल में आपको पश्चाताप न करना पड़े कि उस समय प्रायश्चित और पश्चाताप का समय भी न मिलेगा।
शुभ सोंचिए शुभ कीजिए।
--------
शिव सृष्टि का स्वभाव है : आलेख : ४१ .
----------
सृष्टि का मौलिक और प्रथम तत्व शिव : सृष्टि का मौलिक और प्रथम तत्व शिव सृजनात्मक पालक संहारक और कल्याणकारी सत्ता है जिसके भीतर * विखण्डन और संलयन की प्रक्रियाएँ अनवरत और अबाध चलती रहती है और आज इसकी पुष्टि भी स्वीकार कर रहा है जिसे ईश्वरीय कण कहा जा रहा है और अभी तक वही कण चैतन्य समझा जा रहा है।
चिद् बिन्दु का सिद्धान्त भी यही है और इसकी पुष्टि भी करता है। शिव परम चैतन्य कल्याणकारी चैतन्य ऊर्जा और शक्ति के संयुक्त रूप हैं जिसे भारतीय धर्म दर्शन और चिन्तन में अर्द्धनारीश्वर कहा गया है। विश्वात्म चिन्तन में हर पुरूष अर्द्धनारीश्वर ही है जो शक्ति रूपी स्त्री के साहचर्य से सृजन करता रहता है। यह प्रकृति और प्रवृति सभी चेतन प्राणियों में पायी जाती है।
वह विश्वात्मा न तो सृजित है और ना ही सृजन का कारण है कि वह स्वयं में ही कार्य और कारण है। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बड़े मिट्टी के बर्तन में समभाग गोबर और दही को मिलाकर उस हाँडी का मुँह बन्द कर छोड़ दें, एक माह के उपरान्त उसमें से बिच्छु पैदा होने लगेगा। दो या दो से अधिक पुद्गलों का योग एक तीसरे चैतन्य को जन्म देता है।
शिव शून्य है : शिव शून्य है, सत् है असत् भी है, धन है ऋण भी है, काम भी है मुक्ति भी है, ज्ञान है विज्ञान भी है, मन भी है चित्त भी है, क्रोध है क्षमा भी है जीवात्मा है पर ब्रह्म परमात्मा भी है बुद्ध भी है और अर्हत् भी है सृजन लय और विनाश होते हुए इससे परे भी है और अंत में * भैरव है, भरण रवन और वमन करने वाला, काल के उपर विराजने वाला स्वयंभू महाकाल जिसे जानकर भी नहीं जाना जा सकता है कि वह * अज्ञेय है।
--------
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम : सर्वयुग पुरुष : आलेख : ४० .
------------
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम : आज भगवान श्री राम की जयन्ती है जिसे वैश्विक स्तर पर इनके भक्त, श्रद्धावान और अनुगामी एक उत्सव, त्योहार और पर्व के रुप में मनाते हैं। श्री राम सिर्फ एक युग के ही महापुरुष और विभूति नहीं थे, अवतारी ही नहीं थे बल्कि अपने कृत्यों से अकाल पुरुष, सर्वयुग पुरुष,सार्वकालिक और सार्वभौमिक बन गए। उन्होंने समस्त समाज और आधारभूत संरचनाओं के लिए जिन मान्यताओं और मापदण्डों की स्थापना की,उनसे वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। वे अवतारी होने के कारण या हिन्दू समाज के आराध्य होने के कारण नहीं बल्कि हर पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं के पालन और स्थापना करने के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सके।
जयन्ती मनाने के पीछे महती उद्देश्य : आज सिर्फ एशियाई देशों में ही नहीं वरन् वैश्विक स्तर इनकी आराधना साधना और पूजा की जाती है। यहां यह उल्लेखनीय हो जाता है कि आखिर जयन्ती मनाने के पीछे महती उद्देश्य क्या है, जयन्ती मनाने के पीछे वैश्विक समाज को स्मारित कराना होता है कि आज मानव समाज में जो इतनी विकृतियां आयी हैं, रिश्ते अमर्यादित हुए हैं, चहुंओर हिंसा, रक्तपात, शोषण दोहन आदि जो बढ़े हैं उनके पीछे एक ही कारण है कि हमारा समाज स्थापित मर्यादाओं के मापदण्डों को विस्मृत कर गया है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की मर्यादा नष्टप्राय हो चुकी है, इसलिए आज वैश्विक स्तर शत्रुओं के साथ भी मर्यादित व्यवहार : आज भगवान श्री राम की उपयोगिता, उपादेयता और प्रासंगिकता है। माता-पिता, भाई, पत्नी, मित्र, सहयोगी, गुरु,सेवक, भक्त,साधक,आराधक यहां तक कि शत्रुओं के साथ भी उन्होंने मर्यादित व्यवहार किया जिनके सम्मान, पुनर्मूल्यांकन और अनुपालन की आज भी जरूरत है और कल भी रहेगी।
सत्य वही है जो शाश्वत और सनातन है, जिसके गुणधर्म अपरिवर्तनशील हैं, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है और ऐसी ही मर्यादा भगवान श्री राम की है जो किसी मत,पंथ, विश्वास, विचार, सिद्धान्त, सम्प्रदाय आदि से बंधा नहीं बल्कि समस्त मानव समुदाय के लिए प्रासंगिक और उपयोगी है, जिसके सहज और सरल अवलोकन की जरूरत है और समाज को हर अपराध, प्रदूषण, अत्याचार, अनाचार, अपराध आदि से सुरक्षित करने के लिए सबको श्री राम को समझने और अपनाने की जरूरत है,जैसे नीति शास्त्र और आचार शास्त्र होते हैं वैसे ही श्री राम व्यवहार और आचरण हैं जिनका अनुसरण करना जीवन के मोल और मूल्य हैं जिन्हें किसी मत,पंथ, विश्वास, विचार, सम्प्रदाय आदि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए जैसे डाक्टर की जाति और मत आदि हो सकते हैं पर औषधि की कोई जाति,मत,पंथ आदि नहीं होते वही औषधि श्री राम हैं। समस्त मानव समाज को श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाईयां एवं मंगलकामनाऍं
--------
सृजन में द्वैत और अद्वैत आलेख : ३९.
-----------
सृजन शब्द को बोलने और लिखने के पूर्व,यह शब्द सोंच में आते ही एक बात मनो मस्तिष्क में सहज ही उभर कर सामने आती है कि दो के सम्मिलन के बगैर कोई भी सृजनात्मक क्रियाशीलता नहीं हो सकती है। वह दो पदार्थों का सम्मिलन हो या दो जीवों का या दो भावों विचारों का, यह द्वैतवादी क्रियाशीलता है परन्तु इसका उत्पाद एकात्मकता से समावेशित हो जाता है, एकत्व का, का बोध कराता है, अद्वैत हो जाता है।
भौतिक और आध्यात्मिकरूप से यही सत्य है।
दो अणुओं के सम्मिलन से एक नया पदार्थ सृजित होता है। दो विरोधाभासी पदार्थों के सम्मिलन से एक नयी समावेशी रचना होती है। नर मादा के सम्मिलन से एक नया जीव पैदा होता है जिसमें एक ही साथ समावेशी रूप में जो गुण माता पिता के होते हैं , वे स्थूल और सूक्ष्म रूप में संतानों को स्वतःस्फूर्त प्राप्त हो जाते है।
अब इसमें देखने योग्य बातें ये होती हैं कि सभी जीवधारियों में ये गुणधर्म आनुवांशिक होने के साथ-साथ अन्य भौगोलिक और पारिस्थितिकी कारकों से अनुप्राणित और प्रभावित होते हैं जिसके फर्क को न समझने के कारण हमें सर्वत्र नानाविध भिन्नताएँ नजर आती है। इन्हीं भिन्नताओं को समझना
और उसमें एकत्व का बोध होना या करना ही ब्रह्माण्डीय एकात्मकता और सहज एकात्मवाद है।
यही भारतीय जीवन दर्शन और चिन्तन में समावेशित जीवन और उसके सृजन विकास और विनाश की निरन्तरता है। यही शिव शिवत्व और शिव तत्व है जिसे समझना या तो सरल सहज है या अत्यन्त दुष्कर है, विरल है।
इसलिए भारतीय दर्शन और चिन्तन में समावेशित सृजन संचालन और विनाश के भौतिक और आध्यात्मिक समन्वय और सामंजन को समझने के लिए इन चार महासूत्रों को समझना और आत्मसात करना अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य भी है जो प्राचीन भारत से लेकर सम्प्रति भारत के रजकण में व्याप्त है और इसकी स्वीकार्यता सारा संसार मानता हैं। इन चारों महासूत्रों का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक तात्विक और दार्शनि तथा धार्मिक दृष्टिकोण से ही नही है बल्कि इनसे इतर भौतिक नजरिए से भी है।
चार महासूत्रों का अवलोकन : उन चार महासूत्रों का अवलोकन करें, १ .अहम् ब्रह्मास्मि । २ . प्रज्ञानम् ब्रह्म । ३ . तत्वमसी ।४ .अयमात्मन् ब्रह्म । अब इन महासूत्रों को धार्मिक दृष्टिकोण न देखकर * शाश्वत और सर्वव्यापक अर्थों में अवलोकन करें तो एक अद्भुत अनुभूति होगी जो * इलहाम है, अन्तःप्रज्ञा जागरण है, बुद्धत्व है, अरहत्व है, जागृत चैत्तन्य बोध है, ध्यान है, धारणा है , समाधि है और अंत मैं *
वैश्विक मानव एकात्मकता है और इन्ही बोध की जरूरत आज संसार को है और यही चार महासूत्रों को समझकर आत्मसात कर हम संसार को प्रेममय बना सकते है, हिंसा अन्याय शोषण अत्याचार दोहन घात प्रतिघात से मानव समाज की रक्षा कर सकते हैं।
यह कोई * धम्म देसना, धर्म संदेश ,
धर्म प्रेरणा नहीं, जीवन का व्यवहारिक दर्शन है जो संसार के सारे प्रचलित मतों और विश्वासों में समावेशित है। इसी तथ्य को Leo Tolstoy ने ऐसे कहा है कि* we r born as a human being in the world and it is our bounden duty to serve
Man and Mankind.
अगर तुम आदमी के रूप में जन्म लिए हो तो स्वभावतः तुम्हें आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए कि परमात्मा ने इसीलिए तुम्हें आदमी बनाकर धरती पर भेजा है। आज जो भी वैश्विक व्यवस्था है उसका जिम्मेदार कोई अलौकिक सत्ता नहीं, लौकिक सत्ता है।
----------
समय तू धीरे धीरे चल : आलेख : ३८.
------------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
समय की चर्चा : समय के बारे में हम सोते जागते चर्चा करते रहते हैं पर समय के सम्मुख रहते हम समय के मोल और मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। समय ही हमारे सम्पूर्ण जीवन का नियामक निदेशक और नियंत्रक हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम ही सबकुछ कर रहे हैं,पर सत्य तो यह है कि हम समय चक्र में सबकुछ करते रहते हैं। अब एक सवाल उठता है कि अगर समय ही सबकुछ करता और करवाता है तो हम क्या करते हैं। इसका जवाब यह है कि परमात्मा ने हमें इच्छा स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य का अधिकार देने के साथ साथ बुद्धि और विवेक भी दिया है जिसके हिसाब से हमें विचार सृजन करके विवेक सम्मत तरीके कार्यान्वित करना होता है पर अधिकांश समय में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और तब समय की प्रतिकूलताओं का असर हमारे कार्यकलापों पर पड़ने लगता है। हमारे मस्तिष्क की चैतन्य शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि उसका प्रयोग करके इच्छा सृजन करने पर कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जिसपर कालान्तर में हमें पश्चाताप करना पड़े परन्तु यही विपरीत होने पर समय भी विपरीत हो जाता है और मनुष्य मोह, स्वार्थ,क्षणिक सुख आदि विकारों से ग्रसित होने लगता है और इच्छाओं का रुपान्तरण वैसे ही कर्मों में होने लगता है जिसके अच्छे बुरे परिणाम समय पर भोगना पड़ता है। समय की सत्ता अद्भुत है : समय की सत्ता अद्भुत है, जिसके भी दो पक्ष होते हैं या तो समय बिगड़ता है तब बुद्धि भ्रष्ट होती है या बुद्धि भ्रष्ट होती है तब समय बिगड़ता है। इसलिए यह आकलन करना जरूरी हो जाता है कि समय कैसा चल रहा है और इसकी अनुभूति सबको होती रहती है। ऐसी परिस्थितियों में यह देखना जरूरी हो जाता है कि हम समय की गति और चक्र का गंभीरता से अवलोकन करें,यदि समय का चक्र उल्टा चल रहा हो तो बड़ी सोंच समझकर कोई निर्णय लेना चाहिए और समय का चक्र ठीक और अनुकूल हो तो सब निर्णय फलदाई हो जाते हैं इसलिए कहा भी गया है कि समय के चक्र के सही चलने पर मिट्टी भी छुने पर सोना हो जाती है और विपरीत होने पर सोना भी मिट्टी में बदल जाता है।
नेपोलियन : समय की सत्ता : एक विचित्र परन्तु सच्ची घटना नेपोलियन के जीवन की है। वह रुस पर हमले की योजना बना रहा था। उसके मौसम विज्ञानियों ने बताया कि हिमपात एक माह के बाद होगा पर जब उसकी सेना रुस पहुंची तो हिमपात पन्द्रह दिनों पूर्व ही शुरू हो गया और उसकी आधी सेना भूख और ठंड से मर गयी कि रुसी सेना जो अनाज ले जा सके ले गए और शेष को जला दिया था और यही वाटरलू के युद्ध में उसके भयानक पराजय का कारण बना।
यही काल या समय की गति है कि सब अचानक से उलट पुलट हो जाता है हालांकि यह अवस्था द्वन्द्वात्मक है कि नेपोलियन का निर्णय ग़लत था कि उसके काल की गति विपरीत थी। पर एक बात सत्य है कि समय और हमारे बुद्धि विवेक में बड़ा गहरा सम्बन्ध है। अगर हम विवेक सम्मत भी चल रहे हों और काल विपरीत हो जाए तो एक चीज हमें मिलती है कि हमें स्वयं पर पश्चात्ताप नहीं होता कि हम गलत थे,शायद काल का यही निर्णय था और विवेकहीनता हमें पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए काल को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।
इसलिए काल और बुद्धि विवेक में सम्यक् समन्वय करके चलना चाहिए ताकि हमें स्वयं पर पश्चात्ताप नहीं करना पड़े।
--------
दान : सम्पादकीय : आलेख : ३७
-----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
दान एक छोटा सा शब्द है पर इसकी महिमा महान है।इसके भीतर असल में मानवीय दृष्टिकोण है जिसे तथाकथित कर्मकाण्ड का आवरण ओढ़ा दिया गया है जिसे लोग कई रुपों में अंगीकार करते हैं। मूलतः सभी मत पंथों आदि में इसे पूण्य से जोड़कर ही देखा जाता है और यह भी सत्य है कि यही भाव अनुप्रेरक तत्त्व का काम करता है।सब लोग आमतौर पर इसी नजरिए से दान देते हैं कि परमात्मा खुश होंगे और इससे सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मरणोपरांत इसका लाभ मिलेगा।
दान की महिमा : प्राचीन काल से दान की महिमा रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ आदि के दान से धर्मशालाएं,पूजा स्थल आदि बनवाए जाते रहे हैं जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। परन्तु दान वही है जो आपके देने लायक है और प्रदर्शन के परे है। बाईबल कहता है कि दान ऐसे दो कि बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को पता न चले।
राजा हरिश्चन्द्र : दान का यह भाव दुर्लभ : राजा हरिश्चन्द्र ने स्वप्न में अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान देते देखा और विश्वामित्र को सब दान में देकर स्वयं निकल गए। दान का यह भाव दुर्लभ है और मात्र उदाहरण बनकर रह गया है।
आज लोग दान देकर अखबार और खबरों में बना रहना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति छोटे बड़े सबमें व्याप्त है। दान या सहयोग वास्तव में यह कहता है कि जो परमात्मा ने आपको दिया है और जो बांटने योग्य है,उसे जरूरतमंदों के बीच जरूरत के हिसाब से जरूर बांटिए,धन है, वस्त्र है,अन्न है, ज्ञान है,बल और सामर्थ्य है या जो भी संसाधन आपके पास है,जरुर बांटिए और अपेक्षा रहित होकर बांटिए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपके अच्छे बुरे कर्म आपके साथ परछाइयों की तरह चलते हैं जो समय पर फलते हैं।
कर्म वास्तव में बीजरुप होते हैं जिसे सब बोते रहते हैं और उसके फलाफल को आपको ही भोगना पड़ता है, इसलिए दान को एक बंधित कर्म की तरह करते रहिए कि वह संसाधन आपके पास है और इसे दिखावा , प्रदर्शन आदि से बचाइए।
तथागत बुद्ध की एक बड़ी रोचक कथा : इस सन्दर्भ में तथागत बुद्ध की एक बड़ी रोचक कथा है। भगवान बुद्ध एक बार वर्षावास के लिए राजगृह पहुंचे और राजगृह की सड़कों पर बोलने लगे कि, है कोई दाता जो मुझे दान दे। सम्राट से लेकर नगर सेठ तक बड़े बड़े थालों में हीरे मोती स्वर्ण सिक्के आदि लेकर पहुंचने लगे। तथागत ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए बढ़ते चले गए। लोग हतप्रभ रह गए और इसे नहीं समझ सके कि भगवान बुद्ध ने लेने से इन्कार क्यों कर दिया। फिर बुद्ध ने कहा कि, मैं तो समझ रहा था कि मगध की राजधानी दानियों से भरी हुई है पर यह तो निर्धन है और वे बढ़ते चले गए।
स्त्री के दान में प्रदर्शन नहीं : वे धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे थे कि बांसों के झूरमुट से एक कमजोर और धीमी आवाज आयी, हे भगवन, ठहरिए,मेरे पास दान देने के लिए जो है उसे देने के लिए मैं सम्मुख नहीं आ सकती।
बुद्ध ठहर गए और तभी झूरमुट की ओट से स्त्रियों के पहनावे का एक अधोवस्त्र आकर गिरा। भगवान बुद्ध ने देखा और गंभीर होकर उसे उठाया और भावपूर्ण तरीके से उसे सर पर धारण कर लिया और नाचने लगे। नाचते नाचते उन्होंने कहा, राजगृह दानियों से खाली नहीं है। लोगों ने इस दृश्य को देखा पर समझ नहीं पाए कि हम तो इन्हें अपार धन दे रहे थे पर इन्होंने एक अधोवस्त्र को सर का मुकुट बना लिया। इस भाव को स्पष्ट करते हुए तथागत सिद्धार्थ ने कहा कि, उस स्त्री के दान में प्रदर्शन नहीं था और उसने अपना सर्वस्व ही दान कर दिया। धन्य है यह पवित्र धरती और धन्य है वो दानदाता जिसने दान की महिमा की रक्षा कर ली।
अब आप समझने की कोशिश करें कि दान का अर्थ निस्पृह भाव से दान करना होता है जिसमें अपेक्षा और प्रदर्शन नहीं होता है। आप देखेंगे कि आज भी कितने श्रद्धावान लाखों करोड़ों का गुप्त दान देते रहते हैं।
इसलिए जो आपके पास जो है और दे सकते हैं तो देते रहिए।
---------
सत्य वह नहीं जो हम सम्पादकीय : आलेख : ३६
----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
सत्य वह नहीं : मनन चिन्तन और विश्लेषण की आवश्यकता : सत्य वह नहीं जो हम पढ़ते,लिखते, सुनते या बोलते हैं क्योंकि सत्य तो वही है जो सबके लिए ग्राह्य हो और जिसका बोध निरपेक्ष हो।हर व्यक्ति अपने भोगे हुए यथार्थ, पढ़े हुए विषय,देखे हुए दृश्य और सुने हुए विषय को ही समझता है जो प्रायः सापेक्ष ही होता है तब आप कैसे समझेंगे कि यही सत्य है तो आपको उन तथ्यों का मनन चिन्तन और विश्लेषण करना होगा और उनकी तह तक जाना होगा और तभी आप सत्य को जान पाएंगे।
कोई व्यक्ति यह कह दे कि मैंने मीठा करैला खाया है, कोई कह दे कि मैंने जो गन्ना खाया वह खट्टा था। आपको सहज ही विस्मय होगा कि करैला न तो मीठा हो सकता है और न गन्ना खट्टा हो सकता है चूंकि आपने भी उनके स्वाद चखे हैं और आपको भी उनके स्वाद की पूर्वानुभूति रही है तो दूसरे ने कहा और आपने भी सहमति दी, निस्संदेह वह सत्य है।
इस तरह कोई कथन, कोई दृश्य, कोई श्रव्य कथन सिर्फ पहले पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपका साक्षात्कार जब उसे अन्दर से स्वीकार कर लेता है और उसके समर्थन में अन्य साक्ष्य भी होते हैं तो उसका भाव सापेक्ष से निरपेक्ष हो जाता है।
--------
मानना और जानना : सम्पादकीय : आलेख : ३५ .
----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
स्वयं को जानने फिर मानने का ही मोल और मूल्य होता है। जो जानेगा ही नहीं वो मानेगा कैसे और मानेगा तो महज दृष्टिभ्रम होगा, मतिभ्रम होगा और ऐसी अवस्था विक्षिप्तावस्था की होती है और वह ऐसी अवस्था में सिर्फ प्रलाप भर कर सकता है, कोई आर्ष वाणी नहीं बोल सकता है।* When a rational talks, talks with intuition not in vague. He talks what is * right and just.
सिद्धार्थ ने पहले खुद को जाना : सिद्धार्थ ने पहले खुद को जाना, माना और फिर संसार ने इस तथ्य और सत्य को सहजता से स्वीकार कर लिया कि सिद्धार्थ कोई अवतारी पुरूष नहीं थे, शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित चेतना थे। ये बात अलग है कि आमजन की भाषा में उन्होने * आत्मा और ईश्वर की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया पर सीधे सीधे अस्वीकार भी नहीं किया। उनके चिन्तन में * चित्त और उसकी वृत्तियाँ ही आत्मा है और ईश्वर अव्याकृत सत्ता है अर्थात् उसकी स्पष्ट व्यख्या नहीं की जा सकती है। उन्होने * आत्मबोध की प्राप्ति की, अपने स्वचैतन्य बोध और अन्तःप्रज्ञा को जागृत किया और जगत ने * भगवान मान लिया, ध्यान रहे, भगवान कोई भी हो सकता है, अरहत्त्व की प्राप्ति कोई भी कर सकता है पर उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता है। तथागत का सम्पूर्ण चिन्तन * आत्मबोध आत्मचैतन्य और अन्तःप्रज्ञा के जागरण की अवस्था पर आधारित है। मानवमात्र जीवमात्र के सर्वार्थ कल्याण पर आधारित है जिसे * total goodness , right and just कहा जाता है जो हमारे औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन में समावेशित तथ्य* शिवत्व का है। जिसके हृदय में बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण स्थावर जंगम के लिए सम्पूर्ण कल्याण का भाव हो * शिव है कि शिव का अर्थ ही सर्वार्थ कल्याणकारी सत्ता होता है।
सभी कल्याणकारी सत्ता को नमन करना ही शिव और शिवत्व को जानना है जो मत पंथ विश्वास विचार आदि का मूल है। ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताएँ मानने की नहीं जानने का विषय है कि जान कर
मानने का ही मोल और मूल्य है। मानकर तो संसार युगों से चलता आ रहा है और चलता भी रहेगा पर जिसने अंश भी जानने की कोशिश की, उसने तथ्य और सत्य को जान लिया। ये बात अलग है कि तथ्य और सत्य को कभी समग्रता में नहीं जाना जा सकता है। सत्य का अस्तित्व बना रहता है, चारो तरफ बिखरा रहता है जैसे सौर रश्मियों का विकिर्णण होता रहता है और जब उसे एकीकृत और समन्वित किया जाता है तो उससे अग्नि ऊर्जा का सृजन होता है और वैसे ही सत्य भी है। अग्नि का जलना सृजन और विनाश दोनों का काम करती है वैसे ही सत्य का भी अस्तित्व है,यह चेतना की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है पर वह कभी पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है कि पूर्ण और परम सत्य ब्रह्म की सत्ता है जो * प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न दोनों होता है।यह सत्य है और भौतिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि मनुष्य के भीतर फैले अनन्त कोशिका जाल से निर्मित * मन हृदय और मस्तिष्क में समावेशित ऊर्जा का स्थूल और सूक्ष्म रूप है। मन का स्थूल रूप मनुष्य है। हृदय और मस्तिष्क के स्थूल रूपों को तो सहज ही देखा जा सकता है परन्तु उन तीनों के सूक्ष्म रूप को संसार का कोई भी विज्ञान कभी नहीं दिखा सकता है। प्राण है, जीवन का मूलाधार है, चेतना का सर्वोच्च रूप है पर कोई विज्ञान कभी नहीं बता सकता कि प्राण क्या है जैसे आप बोलचाल की भाषा मे बोलते हैं कि हम उसे दिल से चाहते हैं, वह हमें प्राणों से भी प्यारा है अर्थात् हृदय और प्राणों की तरह अनमोल है कि उसके बगैर जीवित नहीं रहा जा सकता है।
सत्य को जो किसी का सत्य हो, किसी व्यक्ति या विषय या सिद्धांत का सत्य हो, समग्रता में कभी नहीं देखा जा सकता है बस देखने की कोशिश भर की जा सकती है। लिविंगस्टोन कहता है, *even the most powerful telescope when observes the cosmological object in the universe, it can observe only the face part if the object and half of the same is always hidden.
और यही यथार्थ जीवन और जीवन से भरे संसार का है। जब आप किसी व्यक्ति/ विषय/ सिद्धान्त आदि का अवलोकन और मूल्यांकन करते हैं तो उसी टेलिस्कोप की तरह करते हैं और उनका एक ही हिस्सा देख पाते हैं और कहते हैं कि हम उसके बारे में सबकुछ जानते हैं और यही दशा * दृष्टिभ्रम और मतिभ्रम की होती है जिससे आपको बचने की जरूरत है।
निष्कर्षतः कोई भी सत्य कभी पूर्ण रूप से दृष्टिगत नहीं हो सकता है, प्रच्छन्न सत्य तो सदैव आवृत ही रहता है। ब्रह्म परम सत्य है पर समग्रता से कोई नहीं बता पाया है कि वह क्या है कि वह अज्ञेय सत्ता है और जिस दिन किसी का उससे साक्षात्कार हो गया, जल जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा कि समस्त संसार अब तक उसका अंश ही जान पाया है। संसार के समस्त धर्म दर्शन और चिन्तन में समावेशित तथ्य यही है कि कालखण्डों में युगधर्म की मांग के अनुरूप उसकी अलग-अलग व्याख्या होती रही है पर अज्ञेय के सत्य की समग्र व्याख्या कैसे की जा सकती है।
उसे न तो नकारा जा सकता है और न समग्रता में स्वीकारा जा सकता है। * सदं एकः विप्रा बहुधा वदन्ति( सत्य हक ईमान और न्याय तो एक ही पर विद्वत् जन अपनी अपनी अनुभूतियों से इसकी व्याख्या अलग-अलग करते हैं।
आप भी जब कभी किसी का आकलन मूल्यांकन करें तो दृष्टि द्रष्टा और दृश्य को समेकित और समन्वित करके करें, भूल की संभावनाएँ न्यूनतम होंगी और आपको खुशी और शान्ति की अनुभूति होगी।
----------
मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति. सम्पादकीय : आलेख : ३४ .
-----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
परमात्मा और प्रकृति ने संसार में समस्त मनुष्यों को समान शारीरिक आधारभूत संरचनाओं से संवारा है अर्थात् बाह्य संरचना भिन्न होते हुए भी मूल बनावट एक ही है समान
ज्ञानेन्द्रियां और समान कर्मेंद्रियां,रंग रुप भौगोलिक कारणों से भले ही भिन्न हो शेष सब समान ही होते हैं।
अब जब उनके स्वभावगत गुण दोषों की बात होती है तो वह भी समान ही दिखाई देते हैं जो जीव जगत के तीन प्राणियों से मेल खाते हैं,वे हैं मधुमक्खी और मकड़ी।
मकड़ी अच्छे फूलों से भी विष
चुस लेती है और मधुमक्खी जहरीले फूलों से भी अमृत चुस लेती है,वैसे ही श्रेष्ठ प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग बुराईयों से भी अच्छी चीजें निकाल लेते हैं और निकृष्ट प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग अच्छी चीजों में भी बुराई ढुंढने का काम करते हैं।
यह संसार का व्यवहार और संस्कार है। हर व्यक्ति में अच्छाईयों और बुराईयों का मिश्रण होता है, कोई भी ऐसा नहीं जो परिपूर्ण हो तब श्रेष्ठ गुणधर्म यह है कि मनुष्य को मधुमक्खी की प्रकृति और प्रवृत्ति अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सर्वत्र अच्छाईयों का ही चयन कर सके और श्रेष्ठ बन सके। संखिया एक प्रकार का तीव्र जहर है जिससे अनेक औषधियां बनती हैं पर वह मूलतः जहर है,अब आप पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल किस रुप में करना चाहेंगे,जहर के रूप में या औषधि के रूप में,जो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है।
----------
सौन्दर्य और हमारी दृष्टि. : अलग अलग : आलेख : ३३.
-----------
सौन्दर्य और हमारी दृष्टि : अलग अलग : इस ब्रह्माण्ड में सौन्दर्य की कोई कमी नहीं, सर्वत्र सुन्दरता बिखरी हुयी है पर सबके अवलोकन के दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं। जिस व्यक्ति के जो भाव विचार होते हैं उसी दृष्टिकोण से वह सौन्दर्य की तलाश करता है। किसी को सुन्दर पुरुष या स्त्री में सौन्दर्य नजर आता है तो किसी को खुबसूरत फूल या प्राकृतिक आधारभूत संरचनाओं में सौन्दर्य नजर आता है आता है तो किसी को सुन्दर भवन आकर्षित करता है।
कोई सुन्दर गीत संगीत को सुनकर भाव विभोर हो जाता है तो कोई सुन्दर साहित्य,लेखन, मूर्ति कला, वास्तुकला, संभाषण आदि में सौन्दर्य की तलाश करता है और अपने दृष्टिकोण से उसे पाकर खुश हो जाता है, संगीत के बारे में तो कहा भी गया है कि जो हृदय संगीत की लहरों से विचलित न हो वह आदमी हृदय विहीन होता है,वह आदमी हो ही नहीं सकता है।
श्री कृष्ण के दर्शन से ज्यादा सुन्दर क्या होगा : रुक्मिणी. राधा. मीरा. : कोई रुक्मिणी, राधा , मीरा और गोपियों से पुछे कि सौन्दर्य क्या है ? सब जानते है उनका जवाब क्या होगा ? कोई मीरा, रसखान ,बिहारी या सूरदास से पुछे कि सौन्दर्य क्या है,तो एक ही जवाब होगा,श्री कृष्ण के दर्शन से ज्यादा सुन्दर क्या होगा ? कोई हनुमान जी से पुछे कि इस ब्रह्माण्ड में सबसे सुन्दर क्या है तो जवाब होगा श्री राम,इस तरह सौन्दर्य तो एक ही है जो समस्त पदार्थों में समाहित है पर नजरें तो अनन्त हैं इसलिए सौन्दर्य के स्वरूप बदल जाते हैं, पर सेनेका कहता है कि इस दुनिया में खुबसूरत नजारों की कमी नहीं है परन्तु सबसे खूबसूरत नजारा किसी आदमी को एकदम विपरीत परिस्थितियों में न हार मानते हुए जूझते हुए देखना है,आप इससे कितना सहमत हैं।
कृष्ण के दर्शन व उनके व्यक्तित्व में अटूट विश्वास रखने वाले अनन्य भक्त भी कहते है ,
'हे माधव ! यदि आप मेरे जीवन के सारथी हो जाए तो मैं किसी ऐसे नूतन विश्व का निर्माण कर ही लूंगा
जिसमें मात्र अनंत ( श्री लक्ष्मीनारायण ) शिव ( कल्याणकारी ) शक्तियाँ ही होगी
होलिका की अग्नि में मेरे अंतर्मन की चिर ईर्ष्या, पीड़ा ,द्वेष ,और बुराई जलकर भस्म हो.....
हे : परमेश्वर : आदि शक्ति : जीवन के इस अंतहीन सफ़र में तू मुझे मात्र ' सम्यक साथ ' प्रदान कर जिससे मेरी ' दृष्टि ' , ' सोच ' ,' वाणी ', और ' कर्म ' परमार्जित हो सके...'
जिन्दगी एक अनवरत संघर्षों की गाथा है : हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी नजरें उतनी खुबसूरती नजर आती है। पर जिन्दगी जो एक अनवरत संघर्षों की गाथा है जिसमें कोई संसाधनपूर्णता में संघर्ष करता है तो कोई संसाधनहीनता में भी संघर्ष करता नजर आता है। कविवर निराला जी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती, संघर्ष करती औरत में जो सौन्दर्य नजर आता है,वह अप्रतिम सौन्दर्य है।
स्तंभ संपादन : सौन्दर्य और हमारी दृष्टि. : अलग अलग :
शक्ति.सम्पादिका. डॉ. नूतन
लेखिका. देहरादून : उत्तराखंड
-----------
आन्तरिक चेतना का जाग जाना : मौन : सम्पादकीय आलेख : ३२.
-----------
मौन शब्द मन से जुड़ा है अर्थात् मन का अभिव्यक्त हो जाना या न होना,ऐसी अवस्था की दो प्रकृति होती है,बाहर से मौन होना और भीतर से मौन होना।भीतर से मौन होना या हो जाना एक दुर्लभ गुण है परन्तु बाहर से मौन होना या हो जाना झूठ से भी जहरीला होता है।
मन की आन्तरिक चेतना का जाग जाना : मौन,मन की आन्तरिक चेतना का जाग जाना है जो गहन साधना की उपलब्धि है। जो व्यक्ति संसार और सांसारिक जीवन के सत्य और रहस्य को समझ लेता है,वह अनर्गल प्रलाप नहीं करता,बस चुप हो जाता है,मौन हो जाता है। उस व्यक्ति के मौन की अवस्था पलायन या मूक होना नहीं है बल्कि वह जब संवाद करता है तो तथ्य तर्क और सत्य से परे नहीं होता,उसके संवाद सोने से खरे, अग्नि की तरह प्रज्वलित होते हैं। वह मौन रहने का कोई हेतु नहीं रखता है। परन्तु ठीक इसके विपरीत कुछ लोग मौन होने, रहने का दिखावा करते हैं और किसी सिद्धान्त से प्रतिबद्धता की बात करते हैं,ऐसा मौन बड़ा घातक होता है जिसके परिणाम विनाशकारी होते हैं।
कुरु सभा : भीष्म पितामह, विदूर और धृतराष्ट्र का मौन : मन को साधकर मौन होना एक बड़ा गुण है जो उचित समय पर समर्थन और विरोध कर सकता है परन्तु विषम परिस्थितियों में मौन रह जाना एक विनाश को आमंत्रित करना है।
कुरु सभा में द्रौपदी पर हो रहे अत्याचार पर भीष्म पितामह, विदूर और धृतराष्ट्र का मौन रह जाना ऐसा ही मौन था जिसमें धृतराष्ट्र पुत्र मोह और भीष्म तथा विदूर राजधर्म से बंधे हुए थे पर धर्म सत्य और न्याय के रक्षार्थ वे अपना मौन त्याग न कर सके जिसने विनाशकारी महाभारत युद्ध को जन्म दिया।
यह प्रसंग आज भी सच है जो निजी पारिवारिक जीवन से लेकर वैश्विक स्तर तक द्रष्टव्य हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हो रहे गलत या अन्याय का हम विरोध नहीं कर पाते हैं जो कई कारणों से बंधे होते हैं। हम या तो निजी हितार्थ चुप रह जाते हैं,भय से चुप रह जाते हैं, अशांति के भय से चुप रह जाते हैं, सम्बन्धों के खराब होने के भय से चुप रह जाते हैं या विवादों में पड़ने आदि के कारण मौन रह जाते हैं जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है।
परमेश्वर की वाणी सच को सच और झूठ को झूठ : यह सत्य है कि व्यवहार में मौन को तोड़कर गलत का विरोध और सच का समर्थन करने के लिए स्वयं का सही होना और आत्मबल आत्मविश्वास का होना बड़ा जरुरी होता है। वही व्यक्ति सच का समर्थन और ग़लत का विरोध कर सकता है जो भीतर से मौन हो जाता है,जो निर्विकार और निर्विकल्प होता है,उसे पंच के आसन पर बैठे परमेश्वर की वाणी बोलनी पड़ती है,उस परिस्थिति में वह किसी का न तो मित्र होता है और न अमित्र होता है,
यहां मुंशी जी की कहानी पंच परमेश्वर को स्मरण करने की जरूरत है जहां अलगू चौधरी,जूम्मन शेख का परम मित्र होते हुए भी अपने मौन को तोड़कर न्याय का पक्ष लेते हुए बुढ़ी मौसी को न्याय दिलाने का काम करता है और इसका मूल्यांकन कालान्तर में जूम्मन शेख भी करता है।
सच को सच और झूठ को झूठ कहने की क्षमता उन्हीं के पास हो सकती है जो भीतर से मौन हो जाते हैं, प्रलाप नहीं करते हैं और जो ऐसे गुण को विकसित कर लेते हैं वे ही युगधर्म नहीं बल्कि शाश्वत धर्म का पालन करना जान जाते हैं। सच तो हर हाल में सच ही रहता है चाहे हम मौन रहें या मुखर रहे, इसलिए भीतर से मौन रहने का सतत् प्रयास करना चाहिए।
--------
बोध कथा और अनुभूति : सम्पादकीय आलेख : ३१ .
--------
बुद्ध के उपदेश : उपयोगिता और उपादेयता : तथागत बुद्ध के उपदेशों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनके उपदेश सिर्फ उपदेश नहीं वरन् जीवन के व्यवहार थे जिनकी उपयोगिता और उपादेयता सार्वलौकिक और सार्वकालिक है।
एक बार तथागत सिद्धार्थ अपने प्रिय शिष्य आनन्द के साथ एक वन मार्ग से गुजर रहे थे और वे मार्ग के वृक्ष, वनस्पतियों, जीव जन्तुओं, चट्टानों आदि को नमन भी कर रहे थे। बीच बीच में किसी सुन्दर और फलदार वृक्ष को देखकर रुक जाते और बड़े भावपूर्ण तरीके से उसे स्पर्श करते और अपनी आंखें बंद कर लेते।
यह सब देखकर आनन्द को बड़ा विस्मय हो रहा था और जब उसकी जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गयी तो उसने पुछ ही लिया, हे भन्ते,ऐसा आप क्यों कर रहे हैं,
बुद्ध एक बड़ी सी शिला पर बैठ गए और आनन्द को भी बैठने का संकेत किया और कहा कि, हे आनन्द, हमारी बातों को ध्यान से सुनो, हम सभी मनुष्य जो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं उनके लिए मंगलकामनाएं करते रहते हैं, यहां तक कि जिन्हें नहीं जानते, भेंट हो जाने पर अभिवादन और मंगलकामनाएं करते हैं।
 सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं : लेकिन हमारी सोंच कहती है कि समस्त संसार में हमें सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं करते रहनी चाहिए। इस संसार की रचना सभी जड़ चेतन के मिलने से हुयी है, हम सभी एक दूसरे से अविच्छिन्न रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। हमारा अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। वृक्ष हमें फल फूल छांव लकड़ियां आदि देते हैं।वन्य प्राणियों को भोजन और आश्रय देते हैं। वन जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी जरूरी हैं। नदियां झरनें पहाड़ वनोत्पाद आदि सभी जीवधारियों के लिए जरूरी हैं। हमारे जीवन के लिए जो जरूरत और जरुरी है,उनकी रक्षा यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा इसलिए हम सबके प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं और इनके लिए मंगलकामनाएं करते रहते हैं कि ये सुरक्षित रहें और इनका संवर्धन होता रहे। आनन्द मौन भाव से सुन रहा था और बुद्ध के प्रति नतमस्तक होकर कहा,हे भन्ते,आपका जीवन दर्शन कितना महान और व्यवहारिक है जिसे सबको समझकर आत्मसात करना चाहिए ताकि जीवन मोल और मूल्य बने रहें और समस्त मानव समाज अपने अस्तित्व में बना रहे।
सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं : लेकिन हमारी सोंच कहती है कि समस्त संसार में हमें सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं करते रहनी चाहिए। इस संसार की रचना सभी जड़ चेतन के मिलने से हुयी है, हम सभी एक दूसरे से अविच्छिन्न रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। हमारा अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। वृक्ष हमें फल फूल छांव लकड़ियां आदि देते हैं।वन्य प्राणियों को भोजन और आश्रय देते हैं। वन जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी जरूरी हैं। नदियां झरनें पहाड़ वनोत्पाद आदि सभी जीवधारियों के लिए जरूरी हैं। हमारे जीवन के लिए जो जरूरत और जरुरी है,उनकी रक्षा यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा इसलिए हम सबके प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं और इनके लिए मंगलकामनाएं करते रहते हैं कि ये सुरक्षित रहें और इनका संवर्धन होता रहे। आनन्द मौन भाव से सुन रहा था और बुद्ध के प्रति नतमस्तक होकर कहा,हे भन्ते,आपका जीवन दर्शन कितना महान और व्यवहारिक है जिसे सबको समझकर आत्मसात करना चाहिए ताकि जीवन मोल और मूल्य बने रहें और समस्त मानव समाज अपने अस्तित्व में बना रहे। सबके प्रति अनुग्रह और उपकार के भाव : अब इस कथा को समझने की जरूरत है कि हमें सबके प्रति अनुग्रह और उपकार के भाव क्यों रखने चाहिए कि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की जरूरत है। निहितार्थ स्वार्थ और अहंकार नाकारात्मक प्रतिस्पर्धा के कारण बनते हैं जिससे तनाव और संघर्षों का जन्म होता हैं और जीवन दुखमय हो जाता है। इस तथ्य को समझने की जरूरत है ताकि जीवन सुखमय हो। हमें सबके प्रति मंगलकामनाएं करते रहना चाहिए।
सबके प्रति अनुराग और अनुग्रह का भाव रखना चाहिए कि मित्रता का भाव सदैव गुणकारी होता है और अमित्रता सदैव हानिकारक होता है। हम अमित्र होकर जन्म नहीं लेते बल्कि सबके प्रति मैत्री भाव ही रहता है जो कालांतर में निहित स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि के कारण अमित्र भाव में रुपान्तरित होते रहता है जो दीर्घायु नहीं होता और अमित्र भाव सृष्टि का गुणधर्म नहीं है। आप यदि सबके प्रति मंगलकामनाएं करते रहते हैं तो आपके प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्वत: स्फूर्त होती रहती है। इसलिए सभी जड़ चेतन के प्रति अनुराग और अनुग्रह का भाव रखना चाहिए कि अंतिम सत्य यही है।
--------
मनुर्भव अर्थात् मनुष्य बनो : सम्पादकीय आलेख : ३० .
-------------
हिन्दू जीवन दर्शन और चिन्तन अद्भुत है जिनमें सिर्फ सिद्धान्त और दर्शन नहीं वरन् सांसारिक व्यवहार भी होता है जिसे वेदों के अतिरिक्त उपनिषदों, गीता, रामायण और महाभारत में देखा जा सकता है।
वेदों में जिस मानवीय चेतना की बात कही गयी है,वह कितना महत्वपूर्ण है, विवेचना का विषय है। मनुष्य जन्म तो लेता है, मनुष्य के रूप में परन्तु मनुष्य होने की जो वांछित शर्तें हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है जिसकी अनुभूति उस कालखंड के मनीषियों को हो चुकी थी इसलिए ऋग्वेद में कहा गया कि,
मनुर्भव अर्थात् मनुष्य बनो : मनुर्भव अर्थात् मनुष्य बनो। एक छोटे से शब्द में कितने अर्थ छिपे हुए हैं विश्लेषण का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि मनुष्य बनों। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य की चेतना इस प्रकार कैसे जागी कि मनुष्य होना कुछ और है, मात्र मनुष्य योनि में जन्म लेने से मनुष्य, मनुष्य नहीं हो सकता है बल्कि मानवोचित गुणों के धारण किए बगैर वह मनुष्य नहीं हो सकता है। दया,प्रेम करुणा,क्षमा, त्याग, अहिंसा, परोपकार,सत्याचरण आदि गुणों के धारण किए बगैर एक व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता है।
वैसे हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिशोध, घृणा आदि दुर्गुण भी मनुष्य में स्वभावगत सम्मिलित हैं और इन्हीं के नियंत्रण के लिए बुद्धि और विवेक भी दिया गया है जिनके प्रयोग से इनके औचित्य और अनौचित्य का निर्णय किया जा सके कि कब क्या जरुरी है परन्तु हर परिस्थितियों में मानवोचित गुणधर्मों का पालन करना ही मनुष्य होना है। इस विषय की विशद् व्याख्या रामायण महाभारत गीता और उपनिषदों में की गयी है जिन पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है कि उन शास्त्रों में अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग तर्क और व्याख्या दिए गए हैं, मैं यहां सिर्फ एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगा। महाभारत के शान्ति पर्व में एक प्रसंग आता है जिसमें राजा रंती देव कहते हैं,
नत्वहम् कामये राज्यम् न सुखम्
न मोक्षम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम्
कामये दुःख तप्तानाम् प्राणीनार्ति दुःख नाशनम्
हे परमात्मा, मुझे ने राज्य की कामना है,न सुख न स्वर्ग न मोक्ष न पुनर्जन्म की कामना है लेकिन जब भी मेरा जन्म मनुष्य के रुप में हो तो उनके दुःख निवारण के काम आ सकुं और मेरे जीवन का ध्येय और लक्ष्य यही हो।
धर्म न्याय और सत्य से अनुप्राणित और अनुप्रेरित हों : आज अगर वैश्विक स्तर पर इस श्लोक के भाव में अन्तर्निहीत भावों को समझकर आत्मसात करने की कोशिश भर की जाए जो पारिवारिक जीवन से लेकर वैश्विक स्तर तक के सांसारिक जीवन में मनुष्य होने की भावना का सृजन हो और जीवन मानवोचित संस्कार और संस्कृति से परिपूर्ण हो जाए और जितने भी प्रकार के संघर्ष और द्वन्द् हों स्वत: स्फूर्त तिरोहित हो जाएं पर यह व्यवहारिक होते हुए भी कठिन है कि इसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा निज का अहंकार है कि हम मनुष्य छोटी से छोटी बातों में भी अहंकार को आड़े ले आते हैं कि हम उससे कौन कम हैं जो उसके सामने झुकूं और यहीं से संघर्ष और तनाव के जन्म होते हैं जो सदैव विनाश के कारण बनते हैं।
तब आप सवाल खड़ा करेंगे कि आखिर रामायण और महाभारत काल में इतने बड़े बड़े युद्ध क्यों हुए और आज भी क्यों हो रहे हैं, पारिवारिक और सामाजिक जीवन इतना तनावपूर्ण क्यों है तो इसका सीधा सा जवाब है कि हम औचित्य और अनौचित्य का विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर पाते हैं जिसके कारण तनाव संघर्ष और बड़े युद्ध होते हैं। यह बात भी सत्य है कि युद्ध की अपरिहार्यता से इंकार नहीं किया जा सकता पर उनके कारण धर्म न्याय और सत्य से अनुप्राणित और अनुप्रेरित हों जिसे धर्म-कर्म से नहीं न्याय सत्य और धर्म( अधिकार और कर्तव्य) से जोड़कर देखा जाना चाहिए और तभी मनुर्भव की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।
----------
कल आज और कल . सम्पादकीय आलेख : ३०.
--------------
अरूण कुमार सिन्हा.
भूत : भविष्य : और वर्तमान : भूत मृत है, भविष्य अनिश्चितता के गर्भ में हैं और वर्तमान जो सम्मुख है, जिसमें सांसें आती जाती रहती हैं,वही पल क्षण सिर्फ जीवित है शेष पल पल अतीत में परिवर्तित होता रहता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम आज के दिन को ही वर्तमान समझ कर जीते रहते हैं जबकि आज के दिन का भी एक एक पल जो आने वाला होता है, भविष्य ही है और एक एक पल जो गुजर गया, अतीत हो गया,भूत हो गया,वह आज के दिन में वापस नहीं लाया जा सकता है। आती जाती सांसों का अवलोकन : इसलिए आती जाती सांसों का अवलोकन करते रहिए और इन्हीं क्षणों में जो क्रियाशीलताएं सम्पन्न हो रही है बस वही वर्तमान है। आती जाती सांसों का अवलोकन करते रहना ही औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन में विपश्यना और बौद्ध दर्शन में विपस्सना है जिसे योगों में एक श्रेष्ठ योग माना गया है। इससे हम अपने भावों और उनसे सृजित विचारों पर नियंत्रण रखने का काम कर सकते हैं और यह क्रिया गृहस्थ जीवन की क्रियाशीलताओं में भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगर लम्बी अवधि तक नहीं तो जब भी आप विश्रामावस्था में हों तो इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसके लाभकारी परिणामों का भी अवलोकन कर सकते हैं।
पृष्ठ सज्जा : शक्ति अनुभूति / शिमला डेस्क.
स्तंभ संपादन : शक्ति रेनू शब्द मुखर / जयपुर डेस्क.
----------
अनुभूति. सम्पादकीय आलेख : २९.
--------------
अरूण कुमार सिन्हा.
टाल्सटाय की एक कहानी : निहित अर्थ : लियो टाल्सटाय की एक कहानी है, द पैरेबल ऑफ़ ए गुड समरिटन जो अद्भुत कथा है जिसे गौर से पढ़ने समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। आमतौर पर लोग कहा करते हैं कि बीज अच्छे हों तो फसल अच्छी होती है। पर इसकी कुछ शर्तें होती हैं।
एक किसान को कुछ श्रेष्ठ बीज दिए गए और कहा गया कि इसे तीन जगहों पर लगा देना है।
उसने कुछ बीज पत्थरों पर डाल दिया, कुछ को कंकरीली झाड़ीदार जमीन पर डाल दिया और शेष बचे को अच्छी मिट्टी में डाल दिया।
कुछ दिनों के बाद देखा गया कि पत्थरों पर पड़े बीजों को पक्षी खा गए और कुछ सूखकर नष्ट हो गये। झाड़ीदार जमीन वाले अंकूरित होकर थोड़े बढ़े फिर झाड़ियों ने उनका विकास रोक दिया और वे समूचित वातावरण न मिलने के कारण सूख गए। पर जो बीज अच्छी मिट्टी में डाले गए, उनमें सही विकास हुआ और वे मजबूत पोधों में विकसित हो गये।
मन की जैसी अवस्था : वैसे संस्कार : जिस व्यक्ति ने उसे बीज दिए थे ,उसने उस किसान ने नतीजा बताने को कहा तो किसान ने तीनों के परिणाम बता दिए। फिर उस आदमी ने उससे पुछा कि ऐसा क्यों हुआ कि बीज तो एक ही थे पर परिणाम अलग अलग क्यों हुए, किसान चुप रह गया। तब उस व्यक्ति ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि,
बीज बाह्य और आन्तरिक भाव हैं और मन जमीन है। मन की जैसी अवस्था होगी,मन के जो संस्कार होंगे,बीज रुपी भाव वैसे ही विचारों में पनपेगें और विकसित होंगे। मन यदि आपका पाषाण की तरह कठोर होगा तो विचार निर्जीव और निष्प्राण होकर मर जाएंगे जैसा कि पत्थर पर पड़े बीजों के साथ हुआ। मन यदि कुसंस्कारों से भरा पड़ा है तो विचार सृजित होंगे पर कुसंस्कारों के कारण वे कुछ बढ़ेंगे तो जरूर फिर स्वत: नष्ट हो जाएंगे पर मन की जमीन यदि उर्वर परिष्कृत और परिमार्जित हो तो भाव भी अच्छे विचारों में परिणत होकर मजबूती से विकसित होंगे और श्रेष्ठ विचारों को फैलाने का काम करेंगे।
मन ही हमारा संचालक है,मन के भाव अच्छे, परिष्कृत और परिमार्जित हों तो हमारे जीवन की क्रियाशीलताएं भी अनुशासित और श्रेष्ठ होंगी।
मन हमारी चेतना का दूसरा तल है जो बुद्धि और हृदय के बीच की चेतना है जो सदैव संश्यात्मक और अनिश्चयात्मक अवस्था में रहती है इसलिए मन जब भी निर्णय ले तो उसे अपने हृदय की संवेदना, बुद्धि की चेतना और मस्तिष्क की चेतना से तौलकर ही निर्णय लेना चाहिए। वैसे मन अगर शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित हो तो उसके विचारों को हृदय बुद्धि और मस्तिष्क से स्वत: स्फूर्त सम्पर्क हो जाता है और निर्णय सम्यक् होता है।
इसलिए मन रुपी जमीन को उर्वर और अनुकूल रखने का सदैव प्रयास करते रहना है कि अपने निर्णय और कर्म पर दुःख और पश्चाताप न हो। अगर कोई ग़लत निर्णय कभी हो भी जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति न हो ,यह भी अच्छे मन पर ही निर्भर करता है। मन की महत्ता को जैन और बौद्ध दर्शन और चिन्तन के साथ साथ औपनिषदिक दर्शन में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए मन की गतिविधियों का सदैव अवलोकन करते रहने से वह धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आने लगता है और जिसका मन अनुरागी अनुशासित और स्थिर होता है,उसका जीवन भी श्रेष्ठ होता है।
पृष्ठ सज्जा : शक्ति अनुभूति / शिमला डेस्क
स्तंभ संपादन : शक्ति रेनू शब्द मुखर / जयपुर डेस्क
----------
प्रार्थना के स्वर : सम्पादकीय आलेख : २८.
------------
प्रार्थना : परमात्मा के प्रति आभार : प्रार्थना की नहीं जाती,वह तो प्रतिकूलताओं में, अनुग्रहित होने की अवस्था में, परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हृदय से झरने की तरह फूटकर बह निकलती है।
यह अभ्यास का विषय नहीं स्वतःस्फूर्त प्रवाह है और परमात्मा इसे ही सुनते हैं और निर्णय लेते हैं।
यह कोई योजना नहीं कि बनायी जाए कि चलो आज अमूक काम करते हैं, विचार किया,योजना बनायी और उसे पुरा करने चल दिए,वह तो एक आयोजन या कर्मकाण्ड हो गया,वह कभी प्रार्थना हो ही नहीं सकती, प्रार्थना तो हृदय की, अन्तरात्मा की एक पवित्र प्रतिध्वनि है जिसकी गुंज चतुर्दिक होती है। प्रार्थी याचक नहीं होता बल्कि पूर्ण समर्पण भाव से मौन होकर अपने इष्ट के सम्मुख समर्पित भाव से बैठ जाता है और वाणी से नहीं अन्तर्वाही वाणी से अपने इष्ट को सबकुछ कह जाता है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती,किसी स्थान की जरूरत नहीं होती बल्कि जहां और जिस हाल में हैं, वहीं प्रार्थना हो सकती है।
प्रार्थना और याचना : ध्यान रहे कि प्रार्थना और याचना लगभग एक तरह प्रतीत तो होती है परन्तु दोनों में बड़ा फर्क होता है। वह परम चैतन्य सत्ता तो ऐसे ही सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं होती है बल्कि जिसके हक में जो मिलना है,उसे प्रदान करते रहते हैं फिर याचना क्यों,यह सवाल बड़ा व्यवहारिक है।
हम हमारे घर में भी अपने अभिभावक से वांछित वस्तुओं को पाते रहते हैं या बगैर मांगे भी उनकी पूर्ति भी होती रहती है परन्तु कभी-कभी वस्तु विशेष की जरूरत होने पर कहना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों में आपको उस परम चैतन्य सत्ता या परमात्मा को कहना पड़ता है जो याचना है,मांग है पर वह प्रार्थना नहीं है। जहां याचना होगी वहां प्रार्थना नहीं हो सकती और जहां प्रार्थना होगी वहां याचना नहीं होगी।
प्रार्थना तो मौन रुदन : प्रार्थना तो मौन रुदन है, उनसे प्राप्त भेंटों के प्रति अनुग्रह के भाव हैं, दुःख विपत्ति में त्राण पाने का आर्तनाद है जो हठात मुंह से निकलता है कि , हे परमात्मा,अब तेरे सिवा मेरा रक्षक कोई और नहीं है,बस अब रक्षा कर और यह भी मौन ही होता है। वह कभी कभी आंसूओं के रुप में चुपचाप आंखों से फूटकर बह निकलते हैं और प्रभु के श्री कर्णों तक पहुंच जाते हैं अर्थात् माने तो ध्वनि रहित पीड़ाओं की अभिव्यक्ति ही प्रार्थना है।
जैसे बच्चे की मुस्कान और रुदन की कोई भाषा नहीं होती वैसे ही प्रार्थना है जो वैश्विक स्तर पर सभी मत विश्वास विचार सम्प्रदायगत मतों आदि में स्थापित विश्वास है कि प्रार्थनाएं धरती पर की जाती है और असर आसमान पर होता हैं और आशीर्वाद नीचे आते हैं। कहा भी गया है कि सब सारी चेष्टाएं और प्रयास विफल हो जाएं तो अंतिम अस्त्र-शस्त्र जो है वह प्रार्थना ही है कि वह अन्तर्रात्मा की आवाज होती है,अन्त: करण की ध्वनि होती है जिसकी असर गहराईयों तक होती है।
किसी की बददुआ न लें : इसलिए हो सके तो सबके लिए दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, किसी को बददुआ न दें कि यह वह ध्वनि है जिसकी प्रतिध्वनि लौटकर आती है। हां, कभी-कभी एक पीड़ित के मुंह से पीड़क के प्रति आह निकलती है जो एक तरह से बददुआ ही होती है जो असर करती है इसलिए आप सदैव कोशिश करते रहें कि किसी की बददुआ न लें पर जीवन व्यवहार बड़ा अद्भुत है कि ऐसा होता रहता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको ऐसा महसूस हो तो पीड़ित से खुले दिल से क्षमायाचना कर लें और जो पीड़ा आपने दी है उसका प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों हो जाए और आप अपराध मुक्त हो जाएं। विनती,विनय प्रार्थना आदि अनुग्रह के ही शब्द है और सबको उस परम चैतन्य के प्रति सदैव
अनुग्रह और उपकृत होने के भाव रखने चाहिए,यही मुक्ति भाव है,वैसे जैसे माता पिता के ऋणभार से कभी मुक्ति नहीं होती वैसे ही ईश्वरीय अनुग्रह से कभी ऋणमुक्ति नहीं हो सकती है परन्तु उनके प्रति अनुराग और अनुग्रह के भाव तो रखना ही चाहिए और यही भाव प्रार्थना के भाव हैं।
----------
दुःख और पीड़ाएं : चिन्तनका साधन : सम्पादकीय आलेख : २७ .
------------
जिन्दगी वह नहीं : जिन्दगी वही नहीं जो आप देख रहे हैं बल्कि जो आपकी दृष्टि और सोंच से परे है,वे परिदृश्य भी जीवन के अंग हैं। हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने की परम्परा पर चलते हैं पर जीवन तो रहस्यमय है, भविष्यगामी घटनाएं जब वर्तमान में आकार लेती हैं तब आप इसे सच मानते हैं। इसलिए सच और झूठ के बीच किसी विभाजक रेखा को खींचना इतना सहज नहीं होता है। अतीत में जो घटनाएं घट गयीं ,क्या आपने कभी सोंचा था कि ऐसी भी घटनाएं जीवन में घट सकती हैं, अच्छी और अनुकूल घटनाएं
आपको प्रसन्न ऊर्जावान और आशावान बनाती हैं और इसके विपरीत होने पर आप दुखी और निराश हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जीवन की घटनाओं का भी एक मौसम होता है और जैसे मौसम बदलता है ठीक वैसे ही आपका जीवन भी बदलता है।
आपके साहस, आस्था और विश्वास की परख : हां, ये बदलाव कभी कभी अल्पकाल में हो जाता है और कभी समय लगता है,पर बदलता जरुर है और ऐसे कालखंड में ही आपके धैर्य,आपकी सहनशीलता, आपके साहस, आस्था और विश्वास की परख होती है। पर ध्यान रहे कि उनका कोई विकल्प नहीं है और आपको उन्हीं के आसरे चलते रहना है।
यही अवसर खुद को परिष्कृत और परिमार्जित करने और नवनिर्माण करने का होता है। दुःख और पीड़ाएं सिर्फ हमें पीड़ित नहीं करती बल्कि चिन्तन और साधने के अवसर देती हैं और आपके भीतर की दबी ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने आती हैं। सबको अपने जीवन में तपना पड़ता है, झेलना पड़ता है कि बगैर झेले और तपे कुछ नया नहीं बन सकता है। इसलिए सुख और अनुकूलताओं में आपको जीवन को समग्रता में देखने और समझने के अवसर नहीं मिलते, ये अवसर प्रतिकूल समय ही देते हैं और इससे कोई नहीं बचा है, इसलिए सब परिस्थितियों को सहजता और सरलता से जीने की कोशिश करनी चाहिए कि समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताओं का परिणाम ही जीवन की परिवर्तनशीलता है।
पृष्ठ सज्जा : शक्ति अनुभूति मंजिता स्वाति / शिमला डेस्क
स्तंभ संपादन : शक्ति रेनू शब्द मुखर / जयपुर डेस्क
----------
हम और ईश्वरीय सत्ता के सम्बन्ध : सम्पादकीय आलेख : २६.
-------------
जगत मिथ्या , ब्रह्म सत्य : वैदिक काल की मानवीय चेतना आमोद प्रमोद और यज्ञादि से जुड़ी हुयी थी जो जीवन के अंत पर कभी चिन्तन नहीं करती थी परन्तु चेतना के बौद्धिक विकास होने के साथ साथ मनुष्य ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है,अंत होने के बाद क्या होता है, सृजन और विनाश का क्या सम्बन्ध है, क्या कोई अलौकिक सत्ता मनुष्य को और समस्त प्राकृतिक व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करती है और फलस्वरूप वेदांत या औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्म की अवधारणा को धर्म और कर्मकाण्ड के नजरिए से उठकर मुक्ति दाता के रुप में देखा जाने लगा।
यह औपनिषदिक दर्शन का ही प्रभाव था कि आदिगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की घोषणा करते हुए कह दिया कि,जगत मिथ्या , ब्रह्म सत्य अहं ब्रह्मास्मि
और फिर ईश्वरीय सत्ता से समन्वय और तादात्म्य स्थापित करने के मार्ग की खोज होने लगी।
गीता : ज्ञान मार्ग , भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग : गीता ने ज्ञान मार्ग , भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग का संदेश दिया। नवधा भक्ति की अवधारणा विकसित हुई पर ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि निष्ठा समर्पण का बोध कैसे हो तो कालान्तर में दो मार्ग यथा,वानरी मार्ग और मार्जारी मार्ग के मार्ग की खोज की गई और इसे सारे मार्गदर्शनों से भिन्न माना गया कि इनमें किसी कर्मकाण्ड दर्शन चिन्तन शोध खोज और योग की जरूरत नहीं थी। यह सर्वजनहिताय और सर्वजनसुखाय का मार्ग था। जीवन दर्शन और व्यवहार दोनों है। ईश्वर की खोज आर्त ज्ञानी भक्त या साधक करते हैं, वेदों उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके उस सत्ता की खोज करते हैं परन्तु जीवन सहजता और सरलता से कर्तव्य पालन करते हुए ईश्वरीय कृपा से सुरक्षित गुजर जाए उसका यही मार्ग सहज पाया गया।
अब सवाल उठता है कि वानरी मार्ग और मार्जारी मार्ग है क्या तो इसे समझना भी बड़ा सरल है। वानरी का अर्थ मादा वानर है जो यहां ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि वानरी के पेट से उसका बच्चा एकदम से पुरे विश्वास के साथ चिपका होता है और वानरी कितना भी उछल कूद करती रहे, वह नहीं गिरता है। एक प्रकृति यह है कि आप ईश्वर से उसी तरह चिपक जाइए और काल कितना भी उछल कूद करे आप उनकी सुरक्षा चक्र से सुरक्षित रहते हैं।
पूर्ण आस्था श्रद्धा और विश्वास : अब मार्जारी मार्ग को समझने की कोशिश करें,मार्जारी का अर्थ बिल्ली होता है और बिल्ली जब अपने बच्चे को कहीं भी असुरक्षित देखती है तो अपने दांतों में दबाकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है और बच्चे को उसके तीक्ष्ण दांतों से कोई हानि नहीं पहुंचती है। जिन तीक्ष्ण दांतों के जरा सा दवाब से उसके शिकार मारे जाते हैं उन्हीं तीक्ष्ण दांतों से बच्चे सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाते हैं।
आपके सामने दोनों अवस्थाएं स्पष्ट है,या तो पूर्ण आस्था श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर को वानरी बच्चे की तरह पकड़े रहिए या ईश्वर बिल्ली की तरह आपको सुरक्षित रखने के लिए जैसे और जहां ले जाए, बने रहिए।
ईश्वर सदैव अवसर देते रहते हैं और आपको सुरक्षित रखने का काम करते रहते हैं,आपको अवलोकन करते रहना है और अपने विहित कर्तव्यों का पालन करते रहना है और साथ ही अतीत के कृत कर्मों का पश्चाताप और प्रायश्चित कर लेना है। आपकी अन्तश्चेतना जिसे गलत मानती है,उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है।
वानरी और मार्जारी मार्ग सहज योग की तरह है, ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण कि यह भी एक योग-साधना का ही रुप है,जैसे साधना गति में होती है तो नृत्य में रुपान्तरित हो जाती है और स्थिर होने पर समाधि में रुपान्तरित हो जाती है वैसे ही ये मार्ग समर्पण योग का मार्ग है।
---------
अनुभूति : सम्पादकीय आलेख : २५.
----------
दो स्वरूप होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म : समस्त ब्रह्माण्ड में पदार्थों के दो स्वरूप होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म जो सर्वत्र दृष्टिगोचर हैं। ऊर्जा हर पदार्थ में समाविष्ट है परन्तु अदृश्य है परन्तु उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष होती रहती है। जब हम निराहार रहते हैं या शरीर रुग्णावस्था में रहता है तो मन और तन दोनों शक्तिहीन या ऊर्जाहीन महसूस होते हैं और भोजन मिलते ही या व्याधियां खत्म होते ही शरीर ऊर्जावान हो जाता है।
शरीर स्थूल है और ऊर्जा सूक्ष्म है जिससे यह पता चलता है कि हमारा जीवन स्थूल और सूक्ष्म दोनों सत्ताओं से निर्मित है पर मनुष्य सांसारिक जीवन में सिर्फ इसी स्थूलता पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है जिससे उसे जीवन के यथार्थ का बोध नहीं हो पाता है।
हमारे कर्म स्थूल हैं, दिखाई पड़ते हैं और समझ में आते हैं परन्तु उसके परिणाम सूक्ष्म से रुपान्तरित होकर स्थूल में दिखाई पड़ते हैं और इसी भेद को समझना जीवन के यथार्थ को समझना है।
हम जब सामर्थ्यवान और ऊर्जावान होते हैं तो इस पक्ष को विस्मृत कर जाते हैं और जीवन के स्थूल पक्ष को ही देख पाते हैं और सूक्ष्म पक्ष गौण हो जाता है। हमारी समस्त क्रियाशीलताऍं भौतिक और स्थूल होती हैं और उनकी परिणति सूक्ष्म से स्थूल में रुपान्तरित होती रहती है जो हमारे दुःख सुख का कारण बनती हैं। जैसे आप किसी बैंक में एक खाता खोलते हैं और हर माह कुछ राशि जमा करते रहते हैं जो एक छोटी या बड़ी राशि हो सकती है परन्तु एक निश्चित अवधि के बाद वह एक बड़ी राशि में परिणत हो जाती है। वैसे ही स्थूल क्रियाशीलताएं सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे रुपान्तरित होकर एक बड़े परिणाम को जन्म देती है जो आपके कर्मों के समानुपातिक होती है,यही स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में ऊर्जा का रुपान्तरण है जो मनुष्य के जन्म से मरण तक चलता रहता है। यही बौद्ध और जैन दर्शन में संसार चक्र है जो हमारे औपनिषदिक दर्शन में भी वर्णित है। यह जीवन का व्यवहार और व्यवहार का यथार्थ है पर इसका बोध मनुष्य को स्थूल रुप में होता है और वह सूक्ष्म को भूल जाता है।
पाप और पुण्य की अवधारणा : ठीक इसी प्रकार पाप और पुण्य की अवधारणा है, दोनों स्थूल और सूक्ष्म होते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी अनुभूति अलग होती है और कोई बुरा या ग़लत करने पर उसकी अनुभूति अलग होती है और हर आदमी को इसकी अनुभूति होती है पर वह इसे दिनचर्या समझ कर भूल जाता है। अच्छे और नेक काम से उत्पन्न ऊर्जा साकारात्मक होती है जो संचित होती रहती है और ऐसे ही बुरे कर्मों से उत्पन्न ऊर्जा नाकारात्मक होती है,वो भी संचित होती रहती है और इनकी अंतिम परिणति स्थूल रुप में एक दिन दृष्टिगोचर होती है और पुनः दोनों में संघर्ष होता है और जो पक्ष शक्तिशाली होता है,वैसा ही परिणाम देता है।
इसलिए जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों पक्षों को समझना और आत्मसात करना जरूरी होता है और संभवतः हिन्दू जीवन दर्शन में पूर्वजन्म और भोग के दर्शन का आधार यही है।
---------
निर्णय और हम : सम्पादकीय आलेख : २४.
-------------
पूर्वानुभूतियों का भाव : भव अर्थात् संसार के अवलोकन से और पूर्वानुभूतियों से भाव अर्थात् विचारों के जन्म होते हैं और ये विचार हमें आन्तरिक और बाह्य रूप से प्रभावित करते रहते हैं। विचार एक प्रवाहमान नदी के समान होता है जो सतत् बनते रहता है।
विचारों का सम्बन्ध सिर्फ मन से ही नहीं होता बल्कि यह हृदय और मस्तिष्क से भी जुड़ा होता है। चेतना के जितने तल होते हैं वे अलग - अलग रुपों में मनुष्य के कई अंगों से जुड़े होते हैं जो विचारों के सृजन में अलग - अलग भाव पैदा करते रहते हैं।
मन चेतना का वह तल है जो सदैव संश्यात्मक और अनिश्चयात्मक अवस्था में रहता है इसलिए मन के द्वारा लिए गए निर्णय सही और ग़लत दोनों हो सकते हैं। हृदय अपेक्षाकृत कोमल और संवेदनशील होता है और इसके निर्णय भी संवेदना में आकर लिए जाते हैं जो आम तौर पर सही तो होते हैं परन्तु एकदम से सटीक नहीं होते परन्तु जब निर्णय मन हृदय और मस्तिष्क के एक तारतम्य रख कर लिए जाते हैं तो भाव संवेदना और औचित्य एक साथ काम करते हैं और वह निर्णय बिल्कुल सही होता है।
द्वन्द संवेदना और औचित्य में पारस्परिक संघर्ष होते हैं जहां मनुष्य के अन्तर में भारी संघर्ष होता है परन्तु अंत में औचित्य और अनौचित्य के बाद जो सत्य होता है,वही अंतिम निर्णय होता है और इस निर्णय में संवेदना, कोमलता,सहजता तथ्य और तर्क सब सम्मिलित होते हैं।
परन्तु व्यवहारिक जीवन में मनुष्य इतनी गंभीरता से विचार नहीं कर पाता और मन या हृदय हावी हो जाता है और निर्णय तत्काल तो अच्छे लगते हैं पर दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते।
इसलिए छोटे मोटे विषयों पर सहजता से परिस्थितियों के अनुरूप जो निर्णय लेना हैं ले सकते हैं परन्तु जिससे आपका जीवन परिवार मित्र समाज आदि प्रभावित होने वाले हों तो मन हृदय और मस्तिष्क का तालमेल होना अनिवार्य है।
----------
परीक्षा और परीक्षार्थी : सम्पादकीय आलेख : २३ .
------------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
धैर्य सहनशीलता और सामर्थ्य की परीक्षा : वह परम चैतन्य सत्ता सदैव सबकी क्षमता धैर्य सहनशीलता और सामर्थ्य की परीक्षा लेता रहता है और साथ भी नहीं छोड़ता। अब परीक्षार्थी पर निर्भर करता है कि वह जाॅंच में कैसे उत्तीर्ण हो।समय समय पर वह सांकेतिक रुपों में सहयोग और दिशानिर्देश भी देता रहता है, इसलिए धैर्य साहस और उनके प्रति अपनी निष्ठा श्रद्धा समर्पण और विश्वास को बनाए रखें कि वह किनको किस रुप में प्रक्षेपित करना चाहते हैं,यह रहस्यमय खेल आज भी समझ से परे है।
श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध का निर्णय अकेले ही कर देते परन्तु अपने सखा और भक्त अर्जुन की दबी हुयी क्षमताओं और सामर्थ्य को जगाना चाहते थे और श्रीमद्भगवद्गीता उसकी ही परिणति है।
श्री राम जब रावण के विरुद्ध अभियान छेड़ते हैं तो श्री हनुमान जी का चयन करने के पीछे भी यही उद्देश्य था और इसलिए श्री हनुमान जी सार्वलौकिक और सार्वकालिक संकटमोचन बन गए।
द बुक ऑफ़ जॉब The book of Job जिसे ईंजिल के समान सम्मान प्राप्त है उसमें भी परमात्मा अपने भक्त की इसी तरह की परीक्षा लेते हैं। शैतान, भगवान को उकसाते रहता है, परमात्मा भी जाॅब के साथ वैसे ही अति पर चले जाते हैं पर जाॅब अंत तक कुछ नहीं कहता पर उसकी पीड़ाएं जब चरम पर पहुंच जाती हैं तब वह सिर्फ इतना कहता है कि, हे प्रभु, बस मेरा अपराध बता देना और इतना कहते ही उसकी सारी पीड़ाएं समस्याएं समाप्त हो गयी, सबकुछ यथावत हो गया।
हो सकता है कि ईश्वरीय निष्ठा को मजबूत करने के लिए ऐसी कथाएं सर्वत्र उपलब्ध है पर यह महज कल्पना नहीं हो सकती है कि कल्पनाओं की भी कुछ पृष्ठभूमि होती हैं बगैर बुनियाद के कोई भवन नहीं बनते हैं। जो अनिश्वरवादी हैं, नास्तिक हैं, उन्हें शायद ऐसी कथाएं कपोल कल्पित लगे परन्तु बिना बीज के सृजन नहीं हो सकता है।
प्रकृतिवादी और भौतिकवादी समस्त ब्रह्माण्डीय रचना को जड़ और चेतन की संयुक्त परिणति मानते हैं कि समस्त जैविक व्यवस्था जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, ऐसा विख्यात चिन्तक और लेखक एम एन राय का कहना है।अनेक भौतिकविद किसी अलौकिक सत्ता के अस्तित्व से इन्कार करते हैं। स्टीफेन हाकिंग्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था परन्तु* नवीनतम बिग बैंग सिद्धांत के उपरान्त जिस अंतिम क्षण में अंतिम भौतिक कण की खोज हुयी उसे हिंगिस बोसोन कहा गया परन्तु वह इतना रहस्यमय था कि उसे * God's Particle या ईश्वरीय कण कहा गया।
अल्बर्ट आइंस्टीन अलौकिक और रहस्यमय सत्ता : अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान भौतिकविद् को भी अंतिम क्षणों में कहना पड़ा था कि ब्रह्मांड की क्रियाशीलताओं की जटिलताओं को देखने के बाद यह सहजता से कहा जा सकता है कि अज्ञात अलौकिक और रहस्यमय सत्ता है जो इस ब्रह्माण्ड का संचालन करती है।
ईश्वरीय सत्ता आज भी ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय की सत्ता से जुड़ी हुई है। नास्तिक ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता पर वह प्रमाणित नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है और आस्तिक मानता है कि ईश्वर है पर वह भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि ईश्वर है। इसलिए ईश्वरीय सत्ता अज्ञेय है
जिसके बहुआयामी स्वरूप हैं। मसीहा, पैगम्बर,देवदूत, अवतार, भगवान आदि उसी बहुआयामी स्वरूप के प्रतिनिधि हैं। जो हमारी विपत्तियों को दूर करने में,हल करने में अचानक से मदद कर दे,वह भी उसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है।
जीण महावीर और तथागत सिद्धार्थ ने भी ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार किया था पर आज उनके ही अनुयायियों ने उन्हें भगवान बना दिया।
नेकी, सदाचार, सदाशयता, सत्य, धर्म और न्याय ईश्वरीय गुण हैं बस इन्हें स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें यही परम धर्म और अंतिम सत्य है, हर अमंगल के पीछे कुछ न कुछ मंगलमय विभु की मंगलकामनाएं छुपी रहती हैं,इस पर नजर रखिए और चलते रहिए।
---------
अहं ब्रह्मास्मि सम्पादकीय : आलेख : २२.
------------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
हिन्दू जीवन दर्शन : हिन्दू जीवन दर्शन और चिन्तन मूल रूप से वेद और उपनिषद आधारित है जिनमें पांच महासूत्रों या महावाक्यों की अवधारणा की गयी है जो अध्यात्म और आत्मबोध तथा आत्मचेतना की चरम सीमा है जिनमें हर सूत्र भीतर से एकत्व बोध को समाहित किए हुए हैं। वे सूत्र वाक्य हैं,
अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि
तत्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म।
इनके अलावे अन्य प्रमाणों में एक और सूत्र मिलता है जो शुद्ध विज्ञान और विशुद्ध अध्यात्म भी है औरवह सूत्र वाक्य है,
यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे
यत् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे।
सारे सूत्र वाक्यों की अपनी अहमियत है पर इनमें जीव जीवात्मा और परमात्मा के अन्तरंग सम्बन्धों को कुछ प्रभावी ढंग से व्याख्या करते हैं।
गीता में कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग : भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग की वृहद् व्याख्या की है जिसमें ज्ञानयोग की अपनी महत्ता है इसलिए कहा गया कि, प्रज्ञान ब्रह्म अर्थात् ज्ञान की अन्तर्चेतना ही ब्रह्म है। साधारण ज्ञान और चेतना से जीव आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जाना जा सकता है कि साधारण ज्ञान से स्थूल अवस्था का बोध होता है, भौतिक पदार्थों का ज्ञान स्थूल ज्ञान से होता है जिनका अवलोकन निरीक्षण और निष्कर्ष निकाला जा सकता है परन्तु सूक्ष्म का बोध इस ज्ञान से नहीं हो सकता है। आप माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जीवाणु और वायरस आदि का अवलोकन तो कर सकते हैं परन्तु मन भाव विचार आवेग मस्तिष्क की गतिविधियों आदि का अवलोकन और विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, इनकी अनुभूति inner conscience and instinct से ही हो सकती है और यही प्रज्ञान है जिसकी प्राप्ति गहन अध्ययन और साधना से होती है। इसलिए यह सूत्र वाक्य कहता है कि ब्रह्म का ज्ञान प्रज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान जब आपकी चेतना के चरम पर पहुंचता है तब उसका रुपान्तरण प्रज्ञान में हो जाता है और इस प्रज्ञान का जागरण सद्गुरु के माध्यम से भी हो सकता है। सिद्धार्थ ने इस परम चेतना की प्राप्ति गहन साधना से की थी वहीं अर्जुन को इसका बोध गीतोपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने दिया था।
मनुष्य को जिज्ञासु होना पहली शर्त : इसके लिए मनुष्य को जिज्ञासु होना पहली शर्त है और इसलिए औपनिषदिक दर्शन में कहा गया है कि, अथातो जिज्ञासा धर्म: अर्थात् बगैर जिज्ञासा के धर्म को नहीं जाना जा सकता है,उसी तरह सांसारिक जीवन में भी विकास के जितने संसाधन विकसित किए गए हैं, जिज्ञासा के ही परिणाम हैं। बगैर जिज्ञासा के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जिज्ञासा ही उसे शोधक अन्वेषक और आविष्कारक बनाती है और यह व्यवहारिक जीवन में भी अनुभूत है। यही जिज्ञासा कार्य और कारण के सिद्धान्त की भी व्याख्या करता है और इसी की सहायता से कोई सही निर्णय पर पहुंच सकता है। शेष सूत्र भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जिसे व्याख्यायित करना इस पटल पर असंभव नहीं तो दुष्कर जरुर है। फिर भी यह बताना जरूरी है कि आत्मा ही परमात्मा है और सबमें एक ही सत्ता अवस्थित है। जो आप हैं वही सब हैं, आप ही उस परब्रह्म का विस्तार हैं इसलिए एक सूत्र वाक्य कहता है कि, यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे अर्थात् जो मनुष्य के शरीर में, भौतिक पिण्ड में है वह सब है जो ब्रह्माण्डीय अस्तित्व में है अर्थात् जो मनुष्य है वह ब्रह्माण्डीय पिण्ड का ही लघु रुप है। जिस प्रकार पीपल या बरगद के लघु बीज में एक विशाल वृक्ष छुपा होता है वैसे ही मनुष्य का शरीर है जो बीज रुप है और प्रज्ञान से विस्तार करके उस चेतना को ब्रह्म में समाविष्ट किया जा सकता है।
सन्दर्भ बड़े रहस्यमय और दीर्घ हैं इसलिए समझना यह है कि मानवीय चेतना ही सम्पूर्ण बोध का आधार है,आपकी चेतना जितनी विकसित होती जाएगी,आपकी आत्मा उतनी ही चैतन्य होती जाएगी और जब यह चेतना अपने चरम पर पहुंचेगी तो आप भी उद्गोष कर सकते हैं, अनहलक अनहलक या अहं ब्रह्मास्मि और यही अवस्था अर्हत्व या बुद्धत्व की है,यही प्रज्ञान है,यही अंतिम बोध है कि इसके बाद सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं और शेष शून्य या शिव रह जाता है।
-------------
संसार और अनुभूति : संसार है एक नदियां : सम्पादकीय आलेख : २१ .
-----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
 |
न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं सुख दुःख दो किनारें हैं : कोलाज : डॉ. सुनीता शक्ति* प्रिया. |
मन: स्थिति : संसार न तो सुखमय होता है और ना ही दुखमय होता है। संसार वही रहता है परन्तु मनुष्य की भौतिक और सूक्ष्म अवस्थाओं पर संसार की अनुभूतियां बदलती रहती है। तन दुखी हो तो मन दुखी हो जाता है और तन मन दोनों दुखी और पीड़ित हो तो सब दुखमय प्रतीत होता है। संसार निरस और निष्प्राण दिखाई देने लगता है। इस मन: स्थिति का आधार मूल रूप से तन और मन दोनों ही है।
एक व्यक्ति शरीर से व्याधिग्रस्त है तो मन भी व्याधिग्रस्त हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हैं परन्तु वांछित संसाधनों के अभाव हैं तो भी मन दुखी हो जाएगा और ऐसी परिस्थितियों का आना जाना अनवरत लगा रहता है , फर्क व्यक्ति के अवस्था के समानुपातिक होता है। सत्ता में बैठे हुए एक व्यक्ति से सत्ता छीन जाती है परन्तु सारे संसाधन उपलब्ध हैं,तन सुखी है परन्तु मन पीड़ाओं से प्रभावित है, सत्ता चली गयी, सत्ता छीन जाने का दुःख है,यह भी एक भौतिक पीड़ा है जो उसे दग्ध करती है।
संसार में पीड़ाएं अनन्त हैं : भौतिक संसार में पीड़ाएं अनन्त हैं, सुख भी अनन्त हैं जो अलग-अलग तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करता है। फिर भी जीना है कि उम्मीदें बन्धी हुयी हैं, जिम्मेदारियां और जवाबदेहियां बन्धी हुयी जिसे लेकर वह अपनी जिजीविषा को जीवित रखता है और संघर्ष करता है। परिस्थितियों के बीच तालमेल और समन्वय बनाकर चलने और जीने की कोशिश करता है कि किसी के पास इनका कोई विकल्प नहीं होता है और इसे ही अन्तिम विकल्प मानकर वह दुःख में, पीड़ा में और संघर्षों में तुलनात्मक सुख चैन की खोज करता है।
वह दुःख और संघर्षों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करता है, अपने से अधिक पीड़ित और दुखी को देखकर अपने साहस विश्वास और संघर्षों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ता है और ऐसे वक्त में आत्मविश्वास, सहनशीलता धैर्य और अपने इष्ट पर भरोसा करके चलते रहना होता है कि यही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है जो उसके मन: स्थितियों पर निर्भर करता है। इतिहास के उन उदाहरणों और जुझारू व्यक्तियों की खोज करनी पड़ती है जो एकदम से विकट और असंभव परिस्थितियों से जूझते हुए अपने को फिर से खड़ा कर अपने अस्तित्व को स्थापित कर लेते हैं और ऐसे इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देते हैं।
पृष्ठ संपादन : डॉ. सुनीता शक्ति* शालिनी प्रिया . दार्जलिंग डेस्क
पृष्ठ सज्जा : शक्ति. सीमा अनीता मंजिता अनुभूति / शिमला डेस्क.
--------
सत्य अहिंसा करुणा त्याग और क्षमा : जीवन के नैसर्गिक गुण. सम्पादकीय आलेख : २०.
-----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
जीवन के नैसर्गिक गुण : सत्य अहिंसा करुणा त्याग और क्षमा जीवन के नैसर्गिक गुण हैं जिन्हें हम प्रदर्शन और पाखण्ड का विषय बना देते हैं।इन गुणों में सहजता सरलता और ग्राह्यता होनी चाहिए जिसकी अनुभूति एक आम आदमी को भी सहजता से होनी चाहिए। आज वैश्विक स्तर पर इन नैसर्गिक गुणों का सामाजीकरण के बजाय राजनीतिकरण किया जा रहा है।
हिंसा रक्तपात अनाचार अत्याचार बलात्कार आदि जघन्य अपराधों की घटनाओं का सृजन करके हम उपवास धरना प्रदर्शन और मुआवजा दिलवाने का काम करते हैं। आपदाग्रस्त और दुर्घटनाग्रस्त घटनाओं पर वांछित सहयोग ओर सुरक्षा देने के बजाय विडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर परोसा जाता है मानो वे मनोरंजन के दृश्य हों,क्या यह प्रकृति और प्रवृत्ति हमें धीरे धीरे मानवीय वृत्ति से दानवी
वृत्ति की ओर नहीं ले जा रहा है, पर हम परिणामों पर चर्चाएं करते हैं जबकि उसके पीछे के कारण समुदयों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि भविष्यगामी कुपरिणामों से बचा और बचाया जा सके, परन्तु सबकुछ औपचारिक होता जा रहा है, हमारा व्यवहार और आचरण भी औपचारिक होते जा रहे हैं। कृत्रिमता ही आज सहज और सरल माना जाने लगा है। हम जीवन मोल और मूल्यों से शून्य होते जा रहे हैं।
मैं एक दो घटनाओं का जिक्र करना जरूरी समझता हूॅं, एकबार अमरीकी राष्ट्रपति जौनसन सीनेट में भाषण देने जा रहे थे। उनका पुरा काफिला ह्वाईट हाउस से निकल कर जा रहा था।
रास्ते में एक दलदली गड्ढे में उन्होंने एक सुअर को फंसे देखा। सुरक्षाबलों की गाड़ियां निकल गयी थी,इनकी गाड़ी बीच में थी, इन्होंने चालक को गाड़ी रोकने को कहा और कोई कुछ समझे इससे पहले बगैर किसी को कुछ कहे उस गड्ढे में उतर गए और सुअर को खींच कर बाहर कर दिया। उनका सुट कीचड़ से सन गया, सीनेट का समय भी हो रहा था। उनके सुरक्षाकर्मियों ने पानी की व्यवस्था की और उन्होंने पैंट और जूते साफ किए और गाड़ी में बैठ गए और उसी हालत में वे सीनेट में अपना शानदार भाषण दिया। यह चर्चा सीनेट में हो गयी, उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि, सीनेट देर से पहुंचने पर क्षमा मांग लेता, पैंट जूते को तो बोलना नहीं था पर एक निर्दोष जीव का मर जाना मुझे जीवन भर सालता रहता कि मैंने एक जीवन रक्षा नहीं की, यही सहज करुणा त्याग और मानवीय चेतना है जिसकी अनुभूति सबको होनी चाहिए। अब एक सवाल यहां उठता है कि जो स्वयं मांसाहारी हो उसके भीतर ऐसी करूणा कैसे जागी,तो देखा जा सकता है कि हम मांसाहार करते हैं पर एक ट्रक के पहिए में फंसे भेड़ या बकरे को छोड़ देने के बजाय बचाने की कोशिश करते हैं, दरवाजे पर बैठे भूखे कुत्ते को रोटी जरुर देते हैं।
सिद्धार्थ के तथागत के रुपान्तरण : सिद्धार्थ के तथागत के रुपान्तरण के पूर्व मांसाहार की चर्चा मिलती है,पर देवदत्त के बाण से आहत हंस को गोद में उठाकर रोने लगे, उसका इलाज किया और स्वस्थ किया। यह सहज संवेदना और करुणा है जो स्वत:स्फूर्त पैदा होती है, उसमें कोई बनावट, पाखंड, दिखावा या प्रपंच नहीं होता है।
यद्यपि मैं भी शाकाहारी नहीं हूं परन्तु अपने पालतू श्वान के निधन पर कितने दिनों तक अकेले में रोता रहा और आज भी उसकी स्मृतियां मुझे भीतर तक आहत कर जाती है। जब कोई अपना और अंतरंग बीमार होता है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो क्या आपका मन पीड़ित और आहत नहीं होता पर उसमें औपचारिकता भीतर से खलती है,हम खैरियत भर पुछने की औपचारिकता पुरा करते हैं पर कुछ लोग भीतर से आहत और चिन्तातुर हो जाते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और ये सहजता स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है।
आपदाएं विपदाएं हमें परेशान जरूर करती है पर संवेदनशील और भावुक भी बनाती हे कि हम दूसरे की पीड़ाओं को सहजता से समझ पाते हैं। लोग रोज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं,मरते हैं पर हम भीतर से आहत नहीं होते कि उनसे हमारी आत्मीयता नहीं होती परन्तु अपनों के दुख हमें आहत करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि किसी बड़ी दुर्घटना में हताहतों के प्रति मन से आह नहीं निकलता कि, आह, बड़ा बुरा और दुखद हुआ और तभी तो हम उनकी आत्मा की शान्ति और परिवार के लिए दुआएं करते हैं।
अंत में दुःख पीड़ा कष्ट आपदा विपदा आदि किसी को नहीं छोड़ते वैसे ही हमें करुणा प्रेम दया त्याग क्षमा संवेदना और सहयोग नहीं छोड़ना चाहिए।
--------
जीवन की सार्थकता, मोल और मूल्य. सम्पादकीय आलेख : २०.
---------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
जीवन की सार्थकता, मोल और मूल्य : जीवन की सार्थकता, मोल और मूल्य, रिश्तों और सम्बन्धों का सच आपको कब पता चलता है, इसकी दो परिस्थितियां या दो हालात हैं,या तो विपरित परिस्थितियों में अनुकूलताओं में जी रहे हों या प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहे हों या संघर्षों के दौर से गुजर रहे हों तो इन परिस्थितियों का अवलोकन करते रहें जो बाहर से दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है सीधे-सीधे दिखाई नहीं पड़ता है पर अनुभूतियां तो रहती है।
इसलिए मैंने बार बार अपने आलेखों में बताने की कोशिश की है कि ये सारी परिस्थितियां आपकी उपयोगिता और उपादेयता सिद्ध करती है और वो उपयोगिता तथा उपादेयता का आधार सिर्फ धन नहीं होता बल्कि उनमें जज्बात और अहसास भी होते हैं। कुछ भविष्यगत विचार भी होते हैं कि कल आप एकाएक बहुत बड़े आदमी हो जाएं और सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएं।
भयजनित प्रेम और आवश्यकता जनित रिश्ते : लेकिन एक बात तो है स्पष्ट कि भयजनित प्रेम और आवश्यकता जनित रिश्ते कभी स्थाई भाव लेकर नहीं चल सकते हैं,भय खत्म हुआ कि प्रेम खत्म और जरुरत खत्म हुयी तो रिश्ते खत्म और हमारी नज़रों में यही सच है।
श्री राम ने जब सागर को भयाक्रांत कर दिया तो वह करबद्ध विनती करते हुए उनके सम्मुख प्रेम भाव प्रकट करते हुआ और क्षमा मांगने लगा। श्री राम निशस्त्र ( साथ में सेना नहीं थी ) थे उन्होंने वानर भालू आदि से आवश्यकतानुरुप उनकी मदद ली जबकि वह सक्षम थे पर यह बताना चाहते थे कि सबको सबकी जरूरत कभी न कभी पड़ ही जाती है, इसलिए अपेक्षा भाव को निस्पृह भाव से रखना चाहिए और उपेक्षा भाव का त्याग करना चाहिए।
धन पद प्रतिष्ठा आदि रिश्तों की सीमाएं : इस भौतिक संसार में जीने के लिए वांछित धन जरुरी है, पर अतिरेक होना दिग्भ्रमित करता है। आज की तारीख में धन पद प्रतिष्ठा आदि रिश्तों की सीमाएं तय करते हैं। आज की सामाजिक आधारभूत संरचनाओं में यही सब कुछ ( कुछ अपवादों को छोड़कर ) तय करता है कि सामाजिक सम्बन्ध और पारिवारिक रिश्तों में कितनी गर्माहट है, कितनी वेदना और संवेदना है।
आज हम सबके रिश्ते अंधेरी गुफाओं में भागते नजर आ रहे हैं, उन अंधेरों में हम सब ऐसे जी रहे हैं जैसे अंधेरी रातों में चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं और एक दूसरे को नहीं देखते हैं।
चैतन्य जीव : धरती पर दो प्रकार के जीव होते हैं,एक कशेरुकी ( रीढ़धारी ) और एक अकशेरुकी ( रीढ़ विहीन ) जिनमें रीढ़धारी अपेक्षाकृत चैतन्य होते हैं और रीढ़धारियों में मनुष्य स्वचैतन्य होता है, बौद्धिक और विवेकशील होता है और यह सबकुछ उपयोगिता और उपादेयता पर तय करता है कि अभी और कल किसकी जरूरत है या हो सकती है। सारी चीजें जरूरत, जज्बात और अहसास तथा पारस्परिक पर टिकी हुयी हैं और ऐसी मानसिकता में हम सब जीते हैं जिसकी अनुभूति सबको होती रहती है पर सब इसको अपने अपने हिसाब से व्यक्त करते रहते हैं, कुछ बोलकर तो कुछ लिखकर अपनी अभिव्यक्ति देते रहते हैं।
धन के रहने से, बड़े पद पर रहने से जीवन के मोल और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। किसी को दस करोड़ की लाटरी लग जाए या एकाएक वह स्वयं या उसकी संतानें बड़े पद पर चले जाएं तो एकाएक चमत्कार हो सा हो जाता है। वही व्यक्ति जो उपेक्षित था, हाशिए पर था, वह शीर्ष पर चला जाता है। उसके सारे दोष गुणों में बदल जाता हैं, वह सबके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है।
पर ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, कुछ स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है और ना दुःख, कण कण रोज बदल रहे हैं पर इस बदलाव का हम अवलोकन नहीं करने के कारण द्वन्द्व में रहते हैं और दुखी रहते हैं। अनेकानेक रुपों में दुःख सुख भोगा करते हैं। हम परिणामों और हालातों पर ही चिन्तन करते रहते हैं पर उन कारणों पर नजर नहीं रखते जिनसे सब बदलाव हो रहे हैं और यही महत्वपूर्ण है जो हम सबको समझने की जरूरत है। संसार इसी चक्र पर चल रहा है और चलता रहेगा। समय क्षीप्र गति से चलायमान है जो इसके मार्ग में रुकावट बनता है या रोकने की कोशिश करता है, इसके दो पाटों में पिस कर रह जाता है।
समय की पहचान कीजिए : समय की पहचान कीजिए कि यही आपकी उपयोगिता तय करता है, आपको महत्वपूर्ण या महत्वहीन बनाता है जो मेरे निज की अनुभूति है। दुःख में निराश न होइए और सुख में अति उत्साहित न होइए, सबकुछ बदलते रहता है। सत्य स्थिर है, शाश्वत है, चिरन्तन है परन्तु असत्य अस्थिर और रुपान्तरित होते रहता है और यही दुःख और सुख है।
परन्तु एक अद्भुत चीज भी देखी जाती है कि कुछ लोग दुःख में पैदा होते हैं और दुःख में ही मर जाते हैं और कुछ लोग सुख में पैदा होते हैं और सुख में मर जाते हैं जिसे लोग प्रारब्ध से जोड़ते देखते हैं पर यह प्रारब्ध भी आज तक अज्ञेय सत्ता है।
किसने पूर्व जन्म को देखा जाना है, हमने आजतक ऐसी अनुभूति नहीं की है। कहते हैं कि तथागत सिद्धार्थ ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की और जीवन चक्र से मुक्त हो गये पर उनके जाने के बाद उनके किसी अनुगामी को हमने यह घोषणा करते नहीं देखा कि उनको निर्वाण महापरिनिर्वाण या कैवल्य की प्राप्ति हो गयी। कभी-कभी हमें आजीवकों या चार्वाकियों की सत्य प्रतीत होती है कि
देहस्स भस्मीभूतस्स पुनर्जन्म कुतो।
देहस्स भस्मीभूतस्स पुनर्जन्म कुतो: धरती पर जो है जो दृश्य या अदृश्य है,वही सत्य है। ये बात अलग है कि वे भी इसे सत्यापित नहीं कर पाए कि ईश्वर नहीं है और आस्तिक भी सत्यापित नहीं कर पाए कि ईश्वर है, है तो कैसा है।
हम सब अपने अपने मत विश्वास आस्था श्रद्धा के अनुरूप अपने को उस परम सत्ता को साकार निराकार रुप में जोड़ लेते हैं पर हमारी नज़रों में वो * अज्ञेय है जिसे कभी नहीं जाना जा सकता है।
तो शेष क्या बच जाता है, बस अच्छा सोचिए, अच्छे विचारों का सृजन कीजिए और अच्छा करते रहिए और यही आपके जीवन को सुनिश्चित करेगा कि आपकी मृत्यु के समय आपके सीने पर, आत्मा पर कोई बोझ नहीं रहेगा और यही मुक्ति है बाकी सब शब्दों की महज बाजिगरी है जो हर वैश्विक समाज के कथावाचक सुनाते रहते हैं।
===========
श्री शिव राम कृष्णाय नमो नमः
शिवोहम शिवोहम शिवोहम।
============
-----------
स्वयं की खोज : दास्तानें लैला मजनूं : सम्पादकीय आलेख : १९.
---------------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
स्वयं को जीना : दास्तानें लैला मजनूं : श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा :
स्वयं को जीना : स्वयं को जीना और स्वयं में तल्लीन हो जाना, स्वयं को पाना और स्वयं को खोना, ये जीवन की अलग-अलग अवस्थाएं और अनुभूतियां हैं जिसे अनुभूत करने के लिए बड़ी लम्बी यात्रा करनी होती है।
स्वयं को जीना और उसमें तल्लीन हो जाना बड़ी बेहतरीन और सूक्ष्म कला है, अद्भुत और अद्वितीय
हुनर है। यह अद्भुत अवस्था लगभग हर मनुष्य के साथ उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति के साथ समावेशित है।एक संगीतज्ञ,एक गायक, एक चित्रकार जैसा रचनाकार एक साधक और तपस्वी की तरह होता है, प्रेम में डूबा हुआ एक व्यक्ति भी उन्हीं साधकों की तरह ही होता है जो प्रेम में डूबने की अवस्था में अपने अस्तित्व को एकदम से भूल जाता है।
दास्तानें लैला मजनूं : कहते हैं एकबार मजनूं लैला लैला कहते हुए एक रेगिस्तान से होकर भागा जा रहा था। उसी रास्ते में अपने लाव लश्कर के साथ एक बादशाह भी मौजूद था। नमाज़ का वक्त था,वह जाजिम बिछाकर नमाज अदा कर रहा था। मजनूं अपनी धुन में चला जा रहा था और बेखूदी में वह जाजिम पर दौड़ते हुए चला गया कि वह बेसुध था। बादशाह यह सब देख रहा था कि वह होश में था। दूसरे दिन बादशाह ने उसे पकड़ बुलवाया और कहा, अरे बेवकूफ, क्या तुम अंधे थे कि तुम्हें नजर नहीं आया कि हम नमाज अदा कर रहे थे, इसे सूली पर चढ़ा दो,
उसने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया, ' हां हुजूर, हम तो इश्के मिज़ाजी ( सांसारिक प्रेम ) में गुम थे जो
आपको न देख सके पर आप तो अल्लाह की इबादत में थे, इश्के हकीकी ( अलौकिक प्रेम ) में थे फिर आपने हमें कैसे देख लिया, हम तो हकीकत में गुम थे पर आप तो अल्लाह के साथ फरेब कर रहे थे, फिर हमें सजा क्यों ?
सुल्तान बेवकूफ नहीं था, वह हकीकत समझ गया और उसने मजनूं को माफ करते हुए, माल असबाब देते हुए बाइज्जत विदा कर दिया और खुद फकीर बनकर निकल गया।
श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा : स्वयं को जीना और स्वयं में तल्लीन हो जाना जीवन के अर्थ की चरम सीमा है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही दिवानी होकर नाचते गाते साधुओं की जमात में मिलकर बेसुध हो जाती थी, गोपियां श्री कृष्ण के बंशी की आवाज सुनकर वैसे ही बेसुध होकर भागती चली जाती थीं कि उन्हें अपने पति और पुत्र का भी लोकलाज और मोह खत्म हो जाता था,सारे भाव तिरोहित हो जाते थे बस श्री कृष्ण की छबि उनके जेहन में रहती थी। यही अवस्था योग की है कि जब हम किसी से पूर्णतः जुड़ जाते हैं तो स्वयं को पाने खोने और स्वयं में तल्लीन हो जाने की अवस्थाओं का समेकन हो जाता है।
मंसूर ने एकाएक चिल्लाना शुरू कर दिया,अनलहक अनलहक अर्थात् मैं ही हक हूॅं,सत्य हूॅं और ख़ुदा हूॅं। उसे इलहाम हो गया कि खुदा खुद से जुदा नहीं है, यही सच है जिसे महावीर बुद्ध नानक कबीर रविदास मीरा आदि ने जान लिया था और सबने अपने को जाना और खो दिया। सबके सब स्वयं में तल्लीन हो गए और उनमें सबकुछ नवीन और मौलिक हो गया।
एक शराबी शराब के नशे में,एक अपराधी अपराध करने में, एक शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया में ऐसे ही गुम हो जाता है और उसके सामने सिवाय उस अवस्था के कोई और बोध नहीं होता है और वह उस दुनिया में जीवित रहता है जहां द्वैत अद्वैत हो जाता है। जीवन के इस सच को जानने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। जो कुछ आप जी चुके भोग चुके उन्हें विस्मृत करते हुए उन भावों को तिरोहित करना पड़ता है और तभी स्वयं को जानने,खोने और फिर स्वयं में तल्लीन हो जाने की अवस्था प्राप्त होती है।
यह भी सत्य है कि आप राम कृष्ण महावीर बुद्ध मंसूर मीरा आदि नहीं बन सकते परन्तु सद्गुरु कबीर के शब्दों में लाल की लालिमा तो पा ही सकते हैं,
लाली मेरे लाल की जित देखौं तित लाल
लाली देखन मैं गयी मैं भी हो गयी लाल।
स्वयं की खोज में स्वयं का भाव तो तिरोहित होना : कालिख की कोठरी में घुसने पर कालिख तो लगनी ही लगनी है वैसे ही स्वयं की खोज में स्वयं का भाव तो तिरोहित होना ही होना है, लाली देखते देखते तो लाल हो ही जाना है, यह सिर्फ आख्यान या दर्शन नहीं बल्कि व्यवहार में भी सत्य है।
सांसारिक जीवन में भौतिक उपलब्धियां करनी है, अभिष्ट को पाना है तो सिर्फ अभिष्ट ही नजर आना चाहिए, शेष भावों को तिरोहित हो जाना चाहिए, पक्षी नहीं सिर्फ आंख की पुतली नजर आनी चाहिए तभी कुछ पा सकते हैं,बगैर स्वयं में स्वयं को तल्लीन किए बिना जो मिलेगा, क्षणिक होगा, आएगा और जाएगा,सुख जाएगा दुःख जाएगा, दुःख जाएगा सुख आएगा और यह क्रम चलता रहेगा और यही संसार है जो नित परिवर्तनशील और नाशवान है।
शराब के नशे में कब-तक गुम होते रहोगे,एक समय आएगा कि यह भी सुख नहीं देगा,स्थायी सुख अर्थात् आनन्द की अवस्था को पाना है जो कभी न जाएगा, एकबार मिल गया तो मिल गया, एकबार लालिमा मिल गयी तो मिल गयी।
क्या यही संसार है, फिर लोग जी कैसे रहें हैं, इतनी भाग - दौड़ क्यों है,मारा मारी क्यों है,बस अहंकार और महात्वाकांक्षा की लड़ाई और संघर्ष है और वह भी कब-तक जब-तक शरीर में बल है, रक्त संचार तीव्र है,
प्राणों में उत्तेजना है,ये सब निर्बल हुए कि सब खत्म और खोज जारी पर तब तक लाल की लालिमा भी समाप्त, इसलिए निर्बल होने के पूर्व स्वयं को स्वयं में तल्लीन करने का हुनर सीख लेना है और मजनूं की तरह बेखुदी में गुम हो जाना है।
============
अरुण कबीर
------------
हृदय में एक राग : प्रेम राग : आलेख : १८.
-------------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
हृदय में एक राग : राग सिर्फ वाद्ययंत्रों से ही नहीं निकलते बल्कि सबके हृदय में एक राग बसता है जो सुषुप्तावस्था में रहता है जिसका प्रस्फुटन तब होता है जब मन हृदय मस्तिष्क और अंत में आत्मा पीड़ित हो जाती है और उसी राग का नाम भक्ति और प्रार्थना है।
जब किसी की पीड़ाओं को दुःख तकलीफ को कोई नहीं सुनता तो भीतर से आर्तनाद उठता है,वही हृदय का आत्मा का राग है।
हरि की रक्षा : गज ग्राह : हिन्दू पौराणिक गाथाओं में गज ग्राह के संघर्षों की एक कहानी आती है,गज अर्थात् हाथी के पांव को ग्राह अर्थात् मगरमच्छ अपने जबड़े में जकड़े हुए हैं और बचने का कोई उपाय नहीं रह गया था तो हाथी ने श्री हरि के चरणों को स्मरण करते हुए चिंघाड़ता है,
हे नारायण हे नारायण मेरी रक्षा करो। कहते हैं श्री विष्णु उसके आर्तनाद को सुनते ही सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ पड़े और गज की रक्षा की।
परमात्मा सब की रक्षा करते है : परमात्मा हर क्षण किसी न किसी रुप में सबके पीछे खड़े रहते हैं, बस एकबार हृदय की गहराइयों से आवाज देने की जरूरत है,वे रक्षार्थ आ खड़े होंगे और आपको पता भी न चलेगा कि कब आपकी सहायता हो गयी और आप सुरक्षित हो गए। बस एकबार पुकार कर तो देखिए।
हर हर महादेव जय सदाशिव सबका कल्याण हो।
----------
वक्तव्य, वक्ता और श्रोता.सम्पादकीय : आलेख : १७ .
-----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
आप कुशल वक्ता हैं और जिस भी विषय पर आप बोलते हैं, तथ्यात्मक और तार्किक बोलते हैं परन्तु ध्यान रहे कि पहले आपको श्रोता वर्ग के मानसिक स्तर का आकलन करना होगा अन्यथा आपकी सारी विद्वता और क्षमता व्यर्थ जाएगी और आपके सारगर्भित वक्तव्य को अनर्गल प्रलाप समझा जाएगा।
जहां आस्तिकों की भीड़ हो और एक मत के मानने वाले ही लोग हों वहां चार्वाक दर्शन पर आपके वक्तव्य वैसे ही होंगे जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या आस्तिक चार्वाक को
सुनना पसन्द नहीं करेंगे, करेंगे पर उनके मस्तिष्क के दरवाजे खुले होने चाहिए कि उनके हृदय में ईश्वर है
पर मस्तिष्क को चैतन्य होना चाहिए ताकि वे सुनें मनन और विश्लेषण करके कुछ प्राप्त कर सकें कि आस्तिकता और नास्तिकता दो ध्रुव नहीं हैं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसकी धूरी एक ही है।
ईश्वरीय सत्ता : भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे पर ईश्वरीय सत्ता को सीधे इन्कार न करके अव्याकृत प्रश्न या अस्तित्व बताते थे कि वह कालखंड ऐसा ही था जिससे आत्मा परमात्मा के नाम पर चल रहे कर्मकाण्ड से सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचनाओं को बचाकर एक नयी दिशा देनी थी।
इसलिए तत्कालीन समाज को यह बताया गया कि मनुष्य ही श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ गुणधर्मों का पालन करके जीवन को परिष्कृत और परिमार्जित करके भगवत्ता को प्राप्त कर भगवान की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है की मानव का सर्वश्रेष्ठ रुपान्तरित रुप ही भगवान है। आप ईश्वर या ब्रह्म या परब्रह्म नहीं बन सकते पर भगवत्ता पाकर ईश्वरीय सत्ता में स्वयं को समावेशित करके विराट हो सकते हैं।
अब यदि आमजन के समक्ष आप भगवान बनने की बात करते हैं तो हास्य के पात्र बनते हैं कि उनकी नजरों में भगवान एक अलौकिक सत्ता है जो आदमी नहीं हो सकता है। लेकिन आपने किसी को यह कहते तो सुना होगा कि अमूक व्यक्ति तो मेरे लिए भगवान बन कर आया था या है, अर्थात् उस व्यक्ति ने उसके लिए कुछ ऐसा कर दिया जो आम आदमी किसी के लिए नहीं कर सकता है और यही अवस्था जब विराट रूप धारण कर लेती है तो उस व्यक्ति का स्वरूप भगवान का हो जाता है।
लघु से विराट का रुपान्तरण : अब सुनने वालों की भीड़ कृष्ण भक्तों या राम भक्तों या शिव भक्तों की हैं तो वह आपके इस व्याख्यान को कतई सुनना पसन्द नहीं करेगा परन्तु एक शुद्ध बुद्ध सुनेगा और उसी में शिव राम कृष्ण महावीर बुद्ध जीसस नानक आदि के अस्तित्व की खोज करेगा कि सबने विराटता को प्राप्त किया हुआ है। लघु से विराट का रुपान्तरण ही मानव से भगवान बनना है।
कृष्ण का गोपाल और कन्हैया से योगेश्वर कृष्ण बनना,राम का रघुनंदन से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना,
गौतम सिद्धार्थ का तथागत बुद्ध बनना और महावीर का जीण महावीर बनना ऐसी ही घटनाएं हैं जिसे समझने के लिए मन हृदय और मस्तिष्क के विराट होने की जरूरत होती है अन्यथा बुद्ध वचन को
बौद्ध मत का संदेश समझा जाएगा। सुकरात, गैलेलीयो, मंसूर आदि ऐसे बुद्ध वचन बोलने वाले थे जिन्हें तत्कालीन समाज ने नहीं स्वीकार किया और कालान्तर में उन पर शोध होने लगे। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा भी है कि,
कबीर
हीरा तहं न खोलिए जहां खोटी हो हाट
कसके बांधों गाठरी लेकर चल दो बाट।
अरुण कुमार सिन्हा कबीर,
कवि, साहित्यकार, चिन्तक,आलेखक.
दुमका, झारखण्ड.
-----------
स्वर्ग और नरक : आपके भीतर ही : सम्पादकीय : आलेख : १६.
----------
अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड
आपके भीतर ही स्वर्ग और नरक : पृथ्वी की तरह स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आपके भीतर ही स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा या कल्पना लगभग सभी मत पंथ विश्वास विचार और सम्प्रदायों में किसी न किसी रूप में है जो मनुष्यों को संयमित अनुशासित और नियमित करने के लिए बनायी गयी हैं।
वैश्विक स्तर पर सभी धर्म शास्त्रों एवं संदेशों में कर्म की श्रेष्ठता को मान्यता दी गयी है और सबको मानवोचित कर्म और विहित कर्तव्यों का पालन करने को कहा गया है कि जीवन जो परमात्मा ने दिया है,
उच्छृंखल और अमर्यादित न हो कि जो क्रियाशीलताएं अपनी मर्यादा और सीमाओं से बाहर गयी हैं, विनाश का कारण बनी हैं इसलिए कहा गया कि बुरे और प्रकृति के विरुद्ध किए गए कर्म ही दुःख पीड़ा और क्लेश के कारण बनते हैं।
अति सर्वत्र वर्जयेत्. इसलिए सभी धर्म शास्त्रों में अति से बचने को कहा गया है। जैन और बौद्ध दर्शन में अति से बचने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। यही अति व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी और अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को अहंकारी बना देती है और यही अहंकार व्यक्ति को पतनोन्मुख बना देता है जो रावण जैसे ज्ञानी का भी नाश कर देता है और नरक गामी बना देता है।अब्राहमिक मतों : अब्राहमिक मतों में भी द डे औफ जजमेंट या कयामत का दिन या दिने अखिरत की चर्चा की गयी है जहां कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का अंतिम भोग तय किया जाता है और उसकी कोई माफी नहीं होती, वास्तव में मरने के बाद क्या होता है, अभी तक शोध और विवेचना का विषय है परन्तु जीवन सही मार्ग पर चले इसके लिए यह तय किया गया है।
जन्म जन्मांतर तक पुनर्जन्म की व्यवस्था : भारतीय उपमहाद्वीपीय आध्यात्मिक और कर्म काण्डिय व्यवस्था में इससे इतर व्याख्या है जो स्वर्ग नरक भोग के साथ जन्म जन्मांतर तक पुनर्जन्म की व्यवस्था है जो स्वर्ग नरक और मोक्ष या कैवल्य या निर्वाण की अवस्था से जुड़ी हुयी है।
स्वर्ग का सुख और नरक का दुःख : स्वर्ग का सुख और नरक का दुःख सूक्ष्म और भौतिक दोनों है जो हिन्दू जीवन दर्शन के मुख्य अंगों में से एक है जिसे नियति या प्रारब्ध कहा गया है।
भौतिक जगत में एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी स्वर्ग है और इसके विपरीत की अवस्था नरक है। कहा भी गया है, पहला स्वर्ग निरोगी काया दूजा स्वर्ग हो घर में माया ( धन संपदा) तीजा स्वर्ग सुशीला नारी चौथा स्वर्ग संतान आज्ञाकारी
अर्थात् शरीर निरोगी हो,घर में समृद्धि हो, स्त्री सुशील हो और संतानें मर्यादित हों तो यही स्वर्ग है और इसके विपरीत चारों अवस्थाएं ही नरक है और ये अवस्थाएं द्रष्टव्य हैं जिसकी अनुभूति भौतिक और सूक्ष्म दोनों रुपों में होती है जो सबकी अनुभूति है।
चार्वाक दर्शन स्वर्ग नरक का खंडन : चार्वाक दर्शन इसीलिए स्वर्ग नरक का खंडन करता है और भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। चार्वाकों में श्रेष्ठ पूरन कस्सप कहते हैं कि कोई सत्ता भौतिक जगत से इतर नहीं है, यहां सबकुछ स्वत: स्फूर्त है, कोई कारण नहीं सब अक्रियावादी व्यवस्था है परन्तु बाद में बुद्ध ने इसका खंडन करके कारण और कार्य के सिद्धान्त को जन्म दिया जिसे संसार चक्र कहा जाता है जो कर्मजनित फलाफल के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए मेरी राय में मनुष्यों की चेतना ज्यों ज्यों जागृत होती गयी, त्यों त्यों जीवन के मापदण्ड और नियामक कारक बदलते चले गए पर नहीं बदले कर्म के फलाफल के सिद्धान्त और यही कालांतर में स्वर्ग नरक की अवस्था की कल्पना या अवधारणा को जन्म दिया कि स्वर्ग या नरक दोनों है, भौतिक भी और सूक्ष्म भी है। जीवन सुखमय है तो स्वर्गमय अनुभूति होती है और जीवन दुखमय है तो नरकमय अनुभूति होती है।
आपने अपने परिवेश और यात्रा आदि के क्रम में भिखारी बुरी तरह दिव्यांग या व्याधिग्रस्त आदि को देखा होगा, जिन्हें देखकर लोग यही सोचते हैं कि हे परमात्मा,ऐसी जिंदगी किसी को न देना परन्तु वह जीवन का दुःख भोग है जो भौतिक और सूक्ष्म दोनों रुपों में नरकमय है,उसी क्षण आपकी नजरें एक बढ़िया कार से एक सुखी स्वस्थ समृद्ध परिवार को उतरते देखकर कहते हैं,अहा, क्या जिन्दगी है,इनके पास सबकुछ है, स्वर्गमय जीवन है।
पर सबकुछ परिवर्तनशील है,सारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं और अनुभूतियां भी बदलती रहती है। बाईबल दर्शन : बाईबल कहता है, The God is in the heavens and everything is right on the earth,
पर ऐसा तभी हो सकता है जब हम सब जीवन के मोल और मूल्यों को समझते हुए एक मर्यादित और संयमित जीवन जिएं जो आमतौर पर व्यवहार में नहीं हो पाता है और जीवन का स्वरूप बदलता रहता है।
जबतक शरीर में रक्त संचार तीव्र रहता है, ऊर्जा बनी रहती है तब तक हम जीवन को अपने तरीके से जीते रहते हैं और शरीर के व्याधिग्रस्त होने या कमजोर होने पर समय हमें जीने लगता है और अनुभूतियां बदल जाती है।
स्वर्ग का रुपान्तरण नरक में हो जाता है,यही स्वर्ग और नरक की अवस्थाएं हैं जो मनुष्य को चैतन्य काल से अनुप्राणित करती रही हैं कि स्वर्ग और नरक भौतिक और सूक्ष्म दोनों प्रकार की अनुभूतियां हैं जो सबको सही जीवन मार्ग अपना कर चलने की प्रेरणा देती है कि मनुष्य अपने इर्द-गिर्द इनका निर्माण करता रहता है।
सिर्फ मनुष्य ही नहीं देवदूतों पैगम्बरों अवतारी पुरुषों संतों संन्यासियों आदि को भी इन दोनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ा है। जिसस का क्रुसिफिकेशन,राम का वनवास कृष्ण का संघर्ष पाण्डवों का वनवास आदि इसके जीवन्त उदाहरण हैं जो कर्म के सिद्धान्त से जुड़े हुए हैं और इनके पीछे उपरोक्त जीवन दर्शन जुड़े हुए हैं जो मत मतान्तरों में विभक्त हैं पर स्वर्ग नरक सबके लिए है जो भोग काल से जुड़े हुए हैं।
लेखक कवि विचारक : अरुण कुमार सिन्हा. झारखण्ड
आलेख : संपादन. शक्ति : रेनू शब्द मुखर / जयपुर.
आलेख : पृष्ठ सज्जा. शक्ति अनुभूति / शिमला.
-----------
स्वयं जागना होगा : सम्पादकीय : आलेख : १५ .
------------
इसके पहले कि कोई आपको जगाने की कोशिश करे, स्वयं जागने की कोशिश करें कि आपका जागना ही आपका जीवन है।
जागना सूक्ष्म और स्थूल दोनों हैं,निन्द से तो घड़ी की घंटी भी जगा देती है पर अपनी चेतना और चैतन्य बोध को तो आपको स्वयं जागृत करना होगा और ऐसा इसलिए जरूरी है कि
मृत्यु पूर्व मनुष्य की समस्त स्मृतियां जीवन्त हो उठती है और मृत्यु के ठीक पूर्व आपकी चेतना आपसे ही सवाल करती है कि आपको क्या करना था और आपने क्या किया और तब आपको अपने कृत कर्म आईना बनकर आपके सामने जीवन्त हो उठते हैं और उस वक्त सिवाय
आंसू और पश्चाताप के आपके पास कुछ नहीं रहती है।
इसलिए आत्मिक चेतना को इसी क्षण से जागृत और आत्मसात करना शुरु कर दीजिए कि कोई बाहरी प्रकाश आपके भीतरी अंधकार को नहीं मिटा सकता है और यही आन्तरिक तमस आपको समझना है वो क्या है
और इसकी परख होते ही आप उस अंतिम क्षण की सुखद अनुभूति के लिए तैयार हो जाते हैं और पश्चाताप के भाव तिरोहित हो जाते हैं।
विचार करें।
===========
अरुण कबीर।
---------
जीवन मोल : सम्पादकीय :आलेख : १४.
----------
धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि आप कमा सकते हैं,संचय भी कर सकते हैं पर इनके भोग भाग्य के लिए जो सबसे अनिवार्य वस्तु है जिसके बगैर यह निरर्थक है वह है श्वांस जो न तो कमाई जा सकती है और न संचय की जा सकती है। प्रकृति ने इसे गिनकर सभी जीवित प्राणियों को दिया है और लोग उसी की उपेक्षा करते हैं। जो गिनती की है, निश्चित है,न कम न ज्यादा, उसपर आपका ध्यान कभी नहीं जाता और जिसकी गिनती की जा सकती है,आप उसी के पीछे दीवानेबने फिरते हैं।सांस है तो जीवन है और जीवन है तो दुःख सुख का भोग भाग्य है।
सांस की तरह ही मूल्यवान प्रेम और संवेदना है जो अभौतिक है, इन्हें भी न तो क्रय विक्रय किया जा सकता है और ना ही संचय किया जा सकता है परन्तु इसके बगैर भी जीवन अर्थहीन ही हो जाता है।
प्रेम और संवेदना, जीवन के दो ही तो मोल और मूल्य हैं। जिनके हृदय में सहज प्रेम का वास होता है वहीं सहृदय होते हैं और जो सहृदय होते हैं वही सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील भी होते हैं।
सभी मत पंथ विश्वास विचार सम्प्रदायगत वर्ग आदि भी इनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही भक्ति मुक्ति मोक्ष आदि का मार्ग है। ईश्वरीय सत्ता भी इसी प्रेम से बंधी है। पूजा जप तप साधना आदि अगर प्रेम से वेदना से अनुप्राणित न हो तो वह प्रदर्शन मात्र ही हो सकता है, उसमें यथार्थ हो ही नहीं सकता है। कहा भी गया है,पूजा जप नेम अचारा नहीं जानत हौ दास
तुम्हारा, जिसके हृदय में प्रेम बसा हो उसे किसी नीति नियम की जरूरत नहीं होती है।
रामायण के दो पात्र शबरी और निषादराज इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। शबरी प्रेमपूर्ण हृदय से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती है और श्री राम आ जाते हैं, निषादराज प्रेम-भाव से चरणामृत पान करता है और दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही पात्र जैन और बौद्ध दर्शन में दिखाई पड़ते हैं। बाईबल में भी एक कथा अबू बेन अदम की आती है जो चर्च नहीं जा पाता कि वह लोगों की सेवा में लगा रहता है पर ईश्वर की सूची में सबसे उपर उसी का नाम होता है।
हिन्दू जीवन दर्शन में जिन पंचमकारों की यथा,काम क्रोध मद मोह लोभ की चर्चा की गयी है,वह प्रेम सेवा भाव और संवेदना के आते ही तिरोहित हो जाते हैं।
आम आदमी भी श्रेष्ठ स्थान को पा लेता है। परिवार और समाज के जीवन मोल और मूल्य भी यही हैं जिनके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है।
एक सरमन कहता है,
A heart which is filled with love passion and sensitivity is the place where God lives.
इसलिए सबसे प्रेम भाव और सबके प्रति सेवा भाव रखिए,यही मोक्ष, कैवल्य और निर्वाण का मार्ग है।
----------
जीवन भूत : वर्तमान और भविष्य : आलेख : १३ .
-----------
जीवन भूत वर्तमान और भविष्य का एक अद्भुत समागम है जहां अपेक्षित और अनापेक्षित घटती रहती हैं,घटती हैं और घटती रहेंगी।
जो घटनाएं घट गयी वो पथ-प्रदर्शक हैं,जो घट रही हैं साथी हैं और जो घटने वाली हैं,न मित्र हैं न अमित्र हैं कि वे भविष्य के गर्भ में हैं, अनुकूल हों तो मित्र हैं और प्रतिकूल हों तो अमित्र हैं।
इसलिए समय का सम्मान करते रहें,यही था,यही है और यही रहेगा।
========
आपका दिन मंगलमय हो।
सादर सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम।
========
⭐
---------------------
अभी - अभी : हम और हमारी नागरिक चेतना : आलेख : १२.
-------------
⭐
विद्यार्थी जीवन में हमलोगों ने छठे वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर तक * लोकतंत्र
और इसकी सफलता को पढ़ते रहे हैं और आज भी पढ रहे है परन्तु जरूरत है, इसकी सफलता और विफलता के जिम्मेदार कारकों को समझना और उसके निदानों की खोज करना, वैश्विक स्तर पर बदलते सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मोल एवं मूल्यों के सन्दर्भ में बदलते लोकतांत्रिक मापदण्डों का अवलोकन व विश्लेषण करना और उसकी स्थिरता की खोज करना है। एक तरफ हमारे सामने ** Democracy is the govt. Of the
People, for the People and by the People है , * Democracy provides the broader Spectrum for the broader development of the Human Qualities Virtues and Potentialities है तो वहीं * जम्हूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिसमें इन्सान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता और अब समय है वैश्विक स्तर पर
इसमें वांछित संशोधन व सम्यक् बदलाव करने की जिसके लिए * समग्र नागरिक चेतना की अपरिहार्यता है।
मै अब निजी तौर पर बड़े बड़े * राजनीतिक दार्शनिकों चिन्तकों और राजनेताओं को उद्धृत करना गैरमुनासिब सा समझता हूँ कि आज तक उनकी बातों को या तो आम जन तक नहीं पहुँचाया गया या * हमारे लोगों ने जानबूझ कर इसे समझने की कोशिश नही की।
हमारी अब तक की जो समझ और अनुभूति रही है, राजनीतिक व गैर राजनीतिक लोगों के साथ* interaction से जो बाते समझ में आयी है , वह यह है कि हमारे मुल्क़ में
* बुनियादी और मौलिक शिक्षा त्रुटिपूर्ण
और समयानुकूल मांगों के अनुरूप नहीं रही है, शायद अब सुधर जाए और दूसरे
नागरिक चेतना का सख्त अभाव रहा है जो * सुरसा की तरह मुँह फैलाए जा रही है और उसके पीछे भी यही शिक्षा है।
बच्चे तो * गूँथी हुयी मिट्टी के ढेर की तरह है, जैसे ढालो, ढलते जाएँगे और फिर जैसी आकृति देना चाहें, दे सकते हैं और इस दिशा में * नागरिक चेतना और भारत जैसा विषय स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने की सख्त जरूरत है ताकि बच्चे शुरू से अपने कर्तव्यों का पालन करना अपने संस्कार और चरित्र में शामिल कर लें। हालांकि * नागरिक चेतना का अभाव वैश्विक समस्या है पर भारत तो इसका
शिकार है। यातायात, विधि व्यवस्था, विकास, पारस्परिक सम्बन्धों की निर्भरता, मानवोचित मूल्यों के विकास , कानून और न्यायपालिका का सम्मान, सामाजिक स्तरीकरण में बदलाव, सामाजिक आधारभूत संरचना के प्रति
संवेदनशीलता, राजनीतिक सूझ बूझ और चयन , सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता जैसे मुद्दे इसी परिष्कृत शिक्षा
और नागरिक चेतना के विकास पर निर्भर करते है।
ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग इन मूल्यों का सम्मान नहीं करते परन्तु
भारतीय समाज ( अधिकांश) को इनसे शायद कोई लेना देना नहीं है।
राजनीतिक दर्शन और चिन्तन में साम्यवाद के बारे में एक जगह हमने पढ़ा था कि * Are u going to farming " Roses, then u must
Know the basic art of farming roses and those r, testing and preparing the soil, reading the
atmosphere, uses of fertilizer and pesticides and seasonal
Branch cutting and caring instinct and there will be a nice farming of Roses.
और यही हकीकत लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ है कि हमने
इसकी उन पृष्ठभूमियों को मज़बूत करने
की कोशिश ही आज तक नहीं की या इन्हें जानबूझ कर पनपने ही नही दिया गया।
आज साम्यवाद वैश्विक स्तर पर इसलिए पतोन्मुख होता चला गया कि
इसे महज एक राजनीतिक दल ही समझा गया, जीवन शैली और दर्शन तथा चिन्तन नहीं समझा गया, कालखण्डों में वांछित मानवोचित मूल्यों और जरूरतों उसभें समावेशित नहीं किया गया। उसके स्थापित module को ही ग्राह्य माना गया और ठीक इसी प्रकार लोकतंत्र है, यह समय और सभ्य समाज की मांग है पर इसकी भी देखभाल नहीं की गयी तो * लोकतंत्र का पौधा जिन्दा तो दिखाई देगा पर * एक जिन्दा मांस पिण्ड की तरह जो हिलता डूलता तो दिखाई देगा परन्तु गतिमान नहीं होगा।
हमने खाना पीना और नित्य क्रिया तो सीख लिया पर उसके हुनर और गुणवत्ता को नहीं सीखा।
अब भी वक्त है कि हम घर से इसकी शुरुआत करें और नागरिक चेतना युक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। विशेषकर
भारत जैसे विशाल आबादी वाले * बहुभाषायी, बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक तथा बहुआयामी देश के लिए तो इस सोंच का सृजन पोषण और संरक्षण तथा संवर्धन अपरिहार्य है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी बदलाव की ओर इंगित करते हुए पार्थ को * सम्यक् चेतना और कर्तव्य पालन की सीख देकर महानायक और कालातीत योगेश्वर कृष्ण हो गए। कोई भी व्यक्ति समाज संस्था और राष्ट्र अपने
मोल मूल्यों तथा जड़ो से कटकर लम्बे समय के लिए जीवित नहीं रह सकता है, जीवित और क्रियाशील रहना है तो सबको * पुरे सामर्थ्य के साथ बदलना होगा। यही लजह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में समय समय पर
* संविधान और प्रशासनिक तंत्र में
वांछित बदलाव किए जाते रहे हैं। समय रहते ही बदलाव किए जाते रहे हैं
और नहीं तो समय अपने हिसाब से सब
बदल देता है और इन सबके मूल में * नागरिक चेतना ही है। मेरी प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दर्शन चिन्तन या दल से नहीं है किये सब परिवर्तनशील हैं और समय की मांग के अनुरूप स्वयं को बदलते रहते हैं पर नहीं बदलते हैं जीवन के मोल और मूल्य और उसे ही बनाए रखना नागरिक चेतना का प्रथम कर्तव्य है।
विचार करें।
========
अनन्त शुभकामनाएँ ।
असीम मंगलकामनाऍं।
सादर सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम
-------
जीवन और अनुभूति : आलेख : ११
----------
संसार वही रहता है, हम वही रहते हैं, समाज परिवार और परिवेश भी वही रहते हैं, जीवन जो हम जी रहे होते हैं वही रहता है परन्तु सुख और दुःख में जीवन की अनुभूतियां बदलती चली जाती हैं।
सुख में सबकुछ ग्राह्य लगता है,लोग अच्छे लगते हैं, आहार विहार भी अच्छे लगते हैं, प्रकृति के सौंदर्य अच्छे लगते हैं परन्तु दुःख के आते ही सबकुछ बदल जाता है। जीवन और संसार को देखने भोगने का नजरिया बदल जाता है।
संसार लोग और परिवेश वही रहता है पर जो दुःख में रहता है,उसे जीवन रसहीन सा लगने लगता है। उसका सारा ध्यान उस दुःख पर केंद्रित हो जाता है जिससे उसका जीवन दुखमय हो गया है। अब यहीं व्यक्ति के सशक्त अस्तित्व और व्यक्तित्व, संघर्षशील चरित्र, जीवटता और जिजीविषा की परख होनी शुरू हो जाती है।
ऐसा नहीं है कि सुखी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है पर दुखी की तुलना में उसके संघर्षों की
प्रकृति अलग होती है। वह उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ता है और दुखी अपने दुःख के साथ संघर्ष करते हुए संघर्ष करता है।
परन्तु जीवन का दर्शन और व्यवहार को यहीं पर बदलने की जरूरत होती है। मानसिक और आत्मिक शक्तियों को समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हर वैसे व्यक्ति को अपने अतीत में झांकने की जरूरत होती है कि जब जब उसके जीवन में प्रतिकूलताएं उत्पन्न हुयी हैं तो उसने क्या किया है,कैसे उस पर विजय पायी है या वे समस्याएं हल हुयी हैं तो कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं, पहला कि वह समस्याओं का आकलन करता है,उनकी जड़ों की तलाश करता है,अपने आराध्य या इष्ट को स्मरण करता है, धैर्य के साथ विश्लेषण करता है और धीरे-धीरे सहनशीलता के साथ आगे बढ़ता है तो पाता है कि समस्या जितनी गंभीर नहीं थी,उसने नाकारात्मक तरीके से सोचकर गंभीर बना दिया था।
हर प्रतिकूलताओं में
साहस, धैर्य, सहनशीलता,
सही दिशा में प्रयास, आत्मविश्वास और आत्मबल, अपने शुभेच्छुओं के सहयोग और अपने इष्ट को स्मरण रखने की जरूरत होती है और अंत में वह व्यक्ति स्वयं ही अपना अंतिम अस्त्र-शस्त्र होता है। अंतिम लड़ाई उसे स्वयं लड़नी होती है और वही विजयी होता है।
धैर्य,साहस, सहनशीलता, जिजीविषा और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं होता है और स्मरण रहे कि संसार की समस्त क्रियाशीलताऍं और घटनाएं कालबद्ध है,सब
सुख दुःख का समय निर्धारित और निश्चित है फिर धैर्य के साथ अवलोकन कीजिए और बदलाव की प्रतीक्षा कीजिए कि जो आज है कल नहीं रहेगा। भगवान श्रीकृष्ण और तथागत सिद्धार्थ ने अपने अपने दर्शन और व्यवहार में इसी सत्य को दिखाया है और इसी सत्य को समझना जीवन के यथार्थ को समझना और जीना है।
========
आपका जीवन सुखी स्वस्थ और समृद्ध हो।
हार्दिक मंगलकामनाएं
हार्दिक शुभकामनाएं।
सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम।
--------
भीड़ और पहचान : आलेख : १०
------------
भीड़ या समूह का हिस्सा बनने का अभिप्राय अपने वजूद या अस्तित्व को खो देना है। इससे बेहतर अपने पुरे वजूद, अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ अकेले तन कर खड़े रहना है। इसमें पहचान सिर्फ नेता अगुआ या नेतृत्वकारी व्यक्ति का होता है। वह अपनी पहचान को स्थापित कर लेता है और भीड़ या समूह * भेड़चाल में एक समूह बनकर ही रह जाता है।
इतिहास, वैश्विक स्तर पर यही कहता है।
स्वयं का सृजन करने के लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व की अनुभूति करनी होगी।
* सिंहों के लेहड़े( समूह) नहीं हंसों की नहीं पात लालों( एक रत्न)की नहीं बोरियाँ, साधु न चले जमात।
========
अरुण कबीर
अनन्त शुभकामनाएँ
असीम मंगलकामनाऍं
सादर सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम
-------------
अभिव्यक्ति अब के प्रसंगों पर : आलेख : ९
---------
इटली में एक समय एक बेहतरीन चित्रकार हुआ करता था जिसकी कोई भी रचना आलोचना या टीका टिप्पणी से परे होती थी।
एक बार उसने अपने जीवन की शानदार रचना ( चित्र) बनायी तो उसके एक दोस्त ने कहा कि, * शायद इसके बाद तुम चित्रकारी छोड दोगे। आज तक तुम्हारी कल पर कभी आँच नहीं आयी । इस बार एक काम करते है कि इस शानदार तस्वीर को राजधानी के मुख्य चौराहे पर इसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं और एक सूचना दे दी जाए कि * इस तस्वीर में जहाँ कहीं कोई त्रुटि नजर आए तो उस जगह पर एक काला निशान लगा दिया जाए। तस्वीर रख दी गयी और दूसरे दिन देखा गया कि पुरी तस्वीर * काले निशानों से भरी हुयी है और तस्वीर एक तरह से अस्तित्वहीन
हो चुकी है।
दूसरे दिन उसकी प्रतिलिपि इस सूचना के साथ रखी गयी कि इस तस्वीर की
* खासियत और त्रुटि सुधार पर अपनी राय/ सलाह दें।
तीसरे दिन किसी का सुझाव/ परामर्श
और खासियतों पर कोई टिप्पणी नहीं
आयी और तस्वीर सलामत थी।।
यह वैश्विक त्रासदी है और हकीकत भी।
हम किसी व्यक्ति/ वस्तु/ नीति/ सिद्धान्त आदि का जब भी मूल्यांकन/
समीक्षा करते है तब * एकांगी ही करते है। आलोचना करते है, उनकी त्रुटियों की निन्दा करते हैं परन्तु * समीक्षा/ समालोचना नहीं करते है कि सब कुछ
* अच्छा नहीं हो सकता है, उसे अच्छा बनाना पड़ता है या उसके अनुकूल ढल जाना पड़ता है।
उस चित्रकार की तस्वीर बिल्कुल निर्दोष थी परन्तु त्रुटियाँ चुननी थी तो सबने अपने अपने अंदाज़ में, अपने अपने नजरिए और समझ के अनुसार चुन दी परन्तु किसी ने उसकी खासियतें नहीं बतायी और ना ही बेहतरी के सुझाव दे पाए।
आज हमारे समाज की आधारभूत संरचनाओं की ऐसी ही मनोदशा है।
हमारा समाज धीरे-धीरे * भीड़तंत्र का शिकार होता छा रहा है। एक ने नाक पर आपत्ति की तो दूसरे ने आखों पर की और येन केन प्रकारेण तस्वीर ही गायब हो गयी। परन्तु संवाद स्थापित नही हो पाया कि उनकी नजरों में ये गलत है तो क्यों गलत है और इसे कैसे और कितना सुधारा जाए।
भीड़ का निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता है और न हुआ है कि भीड़ किसी एक की नहीं सबकी आवाज सुनती है और उस तुमुलनाद में मौलिक स्वर * नक्कारखाने में तोते की आवाज बन जाती है। भीड़ सदैव से घातक रही है, जब भीड़ चलती है तो उसमें नाना विध
लोग अवांछित तरीके से जुडते चले जाते है और भीड दिशाविहीन और लक्ष्यविहीन हो जाती है। कोई नेतृत्व नहीं रह जाता है और अंत में भीड़ अराजकता का शिकार हो जाती है।
इसलिए स्थिर मन हृदय और मस्तिष्क के साथ वार्ता हो, विचारों के आदान प्रदान हों, समीक्षा और मूल्यांकन हो कि टीका टिप्पणी और आलोचना सिर्फ संघर्षों को जन्म देते हैं,
समाधान तो विमर्श और संवाद से होते हैं।
समस्याएँ चाहे व्यक्तिगत हों या सभष्टिगत हो, संवाद करें, हल निश्चय ही निकलेगा।।
========
शुभकामनाएँ
मंगलकामनाएं ========
सपरिवार सानन्द रहें
सुखी रहें स्वस्थ रहें।
सादर सु प्रभात
सादर प्रणाम
---------
सृजन : और एकात्मकता : आलेख : ८
-----------
सृजन शब्द को बोलने लिखने के पूर्व, यह शब्द सोंच में आते ही एक बात मनो मस्तिष्क में सहज ही उभर कर सामने आती है कि * दो के सम्मिलन के बगैर कोई भी सृजनात्मक क्रियाशीलता नहीं हो सकती है।
वह दो पदार्थों का सम्मिलन हो या दो जीवों का या दो भावों विचारों का, यह * द्वैतवादी क्रियाशीलता है परन्तु इसका उत्पाद * एकात्मकता से समावेशित हो
जाता है, एकत्व का , * Single entity का बोध कराता है, अद्वैत हो जाता है।भौतिक और आध्यात्मिकरूप से यही सत्य है। दो अणुओं के सम्मिलन से एक नया पदार्थ सृजित होता है। दो विरोधाभासी पदार्थों के सम्मिलन से एक नयी समावेशी रचना होती है। नर मादा के सम्मिलन से एक नया जीव पैदा होता है जिसमें एक ही साथ समावेशी रूप में जो ** गुण माता पिता
के होते हैं , वे स्थूल और सूक्ष्म रूप में
संतानों को स्वतःस्फूर्त प्राप्त हो जाते है।
अब इसमें देखने योग्य बातें ये होती हैं कि सभी जीवधारियों में ये गुणधर्म * आनुवांशिक होने के साथ-साथ अन्य भौगोलिक और पारिस्थितिकी कारकों से अनुप्राणित और प्रभावित होते हैं जिसके फर्क को न समझने के कारण हमें सर्वत्र नानाविध भिन्नताएँ नजर आती है। इन्हीं भिन्नताओं को समझना
और उसमें एकत्व का बोध होना या करना ही * ब्रह्माण्डीय एकात्मकता और सहज एकात्मवाद है।
** The whole of the manifestation of different characteristics and qualities
r the single entity of the whole. The total embodiment
Of the Universe is a single entity which emerges out from two different forces, *Negative and Positive. The clash between two different
Objects create an entirely original thing which r observed in the whole Universe in its total manifestation.
यही भारतीय जीवन दर्शन और चिन्तन में समावेशित जीवन और उसके सृजन विकास और विनाश की निरन्तरता है। यही * शिव शिवत्व और शिव तत्व है जिसे समझना या तो सरल सहज है या अत्यन्त दुष्कर है, विरल है।
इसलिए भारतीय दर्शन और चिन्तन में समावेशित सृजन संचालन और विनाश के भौतिक और आध्यात्मिक समन्वय और सामंजन को समझने के लिए * इन चार महासूत्रों को समझना और आत्मसात करना अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य भी है जो प्राचीन भारत से लेकर सम्प्रति भारत के रजकण में व्याप्त है और इसकी स्वीकार्यता सारा
संसार मानता हैं। इन चारो महासूत्रों का
महत्व सिर्फ आध्यात्मिक तात्विक और दार्शनि तथा धार्मिक दृष्टिकोण से ही नही है बल्कि इनसे इतर भौतिक नजरिए से भी है।
उन चार महासूत्रों का अवलोकन करें,
1.अहम् ब्रह्मास्मि ।
2. प्रज्ञानम् ब्रह्म ।
3. तत्वमसी ।
4.अयमात्मन् ब्रह्म ।
अब इन महासूत्रों को धार्मिक दृष्टिकोण न देखकर * शाश्वत और सर्वव्यापक अर्थों में अवलोकन करें तो एक अद्भुत
अनुभूति होगी जो * इलहाम है, अन्तःप्रज्ञा जागरण है, बुद्धत्व है, अरहत्व है, जागृत चैत्तन्य बोध है, ध्यान है, धारणा है , समाधि है और अंत मैं *
वैश्विक मानव एकात्मकता है और इन्ही बोध की जरूरत आज संसार को है और यही चार महासूत्रों को समझकर आत्मसात कर हम संसार को प्रेममय बना सकते है, हिंसा अन्याय अत्याचार शोषण दोहन घात प्रतिघात से मानव समाज की रक्षा कर सकते हैं।
यह कोई * धम्म देसना, धर्म संदेश ,
धर्म प्रेरणा नहीं, जीवन का व्यवहारिक दर्शन है जो संसार के सारे प्रचलित मतों और विश्वासों में समावेशित है। इसी तथ्य को Leo Tolstoy ने ऐसे कहा है कि* we r born as a human being in the world and it is our bounden duty to serve Man and Mankind.
अगर तुम आदमी के रूप में जन्म लिए हो तो स्वभावतः तुम्हें आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए कि परमात्मा ने इसीलिए तुम्हें आदमी बनाकर धरती पर भेजा है। आज जो भी वैश्विक व्यवस्था है उसका जिम्मेदार कोई अलौकिक सत्ता नहीं, लौकिक सत्ता है, जिसके श्रेष्ठ प्रतिनिधि हम हैं।
===========
अनन्त शुभकामनाएँ ।
अशेष मंगलकामनाएँ
=============
-----------
प्रेम और जीवन : सम्पादकीय : आलेख : ७
---------
अरूण कुमार सिन्हा
कवि, साहित्यकार, चिन्तक,आलेखक.
अद्वैत प्रेम : राधा : कृष्ण. शिव : शक्ति.
प्रेम गली अति सांकरी जामे दोउ न समाए
जब मैं था तब हरि नहीं जब हरि है मैं नाय।
कबीर
प्रेम और जीवन : प्रेम तभी तक सरल सहज और सुग्राह्य होता है जबतक मनुष्यों का मन हृदय और मस्तिष्क में सरलता सहजता और निश्छलता होती है।
यही वजह है कि बच्चे प्रेम और मित्रता को जानते हैं समझते हैं और उसे जीते और भोगते हैं।
मनुष्य ज्यों ज्यों बौद्धिक तार्किक होता जाता है, प्रेम कलुषित और कारणिक होता जाता है।मनुष्य जिज्ञासु और अर्थसाधक होता जाता है और भावनात्मक संवेदनशीलता उपयोगिता और उपादेयता आधारित होती जाती है जो संवेदना को ही संवेदनहीन कर देती है।
प्रेम ही सृजन है प्रेम ही शिवत्व है : प्रेम ही सृजन और जीवन के लय और प्रलय के मूल में है। प्रेम जब शिवत्व को धारण करता है तो शिव के तांडव को धारण कर लेता है और जैसे तांडव की प्रकृति और प्रवृत्ति होती है वैसे ही प्रेम हो जाता है जो शिव के सृजन लय और प्रलय से जुड़ा हुआ है।
शिव जब आनन्द तांडव करते हैं तब सृजन होता है,स्थिर होकर भावविभोर होकर स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो लय की स्थिति बनती है, संसार चक्र चलने लगता है और जब रुद्र तांडव करते हैं तब सृष्टि का विनाश होने लगता है। सृजन और लय की अवस्था में शिव प्रेममय रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ आबद्ध हो जाते हैं और जीवन सरल सहज और सुख आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है।
सर्वत्र सुख शान्ति विकास का साम्राज्य हो जाता है और जीवन अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष अर्थात् प्रेय और श्रेय की प्राप्ति में लग जाता है।यही प्रेम की महिमा है जहां समस्त जीव जन्तु पिण्ड आदि एक प्रवाह में आकर्षण से बंधे भागे चले जाते हैं।आप प्रातःकाल का अवलोकन करें,यह सृजन का काल है, समस्त प्रकृति मानों एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए आतुर दिखती है,जिसे भौतिक विज्ञान आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त कहता है वह अध्यात्म या सूक्ष्म जगत में प्रेम है जिससे आबद्ध होकर सब एक दूसरे की ओर भागे चले जाते हैं। प्रेम जगत का सार तत्व है, ब्रह्माण्ड के सृजन का आधार है। लय की अवस्था जब अपने चरम पर पहुंचती है तो उसी बिन्दु से रुपान्तरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि चरम अवस्था परिवर्तन को जन्म देती है, शिव के आनन्दमय स्वरूप में रुपान्तरण होता है, रसहीन भावहीन रंगहीन हो रहे जगत में फिर से नवीन जीवन और प्रेम का सृजन करने के लिए शिव तांडव नृत्य करते हैं। समस्त आधियां व्याधियां आपदाएं तमस कुवृत्तियां आदि नष्ट हो जाती हैं, एक प्रेममय जगत का निर्माण होता है। इस तरह प्रेम की स्थापना के लिए सृजन और विनाश का चक्र चलता रहता है।

मार्क्स : वाद प्रतिवाद और संवाद के दर्शन : संभवतः इसी दर्शन से प्रेरित होकर हीगल, एंगेल्स और मार्क्स ने Thesis, antithesis and synthesis अर्थात् वाद प्रतिवाद और संवाद के दर्शन को जन्म दिया होगा। नवीन जीवन के सृजन के लिए बीज का बोया जाना,उसका सड़ना और फिर एक नये पौधे या जीवन का सृजन होना ही तो संसार का चक्र है पर आधुनिक भौतिक विज्ञानी और दार्शनिकों ने इसके सूक्ष्म पक्ष का अवलोकन नहीं किया।
उन्होंने स्थूल को देखा और सूक्ष्म तथा कारणिक का त्याग कर दिया इसलिए उनका दर्शन रसहीन और प्रेमहीन हो गया, जीवन निर्मम हो गया परन्तु जीवन तो प्रेम के बगैर न तो सृजित हो सकता है और न चल सकता है।
कबीर,तुलसी,मीरा, रहीम का प्रेम : इसी प्रेम को महाकवि वाल्मीकि, कालिदास, कबीर,तुलसी,मीरा, रहीम आदि ने समझा, भगवान महावीर और तथागत सिद्धार्थ ने समझा और इसी प्रेम से अनुप्राणित होकर करुणा,सत्य, अहिंसा, त्याग,क्षमा आदि के दर्शन को जन्म दिया।
भगवान राम और भगवान कृष्ण ने इसी प्रेम को समझकर पुरुषोत्तम और योगेश्वर के पद को प्राप्त किया।
प्रेम, द्वैत नहीं अद्वैत का दर्शन है, व्यवहार है, इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा भी है कि,
कबीर
प्रेम गली अति सांकरी जामे दोउ न समाए
जब मैं था तब हरि नहीं जब हरि है मैं नाय।
पर आजकल प्रेम का स्वरूप बदलकर अपने अर्थ को खो दिया है। प्रेम आकर्षण और मोह ग्रसित होकर संचारी भाव हो गया है, स्थायी भाव को खो दिया है।बिना स्वार्थ और मोह के प्रेम है नहीं और इसलिए संसार रसहीन और भावहीन हो गया है।
माना कि स्वार्थ के बगैर संसार का सृजन नहीं हो सकता और न चल सकता है परन्तु संसार को बनाए रखने के लिए प्रेम की प्रकृति और प्रवृत्ति को परमार्थी बनाना होगा अर्थात् जीवन को एक दूसरे से आबद्ध करना होगा,प्रेम को मोल और मूल्यहीन नहीं बनाना होगा तभी जीवन परिष्कृत और मर्यादित होकर चलेगा
और जीवन में प्रेय और श्रेय दोनों की प्राप्ति हो सकेगी।
===========
अरूण कबीर
कवि, साहित्यकार, चिन्तक,आलेखक।
दुमका, झारखण्ड।
स्तंभ संपादन : शक्ति शालिनी अनीता सीमा.
स्तंभ सज्जा : शक्ति अनुभूति सुष्मिता मंजिता.
हम और हमारे जीवन व्यवहार के नियम : आलेख : ६
----------
⭐
अरूण कुमार सिन्हा
नीति नैतिकता सदाचार परिष्कृत व्यवहार और आचरण विधि का सम्मान अनुशासन ईमानदारी आदि जैसी बातें भी वैश्विक स्तर पर और हमारे देश में
* अलग-अलग स्तर के लोगों के लिए अलग-अलग होती हैं और करिश्मा ये है कि हम रोज इसके बेहतरीन प्रदर्शन रोज देखते हैं। हम समर्थन और सम्मान
* व्यक्ति की गुणवत्ता और काबिलियत देखकर नहीं उसकी हैसियत और रूतबा देखकर करते हैं।।मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र रूप से रूप से होता है परन्तु वह कदम दर कदम अनेकानेक * सामाजिक नैतिक धार्मिक एवं वैधानिक वर्जनाओं से बंधा होता है
तभी तो J J Rousseau कहता है कि,* A man is born free but he is everywhere in chains. परन्तु एक अद्भुत बात है कि ये सारी * वर्जनाएँ और बन्धन समान रूप से सबके लिए नहीं होते हैं जो सर्वत्र दृष्टिगोचर हैं और यह विचित्र विशिष्टताएँ भी हमारे देश में ही मौजूद है। क्या आपको ऐसा लगता है कि
* सामाजिक समता समानता न्याय आदि की अवधारणाएँ जिन्हें वैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, समान रूप से सबको उपलब्ध है,यहाँ भी
* पात्र अपात्र सुपात्र कुपात्र आदि का नहीं बल्कि सामर्थ्यवान और असामर्थ्यवान का फर्क होता है, राजनीतिक रुप से उसकी मजबूती देखी जाती है। सामाजिक वर्गीकरण और स्तरण को दरकिनार करते हुए उन्हीं में से जो ताकतवर और रसूखदार होते हैं, ले लेते हैं या छीन लेते हैं और उसे स्वीकार्य भी करवा लेते हैं और इसका कहीं प्रतिवाद या प्रतिकार भी नहीं होता है और दुनियाँ बदस्तूर चलती रहती है। यह खेल * सदियों से चलता आया है और चलता भी रहेगा जो शायद प्राकृतिक क्रियाशीलताओं का भी सत्य है कि कुदरत उसी की हिफाजत करती है जिसके पास अपने वजूद को बचाने का माद्दा हो अन्यथा कोई व्यवस्था या तंत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। असल में मनुष्य ज्यों ज्यों चैतन्य होता गया, उसने तर्कणा और प्रमाण का सहारा लेकर अपने स्थापित सिद्धान्तों और मान्यताओं को स्थापित करता रहा और आमजन से मनवाता रहा जो समानता स्वतंत्रता और इच्छास्वातंत्र्य और कर्म सिद्धांत के विरूद्ध होने पर भी युगधर्म बनता रहा और यह सब जायज करार दिया जाता रहा है। कुदरत मे समान रूप से पैदा होने,शारीरिक संरचना में बनावट का फर्क होते हुए( भौगोलिक एवं पारिवेशिक कारणजनित) भी मौलिक रूप से सब एक हैं परन्तु समान नहीं हैं।
मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में भिन्नता के अलग-अलग कारण हैं परन्तु * भूख प्यास आवास वस्त्र औषधि शिक्षा रोजगार आदि की सबको जरूरत है और समान रूप से जरूरत है पर व्यवहार में कभी नहीं होता रहा है। इसलिए तो H J Laski कहता है कि,* Without equality there can not be liberty.
इसलिए मानव जीवन की मौलिक क्रियाशीलताओं में समावेशित तथ्य यही है कि कोई आजादी अपने आप में पुरी आजादी तबतक नहीं हो सकती है जबतक कि समाज के हर तबके को अपनी-अपनी जगह पर समान रूप से आजाद होने का बोध न हो। आर्थिक गैरबराबरी को एकदम से नहीं मिटाया जा सकता है परन्तु मौलिक जरूरतों की उपलब्धता में असमानता नहीं होनी चाहिए।
वैश्विक स्तर पर धर्म जाति वर्ग दल सम्प्रदाय आदि के भेद स्थूल/ सूक्ष्म और कारणिक रूप में बने रहेंगे पर एक सोंच को *व्यष्टि-वित्त से समष्टि-चित्त की ओर उन्मुख करना होगा ताकि जिन त्रासदियों और विडम्बनाओं को मौजूदा पीढ़ी झेल रही है, आने वाली पीढ़ियों को न झेलना पड़े या न्यूनतम झेलना पड़े।
अब आप इसे * हमारा अनर्गल प्रलाप भी समझ सकते हैं या निजी विचार भी समझ सकते हैं।पर एक बात तो सत्य है कि
*There is nothing to do with the matter whether it is right or wrong in the matter but read it observe it and then conclude it.
पर जब मनुष्य और मनुष्ययत्व की बातें उठती हैं तो सारे दर्शन और चिन्तन एक तरफ और मनुष्य को श्रेष्ठ शिखर पर बैठाना पड़ता है कि सबके धुरी में मनुष्य ही बैठा है। मनुष्य के इर्द-गिर्द ही सारे ताने बाने बुने जाते हैं। सारे वैज्ञानिक विकास, सामाजिक राजनीतिक चिन्तन, धार्मिक आध्यात्मिक दर्शन, व्यवहार आचरण के नियम, वैधानिक तंत्र आदि की संरचनाओं का केंद्र मनुष्य ही होता है और हम इसी केन्द्रीय पात्र को भूल जाते हैं और अपने अपने हिसाब से चलने लगते हैं जिससे सम्पूर्ण व्यवस्था अराजक और अव्यवस्थित हो जाती है। परिवार समस्त व्यवस्था की प्राथमिक इकाई है और हम उसके प्राथमिक सदस्य हैं, बुनियादी सोपान हैं।हर व्यक्ति को पहले इस बुनियादी आधार के बारे में सोंचना होगा और इसकी जड़ें मजबूत करनी होगी।आपने देखा होगा कि जिनकी जड़ें जितनी मजबूत और गहरी होती हैं वे बड़े बड़े तुफान और झंझावात को झेल जाते हैं और अपने अस्तित्व में बने रहते हैं। फिर तब एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि उनकी जड़ें कैसे मजबूत की जाए कि हर प्रतिकूलताओं में भी वे अपने अस्तित्व में बने रहें तो आपको वनस्पति विज्ञान की ओर मुड़ना होगा और उनके विज्ञान को समझना होगा कि पौधों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वांछित आहार देने की जरूरत होती है वैसे ही मनुष्य को मजबूत अस्तित्व में विकसित करने के लिए सम्पूर्ण आहार की जरूरत होती है और इसी आहार सिद्धान्तों को समझने की जरूरत है कि हम परिवार में पारिवारिक सदस्यों को कैसा आहार देते हैं। यह भी सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। समाज का हर हिस्सा उन स्तरों पर स्वस्थ और समृद्ध नहीं होता है इसलिए यहां भी फर्क हो जाता है। शैक्षिक स्तर यदि सही है तो सोंच सही हो जाती है और सोंच सही हो तो सबकुछ बदलने की क्षमता एक मनुष्य में विकसित हो जाती है।आहार श्रृंखला में मनुष्यों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण आहार सम्यक् शिक्षा ही है जैसे सही आहार शरीर को मजबूत बनाता है वैसे ही सही शिक्षा किसी को वैचारिक रुप से स्वस्थ और समृद्ध बनाती है।इसलिए एक स्वस्थ परिष्कृत और चैतन्य परिवार के निर्माण के लिए सम्यक् शिक्षा जरूरी है ,यही वह कारक है जो सबकुछ बदलने की क्षमता रखता है। मनुष्य को हर बंधन से मुक्त करता है। धर्म, अर्थ,काम और मोक्ष की अवधारणा को समझने की क्षमता देता है और सामाजिक बदलाव का कारण बनता है।मनुष्य और मनुष्ययत्व के आधार पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करता है।हम जिस समाज में रहते हैं वहां नानाविध मानसिकता के लोग रहते हैं और मानसिक विविधता ही संघर्षों और तनाव के कारण बनते हैं परन्तु तमाम विविधताओं के बावजूद भी एक चैतन्य व्यक्ति इससे अप्रभावित रहकर समाज को अपने तरीके से दिशा निर्देश देता रहता है। वही व्यक्ति गुणवत्ता की कीमत जानकर मूल्य मोल की व्यवस्था करता है। वही व्यक्ति स्थान काल एवं पात्रता के आधार पर मूल्यांकन करता है,कब कैसे चीजें बदलती हैं,उसका मूल्यांकन करता है।एक व्यक्ति सदैव महत्वपूर्ण है, बताता रहता है। समय स्थान के आधार पर चीजें बदलती हैं पर जीवन के शाश्वत मोल और मूल्य कभी नहीं बदलते,इस तथ्य की स्थापना करता है।
इस सम्बन्ध में*पैराबुल औफ गूड समरिटान में एक रोचक प्रसंग है कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है,सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इसका जवाब है कि,जो व्यक्ति किसी भी समय हमारे समक्ष मौजूद हैं,सबसे महत्वपूर्ण है कि वही मदद कर सकता है,सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है जो हमारे हाथ में है और इसी समय हम कुछ कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम मनुष्य का भला करना है कि परमात्मा ने बस इसी कार्य के लिए हमें धरती पर भेजा है। बड़ी रोचक और गंभीर बात है जो सारे मत पंथ विश्वास विचार और सम्प्रदायों में पाए जाते हैं और यही समझ मनुष्य को आजादी दिलाती है और समाज राष्ट्र और विश्व को अराजक होने से बचाती है। व्यक्ति के व्यवहार और आचरण को नियमित नियंत्रित और संचालित करती है जिसका आधार सम्यक् शिक्षा और उससे उपजी चेतना है।
---------
हृदय की बात : आलेख : ५
----------
⭐
अरूण कुमार सिन्हा : हृदय की बात
----
जिन्होंने * सम्पूर्ण औपनिषदिक दर्शन और चिन्तन को एक काव्य ( श्रीमद्भागवत गीता) में ढाल दिया, जिन्होंने उद्दात्त और उन्मुक्त प्रेम को प्रदर्शित किया, जिन्होने सम्पूर्ण संसार को * निष्काम कर्म योग का दर्शन दिया, जो परम आनन्द के कारण है, जो सबको आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं , जो सभी प्रेमियों के लिए आराध्य हैं,जिनके स्मरण मात्र से लौकिक व्याधियाँ नष्ट हो जाती है, जो युग पुरूष और योगेश्वर हैं, उन वसुदेव कृष्ण को मैं बारम्बार नमन करता हूँ।
भारत की भारतीयता और आत्मा * शिव राम और कृष्ण में बसती है। बुद्ध महावीर नानक कबीर रविदास तुलसी रहीम मीरा सूरदास और रसखान भारतीय चेतना रूपी उद्यान के सुगंधित पुष्प है जिनसे भारत भूमि सुवासित होती रहती है।पर जब बात श्री कृष्ण की आती है तो एक अद्भुत अनुभूति हृदय में होती है।
अपने काल के ही नहीं जो आज भी प्रासंगिक हैं और यथार्थ चेतना से युक्त है। मैं अकिंचन उन पर क्या लिखूँगा पर हृदय के भावना पुष्प तो इन शब्दों के माध्यम से समर्पित कर ही सकता हूँ पर विराट को तो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है।
एक भावुक प्रेमी जो अपने बालसखा और सखियों से बिछुड़ कर एक आम आदमी की तरह अपने परम सखा * निर्गुण ब्रह्म उपासक उद्धव जी के सामने विलाप करने लगते हैं, " उद्धव,
मोहे ब्रज बिसरत नाहीं", यह पीड़ा जो प्रेम में अन्तस को आहत कर देता है, सम्पूर्ण वैश्विक साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। एक महान कूटनीतिक रणनीतिकार जो * साध्य की प्राप्ति करने में साधन की परवाह नहीं करते है कि * यदि साध्य पवित्र, धर्म और न्याय आधारित हो तो उसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। पार्थ के सखा सारथी और रक्षक, मैत्री धर्म पालन करने वाले,नारी जाति के समुद्धारक, आश्रितो के रक्षार्थ * रणछोड़ बनने वाले और प्रेम की वंशी बजाने के साथ-साथ आपात्काल में * सुदर्शन चक्र उठाने वाले, महान योद्धा * पार्थसारथी का आज हम जन्मदिन मना रहे है परन्तु जरूरत है , उनकी तरह समय पर वंशी वादन की और धर्मार्थ- न्यायार्थ शस्त्र
उठाने की ताकि * न्यायार्थ अपने बन्धुओं को भी दण्डित किया जा सके।
पुनश्च परम चैतन्य आत्मा ( ब्रह्माण्डीय ऊर्जा ) शिव , श्री राम और श्री कृष्ण को बार-बार नमन करते हुए भारत के महान समाजवादी चिन्तक और राजनीतिक दार्शनिक डा. राम मनोहर लोहिया जी को उद्धृत करना चाहुँगा, उन्होने 1955 में *Mankind पत्रिका में लिखा था,
हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो,कृष्ण का विराट हृदय दो,राम का कर्म वचन और मर्यादा दो। हमे असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ-साथ जीवन की मर्यादा से रचो।"
सभी श्री कृष्ण प्रेमियों और साधकों को श्री कृष्णाष्टमी की अनन्त शुभकामनाएँ बधाईयाँ ।
सम्पूर्ण वैश्विक क्रियाशीलताओं मे प्रेम शान्ति और सद्भावना का संचार हो।
श्री राधा मोहन शरणम् । जय जय श्री राधेकृष्ण ।। अरूण सिन्हा। दुमका।
---------
क्षमा और जीणेन्द्र भगवान महावीर: आलेख : ४
---------
तस्मै देसी क्षमादानंयस्ते कार्य विघातकःविस्मृति कार्यहानीनां यद्दहोस्यात्तदुत्तमा
महान्तः संति सर्वेऽपि क्षीण कायस्तपस्विनः क्षमावंतमनुख्याताः किन्तु विश्वे हितापसाः।
अर्थात् दूसरे लोग तुम्हें हानि पहुंचाएं इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर दो और यदि तुम उसे भुला सको तो यह और भी श्रेष्ठ है। उपवास करके तपश्चर्या करने वाले निःसंदेह महान है परन्तु उनका स्थान उन लोगों के पश्चात ही है
जो अपनी निन्दा करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं।
========
सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य, भारतीय धर्म संस्कृति और जीवन दर्शन में समावेशित सत्य और
आदर्श हैं। क्षमा भी उन्हीं तरह का एक
एक परम आदर्श और व्यवहारिक मानवीय मोल और मूल्य है परन्तु जिन भगवान महावीर ने इसे जिस तरह व्याख्यापित करके आत्मसात करने का काम किया, अन्यत्र दुर्लभ है।
जैन धर्म दर्शन कहता है
* जिसके साथ थे तुमने गलत किया वह चाहे जो भी हो उससे क्षमा मांग लो।
स्वयं भगवान महावीर कहते हैं,* मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के समस्त जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव बना रहे। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं
सच्चे मन से धर्म में स्थित हुआ हूं।सब जीवों के प्रति मेरे सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूं और सब जीवों ने जो मेरे प्रति अपराध किए हैं, उन्हें मैं क्षमा करता हूं।
क्षमा करने की ऐसी दुर्लभ भावना ऐसे तो वैश्विक स्तर पर सारे प्रचलित धर्म विश्वास मत सम्प्रदाय आदि में उपलब्ध दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु जिन भगवान महावीर ने क्षमा को जिस रुप में स्थापित किया वह विशुद्ध मानवीय चेतना है जो जीवन की व्यवहारिक कसौटी पर भी खरा उतरता है
ऐसे भी कहा जाता है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। कायर क्षमा नही कर सकते हैं कि उनमें यह दैवी शक्ति और गुण का अभाव होता है।
क्षमा हमारे दैनिक जीवन में भी अहम
भूमिका निभाता है। अगर आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार करता है और जो क्षमा करने की सीमा के भीतर
तो आपको क्षमा कर देना चाहिए। आप जैसे ही उसको क्षमा कर देते हैं वैसे ही आपके हृदय में एक अद्भुत शान्ति की अनुभूति होती है, मन की बोझिलता मानों तिरोहित हो जाती है और इसकी सीधी प्रतिक्रिया उसके भीतर होती है जिसे आप क्षमा कर देते हैं और यह भौतिक विज्ञान भी सत्यापित करता है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया समान रुप से होती है और क्रिया की समानुपातिक होती है।
भगवान महावीर सिर्फ जीवों के प्रति ही
क्षमावान होने को नहीं कहते हैं बल्कि सभी** स्थावर जंगम के प्रति भी क्षमावान होने को कहते हैं कि जिसे आप निर्जीव समझ कर आघात पहुंचाते ( जैसे आप क्रोधवश किसी चीज को ठोकर मार देते हैं या तोड़ देते हैं) हैं वे चीजें भी कभी जीवित रही होंगी, जैसे फर्नीचर कपड़े किताबें आदि जिनकी निर्माण सामग्री कभी जीवित रही होंगी जैसे वृक्ष से ही उपरोक्त चीजें बनायी जाती है।
अब गौर करें कि ऐसी चेतना कितनी गहन होगी जो सजीवों से ही नहीं निर्जीवों से भी क्षमा मांगती है और वह गहन चेतना भगवान महावीर की है जिसे आज समस्त संसार को जरुरत है।
आप इसे निजता के साथ अपनाने और आत्मसात करने की कोशिश भर करके देखें कि जीवन कितना सरल और सहज हो जाता है।
परन्तु हम अस्मिता या अहंकार बोध के कारण स्वयं के भूल अपराध या हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और
इसी कुवृत्ति वाली चेतना के कारण ही अपनी अपराध बोध को स्वीकार नहीं करते और अपनी श्रेष्ठता और विचारों को थोपना चाहते हैं जो बाह्य और आन्तरिक हिंसा को जन्म देता है जिससे व्यक्ति समाज और वैश्विक व्यवस्था नाकारात्मक रुप में प्रभावी होती है।
तत्कालीन प्राचीन यूनानी और रोमन दार्शनिकों और चिन्तकों ने भी इस दर्शन की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है जो सिर्फ दर्शन नहीं जीवन व्यवहार भी है। लियो टाल्सटाय एक जगह पर कहते हैं कि,
*जिन्होंने भूल को अपराध को स्वीकार करना सीख लिया और क्षमा करने के अर्थ और मर्म को समझ लिया, उन्होंने ईश्वर और उसकी सत्ता को समझ लिया।
महात्मा जीसस ने भी सूली पर चढ़ाते समय ऐसा ही कहा था कि,
* हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस्लाम यहूदी सिख बौद्ध आदि बड़े मत व सम्प्रदायों ने भी क्षमा को ईश्वरीय गुणधर्म के रुप में स्वीकार किया है।
आज निज के जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर जितनी समस्याएं बन रही हैं, अस्तित्व में हैं उन सबकी गहराईयों में जाने पर यह सहज ही ग्राह्य हो जाता है कि संवादहीनता और संवेदनहीनता ही सारे तनाव और संघर्षों के कारण हैं और उसके जड़ में क्षमा भाव का नहीं होना है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि किसी परिवार में दो सदस्यों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध सृजित हो गये तो दोनों को समझने की जरूरत होती है कि मेरा दोष अपराध क्या है और इसका बोध होते ही संवाद करना चाहिए और अहंबोध छोड़कर स्वयं की ग़लती के लिए क्षमा मांग ले और दूसरे को गलती स्वीकार करने पर उसे क्षमा कर दे तो तनाव और संघर्ष खत्म हो सकते हैं और यह दर्शन नहीं व्यवहार है पर हम अपने अहंबोध के कारण ऐसा नहीं करते और ना ही कोशिश करते हैं जिसकी परिणति छोटे-बड़े संघर्षों का जन्म होता है।
सही ग़लत वृत्तियां हमारी चेतना में नैसर्गिक है जिसका हमें अच्छी तरह बोध होता है परन्तु इसे स्वीकार करना देवत्व है और यही आचरण हमें मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाता है। इसी देवत्व का प्रदर्शन करते हुए तथागत सिद्धार्थ ने अपने चचेरे भाई देवदत्त को क्षमा कर दिया था।
तो आइए इस महान और पुनीत दिन के अवसर पर हम संकल्पवान बनें कि हमें** क्षमा करने और मांगने के गुण को अपनाना और व्यवहार में लाना है ताकि समस्त मानव समाज में समरसता और समावेशिता का सृजन हो।
=========
आज समस्त विश्व में उन जीणेन्द्र भगवान महावीर की 2622वीं जयन्ती मनायी जा रही है, उन्हें कोटि-कोटि नमन है।
=========
--------
भगवान श्री राम की प्रासंगिकता। आध्यात्मिक मोल एवं मूल्यों में गिरावट : आलेख : ३
--------
अरुण कबीर
आज के सन्दर्भ में जब हम समग्रता में नजर दौड़ाते हैं तो हमारे समक्ष विद्यमान बड़ी चुनौतियों में जो गंभीर चुनौती है, उसमें सामाजिक व्यवस्था में समरसता और समावेशीकरण प्रवृत्तियों का उत्तरोत्तर ह्रास है, आध्यात्मिक मोल एवं मूल्यों में गिरावट है और राजनीतिक प्रदूषण हैं। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हम विरक्त भाव से भौतिक उपलब्धियों पर अपनी ऊर्जा को फोकस किए हुए हैं जिसकी परिणति आज का हिंसक समाज और संस्कृति का फलना फूलना है और इसीलिए श्री राम की प्रासंगिकता अभी अनिवार्यता में बदल गयी है। मध्ययुगीन भारत का हिन्दू समाज जब शैव शाक्त वैष्णव और गाणपत्य वादों के संघर्षों में उलझा हुआ था तो दक्षिण से उत्तर आए स्वामी वल्लभाचार्य स्वामी निम्बकाचार्य स्वामी माध्वाचार्य स्वामी रामानंद और स्वामी रामानुज जिन्होंने इन संकीर्णताओं और संघर्षों को समाप्त करने के लिए एक सूत्र दिया,
जाति पाती पुछे नहीं कोए
हरि को भजे से हरि को होए
और इधर श्री राम की अलख तुलसी कबीर और रहीम अपनी अपनी रचनाओं से जगा रहे थे
तुलसी शिव के श्रीमुख से कहलवाते हैं
संतत जपत संभु अविनासी
शिव भगवान ज्ञान गुन रासी
सोपि राम महिमा मुनि राया
सिव उपदभ किन्हं करि काया
जासु कथा कुम्भज
ऋषि गायी
सोई राम मम इष्ट रघुबीरा।
शैव शाक्त वैष्णव और गाणपत्यों में मुख्यतः भेद शैवों और वैष्णवों के बीच था। वनगमन से लेकर शक्ति पूजा और श्री रामेश्वर शिव आराधना तक श्री राम शव जी के प्रति समर्पित दिखते हैं।
वनगमन के समय श्री राम की चेतना देखिए,
तब गणपति सिव सुमिरि प्रभु
नाई सुरसरिहि माथ
सखा अनुज सिय सहित वन
गवन किन्हं रघुनाथ।
ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समन्वयकारी स्वरूप कि कैसे विराटता और मर्यादा का मिलना होता है और भटकते टूटते समाज को एक नयी दिशा और दशा दी जाती है और यही कारण है कि द पू एशियन देशों में श्री राम आज भी लोकजीवन में जीवन्त हैं। जावा सुमात्रा बाली बोर्नियो
थाईलैंड इंडोनेशिया कम्बोडिया मंगोलिया चीन जापान मौरिशस
सूरीनाम उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान अफ्रिकी देशों आदि प्रदेशों में किसी न किसी रुप में श्री राम उनके लोकसाहित्य और इतिहासों में समाए हुए हैं। इंडोनेशियाई कहते हैं
राम हमारी सभ्यता और संस्कृति हैं, हमने जीवन शैली और धर्म बदला है, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत नहीं बदला है। काकवीन रामायण और रामकेति रामायण दक्षिण की अनमोल विरासत है।
समग्रता में श्री राम निर्दोष त्रुटिहीन सहज सरल ग्राह्य मानव रुप में प्रकाश पूंज हैं, भारत की आत्मा हैं, मनोभूमि हैं, रस हैं प्राणों के प्राण हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी वंचितों पीड़ितों के राम हैं, कोल भील किरात निषाद सबर अरण्यवासियों गिरीवासियों के राम हैं। तत्कालीन खंडित
भारत को एकीकृत करने वाले राम एक संघर्षशील त्यागी और जन्म से लेकर महाप्रयाण काल तक
सम्पूर्ण मनुष्य बनते हुए दिखते हुए राम हैं। एक अपवाद को छोड़कर कोई चमत्कार नहीं,आम आदमी की तरह पत्नी विरह में और भाई को मरनासन्न जानकर विलाप करने वाले श्री राम, रावण की शक्ति को लेकर आम आदमी की तरह शक्ति पूजा और शिव की आराधना करने वाले श्री राम क्या आपको अद्भुत और मोहित करने वाले नहीं लगते, तो आइए हृदयतल से श्री राम के रामत्व की ओर अग्रसर होने की कोशिश तो करें ताकि
इति रमन्ते राम: और कण कण व्यापे राम और इमामे हिन्द की सार्थकता तो कुछ अर्थों में पुरी की जा सके।
जय जय सियाराम।
------
आप और श्रेष्ठता आलेख : २
समस्त संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आत्म चैतन्य है और परमात्मा ने
सबको कुछ न कुछ विशिष्टताएं प्रदान की है जो अपने आप में अद्वितीय होता है और वही श्रेष्ठ है और जो आपके पास श्रेष्ठ है वही सबको देने योग्य है।
दानव,मानव,देवता, भगवान आदि प्राणियों के अलग-अलग स्तर हैं जो मनुष्यों के संस्कार जनित गुणधर्मों से बनते हैं। जिनकी प्रवृत्ति और प्रकृति दूसरों के हक छीनने की होती है,वे दानव हैं,जो मानवोचित गुणों के साथ सबके कल्याण की भावना के साथ जीवित रहते हैं,वे मानव हैं,जो अपना सर्वस्व का वितरण करते रहते हैं अर्थात् दान करते रहते हैं,वे देवता हैं और जिन्होंने सभी बन्धनों अर्थात् काम क्रोध मद मोह लोभ और सभी इच्छाओं पर विजय पा लिया हो,वे भगवान के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं।
भगवान, मनुष्य के विकास की चरम सीमा है जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न कालखंडों में देखे जा सकते हैं। भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं में मानव स्तर से उपर उठकर भगवान के श्रेष्ठ पद तक पहुंचे अनेक विभूतियां हैं जिनके श्रेष्ठ गुणधर्मों को हम अपनाने की , अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। जीवन का श्रेष्ठ मोल और मूल्य यही है।
श्री राम,श्री कृष्ण यदि अवतारी पुरुष हैं तो उसी जगह* भगवान के विशेषण से भी विभूषित हैं। महावीर का जीण महावीर बनना,गोतम सिद्धार्थ का तथागत बुद्ध बनना,मनुष्य से भगवान बनने का अनुपम उदाहरण है। यह भी सत्य है कि भगवान के स्तर तक पहुंचना एक दुष्कर और
दुर्लभ घटना है परन्तु उनके दिखाए मार्गों का अनुसरण करके जीवन को श्रेष्ठ जरुर बनाया जा सकता है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ बनने और अपने श्रेष्ठ को देने की कोशिश करते रहनी चाहिए।
=========
आप सपरिवार सानन्द रहें,सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
सादर सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम
---------
संघर्ष और मनुष्य : आलेख : १
----------
सब जीवित प्राणियों में जन्म के साथ ही अस्तित्व को बनाए रखने का संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन और संघर्ष अनवरत है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। लोग बाहरी खतरों के विरुद्ध लड़ने और संघर्षरत रहने को ही युद्ध की संज्ञा देते हैं परन्तु बाह्य संघर्षों से अधिक मनुष्यों को आन्तरिक संघर्ष करना पड़ता है जो बहुआयामी होते हैं। आन्तरिक संघर्ष जीवन पर्यन्त चलते रहते हैं और लोग भीतर ही भीतर उनसे जूझते रहते हैं जिसमें कभी विजय तो कभी पराजय मिलते रहते हैं।
जीवन संघर्षों में चाहे उसका स्वरूप जो भी हो,विजय मिलने पर मनुष्य उत्साहित और ऊर्जावान हो जाता है और पराजय ठीक इसके विपरीत हतोत्साहित कर देता है। परन्तु ध्यान रहे, जैसे धूप छांव,दिन रात, अंधकार प्रकाश,जन्म मरण आदि सहचर हैं, साथ साथ चलते रहते हैं वैसे ही जय पराजय साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संयमित रहना ही श्रेयस्कर है कि जीतकर अहंकार को न पालें और हारकर हतोत्साहित न हों, एक अच्छे और सच्चे योद्धा की तरह दोनों को स्वीकार करें और समभाव रखते हुए लड़ते रहें कि संघर्षों का कोई विकल्प नहीं होता है। यही भाव जीवन पर्यन्त आपको जूझारु बनाए रखेगा और आप बाह्य और आन्तरिक संघर्षों के विरुद्ध
धैर्य साहस और सहनशीलता के साथ युद्धरत रहेंगे और आपको स्वयं पर गर्व होगा कि आपने एक श्रेष्ठ जीवन जिया है।
=======
आपका दिन मंगलमय हो, सपरिवार सानन्द रहें,सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम
---------
बांटने योग्य विद्या, ज्ञान और धन संग्रह आलेख : ०
----------
कुछ चीजें संग्रह योग्य होती हैं और कुछ बांटने योग्य होती है। विद्या, ज्ञान और धन संग्रह और बांटने, दोनों योग्य होती है। ज्ञान विद्या और धन पहले संग्रह किए जाते हैं और फिर उसे बांटा जाता है। ये तीनों का गुणधर्म है कि जितना बांटा जाएगा, वह स्वत:स्फूर्त बढ़ने लगती है, उसकी सीमाएं विस्तृत होने लगती है और संग्रहित रहने पर उसकी सीमाएं संकुचित होने लगती है। धन के बारे तो सद्गुरु कबीर साहब ने कह ही दिया है,
जो जल बाढ़े नाव में
घर में बाढ़े दाम
दोउ हाथ उलिचिए
यही सयानों काम।
अर्थात् यात्रा के क्रम में यदि नाव में जल भरने लगे और घर में धन का आगम होने लगे तो नाव से पानी को शीघ्र बाहर फेंकना चाहिए और धन मुक्त हस्त से बांटना चाहिए नहीं तो नाव डूब जाती है और अत्यधिक धन मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है और अंत में नष्ट हो जाता है। वैसी ही गति ज्ञान और विद्या की होती है। आप बड़े ज्ञानी और विद्यावान हैं तो समाज को लाभान्वित करें अन्यथा वह कोठार में रखे अनाज की तरह धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है।
परन्तु दुःख बांटे नहीं जाते और ना ही प्रचारित किए जाते हैं बल्कि वे धैर्यपूर्वक सहे जाते हैं। विपत्काल में धैर्य के साथ सहते हुए अपने इष्ट को स्मरण करते हुए समय के अनुकूल होने और दुःख के नष्ट होने का इन्तजार किया जाता है।
दुःख का बांटनहार कोई नहीं होता इसलिए दुःख चुपचाप सहा जाता है और सुख खुले हृदय से बांटा जाता है। यह जीवन दर्शन भी है और व्यवहार भी है।
==========
आपके आरोग्य और सुखमय जीवन की हार्दिक मंगलकामनाएं।
सदा सर्वदा आशीर्वादित रहें।
सु प्रभात
सादर नमस्कार
सादर प्रणाम।
*
टाइम्स मिडिया प्रस्तुति
*
मुन्ना लाल महेश लाल आर्य एंड संस ज्वेलर्स बिहार शरीफ़ समर्थित
--------
सम्पादकीय : पद्य संग्रह. पृष्ठ : २
----------
संपादन.
शक्ति. नीलम.
-----------
कवि
अरूण कुमार सिन्हा.
-----------
अपने और गैरों में हमनें फर्क कहां रक्खा
उनको भी संभाला उनको भी दिल में रक्खा।
सबके रहमो-करम के मुन्तजिर ही रहे हम
ग़म सहे हम हर दर्दे ज़ख्म को चक्खा
कुछ जमाने की बातें थीं कुछ हालात की
अनीश किसी ने जख्मों पे मरहम नहीं रक्खा।
लघु कविता. १०.
अतीत भूलता और छूटता कब है
अतीत भूलता और छूटता कब है
वह तो परछाइयों
की तरह
सदैव साथ साथ चलते रहता है
अंधेरों में तो परछाइयां
साथ छोड़ भी देती हैं
पर कटु मधु स्मृतियों
की लहरें
साथ साथ बहती
रहती हैं
मन कभी आह्लादित तो कभी
आहत हो जाता है
आज को या वर्तमान
को जीने की बात
की जाती है पर
मन मस्तिष्क और हृदय
कब अतीत से कट
पाता है
जीवन का हर पल क्षण तो अतीत में
रुपान्तरित होता
रहता है
काल की आंधियों
में कुछ भी तिरोहित
नहीं होता कि
सिद्धार्थ,
तथागत सिद्धार्थ में
रुपान्तरित होने के
बाद भी
यशोधरा और राहुल
को विस्मृत नहीं
कर पाए थे
लौटकर कपिलवस्तु
उन्हें आना ही पड़ा
था
फिर हम अकिंचन
अपनी स्मृतियों से
स्वयं को कैसे अलग
कर पाएंगे।
लघु कविता. ०९
*
कुदरत और औरत
कुदरत की खूबसूरती और अजीबोग़रीब
फितरत की तरह औरतें भी होती हैं,
जंगल और पहाड़ की औरतें,
गाँव देहात की औरतें,
कस्बों शहरों नगरों महानगरों मेट्रो की
औरतें,
होती तो सब औरत ही हैं,
जिस्म की बुनियादी बनावटें भी एक होती हैं,
पर जेहन जज्बात ओ एहसास अलग-अलग होते हैं,
सबकी दुनियाँ भी अलग-अलग होती
हैं,
उनके खान पान रहन सहन चेहरामोहरा
भी अलग-अलग होते हैं,
यही नहीं,
उनके भीतर की औरत भी अलग-अलग
होती है,
उनकी दुनियाँ में उनके * मर्द भी अलग-अलग ही होते हैं,
पर क्या करिश्मा है कि ये सारी औरतें
मर्द की नजरों में महज औरत ही होती
हैं,
और मर्दों की फितरत भी अलग अलग होते हुए,
औरतों के लिए अलग-अलग नहीं होती,
औरतें मर्दों के लिए बस औरत ही होती
है,
कुछ * सम्मानित व मर्यादित रिश्तों को
छोड़कर,
मर्द की नजर और नजरिए में कोई खास
फर्क नहीं होता,
एक हिंसक जानवर शिकार की जाति प्रजाति नहीं देखता,
औरत भी मर्द की नजरों में कुछ ऐसी ही
होती है,
कि औरत मर्द की नजरों में अदद औरत
ही होती है.
*
लघु कविता. ०८
जीवन और यथार्थ.
जीवन उत्सव भी है
आनन्द भी है
हर्ष है विषाद भी है
वेदना और संवेदना भी है
संघर्ष और यातना भी है
जिजीविषा और मुमूर्षा भी है
विजय का उल्लास और पराजय
की पीड़ा भी है
सौर रश्मियों की तरह कितने रंगों
को अपने भीतर समेटे रहता है जीवन
जिसे समझने के लिए संसार के
त्रिपाश्व से होकर गुजरना पड़ता है
इसके विभिन्न रंगों को समझना पड़ता है
जीवन या तो सहज सरल और अनुभूत
है या ईश्वरीय सत्ता की तरह अज्ञेय है
जिसे कभी भी नहीं जाना जा सकता है
जिसकी जैसी अनुभूति होती है
जीवन वैसा ही रुपायित और
रुपान्तरित हो जाता है
हम हॅंसते हैं तो जीवन भी हमारे संग
हॅंसता है और रोते हैं तो
जीवन भी रोता दिखाई पड़ता है
जीवन हमारी अनुभूतियों का ही
अंतिम परिणति है
भूख और प्यास से पीड़ित से पुछा कि
जीवन क्या है
जिसके सर पर किसी का साया न हो
जिसके सर पर सुरक्षा की छत न हो
जो पल पल अप्रत्याशित भय शंका
असुरक्षा के माहौल में जी रहा है
उससे पुछा कि जीवन क्या है
जिसका सुबह कुछ हो और शाम कुछ हो
उससे पुछा कि जीवन क्या है
वो जिसे विधाता कहते हैं
उससे भी कभी पुछो कि विधाता
तुम्हीं बताओ कि जीवन क्या है
राम के वनवास और कृष्ण के उच्छवासों से जीवन तो समझ में
आता है परन्तु जिन्होंने* अनवरत
वनवास और उच्छवासों की पीड़ा ही
देखी और झेली हो उनसे भी कभी पुछो कि
जीवन क्या है और जीवन का
यथार्थ क्या है
जीवन का यथार्थ क्या है।
*
गज़ल
लघु कविता. ०७
क्यों ज़ख्मों को सब छेड़े जा रहे हैं
क्यों ज़ख्मों को सब छेड़े जा रहे हैं
एक भरता नहीं और लगाए जा रहे हैं
जमाने की फितरत को देखे बहुत
बस उनके सितम को सहे जा रहे हैं
कोई बता सितम की हद होती है क्या
बस जमाने में हम यूं जिए जा रहे हैं
अनीश इबादत में असर न रह गयी
फिर भी इबादत किए जा रहे हैं।
--------
लघु कविता. ०६
आंसू और बरसात की बुन्दें
कवि भी तो आदमी
ही होता है
या आदमी से कुछ
इतर होता है
उसके मन जज्बात
दिलो दिमाग
फितरती तौर पर
बरसात के बादलों की
तरह होते हैं
जज्बातों के सैलाब कब
आंखों से उफन जाए
वह खुद भी नहीं जानता
पर इतना जानता है
कि आंखों से बरसती
बुन्दें
नम और लाल होती
आंखों को
कोई देख समझ न
पाए
वह बरसात में जी भर
कर रोना चाहता है
कि कोई न समझ सके
आंखें बरस रही हैं
या बारिश हो रही है
और वह तन मन
दोनों को तर-बतर
करना चाहता है
जी को बरसे बादलों
की तरह
हल्का कर लेना चाहता
है
जज्बातों के सैलाब को
पानी के साथ बहा
देना चाहता है।
-----------
लघु कविता. ०५
अनकही कथा.
फोटो : स्मिता.
किताब के पन्नों पर
सबकुछ दर्ज नहीं होता
या तो उन्हें छोड़ दिया जाता है
या वे छूट जाते हैं
सच चाहे जो भी हो
जो लिखे नहीं जाते
जो छूट जाते हैं
वे स्मृतियों के गह्वर में
कहीं न कहीं
धरती के गर्भ में गर्म लावे
की तरह खौलते रहते हैं
फूट कर बाहर आने के लिए
वैसे ही व्यग्र और आतूर रहते हैं
जैसे गर्भस्थ परिपक्व शिशु
बाहर आने के लिए
हाथ पैर मारने लगता है
स्मृतियों के दंश और उनसे
उपजी पीड़ाओं को जब
जमीन नहीं मिलती कि
कहीं से फूटकर बाहर निकल
आए और अनकही पीड़ाओं
को कहे सुनाए
और जब ऐसा नहीं होता तो
वे अनकही कथाएँ
शब्दों की बैसाखी लेकर
कोरे कागज की छाती पर
शब्दों का साथ लेकर
उगने लगती हैं और
विस्मृत स्मृतियाँ उनसे उपजी
वेदनाएँ
शब्दों के जंगल में
भावनाओं के वियावाँ में
गाने लगती है
मचलने लगती हैं भावातिरेक
वे गीत गजल कविताएँ
बन जाती हैं
और उन अनकही व्यथा कथा
की वेदनाएँ तिरोहित हो जाती हैं
निज की त्रासदियों से
मुक्त हो जाती हैं
जैसे व्याकुल नदियाँ सागर में
मिलकर एकाकार हो जाती हैं।
---------
लघु कविता. ०४
---------
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस
८ मार्च के उपलक्ष्य में
नारी.
तू श्रद्धा है सम्मान है सृष्टि की पहचान है
क्षमा है दया है त्याग है बलिदान है
जीवन के हर तिमिर तोम में विपदाओं में
तू ही तो बस एक दृश्यमान त्राण
है
नारी,
तू सृजनशीलता की पहचान है।
तू विकट काल में * दुर्गा काली
कात्यायनी है
काल की भी काल झाँसी की महारानी है
तू ही सरस्वती तू ही लक्ष्मी तू ही
माता रानी है
तू हीअग्नि तू ही व्योम तू ही तो
निर्झरिणी है
तू ही पालक तू ही रक्षक तु ही
सब निदान है
हे नारी,
तू ही दुर्गावती
तू ही कर्णावती
तू ही पद्मावती
तू ही आन बान है
तू ही अपाला,घोषा,
गार्गी, मैत्रेई महान है
प्रसव पीड़ाओं को
सह सह कर
सृजन करती महान
है
तू ही सृजन लय
प्रलय
सृष्टि का विधान है
शिव के साथ समावेशित होकर
अर्द्धनारीश्वर का
विधान है
युग युग की तू
युगद्रष्टा और विश्व
का निदान है
अंतिम रूप में तू ही
तो
समस्त ब्रह्माण्ड का विधान है।
======।
सृजनात्मक शक्ति को कोटि-कोटि नमन।
इच्छाएं अनन्त हैं : लघु कविता. ०४.
------------
सुख की इच्छाएं अनन्त हैं,
और दुःख को
कोई आमंत्रित नहीं करना चाहता,
पर दुःख है कि
बगैर किसी को बताए
अतिथियों की तरह चला ही
आता है.
आप उसका स्वागत अभिनन्दन,
करें कि न करें परन्तु
वह अपने हिसाब से आता और
अपने हिसाब से ही जाता है.
कालचक्र है,
कभी कभी दुखों का चक्र
अप्रत्याशित रुप से खींच जाता है लम्बा
पर झेलने के अलावा किसी के
पास कोई विकल्प नहीं होता,
वह जो रोज सबके सुख आरोग्य
की मंगलकामनाएं करता है
वह भी इससे मुक्त नहीं रहता,
फिर भी वह दुआएं देना
सबके लिए मंगलकामनाएं
करना बंद नहीं करता,
उसे इसी में सुख मिलता है और
वह दुःख का भी सम्मान करता है
कभी एक दो पल सुख चैन का
मिल जाए तो वह
आह्लादित भी हो जाता है कि
उसके भोग भाग्य में भी कुछ
आ ही जाता है.
जीवन बस ऐसे ही चलता
रहता है और
इसलिए इस चक्र
को संसार कहा जाता है
जो स्थिर भाव और सम्यक् गति से
अबाध चलते रहता है
चलते रहता है।
---------
पहाड़ और पेड़. लघु कविता ०३
---------
लघु कविता.
पहाड़ और पेड़.
फोटो : मीना : मुक्तेश्वर
लोग भी कहते हैं और
हमनें भी पढ़ा था कहीं
कि
पहाड़ और पेड़ नहीं रोते
हैं
वे तो जड़ संवेदनहीन और अभिव्यक्ति विहीन
होते हैं
पर हकीकत हमारी इस समझ और अनुभूति से
परे है
पर्वत जंगल नदियां पेड़
पौधे सबकी अपनी-अपनी चेतना और संवेदनाएं हैं
जब पर्वत उजाड़ होने लगते हैं
उनके भीतर के जीवन के स्पन्दन और धड़कनों
को निष्प्राण बनाया जाता है
उनके कलकल कलरव
करने वाले झरनों को नजरंदाज किया जाता है
तब पर्वत विलाप करते हैं
पेड़ पौधों की दुनियां जब रसहीन प्राणहीन होने लगती है
सीमेंट और कंक्रीटों के जंगल संसार को खड़ा करने के लिए
उनके जीवित संसार को
उजाड़ा जाता है
जब परिन्दों की ख्वाहिशों और खुशियों को छीना जाता है
धूप ताप से जलते हुए का छांव छीना जाता है
और पेड़ पौधों को निष्प्राण समझा जाता है
तब पेड़ पौधे भी रोते और क्रन्दन करते हैं
पर उनकी इस चेतना और वेदना को पढ़ने और समझने वाली आंखें चाहिए
संवेदनशील अन्तर्मन चाहिए
वरना अनन्त काल तक ये विलाप करते रहेंगे और
हम मनुष्य कंक्रीटों के जंगलों में अपनी दुनियां में संवेदनहीन सोते रहेंगे।
--------
लघु कविता. आँसू : लघु कविता. ०२
आँसू.
कभी मौन नहीं होते
आँसूओं की भी अपनी
भाषा होती है
न कहते बोलते हुए भी आँसू
बहुत कुछ बोल जाते हैं
जो शब्द नहीं कह पाते
आँसू कह जाते हैं
आँसू
हँसते रोते मुस्कुराते और
खिलखिलाते भी हैं
गाते गुनगुनाते भी है
रूदन हास्य और व्यंग्य करते हैं
आर्तनाद करते हैं
मनुहार करते हैं
याचनाएँ प्रार्थनाएँ करते हैं
पर इनकी संप्रेषणीयता बोली
भाषा से इतर होती है
इनको समझने के लिए
मनोभाव में मातृबोध की
जरूरत होती है
जब अबोध शिशु बोल नहीं पाता
तो रोता है
और माँ उसके रूदन भाव को
उसके अर्थ को
जरूरत को
वेदना को
पीड़ा को समझ जाती है
और उसकी जरूरतों की पूर्ति
कर देती है
पीड़ाओं को हर लेती है
ठीक वैसे ही आँसूओं को
समझने परखने के लिए
माँ जैसे हृदय भाव की जरूरत
होती है
आँसू
इसलिए बेशकीमती मोती होते
हैं
जिन्हें यूँ हीं जाया नहीं किया जाता और सबके सम्मुख
निरर्थक बहाया नहीं जाता
जिनकी नजरों में आँसू अदद
पानी नहीं होते
वही उनके मूल्य दे पाते हैं
वही उनका सम्मान कर
पाते हैं।
--------
पितृ देवो भव. लघु कविता. ०१
पितृ देवो भव.
एक पुरूष,
जब पिता बन जाता है,
वह बरगद का वृक्ष बन जाता है,
वह धुप शीत ताप बारिश को बड़ी
शिद्दत से झेलता है,
सबको अपने साए में रखकर
राहत देता है,
अपनी सारी पीड़ाओं को खुद में
समेटे हुए खामोश रहता है,
उसकी पीडाएँ जड़ों से निकलकर
उसके अंग अंग में फैल जाती है,
वह स्वयं को कहता है, सुनता है
पर किसी को कुछ नहीं कहता है,
बस अपने निज की चाहतों को तस्वीर
बनाकर दीवारों पर टांग देता है कि
कल शायद हालात बदल जाएँ
और वह खुद में खुद को पाना सीख
जाए,
वह भी सबके साथ खुलकर मुस्कुराना
सीख जाए,
ये नहीं कि वह हँसता मुस्कुराता नहीं है,
वह तो सबकी खुशियों के लिए सबके
साथ हँसता है,
दर्दों को समेटे हुए खामोशी के साथ जीता है,
बरगद है न, सबके लिए जीना चाहता है,
कई रिश्तों को समेटे हुए खुद के वजूद को भूल जाता है,
खुद पुराने जूतों और जैकेटों को दिखाकर कहता है
अभी तो काम चल जाएगा
तुमलोग की जरूरतें हमसे जरुरी है
एक पिता बस इन्हीं एहसासों और जज़्बातों को समेटे अपनों के लिए बरगद बन जाता है,
हाँ,
बरगद बन जाता है।
-----------
प्रतीक्षा. लघु कविता. ००
--------------
प्रतीक्षा
स्वयं में एक अद्भुत घटना है
प्रतीक्षा
किसी के आने की
किसी के संदेश की
किसी के परिणाम की
किसी आहत के ठीक
होने की
किसी व्याधिग्रस्त के रोगमुक्त
होने की
समय के बदलने की
किसी के रूपान्तरण या
बदलाव की
किसी को समझने की
प्रतीक्षा
जीवन की सारी क्रियाशीलताओं
में सबसे अद्भुत
सबसे रहस्यमयी होती है
प्रतीक्षा की घड़ियाँ बड़ी
बेचैनी और चिन्तन में गुजरती
है,
प्रतीक्षारत के चेहरे को गौर
से देखिए
पढ़िए और समझने की कोशिश
कीजिए
प्रतीक्षा के पल धीरे-धीरे
रूपान्तरित होते जाते हैं
जो कालांतर में ध्यान की तरह
गहरा होता चला जाता है
प्रतीक्षा,
एक गहराई में जाने की
सूक्ष्म अनुभूति है
ध्यान में उतरने के पूर्व भी
प्राणों के सघन होने की प्रतीक्षा
की जाती है
चेतना घनीभूत हुयी नहीं कि
प्रतीक्षा खत्म
स्व का बोध खत्म
जिसकी प्रतीक्षा थी
अवतरित हो गया
साक्षात्कार हो गया
फिर सबकुछ तिरोहित
हो गया।
सबकुछ तिरोहित हो गया।
=========
---------
अपने अपने राम : लघु कविता
-----------
अद्भुत है राम की सत्ता
इनके नाम से ज्यादा महिमा इनके नाम की है,
राम,
आप सिर्फ दशरथ नन्दन , कौशल्या सुत
रघुनन्दन होते तो भी शायद कुछ नहीं होता,
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ज्येष्ठ होते या
हनुमान के आराध्य होते तो भी कुछ
बड़ा नहीं होता,
विदेह के जमाई जानकी वल्लभ होते और अयोध्यापति राजा
राम भर होते,
पर हे राम,
आपको तो एक आदमी से लेकर नर
श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना था,
इसलिए आप वो नहीं बन पाए जो लोग
चाहते थे,
अन्यथा आप एक इतिहास पुरूष भर बन कर रह जाते,
कथा कहानियों में सिमट कर रह जाते,
एक प्रतापी राजा की कथा बन कर रह
जाते,
पर राम,
आपको तो अकाल पुरूष बनना था,
इसलिए आप सौर रश्मियों की तरह
कई रंगों में बँटकर कितने राम हो गए,
दशरथ के राम कि कौशल्या के राम,
कैकेयी के राम कि मंथरा के राम,
वशिष्ठ के राम कि अयोध्या के राम,
भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के राम,
कि जनक , जनक नन्दिनी के राम,
निषादराज के राम कि शबरी के राम,
अहिल्या के राम कि अरण्यवासियों
के राम,
अपने गुण संस्कार से बंधे राम कि
स्वतंत्र राम,
किष्णकिंधा सुग्रीव बाली हनुमान के राम कि
गिरीजनों दलितों पीड़ितों वंचितों शोषितों के राम कि पूरवासियों के
राम,
पत्नी विरहाग्नी में जलता हुए राम
कि एक आदमी की तरह रोते बिलखते
राम,
कण कण तृण तृण पुष्प पौधों जीव
जन्तुओं से ,
सम्पूर्ण व्योम से अपनी अर्धांगनी का पता पूछते
भिक्षा मांगते , याचना करते राम,
उत्तरापथ और दक्षिणापथ को समेकित
करते राम,
सुरसा को सम्मान और लंकिनी को मुक्ति देते राम,
गिलहरी को सम्मान , जटायु को मुक्ति देते राम , लघु को विशाल
बनाते राम, कि
लोकहित जन-वाणी का सम्मान करते
पत्नी का परित्याग करते राम,
वनवासी राम,
रावण के राम कि विभिषण के राम,
धर्म सत्य न्याय के प्रतिष्ठापक रण अभियान करते राम,
शिव के राम कि उमा के राम,
रामेश्वर के राम कि विजय हेतु
अपराजिता/ विजया ( शक्ति) की उपासना करते राम
आम आदमी की तरह भयाक्रांत होते
सशंकित होते राम,
अपनी आस्था और विश्वास, आत्मबल
को सशक्त करने हेतु * शक्ति पूजा करते राम,
विजयोपरान्त लंकापति रावण को सम्मान देते राम,
राम राज की स्थापना करते राम कि लव कुश की कथा सुनते विलाप करते राम,
तुलसी के राम कि कबीर के राम
वाल्मीकि के राम कि अगणित रामायण
के रचनाकारों के राम,
अनन्त नाम है तेरे राम,
जिसका जैसा पड़ा काम
वैसा ही बन गए राम,
रोम रोम में बसने वाले राम,
हे जन नायक हे लोक नायक
कितने तेरे नाम,हे मर्यादा पुरुषोत्तम,
जो जैसे भजे आपको
सबके अपने अपने राम।

---------
वैश्विक नववर्षाभिनन्दन : २०२४.
-----------
आओ मिलकर कुछ नया आगाज करते हैं
अंधेरे घरों में रौशनी का इन्तजाम करते हैं।
जो आ गया है जमीनें गारत पर फना होना है
जो जिन्दा हैं उनके जीने का सामान करतें हैं।
गुजरते वक्त की भी आदमी की तरह अहमियत है
जो नया आता है तो उसका भी इस्तकबाल करते हैं।।
वक्त भी इन्सानो की तरह फितरत बदलता रहता है
जो वक्त सामने खड़ा है *
अनीश उसी के साथ चलते हैं।।
==========
दुआएँ.
बदलने वाले साल को अलविदा
आने वाले साल के लिए दुआएँ,
सब खुश रहें और मुस्कुराते रहें
दिल से सबके लिए ये हैं दुआएँ.
==============
बस मौन रहा करता हूॅं
भरकर उर में पीड़ाओं को
बस मौन रहा करता हूॅं
अपनी खुद को कहता हूॅं
अपनी ही मैं सुनता हूॅं
पीड़ाओं की गाथाएं
अन्तर में हैं दबी हुई
अपने में ही गुनता हूॅं
अपने में ही बुनता हूॅं
स्वप्न संजोए सब चलते हैं
मैं भी तो चलता ही रहा
सपने टुटे पीड़ाएं जागी
अपने में ही सहता हूॅं
अपने से दुःख कहता हूॅं
जब निशिथ में आंखें खुलती
यंत्रणाएं तब तब जगती
सीने में एक आग सी जलती
उसमें खुद ही तपता हूॅं
खुद ही उसमें जलता हूॅं
का से कहूं व्यथा कथा मैं
जग तो सूना सूना है
जलता है जैसे बड़वानल
वैसे ही मैं जलता हूॅं
वैसे ही मैं जलता हूॅं।
--------
मैं कोई दैनिक अखबार
-----------
मैं कोई दैनिक अखबार नहीं हूॅं
अभी अभी पढ़े और रद्दी
कबाड़ की तरह
दरकिनार कर दिए
एक किताब हूॅं जिसमें
कितने अध्याय हैं
कितनी गाथाएं हैं
कितनी कहानियां और
कितने संस्मरण हैं
संघर्षों की
वेदनाओं की
यातनाओं की अनन्त कथाएं हैं
गिर गिर कर उठने की
उठ उठ कर गिरने की
अनन्त गाथाएं हैं
एक एक पन्ने को
गंभीरता से पढ़ना और
समझना होगा कि
इनमें आम आदमी की
पीड़ाएं मिलेंगी जो
आपके अन्तर्मन को
स्पर्श करके यह
एहसास दिलाएगी कि
यह तो मेरी व्यथा कथा है
ऐसा नहीं कि इनमें
सिर्फ वेदना और सिर्फ
संघर्ष ही मिलेंगे
इनमें प्रेम दया क्षमा
और सहनशीलता की
गाथाएं भी मिलेंगी
आदमी के आदमीयत
की कथाएं भी मिलेंगी
मां की ममता
पिता का वात्सल्य
भाई का स्नेह
दोस्त की दोस्ती
आदमी की आदमीयत को लिखा है
इसलिए मुझे जब भी पढ़ना
एक किताब की तरह
पढ़ना और
गंभीरता से पढ़ना कि
मैंने कोई किताब नहीं
एक आम आदमी को
बड़ी संजीदगी से लिखा है।
------------
ज़मीं ओ आस्मां खामोश हैं देखो
----------
ज़मीं ओ आस्मां खामोश हैं देखो
आदमी इस जहां में जिन्दा कैसे है
जिन्दगी कहते हैं जिसे जां कहां है
आदमी तो जैसे यहां पुतले जैसे है
रिश्ते नातों की बातें हैं किताबों की
बस आदमी जी रहा देखो कैसे है
इल्मो हुनर सिर्फ किताबों में नहीं होती
जज्बात ओ अहसास जिन्दगी जैसे है
अनीश जमाने के आबो रंग देखा किया है
जो देखा था कभी यहां अब नहीं वैसे है।
-----------
जमीं तो कभी आस्मां नहीं मिलता
-----------
जमीं तो कभी आस्मां नहीं मिलता
सफ़र में मुकम्मल जहां नहीं मिलता
मुक़द्दर के ये फैसले भी अजीब हैं
ये नहीं मिलता कभी वो नहीं मिलता
गर्दिशों में सितारे भी नहीं चमकते
अंधेरों के साए में साया नहीं मिलता
अनीश दुआएं करते रहे हर लम्हा
असर उनका हमें क्यूं नहीं मिलता
अनीश
*
--------
स्याह रात और सर्द हवाएं भी है
-----------
स्याह रात और सर्द हवाएं भी है
यादें सीने में अभी कायम भी है
रिश्ते बड़े अजाब हैं दर्द अभी है
एहसासों का अंदाज अब भी है
मोहब्बत हो के नफरत हो,होगा
तसव्वुर में वो अक्श आज भी है
अंधेरों में जिया है खौफ कैसा
उम्मीदों की रौशनी आज भी है
क्यों बयां अनीश हकीकत करे
वो कशिश सीने में आज भी है।
-------
ये वक्त भी गुजर जाएगा
--------
एक रोज वो भी सच जान जाएगा
सच जानकर वो बड़ा पछताएगा
जिसे जो चाहे वो हमें समझता रहे
सच एक रोज सामने आ जाएगा
शिकवा शिकायत अब क्या करना
झूठ पर से पर्दा एक रोज हट जाएगा
मुसीबतें फना हो जाएंगी एक रोज
जिस दिन उसका करम हो जाएगा
वक्त के सारे खेल हैं देखा करो
अनीश ये वक्त भी गुजर जाएगा।
-----------
हर चेहरे यहाॅं बदले नजर आते हैं
----------
बोलिए यहाॅं सब कुछ बिकता है
जमीं बिकती आस्मां बिकता है
जिस्मों जां की यहाॅं क्या कहने
यहाॅं तो अब इन्साफ बिकता है
हर चेहरे यहाॅं बदले नजर आते हैं
आम क्या यहाॅं सब खास बिकता है
रहजनों की यहाॅं बात क्या करनी
रहबरों का यहाॅं इमां बिकता है
अनीश परेशां है आबो-हवा देखकर
अब तो शहर का एतबार बिकता है।
*
शहर कब विरां हुआ पता होगा
रिश्ते क्यों बेजां हुए पता होगा
वफ़ा जफा की बातें कौन करे
कौन बेवफा हो जाए पता होगा
मौसमें बहार देखे खिजां क्या पता
कब बदल जाए मौसम पता होगा
दूर तक सफ़र में साथ चलते रहे
कब साथ छुट जाए पता होगा
अनीश को जिन्दगी का सिला मालूम
ये हकीकत भी सबको पता होगा।
*
रिश्ते निभाने हो तो तकल्लुफ कैसी
रिश्ते निभाने हो तो तकल्लुफ कैसी
तकलीफ हो जाए शिकवा न करना
चन्द रोजा जिन्दगी में रखा क्या है
शिकायत हो मुस्कुरा दिया करना
देने वाला नहीं देता सारी नियामतें
जो मिला है शुक्रिया अदा करना
फर्श से अर्श तक उसके खेल हैं
जो न मिला उनसे शिकवा न करना
अनीश कायनात ऐसे ही चलती है
जो मिला है नाफरमानी न करना।
*
सांझ ढले एहसासे गम बढ़ जाता है
सांझ ढले एहसासे गम बढ़ जाता है
तन्हाइयों का साया गहरा हो जाता है
वो जो अपना होने का दावा करता है
वक्त बदलते ही बेगाना हो जाता है
शहर की आबोहवा रोज बदलती है
बदलते वक्त में समां भी बदल जाता है
बेवक्त में सब्र का और चारा क्या है
जैसे भी हो बस जी लिया जाता है
जिन्दगी अनीश कब सुरत बदल ले
वक्त बदलने से सब बदल जाता है
*
अब गुजरे जमाने को आवाज न देना
अब गुजरे जमाने को आवाज न देना
जो आग बुझ गयी हो हवा न देना
रेत पर के निशान मिट ही जाते हैं
अब रेत पर कोई निशां बनने न देना
अफसाने बनते बिगड़ते रहते हैं
नया अफसाना कोई बनने न देना
सफ़रे जिन्दगी सबकी कट जाती है
नये राहों की जुस्तजू होने न देना
अनीश परेशां न हो सब गुजर जाएगा
कभी मुश्किलों को बसर होने न देना।
उम्मीदों को रखना छोड़ दिया हमनें
बस यूं ही जीना सीख लिया हमनें
जमाने के दर्दो गम लेकर जीते रहे
खुद के साथ जीना सीख लिया हमनें
सब्रोकरार का दामन छोड़ा नहीं कभी
जो सितम थे सब अपना लिया हमनें
और कोई सितम हो तो कर ही लो
इस तरह जिन्दगी को जी लिया हमनें
देने वाले ने देनें में कोई कसर न की
अनीश दामन छोटा कर लिया हमनें।
*
1.किसी के आंचल में
इतनी खुशियां
भरी होती है
जो संभाली नहीं
जाती और वो ऐसे
झरती हैं जैसे
किसी विवश और
लाचार की आंखों के
कोरों से
से झरते हुए आंसू
2.कुछ को छोड़कर
बचे लोग ऐसे
होते हैं जैसे
गमलों में लगे पौधे
जो चुपचाप बरगद
की ओर निहारते
रहते हैं पर
गमले के पौधे
कभी बरगद की तरह
विशाल नहीं
हो पाते हैं।
3.आदमी जब भीड़
का हिस्सा बन
जाता है
तो उसका वजूद
खत्म हो जाता है
पर आज के आदमी
के लिए जो
विवश लाचार और
साधनहीन है
उसे मजबूरन भीड़
का हिस्सा बनने की
विवशता हो जाती है।
3.एक आम आदमी
के सामने रोज रोज
कितने सवाल उठते
रहते हैं
लेकिन जब जिन्दगी
खुद सवाल बनकर
उसके सामने खड़ा
हो जाती है तब
सारे सवाल गौण
हो जाते हैं।
सारे शहर में बस वह तन्हा होगा
तन्हाइयों में वह खुब रोया होगा
*
आदमी की कीमत वक्त ही जनता है
इसे जानने में वह बहुत खोया होगा
आदमी की परख में उम्र गुजर गयी
शायद चैन से कभी वह सोया होगा
अनीश चलो ये सब भूल जाते हैं
जो रोया था कभी वही रोया होगा
आज का बोध
कब तक भागोगे
कहाँ तक भागोगे
भागते भागते थक जाओगे
थक कर एक दिन गिर जाओगे
और जिस दिन थक कर
गिर जाओगे
कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा
भागना कोई निदान नहीं
समस्याओं का हल नहीं
पलायनवादी न बनों
जीवन संघर्षों का अनवरत
प्रवाह है
स्वयं के विरूद्ध एक अनवरत
युद्ध है
और इस युद्ध में तुम्हीं * पार्थ
और तुम्हीं कृष्ण हो
दिवा स्वप्न में मत भटको कि
कोई तुम्हें जगाने और तुम्हारे
सामर्थ्य को बताने आएगा
कोई गीतोपदेश सुनाने आएगा
हर युग का अपना युगधर्म
होता है
इसे समझना होगा
इसके मर्म को जानना होगा
और कोई साथ आएगा भी तो
प्रत्यक्ष या परोक्ष अपेक्षाओं के
साथ ही आएगा
स्वयं केशव ने भी इस मर्म को
समझा था
कुरुक्षेत्र के लायक पात्र का चयन
करना था
इसके रहस्य को पहचाना था
और तभी उन्होने अर्जुन को
जाना था
उन्हें पार्थ की ही जरूरत थी
और पार्थ को केशव की जरूरत
थी
*
जीवन
जैसा हमने आपने और सबने देखा सुना जाना भोगा है
सबकी अपनी-अपनी
अनुभूतियाँ एहसास और जज्बात
है,
जीवन जैसा है वैसा ही है पर
यह भी हकीकत है कि वह कभी
गीत है संगीत है खुशी है
गम भी है
दुख है वेदना है पीड़ा है व्यथा है
शोक है विषाद है तो हर्ष और
उन्माद भी है
उत्तेजना है स्थिरता है बेचैनी है
संघर्ष है जंग है हार है जीत है
जय है पराजय है सफलता है
असफलता है
गुलामी है आजादी है
उन्मुक्त असीम आकाश है तो
बंधनों का पिंजरा भी है
जन्म है मरण है पुनर्जन्म भी है
यहाँ शैतानियत हैवानियत है
तो देवत्त्व और भगवत्ता भी है
मोक्ष है कैवल्य है निर्वाण है
वक्ते अखिरत भी है
दुआ है बददुआ है
सफर है मंजिल है
प्रेम है घृणा है अपनापन है
बेगानापन भी है
स्वार्थ है परमार्थ है त्याग है
औरों का बिछाया जाल है और
खुद का बनाया जंजाल भी है
सूरज की तपिश चाँद की शीतल
चाँ…
आज का भी सच।
गुरुर और वजूद
=====
नदियों को यह
गुरुर था कि वे सब
मिलकर सागर के
झील के जलाशय
और बड़े बड़े
जलागारों के अस्तित्व
को बनाए रखती हैं
वे न होतीं तो सागर
का अस्तित्व कैसे होता
सब सुनते रहे पर
सागर जो चुपचाप
गंभीरता से स्थिर था
उसने इसी स्थिरता से
नदियों को बुलाया
और कहा,
ऐ मेरी नदियों,
ये सही है कि तुम सब
लागातार बहकर हमें
भरती रहती हो पर
कभी तुमने सोंचा है
कि
तुम्हारे भीतर जो जल भरा है उसका मूल
स्रोत कहीं और है
जो वाष्पित होकर
बादलों का सृजन करता रहता है
और
बादल बरस बरस कर
तुम्हें भरा करते हैं और
तुम सब जलप्लावित
होकर
हम सबमें खाली होकर
हममें एकाकार होकर
एक नया स्वरूप
पाती हो और
नदियों से सागर में
रुपान्तरित हो जाती
हो
यह सृष्टि का सत्य है
सृजन का सत्य है
परिवार समाज देश
और
समस्त संसार का
सत्य है कि
किसी का अस्तित्व
किसी के अस्तित्व से
जुड़कर ही पूर्ण
होता है।
======
*
प्रथम मिडिया प्रस्तुति
--------
सम्पादकीय : सुविचार संग्रह. पृष्ठ : ३
----------
विचारक.
--------
सुविचार : पृष्ठ : ३ : संपादन.
----------
शक्ति. शालिनी रॉय.
-----------
पृष्ठ सज्जा.
शक्ति. मंजिता / चंडीगढ़.
⭐
सुविचार : संग्रह :
अरूण कुमार सिन्हा.
*
प्रतिक्रिया : जीवन : कसौटी
*
प्रतिक्रिया जीवन की कसौटी है,जिसके जीवन में जैसी प्रतिक्रिया होती है, जीवन वैसे ही रुपान्तरित हो जाता है और प्रतिक्रिया विहीन जीवन तो जीवन जगत में हो ही नहीं सकता है।
रत्नावली की तंज ने रामबोला को तुलसीदास बना दिया,रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गये,अंगुलीमाल बुद्ध के रोकने पर संन्यासी हो गया, महावीर और सिद्धार्थ जीवन में सांसारिक सुखों की निस्सारता और क्षणभंगुरता को देखकर अर्हंत हो गये।
इसलिए हमारे जीवन में प्रतिक्रिया हमारे जीवित होने का प्रमाण है।
*
नकारात्मकता और सकारात्मकता
जीवन में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों भावों का सहज अस्तित्व होता है और सकारात्मक भावों के सृजन का आधार नकारात्मक भाव ही होते हैं,जैसे विद्युत् प्रवाह क्षेत्र के लिए धन और ऋण दोनों आवेशों का होना जरूरी होता है वैसे ही निराशा और आशा है। मनुष्य जब निराशा के अंधकार से घिरने लगता है तो उसी अंधकार से प्रकाश की किरणें फूटकर निकलती हैं और मनुष्य आशावान होकर फिर से उठ खड़ा होता है, संघर्ष करता और विजयी होता है।
------
जीवन : आदर्श : व्यवहार
---------
आदर्श जीवन को मूल्यवान बनाते हैं पर आदर्श को खोखले नहीं होने चाहिए।
आदर्श वही श्रेष्ठ हैं जिन्हें जीवन की कसौटी पर खरा पाया जा सके और व्यवहार में उतारा जा सके।
भोजन वही श्रेष्ठ है जो सुलभ और सुपाच्य होअन्यथा तस्वीरों में बहुत कुछ खुबसूरत होते हैं।
--------
सच : अलंकृत : झूठ
---------
सच को चाहे जितने रुपों में देखा जाए, व्यक्त किया जाए,देखा जाए पर सच अंतिम रूप में सच ही होता है। ठीक इसके उलट झूठ को चाहे कितना भी अलंकृत करके,आवृत करके कहा जाए,देखा जाए पर झूठ तो सदैव झूठ ही रहता है। यह जीवन का व्यवहार है जिसका अवलोकन हमें करते रहना चाहिए।
-------
हर नयी सुबह एक नयी उम्मीद,एक नयी आशा और एक नयी प्रेरणा
-----------
हर नयी सुबह एक नयी उम्मीद,एक नयी आशा और एक नयी प्रेरणा लेकर आती है,अब इसकी विशिष्टताओं का प्रयोग आपके उपर निर्भर करता है कि आप इसे किस रुप में लेते हैं कि मन की चेतना आपकी है और निर्णय आपको ही लेना है जो आपकी जरूरत और जज्बातों पर निर्भर करता है.
-----
शिव ही सत्य है, शिव* ही सुन्दर है .
--------
जो कुछ भी नहीं है,महा शून्य है,शिव है।
जो समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताओं का केंद्र है, शिव है।
समस्त कल्याण, सृजन,लय और प्रलय का आधारभूत केन्द्र शिव ही हैं।
शिं करोति शुभं भवति
शुभं करोति शिवं भवति।
जो शुभ है, कल्याणकारी है, शिव है।
----------
अद्वैत प्रेम *
------------
प्रेम की अंतिम परिणति क्या होती है, अलग-अलग अनुभूतियाँ है पर मूल में *अद्वैत
( Non Dualism) ही हो सकता है और ये विरल में विरलतम है। व्यवहार और आचरण में पारस्परिक जरूरतों और जज्बातों को समझना ही प्रेम है।
---------
मातृ * देवो भव पितृ * देवो भव,
----------
मेरे जीवन के सूत्र वाक्यों में एक है,*मातृ देवो भव पितृ देवो भव, जो मेरी प्रातःकालीन और रात्रि बेला की मौन प्रार्थना है इसलिए मेरे लिए नित दिन* मातृ दिवस और पितृ दिवस है। पिता बनना तो एक सहज जैविक क्रियाशीलता है परन्तु पिता बने रहना एक साधना है,
---------
जीवन की जितनी परिभाषाएं
--------------
जीवन की जितनी परिभाषाएं दी जाती रही है,सब अलग -अलग क्यों होती हैं क्योंकि जीवन भोगा हुआ यथार्थ है जो जैसा भोगता है,उसकी अनुभूति भी वैसी ही होती है।
परन्तु एक तथ्य सबके साथ सही है कि सबके जीवन में उनकी अवस्था के अनुरूप दुःख सुख आते रहते हैं और इसी उतार चढ़ाव का नाम जीवन है।
----------
सुविचार : क्षमा और जीणेन्द्र भगवान महावीर
----------
⭐
तस्मै देसी क्षमादानंयस्ते कार्य विघातकः
विस्मृति कार्यहानीनां यद्दहोस्यात्तदुत्तमा
महान्तः संति सर्वेऽपि क्षीण कायस्तपस्विनः
क्षमावंतमनुख्याताः किन्तु विश्वे हितापसाः।
अर्थात् दूसरे लोग तुम्हें हानि पहुंचाएं इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर दो और यदि तुम उसे भुला सको तो यह और भी श्रेष्ठ है। उपवास करके तपश्चर्या करने वाले निःसंदेह महान है परन्तु उनका स्थान उन लोगों के पश्चात ही हैजो अपनी निन्दा करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं।
----------
सुविचार : सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय
---------
सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य, भारतीय धर्म संस्कृति और जीवन दर्शन में समावेशित सत्य और आदर्श हैं। क्षमा भी उन्हीं तरह का एक एक परम आदर्श और व्यवहारिक मानवीय मोल और मूल्य है परन्तु जिन भगवान महावीर ने इसे जिस तरह व्याख्यापित करके आत्मसात करने का काम किया, अन्यत्र दुर्लभ है।…अभी-अभी।
--------
सत्य प्रकट और प्रच्छन्न
---------
*
सत्य प्रकट और प्रच्छन्न दोनों होता है, पर उनका सार और सत् तो एक ही होता है।
जैसे सूरज घने बादलों की ओट में रहे और न दिखाई दे, फिर भी सूरज का अस्तित्व बना रहता है।
*
--------
राष्ट्रकवि दिनकर जी की पूण्य तिथि ५० वीं पर विशेष स्मरण.
--------
*
"जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को,
जिस तन मे भी बसे, हमारा नमन, तेज को, बल को।
इस यशोगान से जाति - गोत्र से इतर तेजोमय संस्कार और प्रज्जवलित अग्नि सम प्रकाश पूँज को नमन करने वाले युगद्रष्टा और राष्ट्रवादी कवि जिनके अन्तस में प्रेम, सौन्दर्य, श्रृंगार, काम- अध्यात्म, पुरूष और प्रकृति की अवधारणा एक साथ समावेशित हों, उस युगान्तकारी पुरूष " दिनकर" जी की जय॔ती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ ।एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि जिनके स्वर में जनसत्ता की हुँकार, जनवाद की उभार,लोकतांत्रिक मूल्यों और जनशक्ति की ऐसी धमक सुनायी पड़ती है जिसके सामने एकबारगी फ्रांसीसी राज्य क्रांति की हनक भी फीकी पड़ती दिखाई देती है। जरा देखिए तो, " सदियों की ठंडी आग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने …
--------
अहिंसा क्यों और हिंसा क्यों ?
----------
अहिंसा और हिंसा प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति अध्यात्म और जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्राचीन मानव समाज में इसकी कोई अवधारणा या चेतना नहीं थी परन्तु वैदिक काल से इसकी अवधारणा विकसित होने लगी। आरम्भिक अवस्था में ऋग्वेद और यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में सत्य और अहिंसा पहली बार देखा गया परन्तु इसकी व्यापक अवधारणा और व्याख्या जैन मत के 23 वें तीर्थकर ऋषभनाथ और 24वें तीर्थंकर जीण महावीर और कालान्तर में बौद्ध दर्शन में पाया गया। सर्वप्रथम जैन दर्शन में यह सूत्र पाया गया कि,अहिंसा परमो धर्म।
हिंसा से ही अहिंसा की अवधारणा विकसित हुयी। संस्कृत के मूल * हिस्स शब्द से हिंसा की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ प्रहार करना होता है। इसी के विपरित अहिंसा की अवधारणा विकसित हुयी जिसे जैन मत ने व्यापक रुप प्रदान किया। हिंसा को …
------
शब्दों पर गंभीर
----------
हम सब लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बोलते वक्त कभी कभी हम अपने शब्दों पर
गंभीर नहीं हो पाते हैं और कुछ अवांछित भी बोल जाते हैं जिन्हें क्षमा तो किया जा सकता है लेकिन
विस्मृत नहीं किया जा सकता है। जीवन की सारी वाचिक और लेखकीय क्रियाशीलताएं अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं जो वैसी परिस्थिति में पुनर्जीवित हो जाती हैं। लिखने और बोलने में सचेष्ट और जागरूक रहें ताकि उसके लिए पश्चाताप न करना पड़े।
विषयवार शीर्षक देना एक तरह की समीक्षा का सार ही है जो विषय-वस्तु के केन्द्रीय भाव को प्रदर्शित करता है। जिन्होंने संपादन किया, साधुवाद के पात्र हैं। उनके प्रति उपकृत हूॅं।सादर
=========
अरुण कबीर।
चैतन्य होना और स्वचैतन्य होना, जीवित प्राणियों के लक्षण हैं जिसमें स्वचैतन्य होना मनुष्यों के नैसर्गिक गुण हैं। स्वचैतन्य ही हमें अच्छे बुरे का बोध कराता है। किये गये कर्मों का बोध कराता है।
इसलिए अपने जीवन काल में ही यदि किसी कृत कर्म का अपराध बोध हो तो स्वयं से और जिसके साथ हुआ हो उससे खुले मन हृदय और आत्मा से क्षमा मांग लें,यही अपराध बोध का प्रायश्चित और मुक्ति है।
अनीश।
========
जीवन सुखद और दुखद घटनाओं के संयोग का नाम है। अप्रत्याशित रुप से दुःख सुख आते रहते हैं और हम मनुष्यों को दोनों को स्वीकारना होता है।
सुख को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता परन्तु दुःख के आते ही हम सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
स्मरण रहे कि इस संसार में निष्प्रयोजन कुछ नहीं होता है,सबके पीछे कारण समुदय होते हैं,कुछ को हम जान जाते हैं और कुछ को नहीं जान पाते,जिसको नहीं जान पाते वही दुःख ज्यादा पीड़ादायक होता है।
बस घटनाओं का अवलोकन करते रहिए और जीवन को जीने और समझने की कोशिश कीजिए। दुःख भी समझ में आ जाएगा और सुख भी समझ में आ जाएगा। यह भी स्मरण रहे कि न तो दुःख स्थायी है और न सुख स्थायी है। ये अपने हिसाब से बदलते और चलते रहते हैं।
अपना दुःख तो सबको नजर आता है परन्तु दूसरों के दुःख पर नजर रखना और यथासाध्य उनको सहयोग करना …
सत्ता शक्ति और वैचारिक परिवर्तन।
=======
विचार सिद्धान्त और आदर्शों का सीधा सम्बन्ध मन हृदय और मस्तिष्क से होता है। विचारों का निर्माण या हृदय परिवर्तन बल-प्रयोग से कभी नहीं हो सकता है। बल प्रयोग से बाह्य परिवर्तन तो किए जा सकते हैं पर वैचारिक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं जैसे प्रेम बल से,लोभ से,दवाब आदि से नहीं किया जा सकता है वैसे ही वैचारिक परिवर्तन भी है कि इसका भी सम्बन्ध मन और हृदय से होता है।
सत्ता के साथ बल और शक्ति जुड़ी होती है जिससे व्यवस्था और तंत्र तो संचालित और नियंत्रित किए जा सकते हैं परन्तु जनमानस को नहीं बदला जा सकता है। इसका जीवन्त उदाहरण चीन और पूर्व सोवियत संघ है। माओ कहा करता था कि, शक्ति और सत्ता बंदूक की नली से निकलती है अर्थात् सत्ता परिवर्तन बल प्रयोग से किया जा सकता है परन्तु उसका स्वरूप स्थायी नहीं हो सकता है। वहां के कम्यून सिस्…
नेकी और बदी साथ साथ चलती है और इसकी परिणति ही हमारा जीवन है।
जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धान्त कहते हैं और इसे आधुनिक भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करता है वैसे ही समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताएं भी हैं और हम इसके हिस्सा है तो ज्ञात अज्ञात क्रियाएं और इसके समस्त परिणाम के भी हम ही जिम्मेदार हैं परन्तु जीवन में अनायास कुछ ऐसी घटनाएं दुःख या सुख की घटती रहती है जो हमारी समझ से परे होता है उसे ही हम प्रारब्ध या नियती का खेल या प्रभु की लीला कहते हैं,बस इसका अवलोकन करते रहिए, जीवन अवलोकन करने और समझने का ही नाम है।
=======
समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताएं काल से निर्देशित, नियंत्रित और संचालित होती हैं। काल सबकी दिशा दशा को बांध कर चलता है।
इसलिए काल को कभी चुनौती न दीजिए बल्कि काल के संकेतों को समझकर,उसके अनुरूप चलने की कोशिश कीजिए कि काल क्षीप्र गति से चलायमान है और जो इसकी राहों में बाधा बनकर खड़ा होता है,इसके दो पाटों के बीच पीसकर रह जाता है।
ध्यान रहे कि धैर्य सहनशीलता और प्रार्थना ही प्रतिकूलताओं का एकमात्र अस्त्र-शस्त्र है। हम सब काल के चक्र के अधीन हैं।
=======
हमारा अस्तित्व बहुआयामी है। जीवन की क्रियाशीलताओं में हम बहुविध रुप से अपने को प्रस्तुत करते हैं। हम घर और बाहर जितने लोगों के सम्पर्क और सान्निध्य में रहते हैं हमारा व्यवहार और आचरण वैसे ही बनता बदलता रहता है, इसलिए हमारा मूल्यांकन भी उसी के अनुरूप होता रहता है, इसमें हमारा छद्मावरण और व्यवहार भी प्रभावी होता है जिसकी अनुभूति सिर्फ उसी व्यक्ति को होती है और इसलिए हमारा स्वरूप तीन रुपों में उभर कर सामने आता है,
एक जो हम अपने आप को समझते और मानते हैं,दूसरा जो लोग हमें समझते और मानते हैं और तीसरा जो सत्य है कि वास्तव में हम जो होते हैं और इस पर वह व्यक्ति और लोग सदैव भ्रम में रहते हैं।
इसलिए आपको लोग क्या समझते हैं, नहीं समझ सकते परन्तु आप अपना अवलोकन करते रहें,आप धीरे-धीरे वास्तव में सच में रुपान्तरित हो जाएंगे।
=========
=======
लोग कहते हैं कि दृढ़ निश्चय और प्रबल इच्छाशक्ति से सब संभव है पर इसके लिए भी प्रभु के अनुग्रह की जरूरत होती है,गीता कहती हैं।
बस आप श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही अधिकृत हैं,जो आपके विहित कर्म हैं जिसके प्रति भी है,करते रहिए ताकि कल आपको किसी तरह का पश्चाताप न करना पड़े कि हमने ऐसा नहीं किया।
परमात्मा का अनुग्रह सबको मिलता है जो उनके कर्म व्यवहार और आचरण के अनुरूप होता है।
========
आग्रह, पूर्वाग्रह और दूराग्रह, तीनों शब्दों के अलग-अलग और बड़ी महत्वपूर्ण अर्थ और प्रयोग होते हैं।
जब हम किसी काम के लिए किसी से आग्रह करते हैं तो हमारा मन एक उम्मीद और आसरे से भरा होता है और आग्रह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ही कर सकता है,आग्रह किसी अलौकिक सत्ता से नहीं की जाती है और की जाती है तो वह **विनती, प्रार्थना या याचना में बदल जाता है और इसमें व्यक्ति उस परमात्मा के सम्मुख एक याचक के रूप में खड़ा होता है पर उसका मन मस्तिष्क और हृदय किसी पूर्वाग्रह या दूराग्रह से मुक्त होता है।
पूर्वाग्रह और दूराग्रह सांसारिक व्यवहार के विषय हैं। आप किसी व्यक्ति या विषय के बारे में कोई विचार,मत या अवधारणा बनाते हैं तो आपको इन दोनों भावों से मुक्त और स्वतंत्र होना होगा, अन्यथा आप कभी भी उचित और सम्यक् निर्णय नहीं ले सकते हैं।
पूर्वाग्रहित और दूराग्रहित मन कभी भी सही …
आज का विचार।
=======
जीवन त्रिआयामी है, वर्तमान,अतीत या भूत और भविष्य।
लोग कहते हैं कि भूत मृत है, भविष्य अनिश्चित और रहस्यगर्भा है और वर्तमान जीवित है।
मनुष्य स्वभाव से भविष्य के लिए चिन्ता और चिन्तन करता है पर,भूत में जीवित रहता है और वर्तमान को अनदेखा करता है। कुछ विद्वतजनों का कहना है कि अतीत को विस्मृत करो, भविष्य की चिन्ता छोड़ो और वर्तमान में रहो।
परन्तु गृहस्थ या सांसारिक जीवन में यह दर्शन एकांगी और अव्यवहारिक प्रतीत होता है।
अतीत ही वर्तमान का जीवन और भविष्य का दर्पण है। अतीत से हमें नियमित सीख लेते रहना चाहिए कि अतीत हमें सदैव की गयी गलतियों और उसके परिणामों से अवगत और सचेष्ट कराता रहता है और उनकी पुनरावृत्तियों से रोकता है जिससे हम भविष्य के प्रति क्रियामाण रहते हुए चिन्तन करते हैं और उपलब्ध वर्तमान को जी पाने में सक्षम होते हैं।
वास्तविकता भी यही…
आज का मेरा विचार।
=======
विपत्तियां और आपदाएं सबके जीवन में आती है, इससे कोई नहीं बचा है।
गहन विपत्तियां मनुष्य को भीतर से एकान्तिक प्रवृत्ति का बना देती है। वह संसार में, परिवार में, दोस्तों की जमात आदि में रहकर भी वह एक अलग किस्म की अनुभूति करता है और एकान्तिक प्रवृत्ति उसे जीवन को जानने और समझने की ओर
प्रवृत्त करती है। वह जीवन के कितने अनबूझ रहस्यों को अपनी समझ ज्ञान और चेतना से समझने की कोशिश करता है। लोग और संसार को समझने की कोशिश करता है और जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। वह जीवन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करने लगता है ओर उसका बोध और उसकी चेतना रुपान्तरित होने लगती है।
उसके भीतर धैर्य सहनशीलता मौन आन्तरिक समझ आदि की चेतना विकसित होने लगती है कि यह समझ विकसित होने लगती है कि कुछ चीजों के विकल्प नहीं होते और मौन भाव से स्वीकार करना ही अंतिम विकल्…
======
संवाद और हम।
कितना अद्भुत संयोग है, संसार में जितनी भी भाषाएँ हैं, सबके अपने अपने शब्द भंडार हैं। चयन की पुरी आजादी भी है परन्तु फिर भी हम सब संवादहीन होते जा रहे हैं। शब्द अपनी जीवन्तता अर्थ प्रवाह और प्राण मानो खोते जा रहे हैं। संवाद धीरे-धीरे आक्रोष और मौन में रूपान्तरित होते जा रहे हैं। दरअसल हम हमारे भीतर की समझ और संवेदनाओं को या तो जानबूझकर कर कमजोर करते जा रहे हैं या संवाद ही नहीं करना चाह रहे हैं और इसी बिन्दु पर आकर * विडम्बनाओं विरोधाभासों अवसादों और मानसिक त्रासदियों के शिकार होते जा रहे हैं।
संवादहीनता की स्थिति में जैसा कि * सामाजिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि * संवादहीनता आदमी को संवेदनहीन बनाता है और इससे व्यक्तिगत रूप में आदमी हिंसक और उद्वेलित होता जा रहा है और यही निजी हिंसा सार्वजनिक रूप से से बड़े हिंसा या रक्तपात को जन्म द…
====
शब्द पदार्थ ईश्वर और हम।।
किसी का नाम एक संज्ञा भर है, शब्द है।आप जब किसी का नाम लेते हैं जो एक शब्द भर है पर जबतक आपका उससे साक्षात्कार परोक्ष या प्रत्यक्ष न हुआ हो तो आप किसी भी कीमत पर नहीं बता सकते कि वह क्या है और उसका अस्तित्व क्या है। फूल भर कह देने से एक फूल भर का बोध होता है पर कौन सा फूल है, यह भी बताना पड़ता है तब स्पष्ट होता है और उसकी एक छबि आपकी स्मृतियों से गुजर कर मनो मस्तिष्क में बनती है। अब आपने गुलाब को बेली चमेली कमल आदि को प्रत्यक्ष देखा हो या किताबों में देखा हो तभी वह छबि बनेगी। फल मात्र कहने से किसी फल का बोध होता है, किसी विशेष का नहीं, ऐसे ही जितनी वस्तुएँ होती हैं उनका प्रमाण प्रत्यक्षीकरण है। अनुमान से उसे नहीं बताया जा सकता है।
यहीं पर एक विरोधाभास होता है कि एक अचेतन बच्चे से पुछा जाए कि फल या फूल क्या है तो वह सुन लेगा पर…
किसी भी वस्तु व्यक्ति सिद्धांत विचार क्रियाशीलता आदि की जो ज्ञात परिभाषाएँ होती है , वे अपनी जगह स्थिर हैं परन्तु
जब उनके बारे में आपको कुछ लिख ने बोलने के लिए कहा जाता है तो जितने लोग ऐसा करते हैं , एक चमत्कारिक रूप से सबकी अभिव्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है पर जो उनकी मौलिकता होती है, कमोबेश बनी रहती है।
इसमें भी दो परिस्थितियाँ हमारे सामने सवाल बन कर खड़ा हो जाती हैं। आदमी आमतौर पर पढ़कर सुनकर देखकर या साक्षात्कार कर ही तद्विषयक ज्ञान प्राप्त करता है और अपने * मन बुद्धि चित्त अहंकार और विवेक के अनुसार उसका अवलोकन करते हुए विश्लेषण और मूल्यांकन करता है और इसे ही परखना कहते हैं।
एक जौहरी ही हीरा मोती मणि माणिक्य आदि का परख कर सकता है, लोहे की गुणवत्ता की जाँच नहीं कर सकता है, एक लुहार ही कर सकता परन्तु लोहार और जौहरी की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की जा सक…
========
प्रेम: नाम एक रूप अनेक।
====
चर्चा प्रेम की हो और श्री राधे कृष्ण की बात न हो तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता है।इनके प्रेम में एक साथ * लौकिकता और अलौकिकता, भौतिकता और आध्यात्मिकता का बोध होता है। इस प्रेमानुभूति का एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ ।
एक बार श्री कृष्ण सर की वेदना से पीड़ित थे।कोई औषधि कारगर नहीं हो रही थी। नारद जी को आभास होते ही वहाँ पहुँच गए, नमन किया और कुशलक्षेम जानना चाहा। देवकीनन्दन की बात सुनते ही नारद जी द्रवित होकर बोल उठते हैं,
हे केशव, आप कहें तो मैं अपने हृदय के रक्त से लेपन करके इस वेदना को खत्म कर सकता हूँ ।
इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि, हे देवर्षि, अगर कोई भक्त मुझे चरणोदक( चरणामृत/ चरण धोया जल) पीला दे तो मैं स्वस्थ हो जाउँगा।
नारद जी पहले रुक्मिणी जी के पास आते हैं और उनकी व्यथा कथा कहते हैं। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि,
हे दे…
========
सृजनशीलता और हम।
सृजन शब्द को बोलने लिखने के पूर्व, यह शब्द सोंच में आते ही एक बात मनो मस्तिष्क में सहज ही उभर कर सामने
आती है कि * दो के सम्मिलन के बगैर
कोई भी सृजनात्मक क्रियाशीलता नहीं हो सकती है।
वह दो पदार्थों का सम्मिलन हो या दो जीवों का या दो भावों विचारों का, यह
* द्वैतवादी क्रियाशीलता है परन्तु इसका
उत्पाद * एकात्मकता से समावेशित हो
जाता है, एकत्व का , * Single entity का बोध कराता है, अद्वैत हो जाता है।
भौतिक और आध्यात्मिकरूप से यही सत्य है। दो अणुओं के सम्मिलन से एक
नया पदार्थ सृजित होता है। दो विरोधाभासी पदार्थों के सम्मिलन से एक नयी समावेशी रचना होती है। नर मादा के सम्मिलन से एक नया जीव पैदा होता है जिसमें एक ही साथ समावेशी रूप में जो ** गुण माता पिता
के होते हैं , वे स्थूल और सूक्ष्म रूप में
संतानों को स्वतःस्फूर्त प्राप्त हो जाते है।
====
इसलिए उन…
=======
आज की अनुभूति
आप उन चीजों को सुनना देखना बोलना पढ़ना लिखना या सोंचना पसन्द करते है जो आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल हो,यह व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है और यह भाव सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है जो सब पर समान रूप से लागु होता है।
वह व्यक्ति चाहे साक्षर/ निरक्षर/ शिक्षित/ पूर्ण शिक्षित या उद्भट विद्वान ही क्यों न हो, समांगी भाव खोजता रहता है। एक पाश्चात्य चिन्तक का कहना है कि
* a man can be of submissive nature and attitude but after all he needs homogenous group for his survival. A non vegetarian or a vegetarian can survive in a heterogeneous atmosphere or group but latter on he has two options with him, either to be a vegetarian or to be a non vegetarian.
अब सवाल पैदा होता है कि इस मनोवृत्ति का जन्म और विकास कैसे होता है। एक छोटे या बड़े समाज क…
हम और हमारी अवधारणाऍं,
आज का चिन्तन।
=========
साकार, निराकार, सगुण निर्गुण,आस्तिक नास्तिक, टोटम, माना, निर्गुण, द्वैत, अद्वैत,द्वैताद्वैत ,विशिष्टाद्वैत, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद आदि अवधारणाऍं मानव सृजित हैं, विभिन्न कालखंडों में हमने ही युगधर्म की पूर्ति के लिए बनाए और करिश्मा ये है इनसे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है।
इन तमाम सर्जनाओं से हम मनुष्य नानाविध तरीकों से प्रभावित होते हैं, हमारी जीवनशैली सामाजिक लोकाचार आचरण आहार विहार धर्म कर्म और कर्मकाण्ड आदि बदलते रहते हैं परन्तु परमात्मा कल जहाॅं था, इस क्षण भी वहीं है।
जब ईश्वरीय सत्ता अक्षुण्ण अपरिवर्तनशील
अक्षय सार्वभौमिक सार्वकालिक और सार्वलौकिक कल्याणकारी सत्ता है तो हम अनादि काल तक, इस सृष्टि के नष्ट होने तक कितनी भी व्याख्या और तर्क वितर्क कर लें,
मौलिकता को नहीं बदल सकते हैं।
Ways of life, methodol…
==========
चित्र और चरित्र।
हम मनुष्यों की प्रकृति और प्रवृत्ति भी अजीब होती है,हम प्रत्यक्षीकरण में ज्यादा
विश्वास करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि संसार
या ब्रह्माण्ड में सबकुछ प्रत्यक्ष नहीं होता कि कुछ अनुमान पर हैं तो कुछ अनुभूतियों पर टिके होते हैं और हम उनके अस्तित्व को मानते और स्वीकार करते हैं।
हम मन चेतना आत्मा आदि को देख तो नहीं सकते पर उसे मानते और स्वीकार करते हैं,वैसे कुछ मत पंथ आत्मा की सत्ता को सीधे न स्वीकार कर उसे चेतना का महत्तम
रुप मानते हैं पर मानते हैं। ये सब वास्तव में चेतना के ही विभिन्न रुप हैं जो अपने कार्य और अर्थ के कारण अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं जैसे अंग्रेजी में
आप Parts of Speech को पढ़ते हैं कि एक ही शब्द प्रयोग के आधार पर अपने अर्थ को बदल लेते हैं यथा लाईट का अर्थ प्रकाश होता है जो संज्ञा है पर प्रयोग में इसका अर्थ*जलान…
अनुभूति आज की।
=======
आप यदि अचानक से आयी आपदा विपदा में फंसे हुए हों तो स्वाभाविक रुप से विचलित हो जाएंगे कि क्या करें क्या न करें। सारी चेतनाएं समाधान के बजाय समस्याओं पर केंद्रित होने लगेंगी। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले मन और चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए और समस्याओं के बजाय समाधान पर फोकस करना शुरु कर देना चाहिए। जिन लोगों पर आपका भरोसा और विश्वास हो, उनसे परामर्श करना चाहिए।
इसके अलावा धैर्य साहस और हिम्मत को बनाए रखते हुए अपने इष्ट को स्मरण करते रहना चाहिए कि
आपत्काल में धैर्य और साहस स्वयं में एक बड़ी औषधि होती है जो आपकी जीजिविषा को मजबूत करती है। यदि जीजिविषा मजबूत होती रहती है तो आपदाओं से लड़ने का साहस बना रहता है। इस आपदा से पूर्व भी परेशानियां आयी होंगी,आप स्मरण करें कि कैसे उसका सामना किया गया और कैसे प्रभु की कृपा आप…
सुखी को समस्त संसार सुखमय नजर आता है परन्तु दुःखी को ठीक इसके विपरीत नजर आता है।
गृहस्थ जीवन में सुख दुःख का चक्र वर्तुलाकार गति से चलता रहता है और इस चक्र को समझना ही संसार चक्र को समझना है। जो दुःख में दुःख को और सुख में सुख को समझता है, सांसारिक है और जो दुःख सुख में समभाव रखता है, ज्ञानी है कि वह जानता है कि इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है,सब परिवर्तनशील है,जो आज है कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह आने वाले कल में नहीं रहेगा।
फिर एक द्वन्द्वात्मक स्थिति तब पैदा होती है जब आप यह देखते हैं कि कुछ लोग सदैव सुख में और कुछ लोग सदैव दुःख में ही रहते हैं पर सुख वाले का भी अपना दुःख होता है और दुःख वाले का भी अपना सुख होता है जो सबको दिखाई नहीं देता इसलिए द्वन्द्व की स्थिति पैदा होती है।
सब सुख है पर शरीर रुग्ण है, बड़ा दुःख है,सब दुःख है पर परिवार स्वस्थ एवं प…
अनुभूति जीवन की
=======
======
विलियम शेक्सपियर एक जगह लिखते हैं,
Blow Blow Thou
Winter Wind
Thou Art not So
Unkindest Like The Ingratitude Of Human Kind.
हमारी राय में यह कथन कल भी सत्य था,आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा।
अपने लोगों की कृतघ्नता और उपेक्षा से शेक्सपियर हार्दिक रुप से पीड़ित हैं और उसकी ये गहनतम पीड़ा इन शब्दों में अभिव्यक्त होती है। विगत कई महीनों से हमें भी इसकी अनुभूति होती रही है।
लोग आपसे नहीं,आपकी उपयोगिता और उपादेयता की जरूरत से प्रेम करते दिखाई देते हैं और हमनें इस विषय पर कितनी दफा अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है।
चलिए ठीक है कि जरूरतें सबको बांधकर रखती है पर जज्बातों और अहसासों के भी कुछ मोल और मूल्य होते हैं, सबकुछ जरूरतें नहीं होती कि जीवन जरूरतों के अलावा जज्बात और अहसास भी है।
अभी कोई कष्ट और विपदा में है जो एक कालखंड का सत…
========
धन और हम
रिश्तों की अपनी अहमियत और जरूरत है पर सिर्फ दिल जज्बात और प्रेम से रिश्ते नहीं निभाए जा सकते हैं, इसके लिए धन का वांछित रुप में उपलब्ध होना बहुत जरूरी है।
बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है,किसी को आर्थिक मदद करनी है,किसी उत्सव या तीज त्यौहार का आयोजन करना है, आड़े वक्त में या बड़े जरूरत में किसी मित्र की मदद करनी है, बीमार जरूरतमंद की सेवा करनी है, किसी प्रिय को भेंट देनी है,सैर सपाटे के लिए जाना है, अच्छी किताबें और कपड़े खरीदने है,ऐसे सैंकड़ों काम हैं जहां धन की जरूरत होती है।
धन जीवन का अपरिहार्य साधन है जो हर अच्छे बुरे वक्त में साहस देता है। सिर्फ प्रेम, जज्बात, अहसास से रिश्ते और संसार नहीं चल सकते।पर ध्यान रहे कि धन आवश्यकतानुरुप ही होना चाहिए। धन का अति होना व्यक्ति के भीतर कभी कभी अहंकार और उपेक्षा का भाव भी जन्म देता है और अमानवीय भा…
========
धर्म, धर्म का मर्म और युगधर्म।
धर्म तो शाश्वत सनातन सत्य है जो अपरिवर्तनशील है पर हर युग का एक * युगधर्म होता है जिसके मर्म को समझना ही धर्म हो जाता है और यह कालखण्डों में समय की मांग के अनुरूप बदलता रहता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस युगधर्म की पहचान करना अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य भी है।
प्राचीन काल में * द्युत और द्वन्द युद्ध ( जुआ और एक से लड़ने की चुनौती) से इन्कार करने वाले
को क्षत्रिय नहीं माना जाता था। इसलिए शकुनि के सारे षडयंत्र को जानते हुए भी * चौपड़-पासा के आमंत्रण को युधिष्ठिर इन्कार न कर सके कि उन्होंने धर्म( विहित कर्तव्य) को समझा और सबकुछ गँवा बैठे और श्री कृष्ण सोलह कलाओं से युक्त होकर भी इस धर्म के मर्म को समझकर जरासंध से युद्ध करने से बेहतर रण से विमुख होकर * रणछोड़ कहलाए कि एक नायक की तरह उन्हें यदुवंशियों की रक्षा करनी थी…
========
हम और हमारी जीवन शैली
हमारे मुल्क में * मध्यम मध्यम वर्गीय समाज की सबसे बड़ी त्रासदी * सेलीब्रेटिजों के प्रचार प्रसार पर टिकी जिन्दगी है। करिश्मा ये है कि यही वर्ग उच्च बौद्धिक वर्ग होता है। निचले स्तर पर और उच्च स्तर पर ये प्रभावी नहीं हैं कि वे अपने आप में * सेलिब्रेटी होते हैं और उनकी अपनी मौलिकता होती है। नमक तेल दियासलाई साबुन सोडा परफ्यूम पोशाक तेल आटा चावल स्टेशनरी शारीरिक रख रखाव आदि हमारे क्या होंगे, सब उनके * प्रचार पर निर्भर करता है कि हम अपनी मौलिकता खोकर * अनुकरण और प्रदर्शन पर जीने लगते हैं। विशेषकर फिल्मी चरित्र हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करते दिखाई पड़ते हैं। बाल, कपड़े,
बाहरी आवरण आदि हमारे जीवन शैली को प्रभावित करते रहते हैं जीसे सहजता से देखा जा सकता है। यही नहीं हम अपने जीवन के आचरण और व्यवहार में भी मौलिकता छोड़कर पाश्चात्य स…
========
विरोध निषेध और अस्वीकार।
ये तीन शब्द हैं तो बड़े छोटे छोटे परन्तु इनका हमारे जीवन में हर जगह बड़ी महत्ता और महिमा है। नाकारात्मक होते हुए भी इनके साकारात्मक उपयोगिता और उपादेयता से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस पर एक पद बड़ा सटीक बैठता है,
सत सैया के दोहरे अरु नावक के तीर
लेखन में छोटन लगे आ घाव करे गंभीर आकार प्रकार से चीजों के महत्व का आकलन और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है यद्यपि आकार की अपनी महत्ता होती है आंग्ल भाषा में कहते भी हैं कि
Size matters and Size Seizes and Changes Many Activities and Scenarios.
अब हमें विरोध निषेध और अस्वीकरण पर बातें करनी हैं। विरोध का विलोम समर्थन या हिमायत है और विरोध की अंग्रेजी
Protest Against prohibition etc. होता है जिसके अनेकानेक प्रयोग
होते हैं। निज की जिम्मेदारी व जिन्दगी में हम इसका बेहतर…
=====
संसार चक्र और हम।
संसार चक्र को समझना या तो बड़ा सरल सहज और सुग्राह्य है या दुष्कर है।
संसार चक्र में सारी सृजनात्मकताएँ इसी सिद्धांत पर चलती है कि परमार्थ के सार में भी स्वार्थ ही है।
स्वार्थ के बगैर कोई सृजन नहीं हो सकता है।
तब जीवन के मोल और मूल्य क्या हो सकते हैं कि
हम ** स्वार्थ और अपेक्षाओं से रहित नहीं हो सकते तो बस उनकी मात्रा को सीमित और न्यून करनेकी जरूरत है और पीडाएँ
स्वतः रूपांतरित होती चली जाएँगी और यह दर्शन और चिन्तन नहीं बल्कि व्यवहारिक यथार्थ है जो सब रिश्तों में लागू है।
हम अपने विहित * धर्म कर्म का पालन करते रहें बस यही विकल्प है।
इच्छाएँ और कामनाएँ अनन्त हैं
जो हमारे जीवन में एक दूसरे से
अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और दुख संताप क्लेश पीडाओं और क्रोध तथा हिंसा के यही कारण भी हैं।
इच्छाओं का सम्बन्ध मन से है और मन सदैव क्षिप्र गत…
=====
संसार चक्र और हम।
संसार चक्र को समझना या तो बड़ा सरल सहज और सुग्राह्य है या दुष्कर है।
संसार चक्र में सारी सृजनात्मकताएँ इसी सिद्धांत पर चलती है कि परमार्थ के सार में भी स्वार्थ ही है।
स्वार्थ के बगैर कोई सृजन नहीं हो सकता है।
तब जीवन के मोल और मूल्य क्या हो सकते हैं कि
हम ** स्वार्थ और अपेक्षाओं से रहित नहीं हो सकते तो बस उनकी मात्रा को सीमित और न्यून करनेकी जरूरत है और पीडाएँ
स्वतः रूपांतरित होती चली जाएँगी और यह दर्शन और चिन्तन नहीं बल्कि व्यवहारिक यथार्थ है जो सब रिश्तों में लागू है।
हम अपने विहित * धर्म कर्म का पालन करते रहें बस यही विकल्प है।
इच्छाएँ और कामनाएँ अनन्त हैं
जो हमारे जीवन में एक दूसरे से
अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और दुख संताप क्लेश पीडाओं और क्रोध तथा हिंसा के यही कारण भी हैं।
इच्छाओं का सम्बन्ध मन से है और मन सदैव क्षिप्र गत…
=======
जागने के दो अर्थ होते हैं,निन्द से जागना और चेतना से जागना, निन्द से तो समस्त संसार जागता रहता है पर चेतना के साथ जागना ही जागृत होना है। इसलिए जब जागो तभी सबेरा है।
=========
अगर इच्छाएं उत्कट हो और उस दिशा में सही प्रयास हो तो ब्रह्माण्डीय शक्तियां भी उन इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाती है। इसलिए इच्छा के साथ साथ सार्थक प्रयास सार्थक दिशा में होनी चाहिए।
==========
स्मृतियां दुखद और सुखद दोनों होती हैं,सुखद स्मृतियां जीवन को ऊर्जावान बनाती हैं और दुखद स्मृतियां मन को अशान्त
करती हैं परन्तु दुखद स्मृतियां मनुष्य को उन परिस्थितियों से सचेष्ट रहने की भी प्रेरणा देती हैं कि जिन कारणों से उन परिस्थितियों का जन्म हुआ उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वर्तमान में उसकी पुनरावृत्ति न हो और भविष्य सुरक्षित हो। ये बात अलग है कि कभी-कभी दुखद परिस्थितियों का मनुष्य के जीवन में आगमन अनायास और अप्रत्याशित रुप से हो जाता है जिसे धैर्यपूर्वक झेलना पड़ता है।
स्थिर मन और मस्तिष्क से उसका निदान ढुंढना पड़ता है कि उनका कोई विकल्प नहीं होता है।
हर पल क्षण संघर्षों की गाथा है, दुःख सुख है,सुख है सुख है और अगर दुःख है तो दुःख और कष्ट में से ही खुशियों की तलाश करना जीवन है और जीने का हुनर है कि इसका भी कोई विकल्प नहीं है,यही विकल्प है।
विदा लेते वर्ष के दुखद दिनों को विस्मृत करें और आने वाले नए वर्ष के लिए सबके सुखद समय की कामना करें। सबका जीवन सुखमय स्वस्थ और समृद्ध हो,इसकी मंगलकामनाएं करें।
आपका दिन मंगलमय हो,आप सपरिवार सानन्द रहें सुखी स्वस्थ और समृद्ध रहें। हार्दिक मंगलकामनाएं।
सु प्रभात।
*
एम एस मिडिया प्रस्तुति
*
*
--------
सम्पादकीय. शक्ति.दृश्यम : संग्रह : पृष्ठ : ४
----------
संपादन
शक्ति. मीना सिंह / नैनीताल. *
कृष्ण सदा सहायते
.jpg) |
*
*
ए एंड एम मिडिया प्रस्तुति
|
* |
--------
आपने कहा : संदेशें आते हैं : चिठ्ठी आई हैं : पृष्ठ : ५
-----------
सम्पादकीय : संपादन.
शक्ति. डॉ.नूतन स्मृति.
लेखिका. कवयित्री.
देहरादून.
*
आपने कहा :
शक्ति पृष्ठ के विशिष्ट संपादन हेतु आप सभी के लिए अंतर्मन से आभार व्यक्त करती हूँ। इस अंक में रेखांकित समस्त शक्ति स्वरूपा वाग्विभूषिताओं को सादर अभिवंदना !
शक्ति.डॉ.नूतन स्मृति
लेखिका. कवयित्री .
देहरादून.
*
मुझ जैसे व्यक्ति के पास शब्द नहीं है कि आपके प्रति कृतज्ञता के भाव
व्यक्त कर सकूँ कि आपके सौजन्य से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूॅं फिर भी दो शब्द कहना चाहूंगा कि हृदय तल से आपके प्रति अनुगृहीत हूॅं। भविष्य में मेरी विविधतापूर्ण रचनाएं आपके अवलोकनार्थ समर्पित होती रहेंगी।
सादर आभार. सादर अभिनन्दन.
अरूण कुमार सिन्हा. झारखण्ड.
प्रेम की अंतिम परिणति क्या होती है, अलग-अलग अनुभूतियाँ है पर मूल में * अद्वैत( Non Dualism) ही हो सकता है और ये विरल में विरलतम है। व्यवहार और आचरण में पारस्परिक जरूरतों और जज्बातों को समझना ही प्रेम है।
** The whole of the manifestation of different characteristics and qualities
r the single entity of the whole. The total embodiment
Of the Universe is a single entity which emerges out from two different forces, *Negative and Positive. The clash between two different
Objects create an entirely original thing which r observed in the whole Universe in its total manifestation.

 सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं : लेकिन हमारी सोंच कहती है कि समस्त संसार में हमें सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं करते रहनी चाहिए। इस संसार की रचना सभी जड़ चेतन के मिलने से हुयी है, हम सभी एक दूसरे से अविच्छिन्न रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। हमारा अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। वृक्ष हमें फल फूल छांव लकड़ियां आदि देते हैं।वन्य प्राणियों को भोजन और आश्रय देते हैं। वन जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी जरूरी हैं। नदियां झरनें पहाड़ वनोत्पाद आदि सभी जीवधारियों के लिए जरूरी हैं। हमारे जीवन के लिए जो जरूरत और जरुरी है,उनकी रक्षा यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा इसलिए हम सबके प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं और इनके लिए मंगलकामनाएं करते रहते हैं कि ये सुरक्षित रहें और इनका संवर्धन होता रहे। आनन्द मौन भाव से सुन रहा था और बुद्ध के प्रति नतमस्तक होकर कहा,हे भन्ते,आपका जीवन दर्शन कितना महान और व्यवहारिक है जिसे सबको समझकर आत्मसात करना चाहिए ताकि जीवन मोल और मूल्य बने रहें और समस्त मानव समाज अपने अस्तित्व में बना रहे।
सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं : लेकिन हमारी सोंच कहती है कि समस्त संसार में हमें सभी जड़ चेतन के प्रति मंगलकामनाएं करते रहनी चाहिए। इस संसार की रचना सभी जड़ चेतन के मिलने से हुयी है, हम सभी एक दूसरे से अविच्छिन्न रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। हमारा अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। वृक्ष हमें फल फूल छांव लकड़ियां आदि देते हैं।वन्य प्राणियों को भोजन और आश्रय देते हैं। वन जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी जरूरी हैं। नदियां झरनें पहाड़ वनोत्पाद आदि सभी जीवधारियों के लिए जरूरी हैं। हमारे जीवन के लिए जो जरूरत और जरुरी है,उनकी रक्षा यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा इसलिए हम सबके प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं और इनके लिए मंगलकामनाएं करते रहते हैं कि ये सुरक्षित रहें और इनका संवर्धन होता रहे। आनन्द मौन भाव से सुन रहा था और बुद्ध के प्रति नतमस्तक होकर कहा,हे भन्ते,आपका जीवन दर्शन कितना महान और व्यवहारिक है जिसे सबको समझकर आत्मसात करना चाहिए ताकि जीवन मोल और मूल्य बने रहें और समस्त मानव समाज अपने अस्तित्व में बना रहे। 


























.jpg)
























.jpg)


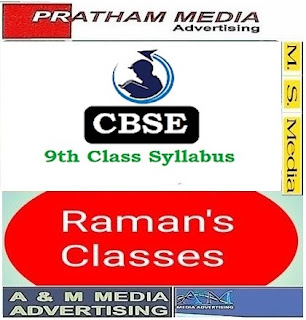
मुझ जैसे व्यक्ति के पास शब्द नहीं है कि आपके प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त कर सकुं कि आपके सौजन्य से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ फिर भी दो शब्द कहना चाहूंगा कि हृदय तल से आपके प्रति अनुग्रहित हूँ। भविष्य में मेरी विविधतापूर्ण रचनाएं आपके अवलोकनार्थ समर्पित होती रहेंगी। सादर आभार सादर अभिनन्दन
ReplyDeleteशक्ति पृष्ठ के विशिष्ट संपादन के लिए आप सभी के लिएअंतर्मन से आभार व्यक्त करती हूँ।
ReplyDeleteशक्ति पृष्ठ के विशिष्ट संपादन हेतु आप सभी के लिए अंतर्मन से आभार व्यक्त करती हूँ। इस अंक में रेखांकित समस्त शक्ति स्वरूपा वाग्विभूषिताओं को सादर अभिवंदना !
ReplyDeleteशक्ति.डॉ.नूतन स्मृति
लेखिका. कवयित्री .
देहरादून.
मैं हृदय तल से आदरणीय महोदया
ReplyDeleteके प्रति उपकृत हूॅं कि उन्होंने बड़ी ही गंभीरता के साथ संपादन किया है और विषयवस्तु को सजाने का काम किया है।
विभिन्न विधाओं की रचनाएं प्रेषित होती रहेंगी और आपकी पारखी नजरों से गुजरती रहेंगी,यही मेरी कामना है जिससे पाठक वर्ग अपनी अपनी अभिरुचियों से लाभान्वित होते रहेंगे।
पुनःश्च हार्दिक आभार अभिनन्दन।
अरुण कुमार सिन्हा कबीर,दुमका, झारखण्ड।
One of the best Blogspots I've ever read.
ReplyDeleteThe reading ambiance is good.
Thank You.
Keshav Aditya. Freelancer. New Delhi.
मेरे दो आलेखों को संपादित करके
ReplyDeleteप्रकाशित करने के लिए शक्ति संपादक समूह को हृदयतल से आभार एवं अभिनन्दन।
एक साग्रह निवेदन है कि अपनी ओर से मेरे आलेखों पर टिप्पणी के दो शब्द कह कर उपकृत करेंगी।
अरुण कुमार सिन्हा,रसिकपुर,दुमका, झारखण्ड।
मैं आदरणीय डाक्टर रमण जी प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूॅं कि उन्होंने इस पटल से जोड़ने का महती काम किया है।
ReplyDeleteअनुग्रहित हूॅं।
अरुण कुमार सिन्हा,रसिकपुर, दुमका, झारखण्ड।
Thanks from the core of heart to the editorial team of the group.
ReplyDeleteArun kumar sinha,
Rasikpur, Dumka, Jharkhand.
जीवन के नैसर्गिक गुण शीर्षक आलेख को संपादित करके प्रकाशित करने वाले संपादक/ संपादक समूह के प्रति और संयोजक डॉ रमण जी के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूॅं।
ReplyDeleteमेरा भी सतत् प्रयास रहता है कि
शिव सारस्वत कृपा से मौलिक रुप
से नवीन विचारों और भावों को आप सब तक पहुंचाने का काम करता रहुं।
आप सबके आरोग्य एवं सुखमय जीवन की मंगलकामनाऍं।
अरुण कुमार सिन्हा
दुमका, झारखण्ड।
दिल को छू लेने वाली कहानी!
ReplyDeleteहृदय के अन्तरतम तल से शक्ति संपादन समूह का हार्दिक आभार
ReplyDeleteअभिनन्दन कि मेरे आलेखों का इतनी संजिदगी से अवलोकन करके प्रकाशित करने की कृपा की जाती है।
उपकृत हूॅं।
अरुण,रसिकपुर,दुमका, झारखण्ड।
I highly appreciate the creativity and contribution to run this literary group.
ReplyDeleteThanks and regards.
Thanks a lot with utmost regards to the editting board Shakti Samuh and gratitude to Dr. M Raman
ReplyDeletefor his great creativity in the field of literary elevation.
Best wishes to all of U.
हमारी कोशिश रहती है कि दर्शन और चिन्तन के साथ साथ उसे व्यवहारिक और प्रयोगात्मक रुप भी दिया जाए ताकि पाठक वर्ग उन आलेखों का अवलोकन करने के साथ साथ उन्हें अपने जीवन के व्यवहार में भी ला सकें।
ReplyDeleteइधर हमारे दो आलेखों का सुन्दर संपादन करके उन्हें प्रकाशित करने के लिए शक्ति समूह का हृदय से आभार एवं अभिनन्दन।
साथ ही डाक्टर रमण जी के प्रति भी उपकृत हूॅं कि वे लेखन कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं।
अरुण सिन्हा, दुमका, झारखण्ड।